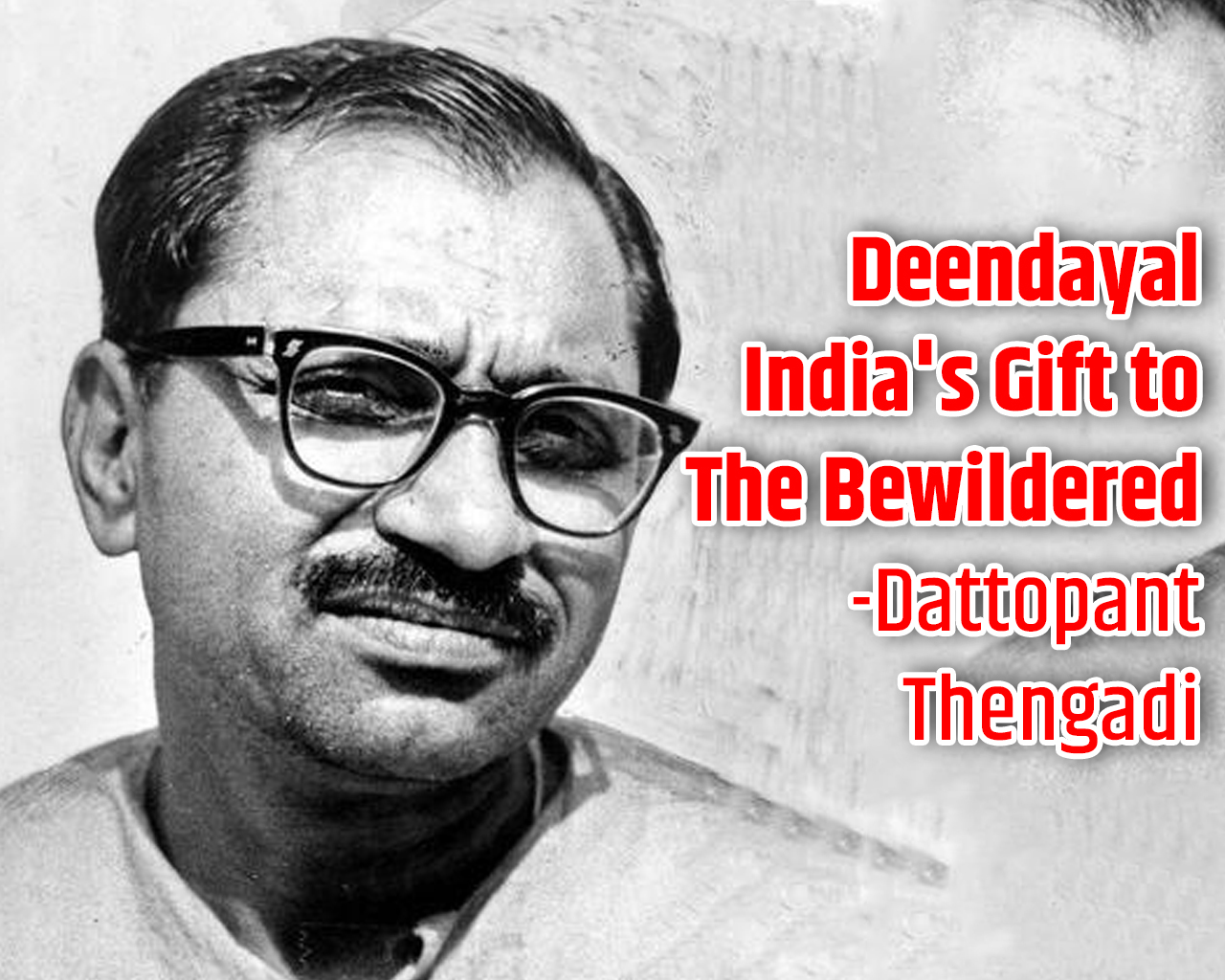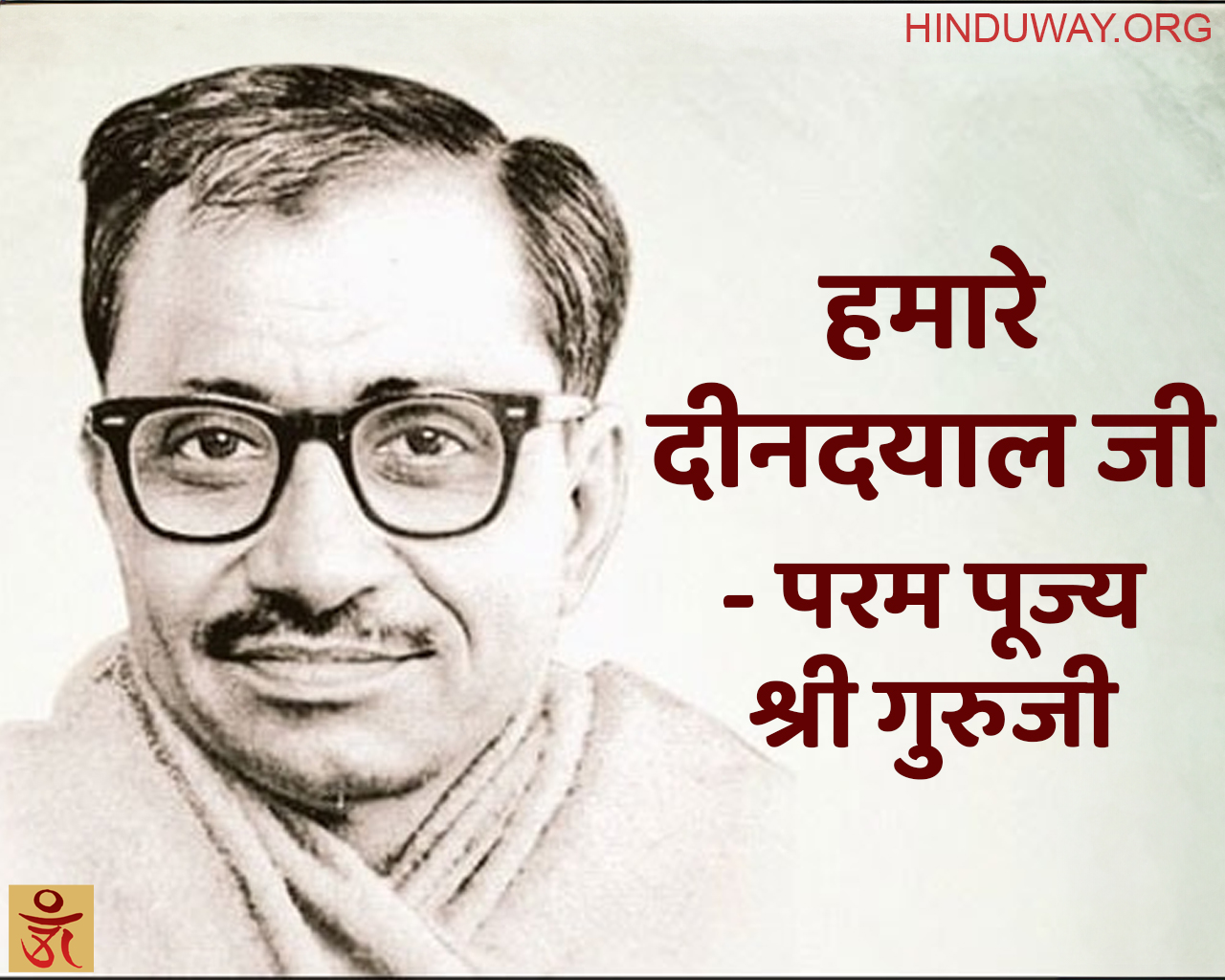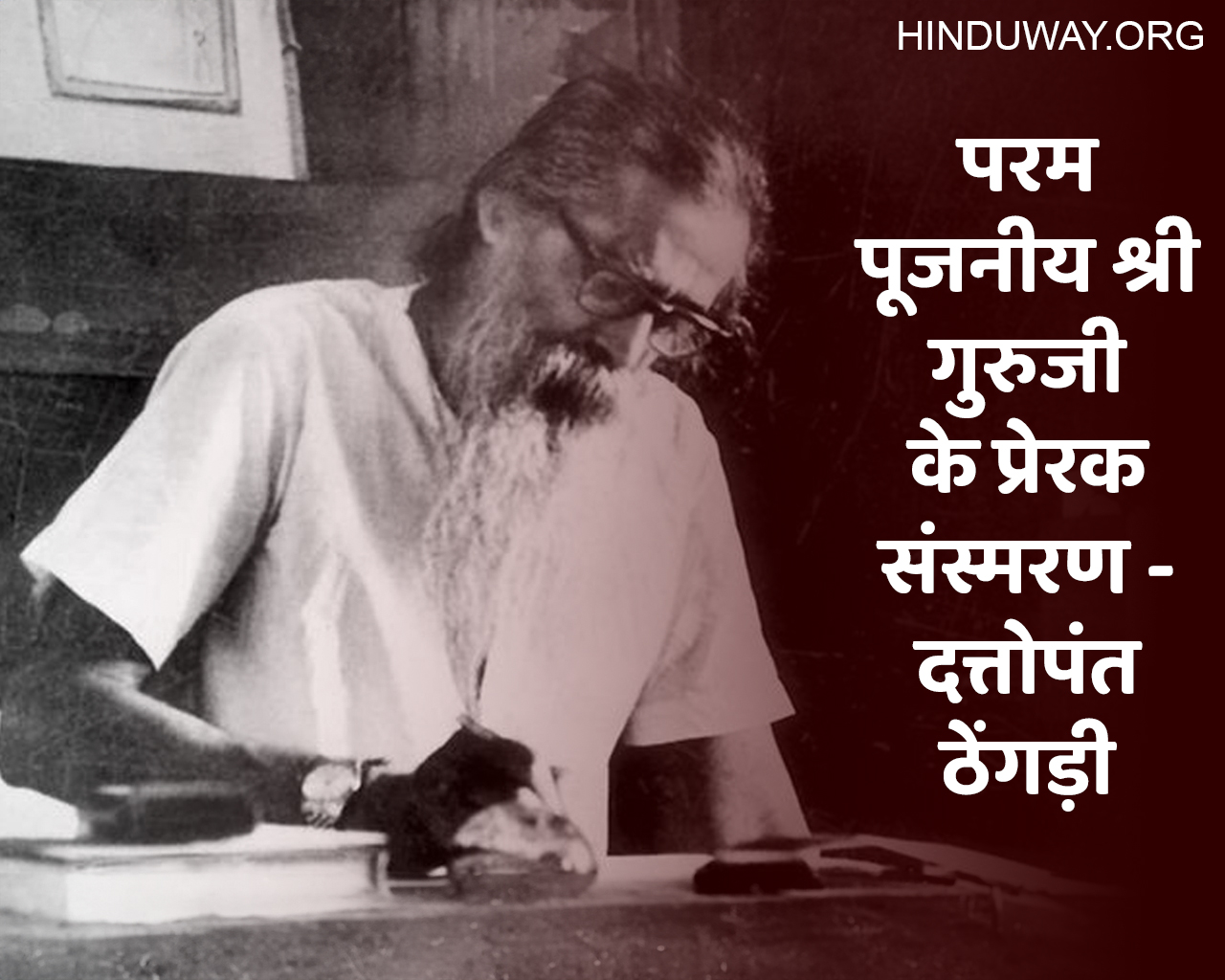” मर्यादानां च लोकस्य कर्त्ता कारयिताचसः ॥” – वा. रा. सुंदरकांड
( अपने आचरण से ) धर्ममर्यादा निर्माण करनेवाले तथा उन मर्यादाओं के अनुसार आचरण रखने के लिए लोगों को प्रवृत्त करनेवाले वह प्रभु (श्रीरामचन्द्र जी ) हैं । – श्री हनुमान जी
सर्वसाधारण व्यक्ति साधना की राह पर चल पड़े, यह बात प्रकृति के अनुकूल नहीं है । “खाओ, पिओ मौज करो” यही प्रवृत्ति नैसर्गिक है ।
यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्
ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् ।
यह प्रवृत्ति ही स्वाभाविक है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इंद्रियों के विषय हैं । उनका इन्द्रियों से संयोग होने से प्रारंभ में अमृतोप सुख प्राप्त होता है, यद्यपि ‘अन्ततोगत्वा इसके परिणाम विषतुल्य निकलते हैं । काम्य विषयों का उपभोग लेने से काम की तृप्ति होती है, ऐसा किसी का भी अनुभव नहीं है । पौराणिक भारत के ययाति का नहीं, आधुनिक योरप के सानोव्हा का भी नहीं । अग्नि में घी डालने से वह और भड़क उठती है, शांत नहीं होती, इसी तरह का अनुभव कामोपभोग के विषय में सभी को आता है । तो भी तात्कालिक होने वाले अमृततुल्य सुख के कारण, प्राणि मात्र उसी ओर खिंचा चला जाता है । इसी कारण मनु महर्षि ने कहा-
” न मांसभक्षणे दोषो – न मद्ये न च मैथुने
प्रवृत्तिऐषा भूतानाम् – निवृत्तिस्तु महाफलं ॥”
इस वस्तुस्थिति के कारण जब कभी किसी व्यक्ति को साधक की भूमिका में देखते हैं तो आश्चर्य होता है, और मन में प्रश्न उठता है कि यह इस भूमिका पर कैसे आया होगा ? इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं ।
श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है-
“शुचीनां रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते” ।
पूर्व जन्म के संस्कार श्रीमद् आद्य शंकराचार्य, श्री संत ज्ञानेश्वर आदि के उदाहरण इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं ।
माता पिता का जीवन तथा उनके द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा । विशेष रूप से माता द्वारा दी हुई प्रेरणा | मदालसा – मैनावती के भारत में तो प्रायः सभी श्रेष्ठ पुरुषों का प्रेरणा स्रोत मातृदेवता रही है, विदेशों में भी ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते हैं । नेपोलियन ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी माता का शब्दशः पूजन नहीं करता वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता । अब्राहम लिंकन कहते हैं, “मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी बनना चाहता हूं वह सब मेरी माता के कारण है ।” पिता की तथा आचार्यों की भूमिका भी इसी तरह प्रेरणादायक हो सकती है ।
जन्मादारम्भ बाल्यकाल में जो परिसर रहता है, उसमें प्राप्त होने वाले संस्कार, आव्हानू, प्रतिक्रियाएं, प्रेरणाएं – इन सबका प्रभाव सम्पूर्ण जीवन पर पड़ता है । जैसे जैसे समय बीतता है, Conscious mind में इनकी विस्मृति होती है, ऐसा भले ही प्रतीत होता हो; किन्तु अन्तर्मन में इनकी छाप अमिट रहती है। प्रारंभिक काल के परिसर के वायुमंडल का सुप्रभाव तथा दुष्प्रभाव अन्तर्मन में अंत तक कायम रहता है, किन्तु यह भी स्पष्ट है, कि हम किस परिवार में जन्म ग्रहण करें, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते । माता पिता का या परिसर का चयन हमारे हाथ में नहीं है । साधक के लिये. सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करा देना, यह भगवान की ही देन है । ‘ईश्वरप्रणिधानाद्वा’ ॥ 23॥ पातंजल॥ बाह्य अनुकूलताओं के बावजूद चित्तवृत्ति का निरोध, तदर्थ अभ्यास, वैराग्य की दृढ़ता, कैवल्य प्राप्ति की इच्छा की उत्कृटता, ये सारी बातें भगवत्कृपाधीन हैं। इस कृपा का संगुण साकार स्वरूप गुरु को माना गया है । ईश्वर ही गुरु है । ” स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात ” ॥ 26 ॥ पातंजल ॥ वही पूर्व देवादि का भी गुरु रहा है, क्योंकि उसको काल की मर्यादा नहीं है । अर्थात् वर्तमान तथा भविष्य काल में भी वही गुरु की भूमिका का निर्वाह करता हैं, सभी के लिये ।
अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार साधकों के मार्ग भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । ज्ञान- भक्ति – कर्मयोग | किन्तु इन मार्गों में साधकों की स्थिति – गति – प्रगति उसी की कृपा का परिणाम तथा कारण भी हुआ करती है। कलियुग में भक्ति मार्ग का महत्व विशेष बताया गया है । भक्ति का मतलब ” नारदस्तु तदर्पित अखिलाचरिता-तद् विस्मरणे परम व्याकुलता इति” । नारद के अनुसार भक्ति याने अपने सभी व्यवहार उसको समर्पित करना और उसके विस्मरण से हृदय में परम व्याकुलता, निर्माण होना भक्ति की कसौटी बताई गई है – ” तत्सुखसुखित्वम् ।” उसके सुख में ही अपने सुख का अनुभव करना । इस अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सोचता है – मैं नहीं, तू ही ” ।
साधना का प्रवास मुमुक्षत्व से प्रारंभ होता है और जीवन के अन्तिम क्षण तक चलते रहता है । सिद्धावस्था प्राप्त होने के बाद भी, क्योंकि तब तक साधना – यह व्यक्ति के स्वभाव का अविभाज्य अंग बन जाता है ।
साधनामय जीवन में एक बार रुचि निर्माण होने के पश्चात् व्यक्ति अन्तर्मुख हो जाता है । विभिन्न ईषणाओं की तुच्छता का अनुभव करता है । लोकेषणा की तुच्छता का भी । सम्पूर्ण जीवन का लक्ष्य याने घनीभूत, निरन्तर, चिरन्तन परमसुख । उसकी ओर बढ़ने में लोक प्रसिद्धि – यह बाधा रूप है, ऐसी उसकी धारणा हो जाती है । परमपूजनीय श्री गुरु जी, एक कविता का कभी-कभी उल्लेख करते थे । अलेक्जण्डर पोप ‘ode to solitude’ का अन्तिम Stanza है :-
“Thus let me live unseen, unknown,
Thus unlamented let me die,
Steal from the world, and not a stone
Tell whose I lie.”‘
यह आत्मविलोपी वृत्ति साधक में स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है ।
‘यदा संहरते चाऽयम् कूर्मोऽगाणीव सर्वशः ।’
यह बात जैसे सभी विषय वस्तुओं के बारे में, वैसे ही सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन के बारे में भी लागू होती है । मन की बहिमुर्खता पूरी तरह समाप्त हो जाने के कारण, साधक की रुचि बाह्य लोक व्यवहार में बिल्कुल नहीं रहती । वह अपने आप में सन्तुष्ट रहता है ।
ऐसा होते हुए भी, साधकों के विषय में प्राचीन काल से दो विचारधाराएं प्रचलित रही हैं | अपने ‘गीतारहस्य’ में लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, कि “जब इस तरह के बर्ताव से, अर्थात् यथाशक्ति और यथाधिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का बंधन छूट जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा अन्त में पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय, तब यह महत्व का प्रश्न उपस्थित होता है कि अब आगे अर्थात् सिद्धावस्था में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, अथवा प्राप्य वस्तु को पाकर कृतकृत्य हो, मायासृष्टि के सब व्यवहारों को निरर्थक तथा ज्ञानविरुद्ध समझ कर, एकदम उनका त्याग कर दे ? क्योंकि सब कर्मों को बिल्कुल छोड़ देना (कर्मसन्यास), या उन्हें निष्काम बुद्धि से मृत्युपर्यंत करते जाना (कर्मयोग), ये दोनों पक्ष तर्क दृष्टि से इस स्थान पर संभव होते हैं । और इनमें से जो पक्ष श्रेष्ठ ठहरे उसी की ओर ध्यान देकर पहले से (अर्थात् साधनावस्था से ही ) बर्ताव करना सुविधाजनक रहेगा । इसलिये उक्त दोनों पक्षों के तारतम्य का विचार किये बिना, कर्म और अकर्म का कोई भी आध्यात्मिक विवेचन पूरा नहीं हो सकता ।”
विवेचना को आगे बढ़ाते हुए तिलक जी कहते हैं कि “पांचवे अध्याय कें आरंभ में अर्जुन ने फिर प्रार्थना की कि उपरनिर्दिष्ट दो मार्गों में से कौन सा श्रेष्ठ है, यह आप मुझे निश्चयपूर्वक बताइये । यदि ज्ञानोत्तर कर्म करना और न करना एक ही सा है, तो फिर मैं अपनी मर्जी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म करूंगा, नहीं तो न करूंगा । यदि कर्म करना ही उत्तम पक्ष हो, तो मुझे उसका कारण समझाइये ।” योगवासिष्ठ में श्रीरामचन्द्र जी ने वशिष्ठ से और गणेशगीता में वरेण्य राजा ने गणेश जी से यही प्रश्न किया है ।
पश्चिम में भी इस विषय पर चर्चा हुई है । अरिस्टोटल अपने ‘Politics’ में कहते हैं कि “कुछ ज्ञानी पुरुष तत्वविचार में, तो कुछ राजनैतिक कार्यों में निमग्न दिखाई देते हैं, और यदि पूछा जाय कि इन दोनों मार्गों में कौन सा बहुत अच्छा है तो यही कहना पड़ेगा कि प्रत्येक मार्ग अंशतः सच्चा है । तथापि, कर्म की अपेक्षा अकर्म को अच्छा कहना भूल है। क्योंकि यह कहने में कोई हानि नहीं कि आनन्द भी तो एक कर्म ही है और सच्ची श्रेयः प्राप्ति भी अनेक अंशों में ज्ञानयुक्त तथा नीतियुक्त कर्मों में ही है । “
ऑगस्टस कांट कहते हैं – “यह कहना भ्रांति मूलक है कि तत्व विचार ही में. निमग्न रह कर जिन्दगी बिताना श्रेयस्कर है। जो तत्वज्ञ पुरुष इस ढंग के आयुष्य क्रम को अङ्गीकार करता है और अपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड़ देता है, उसके विषय में यहीं कहना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता है ।”
यहां पर मुख्य प्रश्न यही है कि ज्ञानोत्तर संसार में व्यवहार केवल कर्त्तव्य समझ कर लोकल्याण के लिये किये जायें अथवा मिथ्या समझकर एकदम छोड़ दिये जायें ? कर्मयोग या कर्मसंन्यास ?
गीता के पांचवें अध्याय के आरम्भ में भगवान ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है कि “संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग निःश्रेयस अर्थात् मोक्षदायक हैं अथवा मोक्ष दृष्टि से एक सी योग्यता के हैं, तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है ।”
” संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तथोऽस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्टते ॥ ( गीता 5.2)
” तस्माद योगाय युज्यस्व” (गीता 2.50 ) तथा “माते संगोऽस्त्वकर्मणि” (गीता 2.47 ) आदि वचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। गीता में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि ज्ञानी पुरुष कर्म का संन्यास न कर ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर भी अनासक्त बुद्धि से अपने सब व्यवहार किया करता है । (गीता 2.64, 3.19, 3.25, 18.9) जैसा तिलक जी ने स्पष्ट किया है, कर्म संन्यास और कर्मयोग- इनमें से जो पक्ष श्रेष्ठ ठहरे उसी की ओर ध्यान देकर पहले से (अर्थात् साधनावस्था से ही ) बर्ताव करना सुविधाजनक होता है ।
सभी साधकों के लिये तिलक जी का यह मार्गदर्शन अति उपयुक्त है’, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इसी श्रेणी में आते हैं । पूर्णरूपेण आत्मविलोपी होकर भगवान के द्वारा निर्दिष्ट कर्म निरपेक्षभाव से करते रहनेवाले को ही संघ में ‘कार्यकर्ता’ – यह संज्ञा प्रदान की जाती है ।
भगवान कहते हैं कि ( अपने धर्म के अनुसार) नियम कर्म को तू कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है ( 3. 8)
योगवासिष्ठ में लिखा है कि जीवनमुक्त ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिए । जब रामचन्द्र जी ने पूछा कि “मुझे बताइये कि मुक्त पुरुष कर्म क्यों करे ?” तब वशिष्ठ ने उत्तर दिया है-
“ज्ञस्य नार्थः कर्मत्यागैः नार्थः कर्मसमाश्रयैः।,
तेन स्थितं यथा यद्यत् तत्तदैव करोत्यसौ॥
कर्मेणवहि संसिद्विमास्थिसा जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहसि॥”
“ज्ञ अर्थात् ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना होता, अतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे वैसा किया करता है। कर्म से ही जनकादि लोगों ने संसिद्धि प्राप्त कर ली। इसी प्रकार लोक संग्रह पर दृष्टि देकर तुझे कर्म करना ही उचित है ।
गणेशगीता में कहा गया है-
” किंचिदस्य न साध्यं स्यात् सर्वजन्तुषु सर्वदा ।
अनोऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कर्म जन्तुभिः ।। (2.18)
“उसका अन्य प्राणियों में कोई साध्य (प्रयोजन) शेष नहीं रहता, अतएव हे राजन् लोगों को अपने-अपने कर्तव्य असक्त बुद्धि से करते रहना चाहिए ।” ज्ञानोचर करणीय कर्मों में ‘लोकसंग्रह’ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गीता
के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, “हैं पार्थ ! त्रिभुवन में न तो मेरा कुछ भी कर्तव्य शेष रहा है, और न कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करने को रह गई है, तो भी मैं कर्म करता ही रहता हूं ( 22 ) क्योंकि जो मैं कदाचित् आलस्य छोड़ कर कर्मों को न करूंगा, तो हे पार्थ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेंगे ( 23 ) । जो मैं कर्म न करूं तो ये सारे लोक उत्सन्न अर्थात् नष्ट हो जाएंगे । (24) हे अर्जुन ! लोक संग्रह करने की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़ कर उसी प्रकार बरतना चाहिए, जिस प्रकार व्यावहारिक कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग बर्ताव करते हैं । (25) कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी पुरुष भेद उत्पन्न न करें, आप स्वयम् युक्त अर्थात् योगयुक्त होकर सभी काम करें और लोगों से खुशी से करायें (26) स्वयम् करते रहना तथा दूसरों से करवाना भी ।
‘लोक संग्रह’ शब्द से सबके मन में अभिप्रेत कार्य एक ही होते हुए भी विभिन्न अधिकारी पुरुषों ने उसकी परिभाषा विभिन्न शब्दों में की है । उदाहरण के लिये ‘तत्वज्ञान विद्यापीठ’ के संस्थापकं तथा ‘स्वाध्याय’ के प्रवर्तक पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले कहते हैं “पशुतुल्य जीवन जीनेवालों को मानव बनाना, जो भोग जीवन के हैं, उनको भाव जीवन का बनाना, जो भाव जीवन के हैं उनको भद्र जीवन का बनाना यह लोकसंग्रह है ।” यहां भाव प्रकट करनेवाली पारंपरिक शब्दावली है-
“कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ।”
संघ के कार्यकर्ता को साधक होने के कारण, तिलक जी ने मार्गदर्शन के अनुसार०इस साधनावस्था में ही यह सब ज्ञान प्राप्त कर लेना, उनके लिये सुविधाजनक होगा- आगे की दृष्टि से ।
इस पृष्ठभूमि पर यह समझना आसान होगा कि संघ कार्यकर्ता की भूमिका का निर्वाह करना किस तरह असिधारा व्रत है ।
अच्छा होता कि वह व्यवहार चतुर बनकर संघ कार्य की झंझट से दूर रहता, अन्य करोड़ों देशवासियों के समान स्वकेन्द्रित पारिवारिक जीवन व्यतीत करता, और उनके समान ही सामान्य प्रापंचिक सुखदुःखों में स्वयम् अपने को व्यस्त रखता । श्रीराम जन्मभूमि पर ही मन्दिर बनाने से या न बनने से उसके पारिवारिक सुख दुःखों में क्या अन्तर पड़ता ? भारत विभाजित रहे या अखण्ड बनाया जाय, इस प्रश्न के उत्तर का उसके व्यक्तिगत जीवन पर कौन सा भला बुरा असर होने वाला है ? उसकी मृत्यु के पश्चात् उद्घाटित होनेवाले हिन्दू राष्ट के परम वैभव से उसको, उसके जीवन काल में, क्या लाभ होगा ? दक्षिण में द्राविड़ कऽघम् के नेता हिन्दुओं पर टीका-टिप्पणी करते समय कहते थे कि ये लोग पागल हैं ।’ यह स्वाभाविक है,
क्योंकि उनके देवता पागल हैं । हनुमान की ही बात लीजिये। सीता उसकी पत्नी नहीं थी, और न ही उसको भगाकर ले जाने का काम हनुमान ने किया था । सीता की समस्या से उस बन्दर का कोई लेना देना नहीं था । फिर भी वह वैसे ही जबरदस्ती समुद्र को लांघकर लंका में गया और अपनी पूंछ जलवाकर वापिस आया। खुद का न कुछ लेना, न देना । पत्नी किसी की उसको भगाने वाला कौन, और ये बन्दर अकारण बीच में आता है और पूंछ जलवा लेता है । इसी तरह का पागलपन संघ कार्यकर्ता करता है । हनुमान – सुग्रीव आदि लोग अपने ही राज्य में आराम से रहते, तो उनका क्या नुकसान होता ? और इतना सारा महत् प्रयास करने के पश्चात् हनुमान को लाभ क्या हुआ ? कहा गया है-
क्या कहें रघुनाथ जी को – सब करम का खेल।
विभीषण को लंका मिली – हनुमान जी को तेल ॥
हिन्दू राष्ट्र को परम वैभव प्राप्त होने के पश्चात् भी संघ कार्यकर्ता को दक्ष- आरम के अलावा कुछ मिलनेवाला नहीं है । और यह बात वह भली-भांति जानता भी है । फिर भी गलत आवेश में आकर वह स्वयम् आजीवन दुखी हो रहा है और परिवारवालों को दुखी बना रहा है । निरा पागलपन किन्तु व्यवहार चतुराई और उसके द्वारा प्राप्त होनेवाला सुख उसकी जन्म-पत्री में ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में उसकी कुण्डली में प्रविष्ट हुआ शनि उसको केवल ढाई वर्ष के लिए तो नहीं सम्पूर्ण जीवन भर दुःखमय बनाता है ।
किसी को भी व्यावहारिक बुद्धि से वंचित रखना और उसके मन में व्यवहार शून्य अध्यात्म की प्रेरणा ठूंस देना, यह दुष्टं ग्रहों के षड्यंत्र का ही एक अंग है, ऐसा माना जा सकता है । किन्तु, स्वयं अपने को सर्वनाश से बचाने के लिए संघ का कार्यकर्ता बुद्धिमानी का एक काम तो कर ही सकता था । मोक्ष को हो परमोच्च लक्ष्य मान लिया तो भी उसकी प्राप्ति के लिये एकान्त में रहते हुए एकाग्रचित से अपनी साधना करते रहना, और वहां तक ही अपनी गतिविधि को सीमित रखना, यह निर्णय तो वह ले ही सकता था । लक्ष्य सिद्धि की दृष्टि से इतना पर्याप्त था । इसके अलावा ‘लोकसंग्रह’ आदि व्यावहारिक कार्य याने मेरे लिये केवल ‘अव्यापारेषु व्यापार’ है, ऐसा तो वह प्रामाणिकतापूर्वक मान सकता था । संसार के निःसार व्यवहार से निवृत्त होकर, अरण्य में जाकर स्मृति धर्मानुसार सन्यासाश्रम ग्रहण करने से वह ध्येय सिद्धि की दिशा में अधिक द्रुतु गति से आगे बढ़ सकता था । वह बुद्धिमानी भी संघ कार्यकर्ता में नहीं दिखाई देती । समर्थ रामदास के समान वह मन में सोचता है, “बुडते हे जन पाहवे ना डोका” (ये लोग डूब रहे हैं यह आंखों से देखा नहीं जाता), और इस कारण “चिंता करितो विश्वाचो ” ( मैं विश्व की चिंता कर रहा हूँ) | वास्तव में वह इस तरह डूबनेवाले लोगों को या विश्व की चिंता याने अध्यात्मसाधना की एकाग्रता में आनेवाली बाधा, रुकावट, विघ्न या अवरोध है, ऐसा वह आन्तरिकतापूर्वक मान सकता था । ऐसा भी उसने नहीं किया ।
संघ कार्यकर्ता साधक है, किन्तु सिद्ध नहीं । साधना की आवश्यकताएं और व्यावहारिक कार्यों की बाध्यताएं, इन दोनों में सन्तुलन तथा समन्वय स्थापित करने की क्षमता सिद्धावस्था में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है । यह बात साधक की नहीं । संघ कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण समाज है, केवल संघ कार्यालय नहीं । समाज में भी केवल सात्विक, सद्गुण सम्पन्न, साधु-सन्तों का ही संगठन वह करे, ऐसी अपेक्षा नहीं है । सम्पूर्ण समाज को सुसंगठित अवस्था में लाना है । अतः समाज के सभी लोगों के घनिष्ठ सम्पर्क में आता है । सत्व रज-तम् – तीनों गुणों से युक्त लोगों में आत्मीयतापूर्वक समरस होना है । कुएं में गिरे व्यक्ति को ऊपर लाना है तो प्रथम स्वयम् कुएं में कूदना पड़ता है (अवतरण), और फिर उस व्यक्ति को उठा कर उसको ऊपर लाना पड़ता है । (उद्धार) पानी में जाकर स्वयम् को ‘पद्मपत्रमिवांभसि’ रखना अति दुष्कर कार्य है । वह करना संघ कार्यकर्ता की साधना का महत्वपूर्ण अंग है । और फिर, प्रत्यक्ष संघ कार्य के अलावा राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओं के लिए तो और भी मुसीबत है ।
साधक के नाते हर एक कार्यकर्ता की परीक्षा प्रत्यक्ष संघ क्षेत्र में होती ही रहती है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इससे भी अधिक कठोर परीक्षा जिनकी लेनी है, उनको अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। अधिक कठोर परीक्षा ।
वैसे तो मनुष्य कहीं भी फिसल सकता है । किन्तु गुसलखाने में बारम्बार पानी के प्रयोग के कारण फिसलन कई गुना अधिक रहती है । कार्यकर्ता को पूर्ण अवधि तक गुसलखाने में रहने के लिए भेजा जाता है और बताया जाता है कि कभी भी फिसलना नहीं चाहिए ।
स्त्री – राज्य में, वहां की सारी सुख-सुविधाओं के वातावरण में, कार्यकर्ता को भेजा जाता है, किन्तु उसे आदेश दिया जाता है कि तुम्हें “मायामच्छिन्दर” नहीं होना चाहिये ।
मनुष्य का ब्रह्मचर्य किसी भी अवस्था में भंग हो सकता है । किन्तु उसको जानबूझ कर मेनका के सामने खड़ा किया जाता है, और बताया जाता है कि तुम्हें ‘विश्वामित्र’ नहीं होना चाहिये ।
कितनी कठोर परीक्षा । किन्तु इसमें उत्तीर्ण होने की जिनकी क्षमता है, ऐसा अनुमान किया जाता है, उनको ही अन्य क्षेत्रों में भेजने की पद्धति रही है । इसीलिये पं. दीनदयाल जी को कहा गया था कि “जब तक राजनीति में तुम्हारी रुचि नहीं है, तभी तक मैं तुमको राजनीति में रखूंगा। जिस क्षण मुझे दिखेगा कि तुम्हारे मन में राजनीति के विषय में रुचि का निर्माण हो रहा है, उसी क्षण मैं तुम्हें उस क्षेत्र से वापिस बुलाऊंगा और संघ कार्य में लगाऊँगा ।”
अन्य क्षेत्रों में कार्यरत साधकों के लिए समय-समय पर श्री गुरु जी द्वारा दिये गये मार्गदर्शन से कुछ प्रमुख अंश निम्न प्रकार हैं
” संघ के अतिरिक्त अन्यंत्र कार्य करनेवालों की दिशा में मोड़ उत्पन्न न हो, सिद्धान्तों में ढीलापन न आये तथा राष्ट्रीय विचारों को तीव्रता किंचित भी कम न हो, यह आवश्यक है ।” (खंड 6/54-55-56/ भाग्यनगर / 2.12.70)
“ अपने स्वयंसेवक समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य करते रहें और उनके जीवन में संघ विचार आधारभूत रहे । अपना कार्य भगवान का कार्य है | भगवान सब सृष्टि में है और सब सृष्टि भगवान में है। ये दोनों बातें हैं । इनका ठीक सामंजस्य हो । इस प्रकार अपने ही बल से समाजोपकारक विभिन्न सत्कार्य पुष्ट होते रहें । परन्तु उनके दोष हमें न लगें, इस ढंग से हम काम करें। जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम राजनीति द्वारा अथवा सत्ता के द्वारा पा सकेंगे, ऐसा संभ्रम हमारे मन में थोड़ा भी न रहे । अपना कार्य राजनीति को उच्छृंखल न होने देने के लिये उस पर अंकुश रखनेवाली शक्ति के निर्माण का कार्य है । परन्तु उसके लिए शर्त यह है कि हम अपने कार्य को खूब बढ़ायें और हम सब अपने निजी गुणों का उपयोग कार्यवृद्धि में करें। और अभिमान रहे कार्य की श्रेष्ठता का न कि अपने व्यक्तिगत गुणों का ।” (खंड 7/67/ आंध्र प्रांत बैठक)
“अपने-अपने क्षेत्र में विशेषतः अपनी राष्ट्रीयता का सुस्पष्ट भाव अधिकाधिक मात्रा में लोगों को समझायें तो नये नये लोग अपने साथ आकर खड़े हो जाएंगे । परन्तु हमने यदि अपने में दुर्बलता रख कर अपने ध्येय के संबंध में लचर भाषा में बताना प्रारंभ कर दिया तो सब समाप्त हो जाएगा, तथा यह ध्येय को पोषक बनने के स्थान पर एक और संकट उत्पन्न करनेवाली बात सिद्ध होगी । (खंड 7 / 109-110/नागपुर/23-3-73)
“ अपने कुछ मित्रों से कहा कि राजनीति मे काम करो। तो उसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें उसके लिये बड़ी रुचि या प्रेरणा है । यदि उन्हें राजनीति से वापिस आने को कहा तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं । अपने को गंदगी उठाने को कहा कि गंदगी उठाना चाहिये । उसी में संघ कार्य होगा। जहां रख दिया वहीं काम करना चाहिए | without reservation तभी कार्य करने की पात्रता उत्पन्न होती है । (खंड 3/32, 33 – सिंदी 16-3-54 )
“अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीति में काम करते हैं । उन्हें कार्य की आवश्यकता के अनुरूप जलसे, जलूस, आदि करने पड़ते हैं । इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है । परन्तु नाटक के पात्र के समान जो भूमिका ली उसका योग्य । निर्वाह तो करना ही चाहिए । पर हम नट की भूमिका से आगे बढ़ कर कभी-कभी लोगों के मन में उसका अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता है। यहां तक कि फिर इस कार्य में आने के लिए वे अपात्र सिद्ध हो जाते हैं । यह तो ठीक नहीं हैं । (खंड 4/4-5/इन्दौर/5-3-60)
“….इस आधार पर हमारी उनसे अपेक्षा क्या है ? संघ के कार्य, सिद्धान्त, अनुशासन, सुव्यवस्था, ध्येयवाद, आदि श्रेष्ठ भावों की इन विभिन्न क्षेत्रों में अभिव्यक्ति होती रहे, यह अपेक्षा । अपने-अपने क्षेत्रों को संघ कार्य के लिये भर्ती का क्षेत्र, (रिक्रुटिंग ग्राउंड) बनायें । उनका संघ कार्य के पोषण एवम् अभिवृद्धि की दृष्टि से उपयोग करें ।” (खंड 4/67-68-69/ इन्दौर वर्ग / 13-3-60)
“जितने भिन्न प्रकार के काम हैं उनका एक दूसरे को सहयोग मिलना और अपने-अपने कार्य के वैशिष्ट्य तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए, बाक़ी के क्षेत्रों में काम करनेवाले अपने बन्धुओं की सहायता करना, इसका भी हमें विचार करना चाहिये। एक दूसरे के साथ मेल करके, सामंजस्य से, अपना-अपना कार्य स्वतंत्र रखते हुए चलाना लाभदायक होगा । परस्पर के सहयोग से कि प्रकार हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, यह सोचना लाभदायक है ।”
” संघ के स्वयंसेवक के नाते से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाले हम सभी के विचारों, भावनाओं एवम् श्रद्धा का अधिष्ठान भी अधिक बलिष्ठ बना रहना चाहिये | अपने – अपने भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों द्वारा अपने साथ जो-जो लोग आते हैं, उनको राष्ट्र भक्ति का योग्य संस्कार देने के लिये अपने संघ कार्य की ओर आकृष्ट करना अपना धर्म है । लोगों के मन में किसी प्रकार की भावना उठने न देते हुए यह कार्यकुशलता से धीरे-धीरे करना है ।”
“… हम स्वयंसेवक हैं । जिस प्रकार कहीं भी रखे गये अंगारे अपने आसपास ऊष्णता फैलाते हैं उसी प्रकार एक-एक अग्निपुंज के समान अपना प्रत्येक स्वयंसेवक हर क्षेत्र में जाकर अपने गुण, अपनी तेजस्विता, अपने व्यवहार – माधुर्य से प्रभाव उत्पन्न करनेवाला चाहिए । अपने चारों ओर संघ के लिए योग्य वायुमंडल तथा अत्यन्त श्रद्धा का भाव उत्पन्न करानेवाला चाहिए । इसके विपरीत यदि अन्य क्षेत्रों में पाई जानेवाली, कई प्रकार की न्यूनताओं को हमने अपने अन्दर आने दिया और वहां दिखाई देनेवाली व्यक्तिगत ईर्ष्या और स्पर्धा का स्वयम् को शिकार बनने दिया तो कहना पड़ेगा कि स्वयंसेवक का कर्तव्य हमनें नहीं निभाया । यदि अन्य क्षेत्रों के वर्तमान गुणावगुणों को लेकर हम चले तथा सोचने लगे कि संघ से अपना कोई संबंध नहीं, तब तो स्वयंसेवक के नाते किसी अन्य कार्य में जाना कदापि उपयोगी नहीं होगा ।”
·
“इसलिए अपने विभिन्न कार्यों में भी अपने मन का पूर्ण संतुलन रख कर, मूल कार्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए, उन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के कार्य का हम अपने इस मूल कार्य के परिपोषण के लिए अधिकाधिक मात्रा में उपयोग करें ।” ( खंड 6 / 30-43 / नागपुर / 8-3-1970)
साधक एकान्त में रहे या सार्वजनिक जीवन में, उसके लिये सबसे खतरनाक बात बताई गई है, स्वयं खुद को पता न चलते हुए, अहंकार का निर्माण, व्यक्तिवाद का उदय ।
किस प्रकार के साधक भगवान को प्रिय होते हैं ? श्रीराम जी कहते हैं-
“कोमल चित दीनन्हि पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया॥
सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥” – ( उत्तर काण्ड 37.2)
” उनका चित्त बड़ा कोमल होता है । वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं । पर स्वयम् मानरहित होते हैं । हे भरत वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं ।”
कितना श्रेष्ठ साधक ! किन्तु श्री सन्तज्ञानेश्वर सोचते हैं कि विशेष सावधानी न बरती गई तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के भी मन में सूक्ष्म रूप से अहंकार प्रवेश कर सकता है । वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे साधकों को अहंकार से बचाने की कृपा करें ।
निरहंकार वृत्ति केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से ही नहीं, विशुद्ध भौतिक कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । यह मानी हुई बात है कि हर एक यश के पेट में आगामी अपयश के बीज हुआ करते हैं, और हर एक अपयश के पेट में आगामी यश के बीज हुआ करते हैं । ये बीज जो कार्यकर्ता देख सकेगा, वह विजय की स्थिति में हर्षोन्मत्त होते हुए, आगामी अपयश के कारणों का उन्मूलन करने के प्रयास में जुट जाएगा, और पराजय की स्थिति में हतोत्साह न होते हुए आगामी विजय के बीजों का सम्वर्द्धन करने लगेगा। इन बीजों का साक्षात्कार करने के लिए बहुत बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं । शांत, स्थिर, स्वच्छ जलाशय में आकाश के सितारों का प्रतिबिम्ब सहज रूप से पड़ता है । वैसे ही कार्यकर्ता का मन ‘सुख – दुखे समे कृत्वा लाभालाभे जयाजयौ’ इस तरह का शांत, स्थिर, स्वच्छ रहा तो आगामी घटनाओं के बीजों का प्रतिबिम्ब उसमें स्वाभाविक रूप से पड़ता है । हषोन्माद या हतोत्साह के कारण मन का जलाशय अस्थिर तथा गन्दा हुआ तो, वह कार्यकर्ता कितना भी बुद्धिमान रहे, वह भविष्य को वेध लेने में असमर्थ ही रहेगा । मन को अस्थिर तथा गंदगी से युक्त बनानेवाले जितने तत्व हैं, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व है, अहंकार ।
इस दृष्टि से साधक सावधान रहता ही है । फिर, संघ में भी उसे इस विषय में बार-बार सचेत किया जाता है। तो भी, स्वयं खुद को पता न चलते हुए साधक ध्येयवाद के स्वर्ग से फिसलकर, व्यक्तिवाद के पाताल तक कब कैसे पहुंच जाएगा,
इसका अंदाजा करना बहुत कठिन है । क्योंकि फिसलने की यह प्रक्रिया अति सूक्ष्म रहती है, खुद के भी ध्यान में नहीं आती। मैं ध्येयवादी हूं । सोचता हूं कि लाल किले पर लाल झण्डा नहीं लगना चाहिए। भगवा झण्डा ही वहां लगना चाहिए । यह सोचते-सोचते दो चार वर्ष के बाद, मेरे मन में विचार आता है कि भगवा झण्डा तो लगना ही है, तो दधों न वह लगाने का काम हमारा मजदूर संघ – किसान संघ करे ? ऐसा करने से ये दोनों संस्थाएं अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य का निर्वाह ही करेंगी । ध्येयवाद के अनुकूल ही यह है । दो चार वर्षों में यह विचार मन में दृढ़ होने के पश्चात् और एक बात मन में आती है। इन दो संस्थाओं के द्वारा ही लालकिले पर भगवा ध्वज लहराया जाएगा, यह तय है, तो क्यों न उस ध्वजारोहण का कार्यक्रम डी. पी. ठेंगड़ी के कर कमलों से ही सम्पन्न हो ? ध्येयवाद की दृष्टि से इसमें बुराई क्या है ? मैं कट्टर ध्येयवादी हूं, और भगवद्ध्वज के ही आरोहण का विचार कर रहा हूं- क्योंकि वह ध्येय सिद्धि का प्रतीक है । यह सब तो ध्येय के अनुकूल ही है ।
और फिर दूसरा भी एक विचार मन में आता है खुद को पता न चलते हुए ध्येयवाद के स्वर्ग से व्यक्तिवाद के पाताल तक । मेरे कर-कमलों द्वारा यह ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न होना ही है तो क्यों न उसकी वडियो कैसेट तैयार की जाए, और टाइम- कैप्सूल ( Time capsule) में उसको भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए । यह तो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए । फिसलन की सूक्ष्म प्रक्रिया ।
फिसलन की इसी सूक्ष्म प्रक्रिया से कितने ही श्रेष्ठ पुरुष अनवधान से अधःपतन की खाई तक पहुंच गए और कितनी ही उज्ज्वल क्रांतियां अंधकारमय प्रतिक्रांतियों में परिणत हो गईं ।
क्रांतियों या महान परिवर्तनों के लिए तत्कालीन परिस्थितियां ही जिम्मेदार रहती हैं, यह सोचना ठीक नहीं है । परिस्थितियों का योगदान अवश्य रहता है, किन्तु निर्णायक भूमिका कार्यकर्ताओं की इच्छा-शक्ति की हुआ करती है। थॉमस कार्लाईल कहत है | Instead of saying that man is the creature of Circumstances, say that man is the architect of Circumstances. ” यही वास्तविकता है । ऐतिहासिक परिवर्तनों का निर्णायक तत्व परिस्थिति नहीं, मनः स्थिति -साधकों की – होता है ।
‘पथिक’ यह अपने ढंग की अनोखी कृति है । दैवी और असुरी शक्तियों का जो संग्राम निकट भूतकाल में भारत की धरती पर हुआ और जो वर्तमान काल में भी चल रहा है – उसका विश्वसनीय इतिहास यानी ‘पथिक’ । सर्वसाधन सम्पन्न आसुरी शक्ति पर मात करने का प्रण किए हुए साधनविहीन देवशक्ति की विजय यात्रा का उज्ज्वल इतिहास | “रावण रथी विरथ रघुवीरा” – इस युक्ति का पुनः स्मरण करा देने वाला
इतिहास | यह संग्राम है धर्म का अधर्म के साथ, सत्य का सत्ता के साथ, साधना का साधनों के साथ । जनसाधारण के मन में उत्सुकता है यह जानने की, कि इस द्वितीय रामायणीय युद्ध में विजय किसकी होगी ?
सामान्य व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय हिसाब करता है, दोनों तरफ साधनों का । सर्वसाधारण धारणा यही है कि जिधर साधन अधिक उधर ही विजयश्री झुकेगी।
हिन्दूराष्ट्र के लिए यह समाधान का विषय है कि इस रणक्षेत्र में सक्रिय सभी लोग – सिपाही हों या सेनापति – स्वयं अपने को साधक की भूमिका में ही रख रहे हैं और अविचल मन से, विशुद्ध साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं । परमपूजनीय श्री गुरुजी के दिए हुए मार्गदर्शन के प्रकाश में वे यह संघर्ष चला रहे हैं । ध्येयवाद के पारसमणि का स्पर्श हृदयों को होने के कारण, लोहे का परिवर्तन स्वर्ण में हो गया है । मनुष्य-स्वभाव – सुलभ दुर्बलताओं का स्पर्श इन हृदयों को नहीं हो रहा है । साधकों की इस विशाल तथा सर्वव्यापी सेना को देखकर 350 वर्ष पूर्व का दृश्य मनःचक्षु के सामने आता है । समर्थ रामदास कहते हैं-
भिक्षण्डी चालल्या फौजा – हरिभक्तांच्यां । ।
“हरिभक्तों की सेनाएं भूखण्ड में संचार कर रही हैं। इस सेना का सम्बल, साधन नहीं साधना है । उसकी सघनता जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही विजयश्री निकट आती जाएगी ।
क्या यह सब विशुद्धता के साथ सम्पन्न होगा ? क्या सभी साधक फिसलन से खुद को बचा सकेंगे ?
इसका उत्तर तो भविष्यकाल ही दे सकता है । किन्तु कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जो इस विषय में सभी को आश्वस्त कर सकती हैं ।
व्यक्तिगत सम्पर्क में आए लोग सभी साधकों के विषय में आश्वस्त हैं कि वे जीवन के अन्तिम क्षण तक अपनी शुचिता कायम रखेंगे । प्रत्यक्ष सम्पर्क में आए अनुभवों के आधार पर उनका यह निष्कर्ष है । कितने ही साधकों से सम्बन्धित कितनी ही आश्वासनकारी घटनाएं । सबको एकत्रित – ग्रंथित किया जाए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ बन जाएगा और ऐसा बनना भी चाहिए । परन्तु स्थानाभाव के कारण यहां एक ही उदाहरण प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा ।
रामजन्मभूमि संघर्ष में जिनको Generalissimo माना गया ऐसे अशोक जी सिंहल से सम्बन्धित यह घटना है । अपने कर्तृत्व के तथा लोकप्रियता और प्रसिद्धि के कारण अहंकारी बनने का भौतिक (नैतिक नहीं) अधिकार सबसे अधिक अशोक जी को ही प्राप्त है । उनका यह उदाहरण ।
नई दिल्ली के फिक्की सभागार में हुआ एक समारोह । अशोक जी को उसमें निमंत्रित किया गया । उनको बताया गया कि यह आयोजन ‘भामाशाह जयन्ती’ के निमित्त है । किन्तु अशोक जी के आगमन के पश्चात् वहां अशोक जी का ही अभिनन्दन समारोह सम्पन्न होने लगा । मालाओं को पहनते – उतारतें समय अशोक जी अपने आप को बहुत उलझन और परेशानी से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनके चेहरे पर से स्पष्ट दिखाई दे रहा था । यह अभिनन्दन कार्य उनके स्वभाव को बिल्कुल जंचनेवाला नहीं था, यह बात उनकी पारदर्शक मुद्रा से सभी के ध्यान में आ रही थी । दिखता था कि ये औपचारिकताएं उनके शरीर के लिए असह्य थीं । किन्तु शालीनतावश मर्यादाओं का भान रहने से तय नहीं कर पा रहे थे कि उस स्थिति में क्या करना उचित था ‘ककर्मकिम कर्मेति’
अन्त में अपने भाषण में हृदयाविष्कार किया। कहा – ” एक बार रामलीला मैदान, दिल्ली में आयोजित किसी सभा में श्री गुरुजी पहुंचे हुए थे । उनका छायाचित्र लेने के लिए पत्रकार यहां-वहां घूम रहे थे । गुरुजी ने अपने अंगवस्त्र से मुँह इस तरह ढांप लिया कि चित्र में चेहरा न आ सके ! पर छायाचित्रकारों से मुक्ति कहां ? दूसरे दिन समाचार पत्रों में उनका चित्र छपा । वैसा ही छाप दिया था जह चित्र और लिखा था ‘Guruji camera shy’ मैंने स्टेशन पर गुरुजी को यह बात बताई, तो वह सहज भाव से बोले -“I am doing my duty and want to go unobserved.” उस समय बात उतनी गहराई से हम लोगों को समझ में नहीं आई । पर अब लगता कि हम लोग जो समाज कार्य में लगे हैं, उनका शरीर सचमुच वह स्थिति सह नहीं पाता है । और आज मैंने स्वयं यह अनुभव किया है कि यह सब हमारे लिए असह्य है ।”
इस पर भाष्य अनावश्यक है ।
किन्तु यह संग्राम बहुत बड़ा है । प्रदीर्घ काल तक चलने वाला है । ‘जय पराजय, प्रगति-अवनति, सुख-दुखों का देख नर्तन’ असंख्य साधकों ने स्वयं अपने को साधना की विशुद्ध राह पर अनवरत चलाना है । इसके लिए विशेष प्रयास अनवरत करते रहना अपरिहार्य है । अहंकार का स्पर्श मुझें कभी नहीं हो सकता’ यह भी एक अहंकार ही है ।
इन सभी फिसलनों से बचने के लिए ऐसे विशुद्ध, परम साधक का चिंतन, मानस पूजन, अखंड करते रहने की आवश्यकता है, जिसका स्मरण संकटमोचन कारक है । जो स्वयं ‘बुद्धिमताम् वरिष्ठ’ तथा ‘वानर यूथ मुख्य’ होते हुए भी ‘श्री रामदूत’ रहने में ही परम सुख का अनुभव करता रहा । जो आन्तरिकतापूर्वक ध्येय देवता को कह सका-
” देहबुद्ध्या तुदासोऽहम् – जीवबुद्ध्या त्वदंशकः।
आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् – त्वमेवाहम् न संशयः॥”
इस मनःस्थिति का शब्दों में वर्णन करना असंभव है ।
आज के देवासुर संग्राम में साधकों ने भीम पराक्रम किए हैं। 1990 की 30 अक्तूबर और 2 नवम्बर को तथा 6 दिसम्बर को । भीम पराक्रम । किन्तु, उनकी इस पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या रही ? अहंकार की ? हर्षोन्माद की?, ‘जितम् मया’ की ?
वे साधक इतने प्रगतिशील नहीं थे। उनके मन-मस्तिष्क में परम – साधक का आदर्श था ।
हनुमानजी का अद्भुत पराक्रम देखकर प्रभु प्रसन्न हुए । हनुमान जी को उठा कर हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। कहा- हे हनुमान् बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाँके किले को तुमने किस तरह जलाया ? हनुमान् जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले-
“साखामृग कै वहि मनुसाई । साखा तें साखा पर जाई ।।
लांवि सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ।”
” बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है । मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस को मार कर अशोकवन को उजाड़ डाला ।”
” सो सब तव प्रताप रघुराई ।
नाथ न कछु मोरि प्रभुताई ।”
“यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी ! आप ही का प्रताप है । हे नाथ ! इसमें मेरी प्रभुता (बढ़ाई) कुछ भी नहीं है । “
“हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हों, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है । आपके प्रभाव से रुई ( जो स्वयं बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है) बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है (अर्थात् असम्भव भी सम्भव हो सकता है ) ।
“नाथ भगति अति सुखदायनी ।
देहु कृपा करि अनभावनी । ।”
” हे नाथ ! मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए ।”
” सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । ‘एवमस्तु तव कहेउ भवानी । ।”
“हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी ! तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ‘एवमस्तु’ (ऐसा ही हरो) कहा । “
रघुकुल नायक का ‘एवमस्तु’ ही साधक का पाथेय है। इसी पाथेय के बल पर पथिक का साधकों का साधना प्रवास फलीभूत होता रहता है ।
हम सभी साधक वसिष्ठ जी के शब्दों में प्रभु से प्रार्थना करें –
“नाथ एक वर मागउँ राम कृपा कर देहु ।
जन्म-जन्म प्रभुपद कमल कबहुँ घटै जनि तेहु । । (उ. काण्ड, 48 ।।
” हे नाथ ! हे श्रीराम जी ! मैं आपसे एक वर मांगता हूं, कृपा करके दीजिए प्रभु (आप) के चरणकमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मान्तर में कभी न घटे । ” इसी प्रार्थना से साध्य, साधक और साधना एकरूप हो जाते हैं । || जय श्री राम ||
| साभार संदर्भ |
| श्री रामकुमार भ्रमर के विख्यात उपन्यास “पथिक” की भूमिका श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने लिखी थी। यह उपन्यास रामकथा पर आधारित है। प्रकाशक-राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 2/38 अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली-110002 |