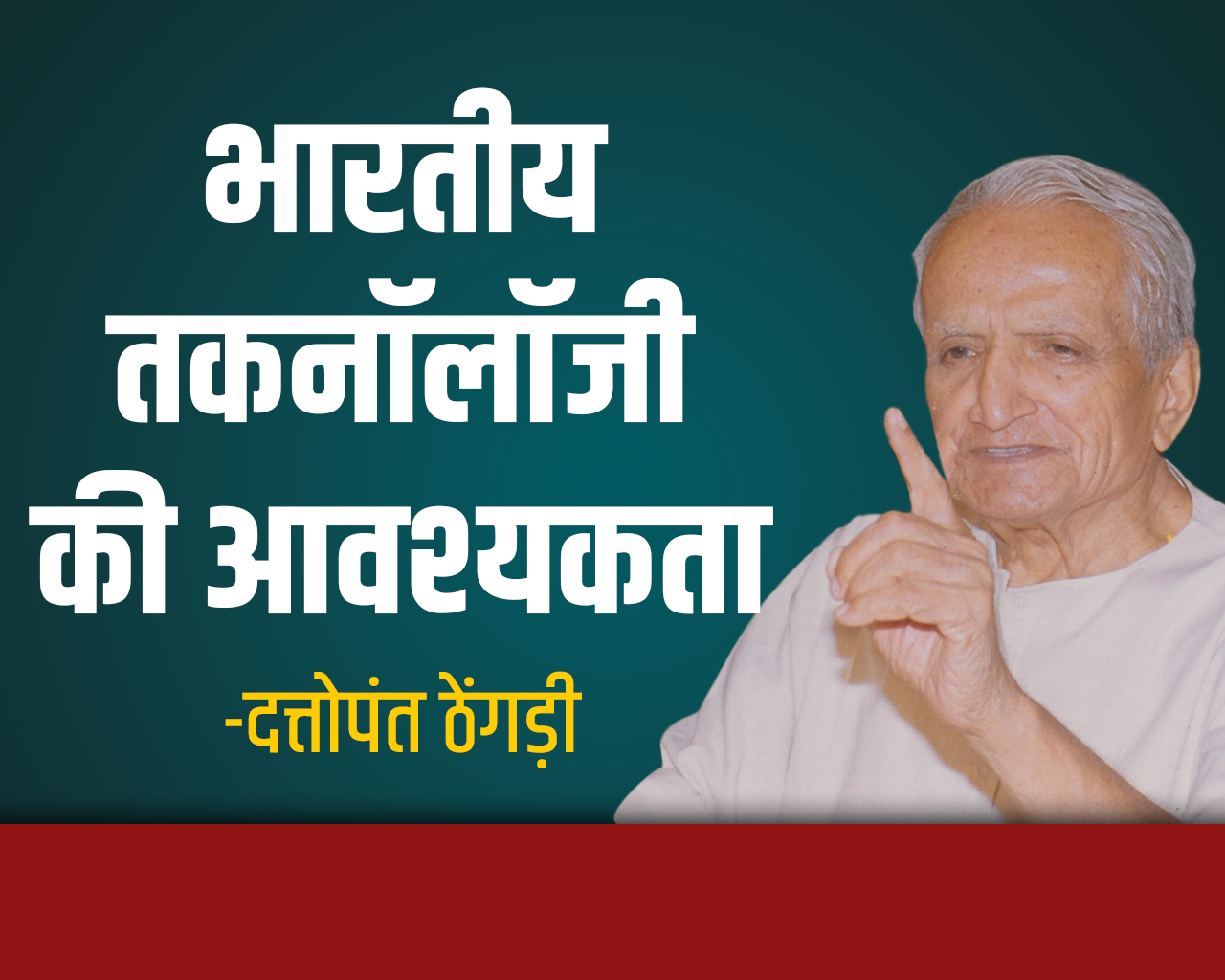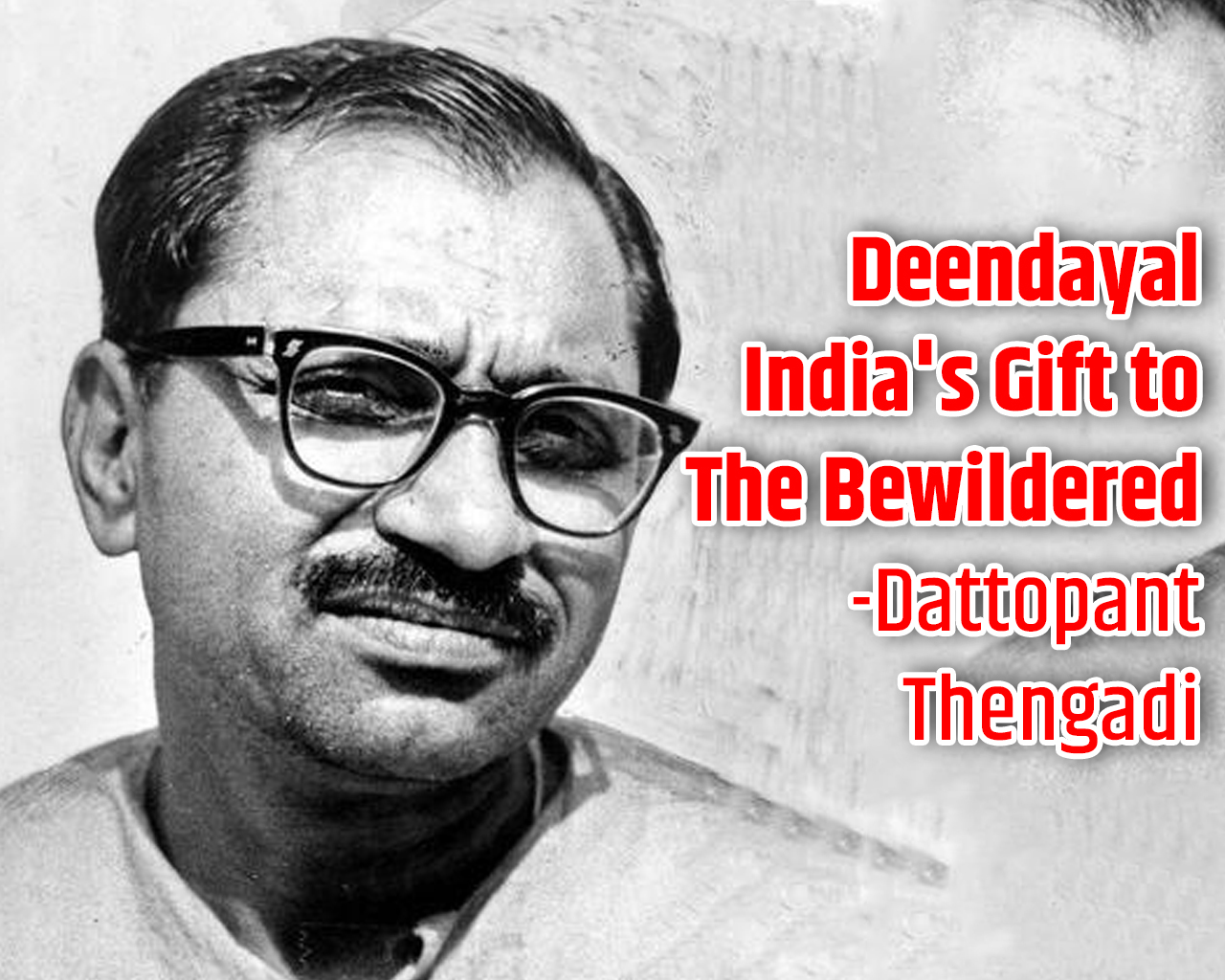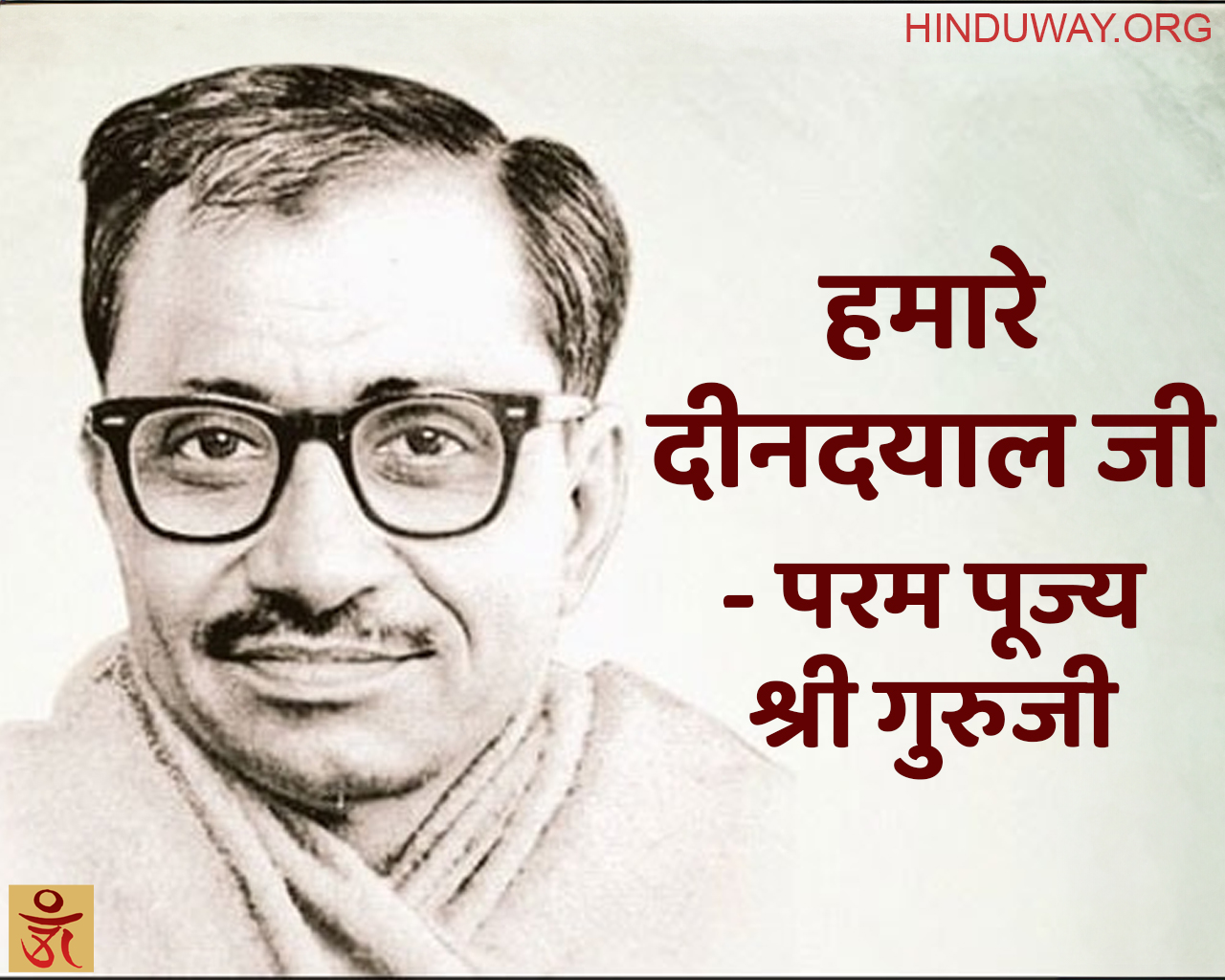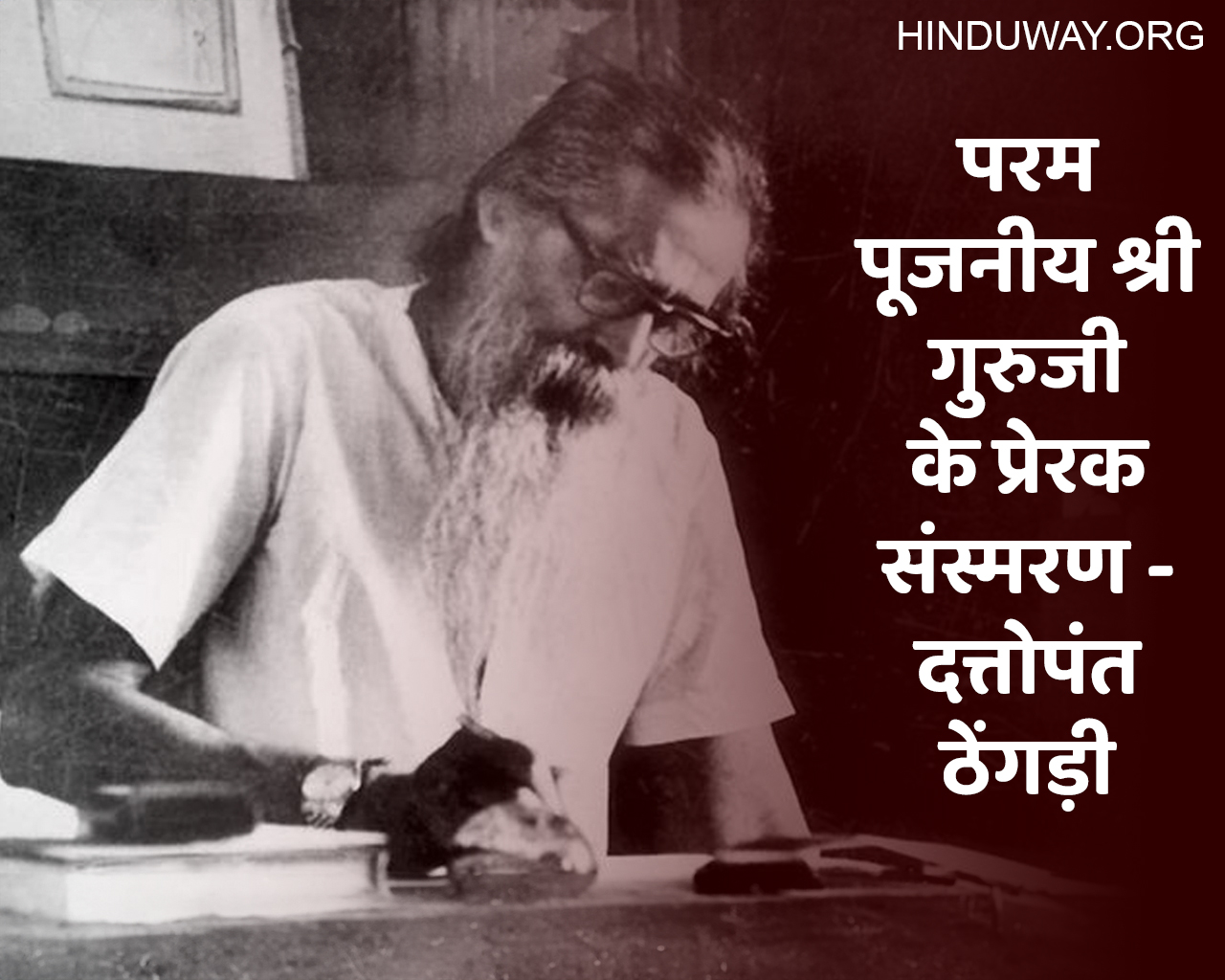हमारे देश के तथाकथित प्रगतिवादी लोग पाश्चात्य सभ्यता की चमक-दमक से अत्यधिक मोहित और प्रभावित है। पश्चिम की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति निश्चय ही प्रभावशाली है। एक विकासशील राष्ट्र होने के नाते, हमारा यह कर्तव्य है कि उनकी भौतिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करें तथा अनुकरण, परिष्करण, अनुकूलन अथवा अस्वीकृति के हेतु उसकी पूरी छानबीन करें।
लेकिन इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि तकनॉलॉजी का अनुकरण आयात तब तक संभव नहीं है जब तक उस तकनॉलॉजी को जन्म देने वाले देश अथवा देशों की संस्कृति के कुछ अंश का भी अनुकरण या आयात न किया जाय । विदेशी तकनीकों, कार्य-पद्धति अथवा तकनॉलॉजी की स्वीकार करते समय हमें उन्हें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के अनुकूल बनाने का ध्यान भी रखना होगा। इस बात के जागरूक प्रयास करने होंगे कि जो कुछ विदेशी है उसे परिष्कृत करके अपने देश की मूल संस्कृति का अभिन्न अंग बना लिया जाय ।
पश्चिम की संकेंद्रीयता
भारतीयों के विपरीत पश्चिमी लोगों ने केंद्रीयता के भाव का पोषण किया है। केवल इतना ही नहीं, जहां पश्चिम को यह श्रेय जाता है कि उसने ऐसे अनेक वैज्ञानिक और धार्मिक आचार्य पैदा किये है जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन खपा दिया, वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक औसत पश्चिम-वासी के पास भावी पीढ़ियों के कल्याण के बारे में सोचने के लिए समय या प्रवृत्ति ही नहीं है। दूरगामी दृष्टि से देख पाने में वह असमर्थ है। बिना इस बात की परवाह किये कि मानव जाति के भविष्य पर इसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है, वह केवल वही चीज स्वीकार और लागू कर रहा है जो उसके अपने या उसकी पीढ़ी के लिए तत्काल लाभकारी है।
उदाहरण के तौर पर वह अपने प्राकृतिक पर्यावरण का निरन्तर दुरुपयोग कर रहा है। वह विनाशकारी तरीके से प्राकृतिक साधनों का शोषण कर रहा है। निस्सन्देहः इसके कारण पश्चिम, पूर्व से आगे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि डेढ़ शताब्दी से भी कम समय में हम प्रकृति प्रदत्त विभिन्न इंधनों के भंडार को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। आज वैज्ञानिक बुरी तरह से अणु- शक्ति के प्रयोग की ओर झुक रहे हैं। लेकिन विश्व के पास यूरेनियम और थोरियम के भंडार भी असीमित नहीं है। आने वाली पीढ़ी के कल्याण पर इसका क्या प्रभाव होगा ?
माता-प्रकृति
हिन्दुओं ने प्रकृति को हमेशा माता के समान माना है। यहां तक कि जब वे गाय की माता के रूप में पूजा करते हैं और उसका दूध निकालते हैं तो भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बछड़े के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध छोड़ दिया जाय और दूध दुहने की प्रक्रिया में रक्तस्राव के कारण गाय की मृत्यु न हो जाय। अपने स्वार्थ साधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल वे भी करते हैं, किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा छोड़ दी जाए और प्रकृति माता का अन्धाधुन्ध ध्वंस न किया जाये। इससे बहुत से तात्कालिक लाभों से वह भले ही वंचित रहे हो, परन्तु प्रकृति का संतुलन बनाये रखा गया है।
भूमि, जल और वायु मुफ्त होते हुए भी प्रकृति की अमूल्य भेंट है। परन्तु पाश्चात्य औद्योगीकरण इन तीनों दिव्य खजानों के साथ हेराफेरी कर रहा है।
भूमि का विनाश
वैज्ञानिक अब इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि रसायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने प्रकृति की जीवन-शक्ति का संतुलन बिगाड़ दिया है, रसायनों और अन्य कृत्रिम पदार्थों ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पुनरुत्पादन की प्राकृतिक प्रक्रिया को दोषपूर्ण व अनिश्चित बना दिया है, जबकि इनका उत्पादन पशुओं और पौधों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। लंबे समय तक कृत्रिम खादों के अत्यधिक प्रयोग ने उपजाऊ भूमि में किसी भी प्रकार की फसल पैदा करने की क्षमता को समाप्त कर दिया है । अत्यधिक सिचाई के परिणाम स्वरूप भूमि का लवणीकरण हुआ है और वनोच्छेदन की बढ़ती हुई प्रक्रिया से कुछ तात्कालिक लाभ भले ही हुआ हो, परन्तु उसका दीर्घकालीन परिणाम रेतीले रेगिस्तानों के विस्तार और बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण की समस्याओं के रूप में हुआ है।
जल प्रदूषण
जलस्रोतों के साथ भी खिलवाड किया जा रहा है। जापान में औद्योगिक कचरे के कारण नदियों और समुद्र तट का जल खतरनाक सीमा तक बोझिल हो गया है। साइबेरिया का शुद्ध जल कागज और अन्य सोवियत उद्योगों के द्वारा प्रदूषित हुआ है । राइन नदी का जल तो इस कदर संदूषित हुआ है कि उसमें सैकड़ों मील तक न तो मछली और न ही पानी के अन्य जीव जीवित बच सकते हैं। कारखानों से निकले तेल पदार्थों की छ: इंच मोटी तह राइन नदी के पानी पर उसके उद्गम से लगाकर कम से कम दो सौ मील तक फैल गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भी ऐसी नदी या झील का मिलना असंभव हो गया है जो औद्योगिक कचरे या ठोस कूड़े-करकट जैसे कागज के डिब्बों, गत्ते के आवरणों या अन्य ऐसी बेकार की चीजों के कारण प्रदूषित नही गया हो। अमेरिका की नदियों में हर रोज कम से कम २००० टन ठोस कचरा बहाया जा रहा है।
औद्योगिकीकरण ने औद्योगिक कचरे की विकराल समस्या उत्पन्न कर दी है। बेकार आटोमोबाइल वाहनों के ढांचे, लाखों टन रद्दी, लोहा, इस्तेमाल करके फेंकी हुई शीशे की बोतलें व टीन के ढक्कन आदि के अम्बार लग गये हैं। भस्मीकरण, पुनर्नवीकरण एवं दोबारा इस्तेमाल करने आदि अनेकों उपाय भी इस समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं।
वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण ने तो और भी कठिन और खतरनाक समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक केन्द्रों के चारों ओर की वायु में ३००० से भी अधिक नये व विदेशी रसायनिक तत्व पाये गये हैं। सारा वायुमंडल ठोस पदार्थों जैसे राख, रबर के टुकड़ों, एसबसटॉस आदि के अतिरिक्त कार्बन मोनोक्साइड, और डायोक्साइड, सल्फर डायोक्साइड और विभिन्न प्रकार की नाइट्रोजन आक्साइड आदि गैसों से भरा हुआ है। इन सब से मानवीय स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप दमा, गलशोध का रोग, फेफड़ों का कैंसर, और वातशोध जैसी बीमारियां फैल रही हैं।
औद्योगिक केन्द्रों के आसपास के वायुमण्डल मे संदूषक पदार्थों के टनों मात्रा में रहने से पौधों और पशुओं के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि भवन, मशीनों और सड़कों पर धुंए और कोहरे का मिश्रण जिसे ‘स्मोग’ कहा जाता है, मोटरावलम्बी पश्चिम के लिये सरदर्द बनता जा रहा है। जापान जैसा देश भी जो पश्चिम का अनुकरण करते समय बहुत सावधान रहता है, ओद्योगीकरण के दुष्प्रभावों से नहीं बच सका है। टोकियो के कुछ भागों में लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के लिये गैस-मास्क पहनने को विवश होना पड़ता है।
कितना अन्धानुकरण
श्री मारिस स्ट्राग ने जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण के बारे सम्मेलन के आयोजन का दायित्व सौंपा गया था, ने कहा है कि पर्यावरण को केवल दौलतमंद देश की समस्याओं से जोड़ने की प्रवृत्ति गलत है। क्योंकि पर्यावरण विकासशील देशों अथवा गरीब देशों के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है। उनके कथनानुसार, यह तमाम दुनिया को प्रभावित करने वाली एक मानवीय समस्या है।
क्या हम भी वही रास्ता अपनाए? क्या हम भी उसी चक्र में भटकते रहें, जहां पहले गलतियां की जाती है और फिर उनमें सुधार का प्रयास किया जाता है ? पाश्चात्य लोगों ने शीघ्रातिशीघ्र भौतिक विकास करने की अशोभनीय जल्दबाजी के कारण पर्यावरण की पूर्ण उपेक्षा की, और अब उनमें से समझदार लोग इस भूल के लिए पछता रहे हैं। क्या हम भी प्रगतिवाद के नाम पर पर्यावरण के पहलुओं के प्रति उतने ही विस्मरणशील हो जाए ? यह प्रश्न इसलिए और भी सार्थक बन जाता है, क्योंकि हिन्दुओं ने प्रकृति माता को दुहने के प्रति एक अलग दृष्टि को अपनाया है। इसे पश्चिम के अनुकरण को अंधी दौड़ के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिये ।
औद्योगीकरण की वर्तमान अवस्था में भी जल और वायु के प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए कानून बनाये जाने चाहिए ताकि यह तय किया सके कि विभिन्न औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण और बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का प्रकार व मात्रा क्या है?, इस प्रदूषण में प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान की कितनी जिम्मेदारी है? और विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्रदूषण की सामाजिक कीमत वसूल करने का तरीका क्या हो? इस संदर्भ में एक और विषय का गहरा अध्ययन किया जाना चाहिए वह है उपयुक्त टेक्नोलॉजी (एपॉप्रिएट टेक्नॉलॉजी)।
पश्चिम को बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीक के पसंद है और उसने उनका विकास भी किया है। साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों इसी तकनीक के पक्षधर है। वह अधिक पूंजी वाले, विशाल उद्योगों को प्रोत्साहन देते हैं। कम से कम लोगों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन, यही पश्चिम की रणनीति है। किन्तु क्या यह भारतीय पर परंपराओं, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल है ?
यह तो सत्य है कि इस समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिये। जो बड़े पैमाने के उद्योग अब तक स्थापित हो चुके हैं, उन्हें अब हम उखाड़ नहीं सकते। भविष्य की योजनाओं में भी जहां-जहां अर्थनीति की आवश्यकताओं की मांग होगी वहां-वहां बड़े पैमाने की उत्पादन की तकनीकों को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी नयी रचना का विचार करते समय उसमें मशीनीकरण को उसका उचित स्थान दिया ही जाना चाहिए।
छोटे पैमाने के उद्योगों का औचित्य
किन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बड़े पैमाने के उद्योगों का विस्तार ही औद्योगीकरण का एकमात्र प्रकार नहीं है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अधिक उत्पादन के लिए उद्योगों का विशालकाय होना आवश्यक नहीं है। अधिक उत्पादन की वर्तमान तकनीकों का रोजगार के अवसरों के साथ कोई मेल नहीं है जबकि इस समय हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की यह सबसे बडी आवश्यकता है। मशीनीकरण के प्रकार भिन्न हो सकते है, मशीनीकरण के रूप अलग-अलग हो सकते हैं। इनमें से कुछ आज के प्रचलित पश्चिमी प्रकार से भिन्न हो सकते हैं। लघु उद्योगों के पक्ष में ये तथ्य भी जाते हैं कि स्वचालित मशीने, कृत्रिम मिश्र धातुएं, ठप्पा डालने की विधियां, नाप-तोल के लघु यन्त्र एवं ऊर्जा वितरण को नयी विधियों के विकास आदि के बारे में नई तकनीकी खोजों के कारण लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन की तकनीकी असुविधायें अब बहुत कम हो गई है।
एकांगी आयोजन
भारी उद्योग थोप तो दिए गए हैं पर वे शेष अर्थव्यवस्था के साथ समरस नहीं हो पाए हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के साथ कोई तालमेल नहीं बैठाया गया है।
औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का सहयोगी न होकर उसके समानान्तर चल रहा है। गैर पूंजीकरण व रोजगार के अवसरों में कमी करने जैसी प्रक्रियाए इस लिए शुरू हुई हैं क्योंकि मनुष्य, कच्चा माल, धन, मशीन, प्रबन्ध, प्रेरणा और बाजार—इन सात तत्वों का पूर्ण और समग्र रूप में विचार नहीं किया गया । भारतीय परिस्थितियों में विदेशी तकनॉलॉजी के प्रवेश ने न केवल बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया है, अपितु कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग न हो पाने की समस्या भी उत्पन्न की है। इन सबसे औद्योगिक नियोजन की ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसमें से उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतम उपयोग करने व राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान नहीं रखा गया है, जो असन्तुलित व एकांगी है।
भारतीय तकनॉलॉजी क्या हो ?
भावी योजना बनाते समय ऐसी विशुद्ध भारतीय तकनॉलाज़ी के विकास पर ज्यादा जोर देना होगा, जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया ऊर्जा चालित होते हुए भी विकेन्द्रीकरण की दिशा में अग्रसर हो अर्थात् जिसमें फैक्टरी के बजाय घर को उत्पादन का केन्द्र बनाया जाय। इन नई तकनीकों से उत्पादन के हमारे साधनों का कम से कम गैर-पूंजीकरण होना चाहिए। हमारे कारीगरों को परम्परागत तकनीकों से नई तकनीकों की ओर जाने में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लघु उद्योगों को प्रबन्ध करने की जो भी कार्यकुशलता आज उपलब्ध है, वह नई व्यवस्था के अन्तर्गत बेकार नहीं जानी चाहिए। कम पूंजीवाले व्यक्तियों को भी पूंजी लगाने का अवसर मिलना चाहिए।
नई टेक्नोलॉजी हमें आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए और उसके द्वारा मशीनों, कल पुर्जों, पूंजी, टेक्नीशियनों इत्यादि चीजों के बारे में हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता समाप्त होनी चाहिए। जहां कहीं अनिवार्य हो वहां बड़े पैमाने के उद्योग लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन प्राथमिकता उत्पादन की विकेंद्रित प्रक्रिया को देनी होगी ताकि उसमें ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को पाटा जा सके, कृषि और उद्योग के बीच अधिकाधिक समन्वय पैदा हो सके और बड़े व लघु उद्योग एक दूसरे के पूरक बन सकें ।
हमारे तकनीशियनों की भूमिका
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे तकनीशियनों को संसार भर की औद्योगिक तकनॉलॉजी का गहन अध्ययन करते हुए उसे आत्मसात् करना पड़ेगा। उन्हें विदेशी तकनॉलॉजी के वे अंश ढूंढकर लागू करने होंगे जो भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। साथ ही उत्पादन की परम्परागत तकनीकों में ऐसे परिवर्तन करने होंगे, जो हमारे कारीगरों के लिए लाभप्रद हो और जिन्हें सरलता-पूर्वक ग्रहण किया जा सके। जिनमें बेरोजगारी बढ़ने का जोखिम न हो, उपलब्ध प्रबन्धकीय और तकनीकी कुशलता नष्ट न हो और उत्पादन के वर्तमान साधनों का पूर्णतः गैर-पूंजीकरण हो ।
इस कार्य में प्रमुख बाधा हमारे नेताओं की मानसिक गुलामी है। हम ऐसी किसी तकनॉलॉजी को प्रशंसनीय नहीं मानते जिसका आयात न किया गया हो। यही कारण है कि डा० शुमाखर द्वारा प्रस्तुत मध्यवर्ती तकनॉलॉजी विचार को भी अपेक्षित गम्भीरता से नहीं लिया गया। इस ब्रिटिश अर्थशास्त्री का कहना है कि तकनॉलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो उपलब्ध पूंजी और श्रम के अधिकतम उपयोग का, हमारे देश में विद्यमान पूंजी के अभाव और भारी बेरोजगारी के आर्थिक सत्य के साथ तालमेल सके बेठा सके। इस तकनॉलॉजी के द्वारा औद्योगिक विकास में लगने वाले प्रत्येक रुपये में रोजगार के अवसर पैदा करने का सामर्थ्य सौ गुना बढ़ना चाहिये, किन्तु साथ ही उत्पादन की प्रति इकाई दर में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
मध्यवर्ती तकनॉलॉजी
डाॅ सुमाखर के अनुसार मध्यवर्ती टेक्नोलॉजी में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के साथ-साथ औद्योगिक कुशलता में तनिक भी कमी ना आने दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर शोध करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर कहां-कहां यह संभव है, कि कुशलता में कोई कमी ना आने देते हुए भी उत्पादन यंत्र के आकार को छोटा किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के बल पर यह कहां तक संभव है, कि गांव से शहरों की ओर आने वाले लोगों की संख्या कम की जा सके। क्या इस आधार पर यह संभव है कि छोटे कस्बों और गांवो में नए उद्योगों को स्थापित किया जाए, जिनमें स्थानीय पूंजी, स्थानीय श्रम, स्थानीय कच्चा माल, स्थानीय प्रबंधन कुशलता और स्थानीय उद्यम प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सके। क्या ऐसे उद्योग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, यदि कुशल बाजार व्यवस्था, समुचित आधारभूत ढांचा और स्वदेशी की भावना की पुनर्स्थापना का सहारा उन्हें मिले। क्या क्षेत्र अनुसार नई योजना बनाना व्यावहारिक एवं उचित होगा? अच्छा तो यह रहेगा कि इस दृष्टि से हम पहले कुछ निश्चित उद्योगों जेसे चमड़ा या चीनी मिट्टी उद्योग को छांट लें और उनके भविष्य पर मध्यवर्ती टेक्नोलॉजी के संभावित प्रभावों का जायजा लें। यह अध्ययन के नए रास्ते खोल सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विशुद्ध देसी टेक्नोलॉजी के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह सत्य है कि उत्पादन की सभी शाखाओं में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा सामान नहीं हो सकती, यहां तक कि एक ही उद्योग के भीतर भी पूंजी व श्रम का समान अनुपात निश्चित करने की दृष्टि से कोई अकेली टेक्नोलॉजी सदैव लाभकारी नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी के कई स्तर साथ-साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन हमें भारतीय टेक्नोलॉजी के ऐसे विकास और उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग पर जोर देना चाहिए जिसमें आय की वृद्धि के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर रोजगार के अवसरों की भी वृद्धि हो सके।
शहरीकरण की दौड़
स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति का अस्तित्व और विकास भी इस समस्या से गहरा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्कृति अपने वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से जो कि मुख्यतः उत्पादन की तकनीक पर निर्भर करता है , संबंध विच्छेद करके केवल शून्य में पनप सके। विदेशी टेक्नोलॉजी कभी अकेले नहीं आती, वह अपने जन्मदाता देश की संस्कृति को भी अपने साथ लाती है। पश्चिम से आयातित विशाल उत्पादन वाली टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा अनुभव यही रहा है।
इन तकनीकों का परिणाम पूंजी और श्रम के शहरी क्षेत्र में केंद्रीकरण में हुआ है। इसके कारण परंपरागत संयुक्त परिवार प्रणाली और गांव की स्वायत्त जिंदगी में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण ने जो समस्याएं पैदा की है, उनका स्वरूप संस्कृतिक होने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक भी है।
भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा और विकास पूर्वकाल में इसलिए हो पाया क्योंकि तीन विभिन्न स्तरों पर अर्थात वंशानुगत परिवार, औद्योगिक या व्यावसायिक परिवार, और क्षेत्रीय परिवार के स्तर पर पारिवारिक वातावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रबंध किया गया था।
एक बार शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में वंशानुगत परिवारों का विनाश शुरू हो जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में एक स्वस्थ पारिवारिक इकाई का गठन बहुत कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरुप वे संस्कार जो पारिवारिक माध्यम से सहज रूप से एक पीढ़ी से दूसरी को मिल जाते थे, अब नए औद्योगिक वातावरण में आगे नहीं पहुंच रहे हैं। पुरानी व्यवस्था तो दूर रही ऐसी किसी नई प्रणाली का भी अभी जन्म नहीं हुआ है, जो इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। परंपरागत, व्यावसायिक या औद्योगिक परिवारों का अस्तित्व पहले ही निरर्थक बन चुका है।
परम्परागत औद्योगिक परिवार
आज न गांव में और ना ही शहर में कोई औद्योगिक या व्यावसायिक परिवार बाकी बचा है किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी संस्कृति के अस्तित्व की रक्षा काफी हद तक सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर आधारित रही है और व्यावसायिक या औद्योगिक परिवार इस ढांचे का अभिन्न अंग रहे हैं। यहां फिर हमारे सामने ,”अजन्मे कल और मृत कल” की समस्या खड़ी हो जाती है। हमारी क्षेत्रीय इकाइयां वे क्षेत्रीय परिवार थे, जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र में बसे हुए सब वंशानुगत परिवार सम्मिलित थे। यह तीनों अंग अपने-अपने स्तर पर स्वायत्तता का उपयोग करते थे। वंशानुगत संयुक्त परिवार को अपने आंतरिक प्रशासन को चलाने के लिए विधि विधान बनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। प्रत्येक औद्योगिक परिवार के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते थे, जिनका किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण अथवा विनिमय से संबंध होता था। आंतरिक प्रबंध के लिए औद्योगिक परिवार को पूरी स्वतंत्रता थी। गांव या परगना स्तर पर भी पारिवारिक जीवन स्वायत था। यह सुनिश्चित है कि इन तीनों अंगों का अपना अनुशासन था, जो परस्पर विरोधी नहीं था और जो राष्ट्रीय अनुशासन ढांचे के अंतर्गत था। प्रत्येक अंग को अपने आंतरिक प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन अपने से वरिष्ठ अंग के अधिकार क्षेत्र में वह अनुशासन का पालन करता था। इन तीनों इकाइयों को मिलकर ही भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा बना था। अब तक का हमारा अनुभव हमें बताता है कि विशाल उत्पादन टेक्नोलॉजी इन तीनों इकाइयों के अस्तित्व के लिए पोषक नहीं है।
नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता
अतः यह अनिवार्य हो जाता है की सबसे पहले उत्पादन की ऐसी नई प्रणाली की खोज की जानी चाहिए जो इन सामाजिक अंगों को जीवित रखने में सहायक सिद्ध हो और द्वितीयत: ऐसे नए रास्ते निकाले जाएं जिनसे विशाल उत्पादन को अपनाने वाली औद्योगिक क्षेत्रों में इन इकाइयों को पुनर्जीवन प्राप्त हो सके।
| साभार संदर्भ |
| दीनदयाल शोध-संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका मंथन के विशेषांक 1980 में प्रकाशित |