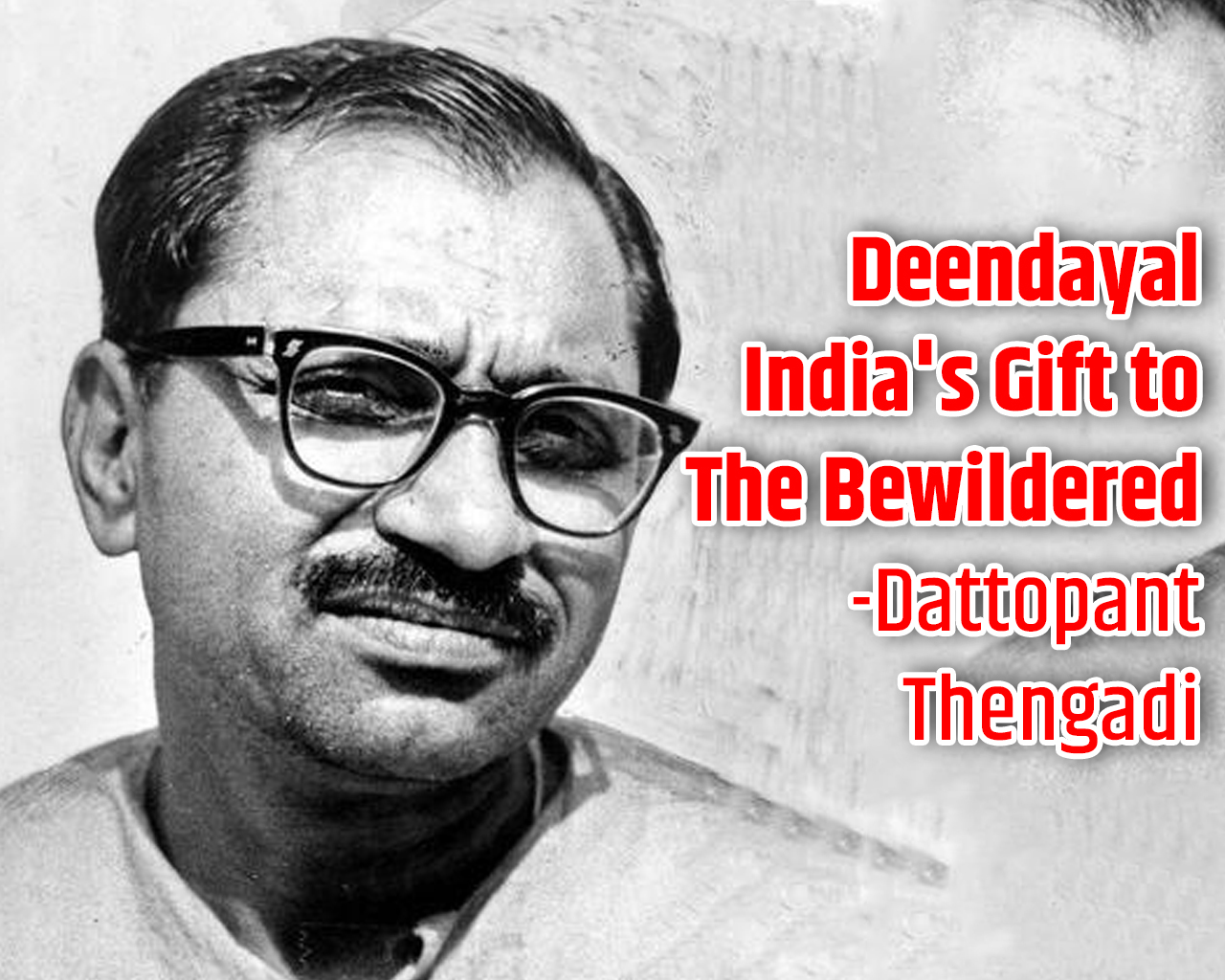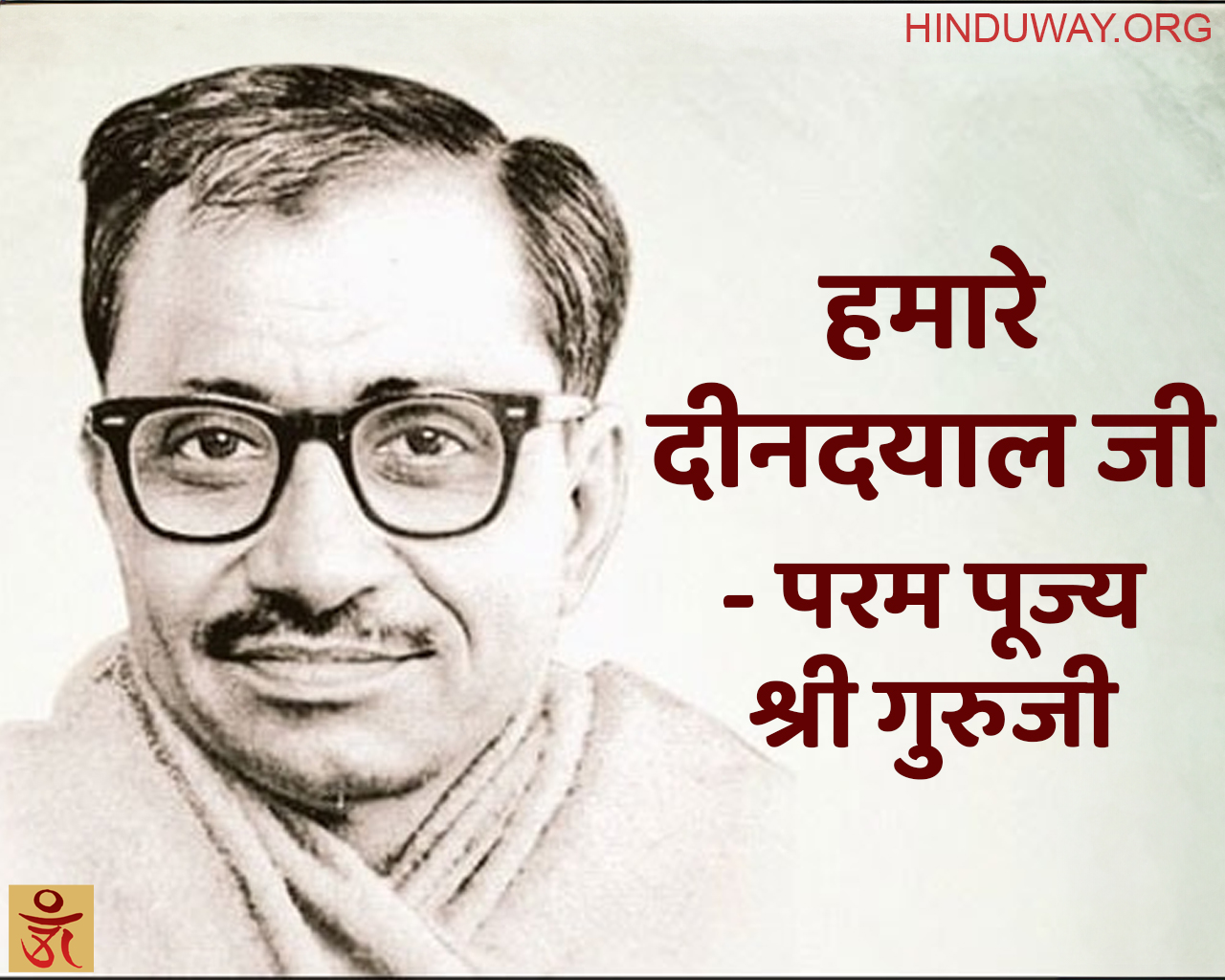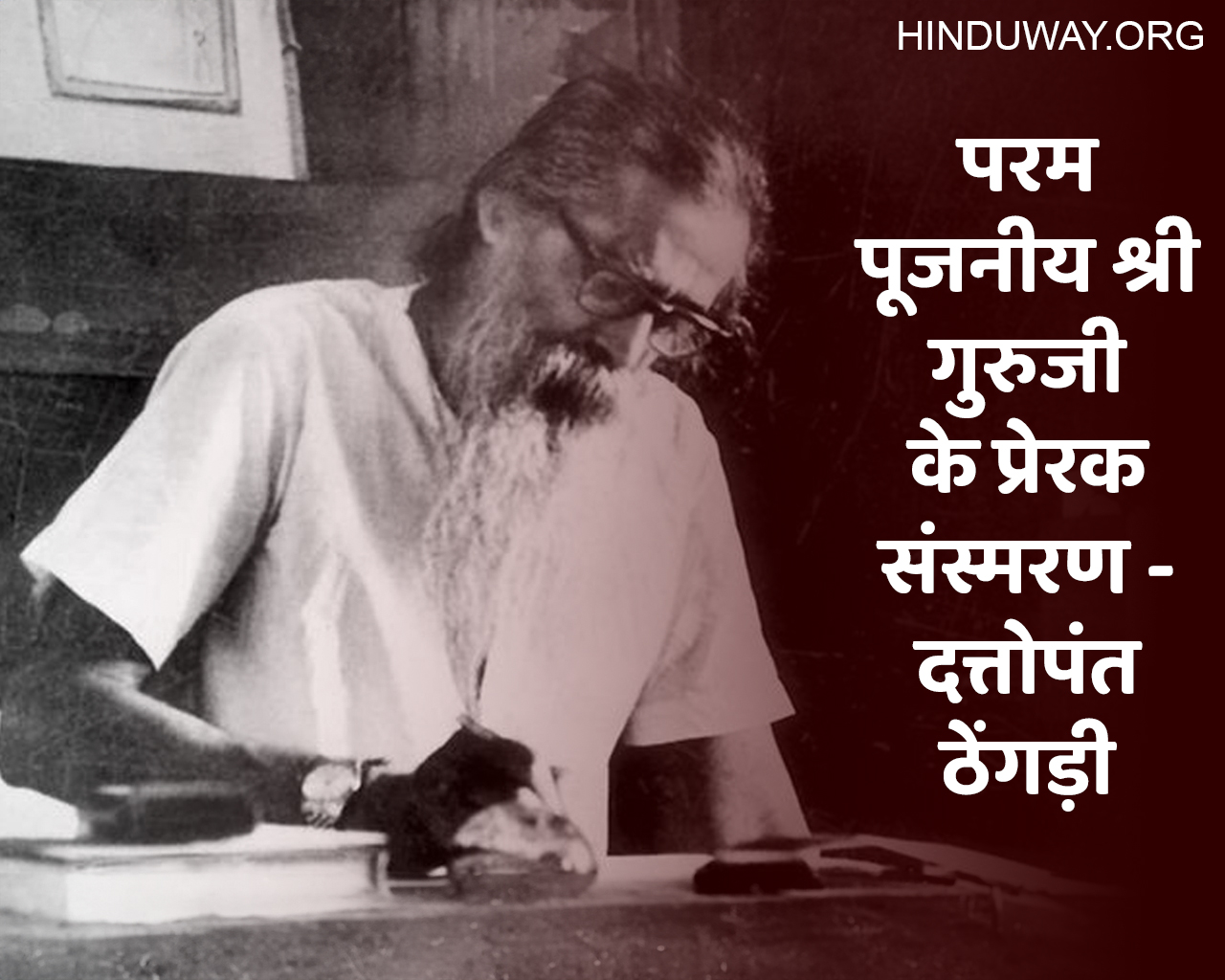पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के महानिर्वाण को ३४ वर्ष हो चुके है (यह लेख १७ मार्च, -१९९१ को पाञ्जन्य में छपा था।) किंतु उनके व्यक्तित्व की आंधी से उड़ी धूल अब तक बैठी नहीं है जिससे उनका उचित मूल्यांकन साफ दृष्टि से किया जाना संभव नहीं है । फिर इसके लिए उचित वातावरण भी देश में नहीं है । सब तरफ राजनीति का बोलबाला है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लोग प्राय: भूल रहे हैं और बाबा साहब ने जिन जीवन मूल्यों को संजोया था वे कालबाह्य हो गए हैं – ऐसा कहने वाले लोग आज ‘व्यवहार चतुर’ माने जाने लगे हैं ।
राजनीति, राजनीतिक दल और राजसत्ता का राष्ट्र के संवर्द्धन में क्या स्थान है, इस विषय में ज्यादातर लोगों में गलतफहमियां हैं । सब कुछ राजसत्ता के जोर पर ही संभव है अत: उस पर काबिज होने की साधनभूत राजनीति ही एकमात्र महत्वपूर्ण काम है, ऐसी अनेक लोगों की धारणा है । पूज्य बाबा साहब की धारणा भिन्न थी । मनुष्य निर्माण व उसके लिए संस्कार परिवर्तन और सामाजिक एकात्मता, यही सब तरह की प्रगति के आधार हैं – ऐसा उनका मानना था । अरस्तू ने कहा है – राजनीति शास्त्र मनुष्य नहीं पैदा करता, वह उसे प्रकृति ने जैसे दिए वैसे ही लेने पड़ते हैं ।’ बाबा साहब भी कहा करते थे- ‘हमें अब अपना हृदय पवित्र करना चाहिए, सद्गुणों की ओर हमारा खिंचाव हो, इस तरह हमें धार्मिक बनना चाहिए । चरित्र ही धर्म का प्रधान अंग है, चरित्र मर्यादा आदि सब धर्म से ही उपजते हैं ।’ धर्म के आधार पर ही वैचारिक संस्कार परिवर्तन और सामाजिक एकात्मता संभव है, ऐसी उनकी श्रद्धा थी । वे मानते थे कि ध्येयपूर्ति हेतु राजनीति का महत्व सीमित है । इसीलिए २७ मई, १९३५ को उनकी धर्मपत्नी रमाबाई के निधन के बाद कुछ दिन एकांत में बिताए और शेष जीवन में राजनीति से धार्मिक विषयों को वरीयता देना तय किया । इसी के अनुरूप २३ जुलाई, १९३५ को उन्होंने घोषित किया कि वे अब राजनीति से निवृत्त हो रहे हैं । पत्रकारों ने उनसे पूछा – ‘आप अब तक दलितों के हितों के जुझारू प्रवक्ता (चैम्पियन) रहे हैं तो क्या आपको यह नहीं लगता कि उनका मार्गदर्शन आगे भी करते रहना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया- ‘हां, मैं उनके हितों का जुझारू प्रवक्ता रहा और मैंने उन्हें उनके अधिकार दिलवाए । लेकिन मैं अब यह नहीं समझता कि मेरा राजनीति में बना रहना अत्यंत अपरिहार्य है ।‘
अपनी राजनीति को वरीयता न देना कई लोगों को गलत लगता है, इसका उन्हें भान था । इस दृष्टि से उनकी प्रखर आलोचना करने वाले कुछ पत्रकार भी उन दिनों थे । जैसे नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने पर २३ मई, १९५४ के ‘टाइम्स आफ इंडिया ‘ ने लिखा-‘अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन ऐसे व्यक्ति की शोकान्तिका है जो समझते हैं राजनीति में तर्क की प्रतिष्ठा है । कोई बात इसलिए समर्थनीय है कि वह तर्कसंगत है । अम्बेडकर मूलत: विवेकी व्यक्ति होने के कारण अथ से इति तक तर्कसंगत बात के लिए जिरह करते हैं । किन्तु राजनीतिज्ञों का बड़ा झुंड विवेक से कोई सरोकार नहीं रखता । वे उल्टा तर्क देने लगते हैं । वे निष्कर्ष तो पहले निकाल लेते हैं फिर उससे तालमेल बैठाने वाली प्रस्तावनाएं गढ़ते हैं ।
‘यह कष्टकारक सच है कि तर्क रूपी जू-जू से संलग्न राजनीतिज्ञ का केवल यही हश्र होगा कि देर-सवेर वह जू-जू उसके विरोधी के बजाय उसे ही काटकर उसका अंत कर दे । राजनीति कोई तर्कशास्त्र नहीं है ।’
उक्त टिप्पणी राजनीति को सीमित महत्व देने वाले ध्येयवादी पुरुषों को व्यवहार शून्य मूर्ख समझने वाले लोगों की मानसिकता की परिचायक है । किन्तु बाबा साहब ऐसी टिप्पणियों से विचलित होने वाले नहीं थे ।
वे कहते थे, ‘समाज की प्रगति में राजनीति से अधिक महत्व सामाजिक आर्थिक पहलुओं का है । अत; इस ओर कार्यकर्त्ताओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए । राजनीति ही सब कुछ है, ऐसी भावना के वशीभूत लोग निर्वाचन काल आते ही टिकट के लिए दौड़ने लगते हैं, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालते हैं, चुनाव में हार जाने पर थककर निराश होकर सो जाते हैं । और जीत गए तो विधान मंडलों में पांच साल तक घुम्मा बने मौन धारण कर बैठना इतना ही काम है-ऐसा ये कार्यकर्त्ता मानते हैं ।’
६ फरवरी, १९५४ को आचार्य अत्रे द्वारा निर्मित फिल्म ‘महात्मा फुले’ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा-‘आज देश में चरित्र ही नहीं बचा है । जिस देश में नैतिकता नहीं होती उसका भविष्य कठिन होता है । फिर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय ही रहेगा । मंत्री देश का उद्धार नहीं करते तो जिसने धर्म भली- भांति समझा है, वही देश को तार सकता है । महात्मा फुले ऐसे ही धर्म सुधारक थे । विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्रीभाव इन धर्मतत्वों से प्रत्येक ने अपना चरित्र बनाना चाहिए । करुणा रहित विद्यावान को मैं कसाई समझता हूं । करुणा के अर्थ में मानव-मानव के आपसी प्रेम से भी मनुष्य को आगे जाना चाहिए ।’
बाबा साहब की ऐसी बातों को आज के ‘व्यवहार चतुर’ मनुष्य चर्च में होने वाले रविवार प्रवचन (संडे सरमन) से अधिक महत्व नहीं देते ।
महापुरुषों से जिनका प्रत्यक्ष संबंध न आया हो, वे लोग या तो उनका मूल्यांकन उनकी विचारधारा को चिपकाए जाने वाले लेबल से करते हैं या उनके आज के अनुयायियों के गुण-दोषों से । केवल लेबल से निष्कर्ष निकाला तो कहना पड़ेगा कि स्वराज्य प्राप्ति से आज तक दिल्ली में गांधीवादी शासन है और कलकत्ता में कम्युनिज्म का । इससे लेबल कितने दिग्भ्रमित कर सकते हैं, यह समझा जा सकता है । वही बात अनुयायियों की भी है । समर्थकों और विरोधियों में जो वैचारिक प्रामाणिकता पहले थी, अब नहीं है । प्राचीन भारत में विरोधी की बौद्धिक प्रामाणिकता संदेह से परे थी । इसीलिए जगद्गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी निर्णायक के पद पर थी । आज ऐसी बौद्धिक प्रामाणिकता नहीं दिखाई देती । अनुयायियों के विषय में एक विचारक ने कहा है, ‘ईश्वर जब किसी महापुरुष को सजा देना चाहता है तो उसे अनुयायी दे देता है । ‘आजकल यह उक्ति कई महापुरुषों के विषय में चरितार्थ होती नजर आती है ।
परवर्ती अध्येता प्रामाणिक होते हुए भी आज की परिस्थिति, घटनाक्रम, दल, व्यक्ति, उनके समीकरण आदि के विषय में पूर्वकालीन परिस्थिति आदि वैसी ही मानने की भूल कर सकता है । इसे अनाक्रोनिज्म (Anachronism) कालगणना का क्रम विपर्यय कहते हैं । विशुद्ध साहित्यकारों की बात छोड़ दें, तो कृतिवीर पुरुषों के प्रतिपादन में कुछ भाग सर्वकालिक सत्य के जैसा रहता है तो कुछ केवल तात्कालिक महत्व का, जो परिस्थिति और श्रोताओं को ध्यान में रखकर अभिव्यक्त प्रतिक्रिया जैसा होता है । गीता न पढ़कर फुटबाल खेलने का युवकों को स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया परामर्श चिरंतन सत्य की श्रेणी में नहीं आता ।
आज देश में एक घातक प्रवृत्ति पनप रही है । लोकमान्य तिलक की विरासत पर महाराष्ट्र का, रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर बंगाल का, महात्मा गांधी पर गुजरात का हक जताया जाता है । इसी तरह संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मणों के, तुकाराम बनियों के, नामदेव दर्जियों के, संत गोरा कुम्हारों के व चोखा मेला महारों के ही माने जाने लगे हैं । इस तरह सम्पूर्ण मानवजाति को ही जिनकी विरासत मिलनी चाहिए उन वंदनीय विश्वमानवों को भी जाति क्षेत्र के संकुचित दायरे में बंद कर दिया जाता है । इसलिए इन श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी यह गलतफहमी होती है कि जो उन्हें विश्व को देना चाहिए था वह अपनी जाति को ही दे दिया ।
इस प्रवृत्ति के विषय में बाबासाहब कहते थे, ‘जातीयता’ के बड़वानल ने गौतम बुद्ध, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि सभी को खाक कर डाला । ‘अपने जाने के बाद यह कूपमण्डूक समाज अपनी भी कहीं यही दशा न कर दे, शायद इस बारे में बाबासाहब सचिंत रहे हों ।’
यह बात मुझे व कई औरों को भी खटकती है कि बाबासाहब को उनके समर्थक और विरोधी भी एक वर्ग विशेष के नेता (सेक्शनल लीडर) के रूप में निरूपित करते हैं । उन्हें रामस्वामी नायकर, बैरिस्टर जिन्ना, लालडेंगा या फिजो के साथ रखना उनके प्रति सरासर अन्याय है और उनके विषय में घोर अज्ञान ही इसका कारण है । पूज्य बाबासाहब पूर्णत: राष्ट्रभक्त, मानवतावादी, धर्मप्राण और सात्विक वृत्ति के महापुरुष थे । संकुचितता का उनके विशाल हृदय में कोई स्थान नहीं था और जब कभी उन्हें परिस्थिति के दबाव में वैसी भूमिका लेनी पड़ती, वे अत्यंत दुखी होते थे ।
११ जनवरी, १९५० को मुम्बई में अपना सम्मान किए जाने के अवसर पर उन्होंने कहा-‘अब तक हम शत्रुता के आधार पर राजनीति करते थे । मुझे लगता है कि अब तक अस्पृश्य वर्ग के सभी नेता कुछ संकुचित दृष्टिकोण से देखते रहे और बरतते भी रहे । कुछ मात्रा में यह दोष मुझमें भी था । हमें यह लगता था कि हिन्दुओं के हाथों में सत्ता आने पर हमारा क्या होगा – लेकिन अब हमें अपनी सोच बदलनी है । अब तक हम अपने वर्ग विशेष के हित की ही चिंता किया करते थे । आगे भी उसे करना है किंतु साथ ही अब हमें देश की स्वतंत्रतावादी रक्षा करने की भी चिंता करनी है । हमारा देश कई बार स्वतंत्र होकर बार-बार पराधीन होता रहा है । हमें मुसलमानों और अंग्रेजों की गुलामी में रहना पड़ा है । स्वाधीनता की जितनी जरूरत सवर्णों को है, उतनी ही दलित वर्ग को भी है । अत: यदि देश पुन: पराधीन हुआ तो वह हम सबका दुर्भाग्य होगा । देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना सभी को अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए ।
“जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तब किस वर्ग को क्या अधिकार देना है यह उन शासकों पर निर्भर था । उस समय हम अन्य वर्गों के लोगों से खिंचे-खिंचे रहते थे । अब अंग्रेज जा चुके हैं अत: हमें अन्य वर्गों एवं दलों से सहानुभूतिपूर्ण सामंजस्य रखना पड़ेगा । वैधानिक रीति से हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी दल से या संग मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा । पुरानी शत्रुता भुलानी होगी । पहले जैसा एकाकीपन अब काम नहीं देगा ।”
इस भाषण को सुनकर कुछ लोगों को लगा कि बाबासाहब अपनी विचारधारा (लाइन) बदल रहे हैं । लेकिन यह बात नहीं थी । जैसे अमरीका के मुक्ति संग्राम में एक ओर बेयर्ड रास्टिन अतिवादी थे और दूसरी ओर मार्टिन लूथर जैसे सबको साथ लेकर चलने वाले नेता, उसी तरह भारत के दलित विचारकों के भी दो प्रवाह थे । एक वर्ग के नेता मानते थे कि सब अस्पृश्य एक साथ आकर सवर्णों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ें, वहीं दूसरी ओर बाबासाहब इस बात को दृढ़तापूर्वक मानते थे कि अस्पृश्योद्धार का प्रश्न सम्पूर्ण हिन्दू समाज का है और उसके लिए सवर्ण और अस्पृश्य दोनों को ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए ।
इसी विचार से उन्होंने २० जुलाई, १९२४ को बहिष्कृत हितकारिणी सभी बनाई थी । सर चिमनलाल सीतलवाड़ उसके अध्यक्ष थे और श्री जी०के० नरीमन, डा० वि०पा० चौहान, डा० परांजपे, बा. ग. खेर आदि उपाध्यक्ष । बाबासाहब स्वयं इस संस्था के कार्याध्यक्ष थे । उद्घाटन भाषण में बाबा साहब ने कहा था – ”हम वरिष्ठ वर्गों से यह अनुरोध करते
हैं कि वे अपनी सारी ताकत राजनीति में ही न खपाकर बहिष्कृत लोगों की उन्नति के काम में भी सहयोग दें । अस्पृश्य समाज भारत की समूची जनसंख्या का छठा भाग है और जब तक इतना बड़ा भाग दीनहीन होकर पंगुवत् पड़ा है तब तक देश उन्नत नहीं हो सकता ।” १४ जनवरी, १९४६ को सोलापुर के भाषण में डा० वि० वि० मुले का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि “उन्हीं की सहायता से मैंने बीस वर्ष पूर्व सार्वजनिक काम आरंभ किए थे । महार सत्याग्रह के समय उन्होंने ब्राह्मणेत्तर दल की यह मांग ठुकरा दी कि यदि आप अपने आदोलन से सब ब्राह्मणों को हटा दें तो हम अपना पूर्ण सहयोग आपको देंगे । उन्होंने कहा, “मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है । दूसरों को हीन समझने की उनकी दुष्प्रवृत्ति से मेरा संघर्ष है । भेदभाव की दृष्टि रखने वाले अब्राह्मणों की अपेक्षा अभेद्य दृष्टि रखने वाला ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय है । अपने आंदोलन में सहयोग देने वाले ऐसे ब्राह्मणों को मैं अलग नहीं कर सकता ।”
एक बार मिलिन्द महाविद्यालय के प्राध्यापक ठकार ने उनसे पूछा, “आप ब्राह्मणों के विरुद्ध क्यों हैं? बाबासाहब ने उत्तर दिया – “बेटे! यदि मैं ब्राह्मणों और हिन्दुओं के विरुद्ध होता तो तुम यहां (नौकरी करते) नहीं होते ।”
सन् १९३६ में सिख धर्म अपनाने का उनका निर्णय हिन्दू समाज के प्रति उनकी आत्मीयता के कारण ही था । बाबासाहब के निर्णय का समर्थन करने वालों में डा० मुंजे, बैरिस्टर जयकर, श्री युगलकिशोर बिरला जैसे विख्यात हिन्दू नेता थे । पू० बाबासाहब ने अपने इस निर्णय के विषय में बड़ी भावुकता से कहा था, “अस्पृश्य वर्ग के सिख धर्म अपनाने के निर्णय का स्वागत श्री शंकराचार्य के साथ ही अनेक प्रसिद्ध हिन्दू नेताओं ने किया है । यह सुझाव भी हिन्दू नेताओं ने ही रखा था और उसे मैंने स्वीकार किया । इस विकल्प को चुनते समय मेरी यही भावना रही कि हिन्दू समाज के भवितव्य की जिम्मेदारी कुछ अंशों में मुझ पर भी है ।” (यह अलग बात है कि बाबासाहब को कतिपय कारणों से अपना यह निर्णय छोड़ देना पड़ा )।
बाबासाहब ने बाद में बौद्धधर्म अपनाने का निर्णय लिया तो उसके विषय में उन्होंने कहा था, “एक बार गांधीजी से अस्पृश्य के प्रश्न पर चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि इस विषय में मेरे आपसे मतभेद होने पर भी समय आने पर मैं ऐसा मार्ग चुनूंगा जिससे देश का कम से कम अहित हो । इसीलिए बौद्ध धर्म अपनाकर मैं देश का अधिक से अधिक हितसाधन कर रहा हूं । बौद्धधर्म भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है । इस देश की संस्कृति, परंपरा तथा इतिहास को जरा भी आंच न आए इसकी चिन्ता मैंने की है । इस देश की संस्कृति और परंपरा के विध्वंसक के रूप में इतिहास में मैं अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता ।”
१३ दिसम्बर, १९४७ को संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था, “आज यद्यपि हम राजकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अलग- अलग खेमों में बंटे हैं फिर भी मुझे विश्वास है कि अनेक जाति-पंथों के होते हुए भी हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे । ऐसा भी एक दिन अवश्य आएगा जब विभाजन की मांग करने वाली मुस्लिम लीग भी ‘अखण्ड हिन्दुस्तान ‘ में ही अपना हित है – यह समझने लगेगी ।”
३१ मई, १९५२ को अपने मुम्बई भाषण में उन्होंने कहा, ” यद्यपि मैं कुछ उग्र स्वभाव का हूं और सत्ताधारियों से मेरा टकराव भी होता रहता है फिर भी मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अपनी विदेश यात्रा में भारत की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा । मैंने कभी भी राष्ट्रद्रोह नहीं किया है । राष्ट्र का हित ही मेरे हृदय में सदैव रहा है । गोलमेज परिषद् के समय भी मैं राष्ट्रहित के मामले में गांधीजी से २०० मील आगे था । “गोलमेज परिषद् में बाबासाहब ने दलित वर्ग को ‘प्रोटेस्टेंट हिन्दू’ अथवा ‘नान कम्फुर्मिस्ट’ हिन्दू के रूप में सम्बोधित करने की मांग की थी ।
११ जनवरी, १९५० को मुम्बई की अपनी स्वागत सभा में उन्होंने कहा – “गत २० वर्षों से मुझे ब्रिटिश एजेंट तथा मुसलमानों का पक्षधर कहा जाता रहा है । मुझे हिन्दू धर्म का शत्रु बताया जाता रहा है । लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत के संविधान के निर्माण का मेरा कार्य देखकर मुझ पर लगाए जाने वाले आरोप कितने निराधार और मिथ्या थे, इसे हिन्दू समाज अनुभव करेगा और एक दिन मुझे अपना उपकारकर्ता स्वीकार कर धन्यवाद देगा ।” पाकिस्तान बनने के बाद बाबासाहब ने वहां के दलितों को परामर्श दिया था कि जो भी रास्ता और साधन मिले उससे उन्हें भारत में आ जाना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अथवा निजाम हैदराबाद के मुसलमानों पर विश्वास करना दलित वर्ग के लिए घातक होगा । दलित वर्ग के जिन लोगों को पाकिस्तान में मुसलमान बना लिया गया था उन्हें भी बाबासाहब ने हिन्दुस्थान में आने पर धर्मान्तरित होने के पूर्व जैसा बंधुभाव का व्यवहार पाने का आश्वासन दिया था । उन्होंने दलित वर्ग को यह परामर्श दिया था कि हिन्दुस्थान के शत्रु निजाम का साथ देकर वे संपूर्ण दलित समाज के मुख पर कालिख पोतने का पाप न करें । उनके शब्द थे- ”जल्दी से जल्दी मुसलमानों को शासक वर्ग बनाने की आकांक्षा से उन्मत्त मुसलमान और मुस्लिम लीग अनुसूचित जातियों के हितों का भी विचार नहीं करेंगे । यह मैं अनुभव से कहता हूं। (The Muslims and the Muslim League charged at they are with passion to make the Muslims a governing Class as quickly as possible will never give consideration to the claims of scheduled castes. This I speak from experience.”)
२५ नवम्बर, १९४९ को संविधान सभा में बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था- “मेरे लिए यह मानना अत्यंत पीड़ा की बात है कि भारत को अनेक बार अपनी स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ा और वह भी अपने ही लोगों के विश्वासघात और देशद्रोह के कारण । क्या इस इतिहास की पुनरावृत्ति होगी ?” यह प्रश्न करते हुए उन्होंने कहा- “हिन्दू समाज के जाति भेद और पंथभेद पुराने शत्रु हैं हीं, उनमें परस्पर विरोधी विचारों के राजनीतिक दलों की और वृद्धि हुई है । इससे मेरी चिन्ता बढ़ गई है।“ इसलिए भारतीय जनता को उन्होंने चेतावनी दी, “इन राजनीतिक दलों ने अपने दलीय स्वार्थ को राष्ट्रहित से श्रेष्ठ माना तो भारतीय स्वाधीनता पुन: संकट में पड़ सकती है, इतना ही नहीं तो वह सदैव के लिए नष्ट भी हो सकती है। इसलिए रक्त की अंतिम बूंद तक हमें अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए संघर्ष करने का निश्चय करना होगा।“
बाबासाहब की वर्ण व्यवस्था के सम्बंध में जैसी अवधारणा थी वैसी ही हिन्दुत्व निष्ठों की भी थी । किन्तु इन हिन्दुत्व निष्ठों का, जो बाबासाहब जैसी ही सोच रखते थे, सवर्ण समाज पर उतना अधिक प्रभाव नहीं और जिनका सनातनी सवर्ण समाज पर अधिक प्रभाव था वे तत्कालीन राजनैतिक नेतागण बाबासाहब की भूमिका को नहीं समझ सके । बाद में १९६९ में कर्नाटक (उडीपी) में हुए विश्व हिन्दू परिषद् के विशाल सम्मेलन ने ‘अस्पृश्यता धर्म, और शास्त्रसम्मत नहीं है” यह उद्घोषित करते हुए, ‘न हिन्दू: पतितो भवेत्’ तथा ‘हिन्दुत्व: सोदरा, सर्वें ऐसा स्पष्ट निर्णय दिया । काश! धर्माचायों की यह घोषणा १९२७ में महार सत्याग्रह के पहले ही की गई होती तो इतिहास को एक नया ही मोड़ मिलता । किन्तु दुर्भाग्य से उन दिनों समाज पर कांग्रेस का प्रभाव था जिसने बाबासाहब को निराश ही किया । बाबासाहब की प्रारंभ से यही इच्छा रही कि अस्पृश्यता निवारक आंदोलन का स्वरूप ‘स्पृश्य बनाम अस्पृश्य’ न होकर ‘हिन्दू सुधारक बनाम हिन्दू पुरातनपंथी’ जैसा हो । इस दिशा में बाबासाहब ने सवर्ण समाज सुधारकों के साथ जो काम किया उस ओर कम लोगों का ध्यान गया है ।
५ मार्च, १९२८ को मुम्बई के ठाकरसी हाल में समाज समता संघ द्वारा आयोजित अंतर्जातीय सहभोजन और २२ मार्च, १९२८ को पंडित पालेय शास्त्री की अगुवाई में लगभग ५०० महार जाति के अस्पृश्यजनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया था । उस समय बाबासाहब के साथ अनेक सवर्ण जातियों के नेता उपस्थित थे । इस बात की ओर कितने लोगों का ध्यान गया है । २५ दिसम्बर, १९२७ को महाड़ में हुई परिषद् के लिए स्वयं लोकमान्य तिलकजी के पुत्र ने शुभकामना संदेश भेजा था । इस परिषद् में बाबासाहब ने हिन्दू मात्र के जन्मसिद्ध अधिकारों का घोषणापत्र जारी किया था । परिषद् ने प्रस्ताव पारित किया था, “सभी हिन्दुओं को एक ही वर्ण का माना जाए । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णभेदी शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगे । हिन्दू पुरोहित वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाएं जिनमें उत्तीर्ण होने वालों को ही पुराहिताई का लाइसेंस (अधिकार पत्र) दिया जाए । इस अवसर पर हुए अध्यक्षीय भाषण में ‘द इंडियन नेशनल हेरल्ड’ के अनुसार बाबासाहब ने कहा, “यदि हम अपने इस आदोलन में सभी हिन्दुओं को एक जाति में संगठित करने में सफल होते हैं तो हम भारतीय राष्ट्र और खासकर हिन्दू समाज की सबसे बड़ी सेवा करेंगे ।
(If we achieve success in our movement to unite the Hindus in a single caste, we shall have rendered the greatest service to the Indian nation in general and to the Hindu community in particular.”)
किन्तु हिन्दू जनमानस पर गांधीजी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का प्रभाव होने के कारण तीव्र इच्छा के बावजूद इस सर्वसमावेशक भूमिका का निर्वाह बाबासाहब के लिए संभव नहीं हुआ ।
बाबासाहब जिस एकमात्र कांग्रेस के १९१८ के अधिवेशन में उपस्थित थे उसमें सर्वप्रथम अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव रखा गया था । उसमें कांग्रेस की भूमिका इस प्रकार रखी थी- “हम जनतंत्र के समर्थक होने के कारण अपने घरों की चार दीवारी के अंदर किए जाने वाले निजी व्यवहार के लिए स्वतंत्र हैं । इस कारण आप अपने घरों में अछूतों को प्रवेश दो ऐसा नहीं कह सकते और अस्पृश्यों के घरों में जाने को भी हम किसी को नहीं कहेंगे । न तो हम किसी को किसी के साथ भोजन करने के लिए कहेंगे और न ही दूसरों को अपने साथ भोजन कराने का आग्रह करेंगे क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न है । प्रत्येक को अपनी जाति व धर्म प्रिय होता है, अपनी जाति के बाहर विवाह सम्बन्ध स्थापित करने को भी हम नहीं कहेंगे । किसी की भी धार्मिक मान्यताओं, रीति- रिवाजों और परस्पर व्यवहार में हस्तक्षेप करने की हमारी इच्छा नहीं । हम केवल इतना ही चाहते हैं कि अस्पृश्यता दूर होनी चाहिए ।“
गांधीजी से बाबासाहब के सभी विषयों पर मतभेद थे । गांधीजी की वर्णाधिष्ठित समाज रचना की अवधारणा से बाबासाहब उनके तीव्र आलोचक बने । वे अपने को ‘प्रोटेस्टेंट हिन्दू’ कहते थे । उनका मानना था कि गांधी जी का ‘हरिजन’ शब्द अस्पृश्यों को आश्रितों की भूमिका में रखता है । वे कहते थे, “इस देश में दो हजार वर्षों से अस्पृश्यता जमी हुई है, यह दुख की बात है । मैं यह मानता हूं कि भारत ही नहीं सारे विश्वभर में दासता और विषमता का वह काल था । मैं यह भी मानता हूं कि दीर्घावधि से चली आ रही यह बीमारी सहसा दूर होने वाली नहीं है, समाज के मानसिक परिवर्तन से ही धीरे-धीरे यह संभव होगी । तब तक मैं प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार हूं किन्तु मेरा दुख यह है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाने वाला शिक्षित समाज सुधारक ही ‘प्रामाणिक’ नहीं है । तब ऐसे लोगों द्वारा पचास वर्ष तो क्या, सैकड़ों वर्ष राह देखने पर भी अस्पृश्यों को न्याय मिलेगा इसकी मुझे आशा नहीं है ।“
नासिक के ‘कोहिनूर’ पत्र में ऐसा वृत्त छपा था कि अत्याचारों से तंग आकर ५०० अस्पृश्यों ने मुसलमान बनना तय किया । उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाबासाहब ने नासिक जिले के अपने लोगों से अनुरोध किया था, ‘वे अपने मन को स्थिर रखें । .. मेरे प्रयत्नों को यश प्राप्त होगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सवर्ण समाज के लोगों में धर्मप्रीति और लोकलाज कितनी है ।“
२० सितम्बर, १९५१ को संसद में अपने भाषण के बीच उन्होंने कहा, “सीता का त्याग कर राम ने अन्याय किया था ।“ इस पर एक सदस्य ने उन पर उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, “हम भी प्रगति के पक्षधर हैं किन्तु विधिमंत्री महोदय हिन्दू धर्म की निन्दा किए बिना भी अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकें तो हमें प्रसन्नता होगी ।“ बाबासाहब ने कहा, “इस बात को यदि आपने पहले कहा होता तो मेरे भाषण में आपत्तिजनक बातें न आतीं । मेरा उद्देश्य किसी भावना को चोट पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं ।“
बाद में मिलिन्द महाविद्यालय के एक प्राध्यापक से बात करते हुए बाबासाहब ने कहा था, “मैं तो नासिक के कालाराम मन्दिर में दर्शन का अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति हूं । आप लोगों ने ही मुझे रामजी से दूर ठेल दिया है । मेरी आकांक्षा तो हिन्दू समाज का सुधारक बनने की है ।“
गांधी युग में बाबासाहब ने जो नीति अपनाई और वक्तव्य दिए उस कटुता के मूल में “हिन्दुत्व विरोध” था या “कांगेस विरोध” इस बात की छानबीन होनी चाहिए । इस दृष्टि से “व्हाट द कांग्रेस हैज इन टु द अनटचेबुल्स” यह पुस्तक पठनीय है ।
हिन्दुत्वनिष्ठ नेताओं के प्रति और गांधीजी के विषय मे बाबासाहब की प्रतिक्रिया सदैव अलग-अलग होती थी ।
उदाहरण के लिए १९ सितम्बर के “टाइम्स आफ इंडिया” में बाबासाहब लिखते हैं – “मैं गांधीजी के ‘कम्यूनल अवार्ड’ से विरोध के आधारों को समझने में असमर्थ हूं । वे कहते हैं कि इस अवार्ड ने दलित वर्ग के लोगों को हिन्दू समाज से अलग कर दिया है। दूसरी ओर हिन्दू हितों के प्रबल समर्थक और प्रखर प्रवक्ता इस विषय में दूसरा ही विचार रखते हैं । लंदन से वापस आने के बाद के भाषणों में डा० मुंजे जोर देकर कहते रहे हैं कि कम्यूनल अवार्ड दलित वर्ग और हिन्दुओं में कोई अलगाव नहीं पैदा करता । इसलिए यह आश्चर्य का विषय है कि राष्ट्रीय और गैर-साम्प्रदायिक कहे जाने वाले गांधीजी ‘कम्यूनल अवार्ड’ के बारे में जहां तक उसका दलित वर्ग से संबंध है उसके घातक अर्थ निकालें जबकि साम्प्रदायिक समझे जाने वाले डा० मुंजे ऐसा कुछ नहीं मानते ।“
I am unable to understand the ground of hostility of Mr. Gandhi to communal award. He says that the communal award has separated the depressed classes from Hindu community. On the other hand Dr. Munje, a much stronger protagonist of the Hindu cause and a militant advocate of its interests, takes a totally different view of the matter in the speeches he has been delivering since his arrival from London. Dr. Munje has been insisting that the communal award does not create any sepa.ation between the depressed classes and the Hindus. It is, therefore, surprising that Mr. Gandhi, who is a nationalist and not known to be communalist should read the communal award in so far as relates to the Depressed classes in a manner quite contrary to that of a communalist like Dr. Munje.”
एक ओर डॉ० मुंजे जैसे हिन्दू हित के लिए सतत-सक्रिय नेताओं की साम्प्रदायिक कहकर, निन्दा करना, दूसरी ओर गांधीजी की जरूरी – गैरजरूरी जय – जयकार करते रहना, हिन्दू समाज की इस प्रवृत्ति के विषय में बाबासाहब के मन में जो संत्रास था वही इस उपहासगर्भ लेखन में प्रकट होता है ।
बाबासाहब के प्रति हिन्दुत्वनिष्ठ लोगों की आत्मीयता प्रसंगानुकूल प्रकट होती ही थी । जैसे ३ फरवरी, १९३७ के टाइम्स आफ इंडिया का यह समाचार देखिए: –
“Vote for Dr. Ambedkar” is the gist of a two column article over the signature of Mr. N.C. Kelkar, Democratic leader in today’s Kesari.
(आज केसरी में गणतन्त्रवादी नेता नृसिंह चिंतामणि केलकर के दो स्तंभों में प्रकाशित लेख का सार है, “डॉ. अम्बेडकर को वोट दो”।)
राष्ट्रीय एकात्मता की भावना बाबासाहब में अत्यंत तीव्र थी । एक बार संविधान सभा की बैठक में “दलितों के सुरक्षित स्थान की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी ऐसी शब्दावली संविधान में आनी चाहिए ।“ इस बात का विरोध करते हुए बाबासाहब ने कहा था कि दलितों के विकास में २५ वर्ष भी लग सकते हैं । तब तक हममें से कोई भी शायद जीवित न रहे । और जो उस समय सत्ता में होंगे उन्हें संविधान में संशोधन का साहस जुटा पाना संभव होगा या नहीं यह नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में यह भारत की राजनीति के गले की हड्डी बन सकती है इसलिए सुरक्षित स्थानों का प्रावधान संविधान में इस प्रकार किया जाए कि इसे चालू रखने के लिए तो प्रस्ताव लाया जा सके, निरस्त करने के लिए नहीं ।

| साभार संदर्भ |
| यह लेख १७ मार्च १९९१ में पाञ्चजन्य में प्रकाशित हुआ था |