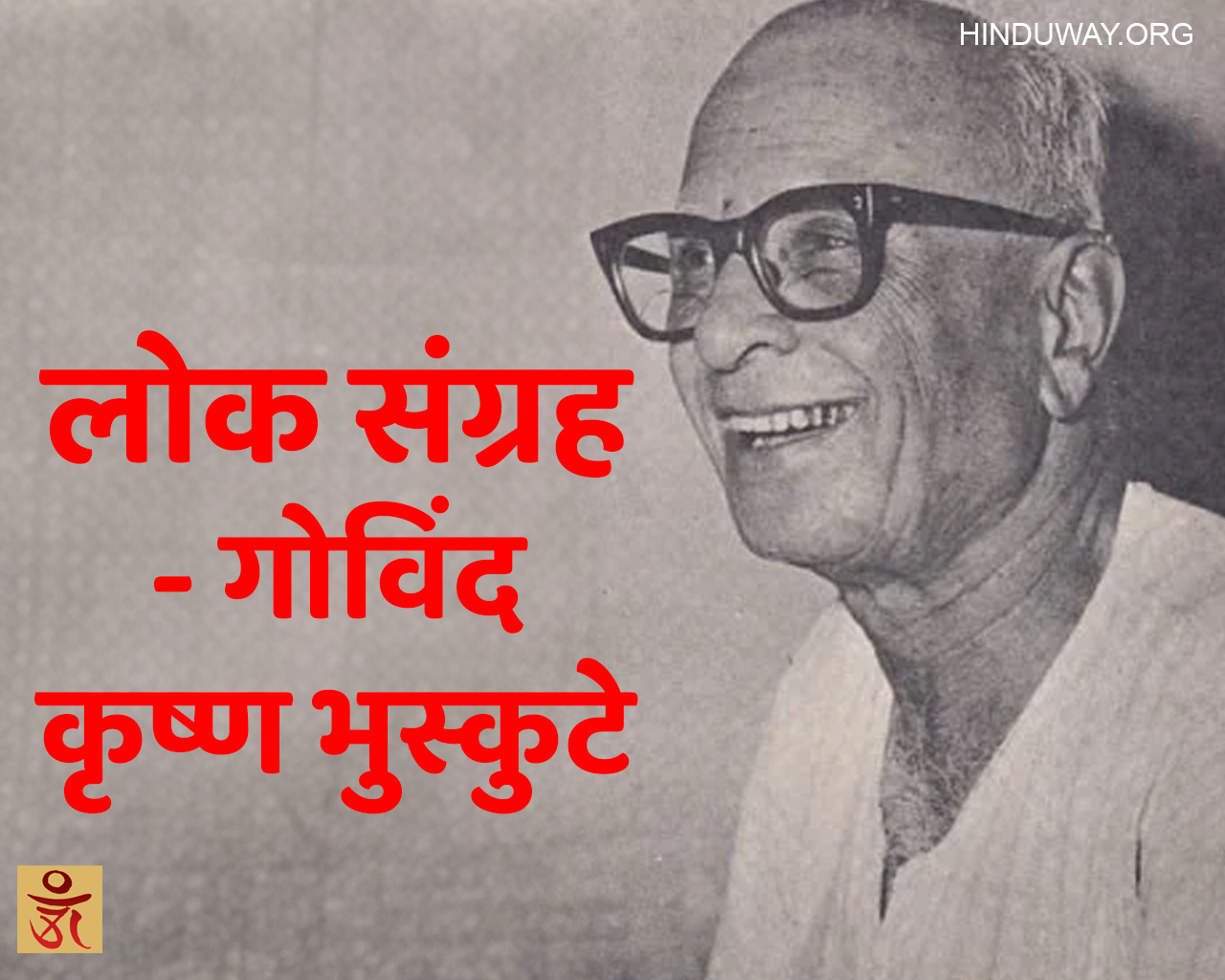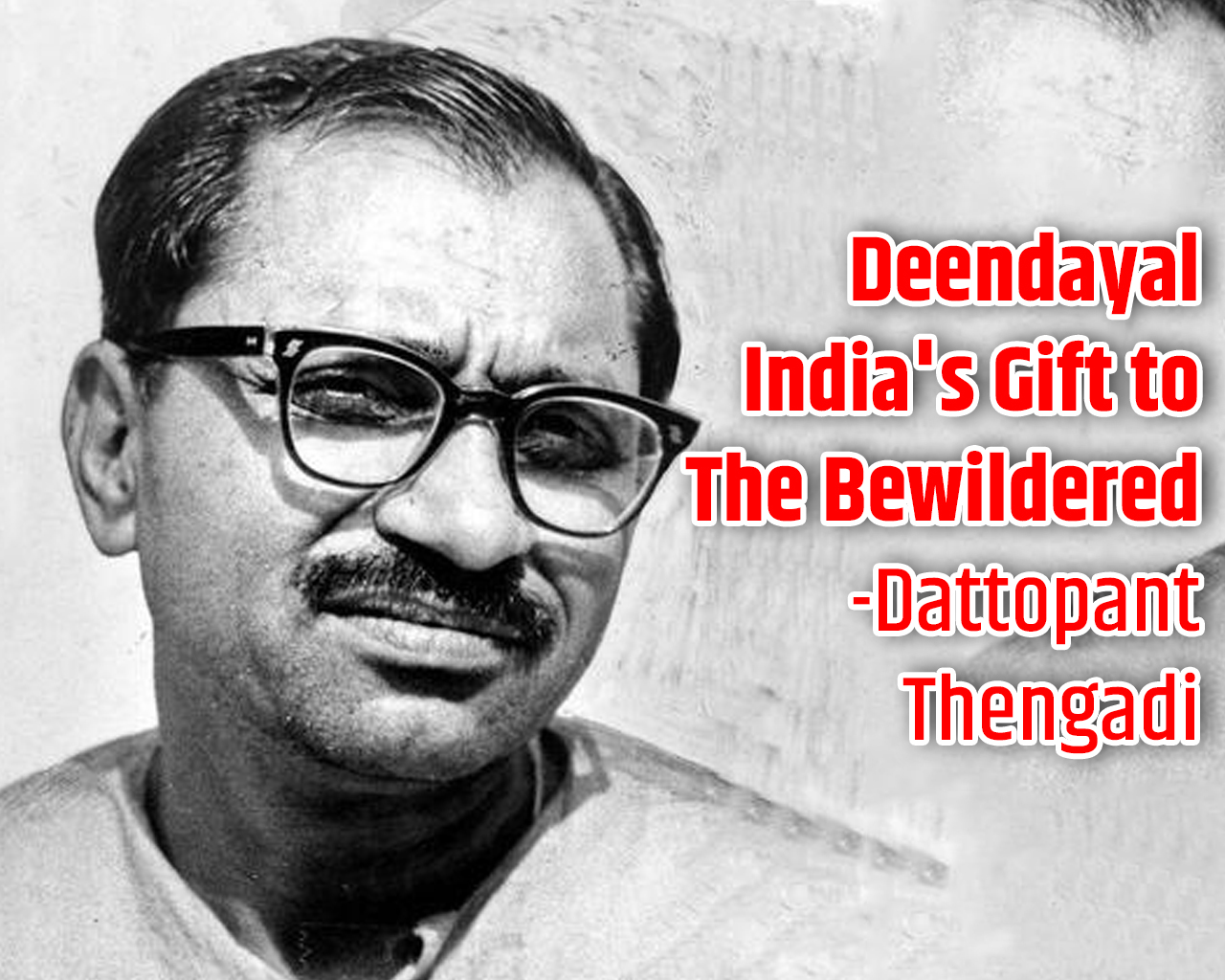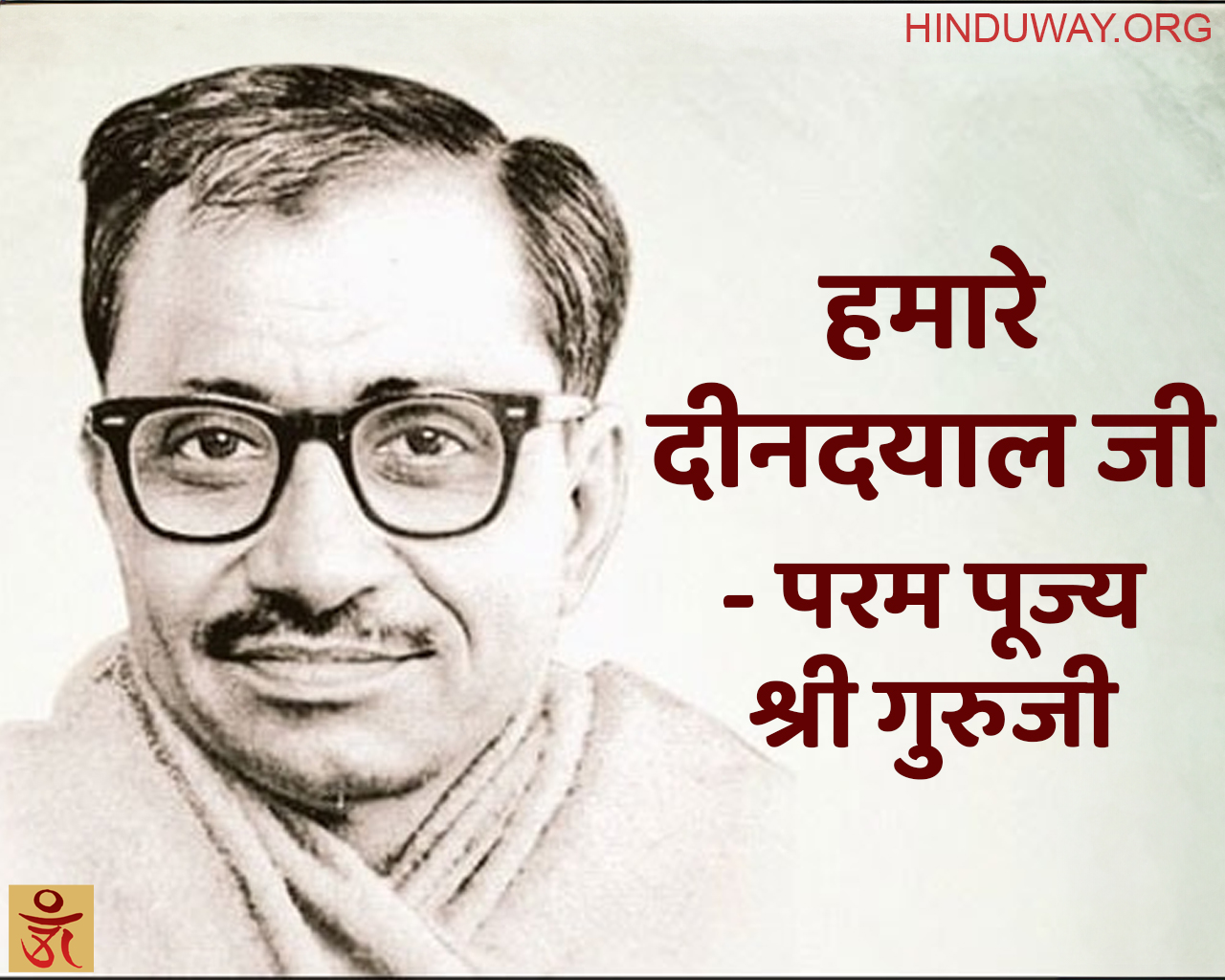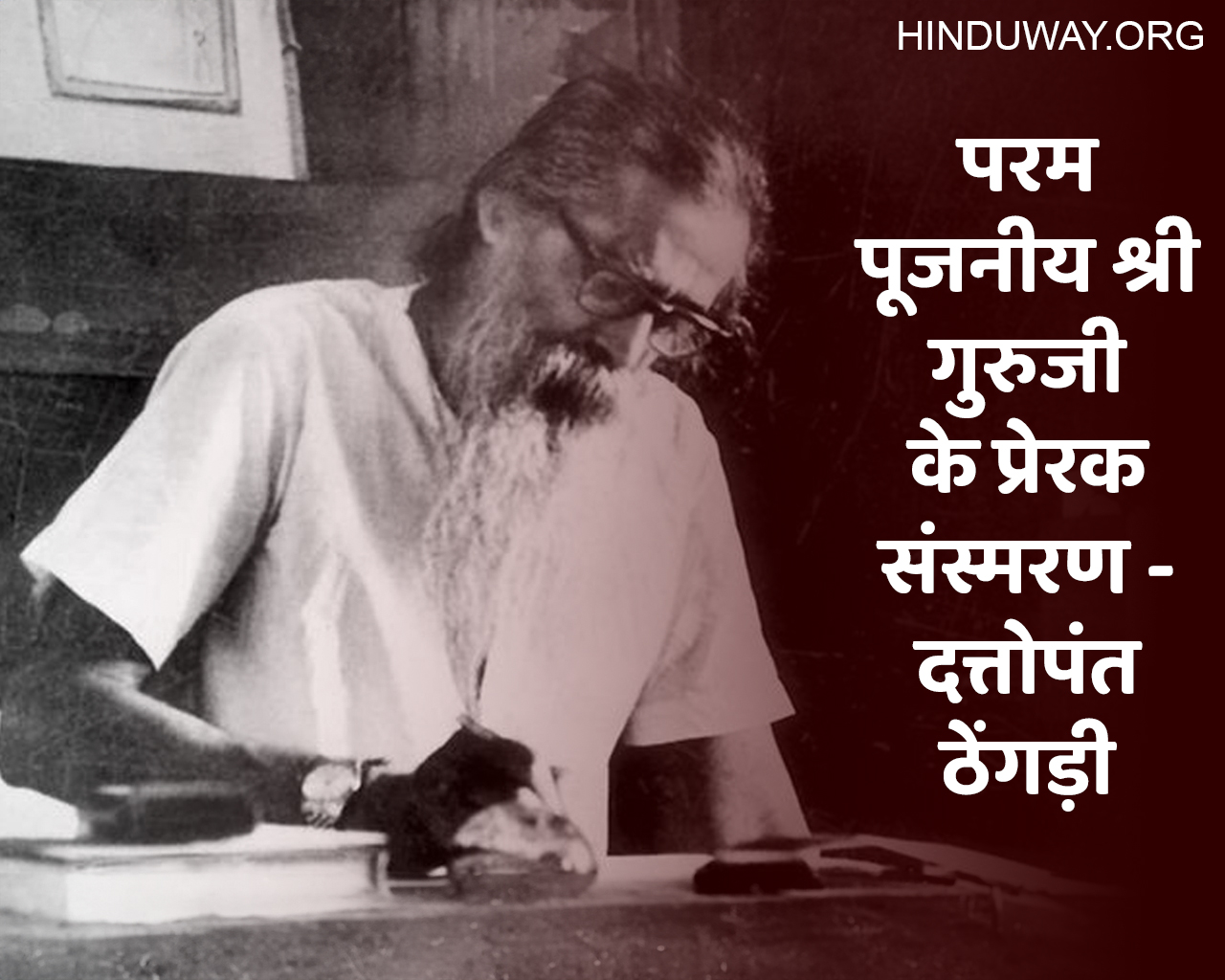शास्त्र और क्रियान्वयन
लेखक- गोविन्द कृष्ण भुस्कुटे
प्रकाशकीय
लोक संग्रह सुनने में जितना सरल है करने में उतना ही कठिन । किन्तु जिन्होने प्रत्यक्ष लोक संग्रह करने में ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया है, उन्हें इसमें कुछ भी कठिन नही लगता। वे मानते हैं कि यद्यपि यह एक शास्त्र है, किन्तु प्रयत्न करने पर उस शास्त्र में पारंगत होना असंभव कार्य नहीं है।
प. पू. डाक्टर हेडगेवार जी के सहवास में ही जिन्होंने इस शास्त्र का अभ्यास शुरु किया था और उनके देहावसान के बाद अर्धशताब्दी बीत जाने पर भी वे अहर्निश इस कार्य में लगे रहे, मान. भाऊसाहब भुस्कुटे (श्री गो. कृ. भुस्कुटे) का इस शास्त्र में गहन अध्ययन था। इसकी क्रियान्विती भी उनके लिये इतनी ही सहज थी।
समय की मांग तथा कार्यकर्ताओं को यह विषय ठीक से बोधगम्य हो, इसलिये उन्होंने इसे बड़े सरल ढ़ंग से एक बार बौद्धिक के रूप में प्रान्त के द्वितीय वर्ष के संघ शिक्षा वर्ग में और फिर प्रान्त के आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में प्रस्तुत किया था। इस बौद्धिक को लेखबद्ध कर जब इसके प्रकाशन के लिये उनसे अनुमति मांगी तो उन्होंने पाण्डुलिपि को स्वयं देखा और कुछ परिवर्तन के साथ हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया ।
कठिन विषय भी कितने सरल और रोचक ढ़ंग से प्रस्तुत हो सकता है इसका अनुमान तो आप इसे पढ़कर ही लगा सकेंगे। ऐसा लगता है कि लोक संग्रह के लिये ही नहीं तो अपने स्वयं के विकास के लिये भी इसे बार-बार पढ़ा जाय।
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण सम्वत २०४७ में प्रकाशित हुआ था जब मान. भाऊसाहब भुस्कुटे जीवित थे। तब के स्वयंसेवकों ने उनके ये बौद्धिक सुने थे अतः उनके इन विचारों को संग्रहित करने के लिये यह पुस्तक उपयुक्त होने से इसकी मांग तेजी से बढ़ी और यह पुस्तक शीघ्र ही समाप्त हो गयी। गत २-३ वर्षों से इस पुस्तक की मांग का दबाब बढ़ रहा है क्योंकि नई पीढ़ी के लिये भी यह पुस्तक उतनी ही मार्गदर्शक है जितनी वह पुराने लोगों के लिये है। इसकी आवश्यकता बढ़ने का कारण यह भी है कि अब मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये मा. भाऊसाहब हमारे बीच नहीं हैं और इस पुस्तक के माध्यम से ही उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सकता है।
नये पुराने सभी कार्यकर्ता इस पुस्तक से लाभान्वित हो यह हमारी भी इच्छा है अतः इसे हम द्वितीय संस्करण के रूप में पुनः प्रकाशित कर, रहे हैं।
प्रकाशक-अर्चना प्रकाशन, भोपाल से साभार
॥श्री ॥
लोक संग्रह
शास्त्र
अपने हिन्दू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए लोक संग्रह करने का साधन हमने अपनाया है। लौकिक भाषा में लोक संग्रह शब्द का अर्थ किया जाता है लोगों को एकत्र करना । आज के जनतंत्र के युग में उसका अपना एक महत्व है, परन्तु उसके द्वारा राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति नहीं की जा सकती। लोगों की भीड़ तो चलचित्र के नटनटनिया अथवा जादूगर भी करते हैं, परन्तु वे राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति नहीं कर सकते। भीड़ में सबका समान ध्येय नहीं होता और यदि हुआ तो भी कृतित्व एवं अनुशासन का अभाव होता है। कहीं आग लगी हो तो लोग एकत्र होते हैं, परन्तु अग्निशामक दल जिस कृतित्व एवं अनुशासन से उसे शांत करते हैं उसका उनमें अभाव होता है। १९५९ में नागपुर में काँग्रेस का खुला अधिवेशन हुआ था । सारा सभामंडप तो खचाखच भरा था ही, परन्तु उसके बाहर भी असंख्य लोग खड़े थे। पं. नेहरु भाषण दे रहे थे, लोग भी दत्तचित्त होकर भाषण सुन रहे थे। इतने में मंडप के बाहर के लोग दूसरी तरफ जाने लगे। मंडप के अंदर के लोग भी उनके पीछे जाने लगे। थोड़े ही समय में आधे से अधिक मंडप खाली हो गया। पं. नेहरु सोच रहे थे कि इतनी एकाग्रता
से मेरा भाषण सुनने वाले ये लोग मंडप के बाहर क्यों जा रहे हैं? उन्हें उत्तर मिला ‘बाहर सिनेमा के एक्टर्स अधिवेशन स्थल पर आये हुए हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ उधर मुड़ी है।’ वे बहुत क्रुद्ध हुए परन्तु उन्हें वह सहन करना पड़ा। इस सारे क्रियाकलाप का दृश्य सम्मुख उपस्थित होने पर एक संस्कृत श्लोक स्मरण में आता है कि:-
‘यस्य कस्य तरोर्मूलं येन केनापि मिश्रितम् ।
यस्मै कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति ॥’
अर्थात ‘किसी एक पेड़ की जड़ लीजिये। किसी वस्तु में वह मिलाईये। किसी व्यक्ति को वह पिलाइये। कुछ न कुछ तो होगा।’ सार यह है कि उसके परिणाम अपने वश में नहीं होते, तथापि जनतंत्रात्मक पद्धति में उसका अपना एक महत्व होता है यह मान्य करना ही होगा। फिर भी यह बात निःसंदेह है कि इस प्रकार की भीड़ द्वारा राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति नहीं की जा सकती।
…अतः लोक संग्रह शब्द का शास्त्रीय अर्थ भिन्न है। वह है लोगों को उन्मार्गगामी बनने से रोकना, उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, अपने ध्येय के प्रति उनमें निष्ठा जागृत करना और कर्तव्य का विकास कर उन्हें एक में गूंथ कर पारस्परिक सहयोग की प्रवृत्ति उनमें निर्माण करना। यह कार्य अपने संगठन ने अपनाया है।
अन्यत्र कार्य करने वाले भी लोगों को एकत्र करते हैं, परन्तु वे उन्हें व्यक्तिनिष्ठ बनाते हैं। उनमें ध्येयनिष्ठा जागृत करने में वे असमर्थ होते हैं, जहाँ उनमें ध्येयनिष्ठा जागृत होती है, वहाँ उनके कर्तृव्य का विकास करने की ओर ध्यान नहीं रहता। और जहाँ कर्तव्य का विकास होता है वहाँ यह नित्य का अनुभव है कि पारस्परिक सहयोग से निरन्तर कार्य करने की प्रवृत्ति का अभाव ही होता है। अहंभाव एवं व्यक्तिनिष्ठा के कारण उनमें संघर्ष होते हैं। जो अन्य लोग संघ के कार्य से प्रभावित होकर संघ के कार्यक्रमों का अनुकरण करते हैं वे भी ध्येयनिष्ठा, कर्तव्य की भावना एवं पारस्परिक सहयोग से अविरत कार्य करने की प्रवृत्ति निर्माण करने में सफल नहीं हुए हैं।
संघ ने यह निर्माण करने में बहुत मात्रा में सफलता प्राप्त की है। यह कैसे करना है इसका रहस्य जाना है। संस्कृत में एक सुभाषित है कि:-
‘सौवर्णानि सरोजानी निर्मातुं संति शिल्पिनः ।
तत्र सौरभनिर्माणे चतुरचतुराननः॥’
शिल्पकार सुवर्ण के और अब कपड़े, कागज अथवा प्लास्टिक के फूल बनाते हैं, परन्तु उनमें सौरभ का निर्माण करने में चतुर चतुरानन ब्रह्मा समर्थ होते हैं। आज कृत्रिम सौरभ (सेंट) भी निर्माण किया जाता है और उसे उन फूलों पर छिड़क कर सुगंधित भी किया जाता है, तथापि स्वाभाविक रुप से सुगंधित फूलों की कुछ अपनी विशेषता होती है।
वास्तव में लोक संग्रह का याने लोगों में ध्येयनिष्ठा जागृत कर, उनके कर्तृत्व का विकास, उनमें पारस्परिक सहयोग की प्रवृत्ति निर्माण करने का रहस्य मानसशास्त्र का अध्ययन कर अपने धर्माचार्यों ने विहित किया है। उसका शास्त्र प्रणीत कर उसका विधान भी किया है। प. पू. डॉ हेडगेवारजी ने अपनी तीव्र ध्येयनिष्ठा एवं निरपवाद समर्पण के भाव के आधार पर उसका विकास कर उसे अपने जीवन में उतारा है। इसलिए वे ऐसे कार्यकर्ताओं की परम्परा निर्माण करने में सफल हुए। अतः अपना यह कर्तव्य है कि उस रहस्य को समझकर हम उसे आत्मसात करें और अपने व्यवहार में उसे उतारें।
लोक संग्रह के लिये आवश्यक गुण
लोकसंग्रह करने की क्षमता अपने जीवन में विकसित करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक गुण होता है अपने हिन्दू समाज के लिए अकृत्रिम स्नेह । अकृत्रिम शब्द का प्रयोग करना इसलिए आवश्यक होता है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग कृत्रिम स्नेह भी करते हैं, यानि स्नेह का आभास निर्माण करते हैं। वास्तविक स्नेह का वहां अभाव होता है। उदाहरणार्थ बीमा एजेन्ट किसी होनहार युवक को देख कर, उसके द्वारा अपने जीवन का बीमा कराया जावे इसलिए उससे मिलता है, उसे अपने घर बुलाकर उसका आतिथ्य करता है, परन्तु एक बार उसने बीमा कराया अथवा पूर्व में ही करवा चुका है यह ज्ञात हुआ कि बाद में उसकी कोई पूछताछ नहीं करता। कोई दुकानदार अपनी दुकान में पाटी लगाता है कि “ग्राहक का संतोष ही हमारा ध्येय है” परन्तु यह उसका वास्तविक ध्येय होता है क्या? वास्तव में यह, उसका साधन होता है, अन्यथा ग्राहक ने जो कोई माल जिस किसी मूल्य में मांगा, उस मूल्य में वह उसे दे देता । परन्तु वैसा वह नहीं करता और ग्राहक को असंतोष से वापस जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि ग्राहक का संतोष उसका ध्येय नहीं साधन है, और साध्य है उसके परिवार का भरण पोषण। इसका अर्थ यह नहीं है कि अकृत्रिम स्नेह का कोई दायरा नहीं होता । अपने परिवार पर वे अकृत्रिम स्नेह करते हैं और उस दायरे के बाहर के लोगों पर कम अधिक मात्रा में उनका कृत्रिम स्नेह होता है। वहां प्रेम का प्रदर्शन मात्र होता है। इस प्रकार प्रेम का दायरा सीमित न करते हुए समूचे राष्ट्र पर अकृत्रिम स्नेह होना नितांत आवश्यक होता है।
अपने ध्येय के प्रति अविचल ध्येयनिष्ठा यह दूसरा गुण है, जो लोक संग्रह क्षमता अपने जीवन में विकसित करने के लिए आवश्यक है। हमें यह नित्य स्मरण में रखना आवश्यक है कि व्यक्तियों पर हम उतनी ही मात्रा में ध्येय निष्ठा का विकिरण (Radiation) करें जितनी मात्रा में अपने पास हैं। हमारे पास यदि एक सौ रुपये हैं तो हम दूसरे को एक सौ ही रुपये दे सकते हैं, इससे अधिक हम दे नहीं सकते। यह जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि जितनी मात्रा में अपने अंतःकरण में निष्ठा होगी उतनी ही मात्रा में हम दूसरों पर उसका विकिरण कर सकते हैं। जिस पर संस्कार किए जाते हैं वह व्यक्ति ध्येयनिष्ठा की तीव्रता को अपने चिंतन से अपनी तपस्या से तीव्रतर और तीव्रतम कर सकता है, परन्तु उसका श्रेय उस संस्कारित व्यक्ति को होगा हमे नही । हम तो केवल उतनी मात्रा में ध्येयनिष्ठा का विकिरण कर सकते हैं जितनी मात्रा में वह अपने पास होगी। इसलिए हमें नित्य चिंतन एवं आत्मनिरीक्षण कर अपनी ध्येयनिष्ठा को तीव्रतम करने का प्रयास करना चाहिए।
यह ध्येयनिष्ठा तीव्रतम करने के लिए हमें आत्मकठोर वृत्ति (an attitude of self denial or self abnegation) का अंगीकार करना नितांत आवश्यक होता है। कर्मप्रवृत्तिमार्ग अपनाने वालों के मन में यह धारणा है कि आत्मकठोरता (ascetic spirit) का विधान निवृत्ति मार्ग के लिए किया गया है, कर्मप्रवृत्ति वालों के लिए नही। परन्तु यह एक बड़ा भ्रम है। प्रवृत्ति धर्म के कट्टर समर्थक महर्षि श्री अरविन्द ने भी कहा है कि व्यवहार में परिपूर्ण मानवत्व प्राप्त करने के लिए आत्मकठोर वृत्ति एक अपरिहार्य साधन है और उसे हम तब तक अमान्य नहीं कर सकते जब तक अपनी शारीरिक जैव प्रवृत्तियों को एवं बुद्धि को निरंतर प्रभावित करने वाली पाशवी वृत्ति से हम मुक्त नहीं हो जाते। स्पष्ट है कि आत्मकठोर वृत्ति अपरिहार्य होती है। पुनः इस आत्मकठोरता के कारण ध्येयनिष्ठा के संस्कार हम अन्य व्यक्तियों पर सुगमता से कर सकते हैं।
तथापि जैसा कि गीता में कहा है कि:-
‘सर्वारम्भाहिदोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।’
अग्नि के साथ धुआ आता ही है उसी प्रकार प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष होता है। अतः इससे कुछ दोष उत्पन्न होने की संभावना सदा रहती ही है। अपने प्रति कठोर होने का परिणाम यह होता है कि दूसरों के प्रति भी कठोर होना, यह उसका स्वभाव बन जाता है। आत्मकठोर मनुष्य दूसरों में दिखने वाले दोष सहन नहीं कर सकता, असहिष्णु हो जाता है। जिनमे दोष दिखते हैं उनके प्रति कठोर रुख अपनाता है। उनके लिए कटु शब्दों का प्रयोग करता है। उन पर क्रुद्ध होता है । फिर लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। उसके सम्पर्क में नहीं आते। फिर वह दूसरों पर संस्कार कैसे कर सकेगा?
लोगों में यदि दोष दिखते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आत्मीयता के आधार पर ही प्रयास करना चाहिए। आत्मीयता के अभाव में उस कार्यकर्ता को लोग त्याज्य मानते हैं, उससे बात नहीं करते अथवा बात कृत्रिम रुप से होती है । क्रुद्ध हुआ कार्यकर्ता रूखे स्वर से बात करता है। अतः वह अंतःकरण को स्पर्श नहीं करती और इसलिए विकास करने में वह सहायक नहीं होती । क्रुद्ध होकर बात करना इसका यह अर्थ होता है कि वह कार्यकर्ता यह सोचता है कि अब इस स्वंयसेवक का अधिक विकास नहीं हो सकता। अधिक स्पष्ट रुप से कहना हो तो यह कहना होगा कि उस क्रुद्ध हुए कार्यकर्ता की दूसरों पर संस्कार करने की और परिणामतः उनका विकास करने की क्षमता कुंठित हुई है। उस कार्यकर्ता का विकास ही कुंठित हुआ है। अकृत्रिम स्नेह होगा, आत्मीयता होगी, तो उस व्यक्ति के दोषों को, मतभेदों को समझते हुए मैं संयम से व्यवहार कर उसका विकास करुंगा ही, इसमें और मुझमें जो हिन्दुत्वजनित एकात्मकता की भावना है, उसका उपयोग संस्कार करने के लिए है यह विचार एवं व्यवहार करने का दृष्टिकोण होगा। इतना ही नहीं तो इस व्यक्ति के विकास में मेरा एवं समाज का विकास निहित है यह अनुभूति रहेगी और गतिरोध दूर होगा ।
अपवाद के रुप में यह भी संभव है कि किसी स्वयंसेवक की ऐसी प्रकृति हो कि उसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर ही समझाना आवश्यक हो । जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ‘क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ’। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को डांट पिलाकर ही उसका विकास किया जा सकेगा। परंतु उसके उस स्वभाव को परख कर योजना पूर्वक क्रुद्ध होना और विकारवश क्रुद्ध होना इसमें बहुत अंतर है। पहले व्यवहार में उसे लाभ होगा एवं हमारा भी संयम रहेगा। दूसरे व्यवहार से वह दूर होगा, निष्क्रिय होगा और विकार के वशीभूत होने से हमारा विकास भी अवरुद्ध होगा।
अतः आत्मचिंतन कर, आत्मनिरीक्षण कर हमने अपनी ध्येयनिष्ठा तीव्र करने के लिए स्वयं आत्मकठोर (puritan) बनना चाहिए, परंतु कठोर दृष्टिकोण (puritanistic outlook) अपना कर दूसरों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। उनके दोषों को उनकी विवशताओं को हम समझें, उन्हें सुधारने के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अंगीकार करें। यह व्यापक एवं आत्मीयतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए धैर्य धारण करना यह सबसे अच्छा साधन है।
धैर्य धारण करना तब तक ही संभव होगा जब तक कि जीवन की विकसनशीलता में हमारा दृढ़ विश्वास होगा। हम अपना स्वयं का आत्म-निरीक्षण करेंगे तो अपनी समझ में आवेगा कि आखिर अकृत्रिम स्नेह, ध्येयनिष्ठा एवं कर्तृत्व अपने में यथा समय विकसित हुए हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क आने पर, उनकी आत्मीयता के जल से सिंचित होने पर दोष नष्ट होकर अपने विकास की गति बढ़ी है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता ही है। विकास की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की गति तीव्र होगी, किसी की गति मंद होगी, परन्तु कुछ अपवाद छोड़ दिए जायें तो सामान्यतः व्यक्ति का विकास होता ही है। हमारा कर्तव्य इतना मात्र होता है कि अपनी आत्मीयता, ध्येयनिष्ठा एवं धैर्य के आधार पर अपने व्यवहार से उसकी गति को तीव्र करते रहें। उदाहरणार्थ प्रत्येक पौधा यथासमय बढ़ता ही है । परन्तु समय-समय पर यदि उसे सिंचित किया गया, खाद दिया गया, उसके चारों ओर उगा कचरा निकाला गया और यदि बागड़ की गयी तो सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित होकर उसका विकास जल्दी होगा, पल्लवित एवं पुष्पित होकर उसमें फल लगेंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता ही है। उसके विकास में सहायक होना इतना मात्र हमारा कर्तव्य होता है।
है
सहायक होने की दृष्टि से प्रथमवार ही नहीं अपितु सदैव यह आवश्यक होता है कि उपदेश ग्रहण करने के लिए कार्यकर्ता की अनुकूल मनोभूमिका (receptive mind) है अथवा नहीं इसका हम सदैव निरीक्षण करते रहें। मनुष्य का मन इतनी गुत्थियों से युक्त होता है कि भिन्न-भिन्न मनःस्थितियों में किए गए एक ही उपदेशके बिल्कुल भिन्न एवं सर्वथा विपरीत परिणाम हमें उसमें देखने के लिए मिलते हैं। जब वह शांत है, एकांत में है, तब किया हुआ उपदेश वह सुनेगा। परंतु जब किसी कार्य को करने की धुन उस पर सवार है, किसी की गलती के कारण वह क्षुब्ध है, चार लोगों से घिरा हुआ है, ऐसे समय यदि हम वहीं उपदेश उसे करेंगे, उसके दोषों की ओर निर्देश करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया उलटी होगी, घमंड भरी वाणी से वह कहेगा कि ‘मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने जो किया वह व्यवहार उचित ही है।’ जिसका मुँह ढका हुआ है उस पात्र में यदि दूध डाला जाये तो वह दूध भूमि पर गिर जाता है, बह जाता है, एक बूंद भी पात्र में नहीं जाता।
स्पष्ट है कि उपदेश कर केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर संतुष्ट होना महत्व की बात नहीं, अपितु हमारे उपदेश को उसने ग्रहण किया अथवा नहीं यह महत्व की बात है। यह तब ही होगा जब आत्मीयता अर्थात मित्रता के साथ विवेक धारण किया हुआ और समयानुकूल अपना व्यवहार होगा। सन्मित्र के लक्षणों का वर्णन करते हुए भर्तृहरि ने कहा कि :-
‘पापान्निवारयति योजयते हिताय
गुह्यंच गूहति गुणान् प्रकटीकरोति ।
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदंति संतः ॥
अर्थात् ‘पाप से निवृत करना, हितकारक योजना बनाना, जो गुह्य (गुप्त रखने योग्य बात अर्थात् दोष) है उसे गुप्त रखना, गुणों का प्रकटीकरण, आपत्ति में उसका त्याग नहीं करना और अवसर आने पर उसकी सहायता करना, संत कहते हैं कि ये सन्मित्र के लक्षण है।’ स्पष्ट है कि उसके दोष सबके सामने नहीं बताना चाहिए। बताने पर जहां एक ओर उसके अहंकार को ठेस लगेगी और उसका उस पर विपरीत प्रभाव होगा, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता के नाते उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा और परिणामतः प्रभावी ढंग से वह कार्य सम्पादित करने में असमर्थ होगा।
अपने में आकलन की क्षमता पैदा करनी होगी
उपदेश ग्रहण करने की उसकी अनुकूल मनोभूमि को देखने के पश्चात् भी उसके विकास में सहायक होने की दृष्टि से कितनी मात्रा में वह उपदेश ग्रहण कर सकता है, कितनी मात्रा में उसकी ध्येयनिष्ठा तीव्र है, कितना उसमें कर्तृत्व है, इसका ठीक ठीक आकलन करने की क्षमता अपने में विकसित करनी होगी। उपदेश ग्रहण करने की उसकी क्षमता से अधिक मात्रा में यदि हमने उपदेश किया अथवा उसे दायित्व दिया तो वह उसके बोझ से दब जावेगा। हमारा किया हुआ उपदेश निरर्थक होगा, हानिकारक होगा और उसमें निष्क्रियता आवेगी अथवा विकृति आवेगी। उदाहरणार्थ- दुबले व्यक्ति को सबल बनाने के लिए हमने उसे अधिक मात्रा में व्यायाम करवाया, तो उसका शरीर दर्द करेगा। उसकी पाचनशक्ति से अधिक यदि उसे पौष्टिक पदार्थ खिलाये तो उसे उल्टी होगी और दस्त होंगे। इसलिए धीरे-धीरे व्यायाम करवाकर थोड़े-थोड़े पौष्टिक पदार्थ खाने के लिए देकर प्रकृति में सुधार हुआ अनुभव कर फिर अधिक व्यायाम करने के लिए तथा अधिक पौष्टिक पदार्थ खाने के लिए देना उचित होगा। किसी बर्तन में तीन लीटर दूध धारण करने की क्षमता हो और हमने उसमें पाँच लीटर दूध डाला और एकदम डाल दिया तो दो लीटर दूध तो बह जावेगा ही, परन्तु एकदम डालने का परिणाम यह होगा कि बर्तन में ढाई लीटर दूध ही रहेगा बाकी का उछलकर गिर जावेगा। इसलिए धीरे-धीरे उसमें दूध डालना चाहिए ताकि तीन लीटर दूध उसमें समा सके। इसलिए व्यक्ति की क्षमता देखकर ही उसे उपदेश करना चाहिए। बर्तन की ग्रहण करने की क्षमता तो नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि वह निर्जीव है, अचेतन है, परन्तु मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ायी जा सकती है, वह सजीव है, चैतन्ययुक्त है और इसलिए विकासशील है । उपदेश ग्रहण करने से अथवा स्वयं के अनुभव के आधार पर वह चिंतन कर अपना विकास कर सकता है।
उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी है और वह अधिक विकास कर सकता है ऐसा यदि अपना निरीक्षण हो तो उसकी ध्येयनिष्ठा बढ़ाने के लिए एवं उसके कर्तृत्व का विकास करने के लिए प्रयोग के रुप में उसे और अधिक दायित्व सौंपना कभी-कभी लाभकारी भी होता है। उस दृष्टि से उसकी क्षमता के संभाव्य विकास के संबंध में अपना अचूक निरीक्षण एवं उसके आधार पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। यह एक अपवाद स्वरुप उदाहरण है। सामान्य रुप से कार्यकर्ता का विकास यथाक्रम ही होता है।
अनुकूल मनोभूमिका बनाने के लिए तपस्या
उपदेश ग्रहण करने की दृष्टि से स्वयंसेवक की ग्रहणानुकूल मनोभूमिका बनाने के लिए तथा उपदेश ग्रहण कर वह अधिक ध्येयनिष्ठ एवं अधिक कर्तृत्वसंपन्न हो सके इसलिए हमको तपस्या करना आवश्यक है। तपस्या करना चाहिए यह कहते ही सामान्य लोग यह समझते हैं कि नाक पकड़कर प्राणायाम करना, ध्यान करना, नाम स्मरण करना अथवा पूजा अर्चना करना अपेक्षित है। जिनकी इन विधियों पर श्रद्धा है वह अवश्य करें । परन्तु यहां भगवद्गीता में निर्दिष्ट तीन प्रकार का तप अभिप्रेत हैं- (1) शारीरिक तप (2) वाङ्मय तप और (3) मानस तप। इन तपों के अनुसार आचरण करना, संस्कार करने की अपनी क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से कार्यकर्ता के लिए अपरिहार्य है। इन तपों को आचरण में लाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वे दिशानिर्देश करने के लिए है। आज के सन्दर्भ में और विशेष रुप से अपने संघ कार्य के परिप्रेक्ष्य में उनके जैसे अनेक व्यवहारों का समावेश करना अशास्त्रीय नहीं होगा। गीता में शरीर तप का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-
‘देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनंशौचमार्जवम् ।
ब्रहचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यतै ॥’
इस शरीर तप में ज्ञानवृद्ध लोगों का आदर करने का विधान है। आज के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि अपने से सहमत अथवा भिन्न विचारधारा भी अपनाकर अपना स्वयं का विचार न करते हुए समाज की स्थिति उन्नत करने के लिए अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो लोग प्रयास करते हैं उनका भी हमें आदर करना चाहिए। अनेक लोगों से परिचय करना, उनसे बार-बार मिलकर आत्मीयता बढ़ा कर उन्हें अपने ध्येय एवं कार्यपद्धति से परिचित कराकर उन्हें अपनी सामूहिक उपासना में भाग लेने के लिए प्रेरित करना- इन चेष्टाओं का भी शरीर तप में समावेश किया जा सकता है। फिर अपना शरीर शुद्ध याने पवित्र रखना चाहिए। जीवन में ऋजुता – प्रामाणिकता अपनाना चाहिए। इंद्रियनिग्रह एवं अहिंसा को अंगीकार करना चाहिए। वाङ्मय तप का वर्णन भी गीता में इस प्रकार किया है:-
‘अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥’
ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जो उद्वेगकारक न हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि चूकिं किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके दोष उसे न बताते हुए उन्हें गुणों के रुप में हम मान्यता दें। इसलिए बाद में कहा है कि सत्य कहना चाहिए और प्रियकर कहना चाहिए, कल्याणकारक कहना चाहिए। सार यह है कि दूसरों में दिखे दोष सब अन्य लोगों को न बताते हुए उसी को एकांत में शांत चित्त से, संयत एवं मधुर वाणी में बताना चाहिए, ताकि वह दोष दूर कर अपने व्यवहार में सुधार करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके और कार्यकर्ता के नाते उसकी जो प्रतिष्ठा है उसे हानि न हो। सत्य एवं हितकर बात बताना चाहिए।
ऋग्वेद में एक मंत्र है कि
‘सक्तुमिव तित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।
अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मी निहिताधिवाचि ॥
अर्थात जिस प्रकार सत्तु छानकर उसका सेवन किया जाता है, उसी प्रकार मन से वाणी को परिष्कृत कर धीर लोग उसका प्रयोग करते हैं। उसके कारण जो असखा (अमित्र) होते हैं वे सखा (मित्र) बनते हैं। ऐसे धीर लोगों की वाणी में लक्ष्मी अधिष्ठित होती है, वाङ्मय तप में स्वाध्याय और उनके नित्य अभ्यास का भी विधान है, यानी अपने धार्मिक ग्रंथों का नित्य पाठ करना, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना, अपनी एवं भिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करना, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के भाषणों एवं उक्तियों को पढ़ना, उनका नित्य अध्ययन करना, इनका आज के संदर्भ में वाङ्मय तप में समावेश करना उचित होगा।
तीसरा है मानस तप । प्रखर ध्येयनिष्ठा तथा आत्मकठोर वृत्ति के कारण एवं अन्य स्वयंसेवकों के अथवा व्यक्तियों के दोषों से या गलतियों से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिये वाङ्मय तप के अनुसार वाणी पर जो संयम करना पड़ता है उसके कारण हमें सफलता तो मिलती है, परंतु वह संयम कृत्रिमरूप से याने जबरन धारण किया हुआ होगा तो अनेक बार उसके परिणामस्वरूप मन पर उसका बोझ आता है और कभी कभी तनाव असह्य होने पर उसका अन्यत्र विस्फोट होता है। हम व्यर्थ ही किसी अन्य व्यक्ति पर अथवा सामान्य रूप से अपने परिवार पर क्रोध उतारते हैं। एक को संतुष्ट करने के प्रयास की परिणति दूसरे में विनाशकारक मनोमालिन्य निर्माण करने में होती है। यह कृत्रिम अथवा जबरन लादा गया संयम लोक संग्रह करने में बाधक होता है, अत: यह आवश्यक होता है कि अपनी वाणी पर अपना संयम हो परंतु जबरन किया हुआ संयम न हो अपितु आंतरिक संयम हो। इसलिए मानस तप का विधान है। उसका वर्णन है:-
‘मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥’
इस तप में यह निर्देश है कि हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए, सौम्य वृत्ति धारण करना चाहिए। कहना न होगा कि यदि हमने निष्काम भाव से अहंभाव रहित होकर प्रयास किया तो यह संभव है। इस प्रसन्नता और सौम्य वृत्ति के कारण स्वयं की प्रेरणा से लोग आपकी ओर आकृष्ट होते हैं। यह प्रसन्न ह्रदयता और सौम्य वृत्ति लोक संग्रह करने के लिए अधिकतम सहायक होती है। हंसते खेलते फिर हम लोगों को बड़े-बड़े सिद्धांत भी समझा सकते हैं, उनके गले उतार सकते हैं। फिर मौन व्रत का निर्देश है। यह तो स्पष्ट ही है कि मौंन व्रत का यह अर्थ अभिप्रेत नहीं कि अपना मुंह बिल्कुल बंद ही रखना, अपितु यह अर्थ है कि दूसरों की आलोचना नहीं करना चाहिए और अपने विचारों का भावात्मक (Positive) प्रतिपादन करना चाहिए।
आत्मनिग्रह याने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपवित्र विचारों को मन में प्रवेश न देते हुए आंतरिक भावना शुद्ध रखना चाहिए। अत: इन तीनों तपों-शरीर, वाङ्मय एवं मानस तपों को करना आवश्यक होता है।
हेतु की पवित्रता
यह यद्यपि सत्य है फिर भी इन तपों को करते समय आंतरिक हेतु शुद्ध होना अत्यन्त महत्व की बात है। आंतरिक हेतु के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। (१) तामस, (२) राजस, (३) सात्विक। अपने मूर्खतापूर्ण निश्चय से, स्वयं को पीड़ा देते हुए अथवा दूसरों का विनाश करने के उद्धेश्य से जब ये तीन प्रकार के तप किए जाते हैं तब यह तामस कहा जाता है। यह निकृष्ट श्रेणी का तप है। इससे ऊँची श्रेणी का तप राजस तप कहा गया है। स्वयं को मान सम्मान प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, आदर प्राप्त हो इसलिए दंभयुक्त भाव से जब ये तप किए जाते हैं तब ये राजस तप कहे जाते हैं वे दोंनो तप अनिश्चित फल वाले और अनित्य तप होते हैं। यह मध्यम श्रेणी का तप है। इससे ऊँची श्रेणी सात्विक तप की है। फलाकांक्षा से रहित होकर श्रद्धा
के साथ जब इन तपों का अवलंब किया जाता है तब वह श्रेष्ठ तप कहा जाता है । यह तप की सात्विक श्रेणी है। वास्तव में इस भावना से किए गए ये तीनों तप व्यक्ति का आत्मिक विकास में इस भावना से किए गए ये तीनों तप व्यक्ति का आत्मिक विकास भी करते हैं। श्रद्धा के साथ ये तप करने का विधान पढ़कर पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित मन विचलित हो सकता है। परंतु योगी श्री अरविन्द ने श्रद्धा के तीन अंग बताये हैं (१) अंतःकरण की सम्मति (२) संकल्प की शक्ति और (३) अंतरात्मा का सानंद समर्पण। वस्तुतः इस श्रद्धा के साथ सात्विक तप करना कार्यकर्ता के शरीर, बुद्धि और मन को स्वस्थ बनाये रखेगा। उसकी कर्मशक्ति बढ़ायेगा और संस्कार्य व्यक्ति की ग्रहणानुकूल मनोभूमिका बनाकर उसमें ध्येयनिष्ठा एवं कर्तव्य बढ़ाने में सहायक होगा।
हम लोगों को परखें
यह स्वाभाविक है कि लोक संग्रह करते समय हम लोगों को परखें और जिन पर संस्कार करने से उनमें गुण विकास होने की संभावना अधिक है उन पर संस्कार करने के अधिक प्रयत्न हम करें। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्यों की ओर ध्यान न दें, उनके दोषों के कारण हम उनसे दूर रहें। समाज के सब स्तरों के और सब प्रकार के लोगों से अपना संपर्क रखना नितांत आवश्यक है। संस्कृत में एक सुभाषित है:-
“अमंत्रमक्षरं नास्ति न वा मूलमनौषधम् ।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ॥”
अर्थात् ‘ऐसा एक भी अक्षर नहीं जिसका मंत्र में उपयोग न हुआ हो, ऐसी एक भी वनस्पति नहीं कि जिसमें कोई औषधि द्रव्य नहीं, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं कि जो सर्वथा अयोग्य हो, दुर्लभ है केवल योजकता । ‘
लोगों को जुटाते समय केवल दोष देखना उचित नहीं उनके गुणों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक गिलास, दूध से आधा भरा हो तो दोष दृष्टि वाला सोचेगा कि आधा गिलास खाली है। परंतु लोक संग्रह करने की इच्छा रखने वाले की यह दृष्टि होनी चाहिए कि आधा गिलास दूध से भरा है। प्रत्येक मनुष्य में गुण एवं दोष दोनों होते हैं। सर्वथा गुण रहित अथवा सर्वथा दोष रहित व्यक्ति मिलना असंभव सा होता है। उनके दोषों को नष्ट करने का प्रयास करना और गुणों का विकास करना यह दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है। बिल्कुल उद्दण्ड व्यक्ति में भी गुण होते हैं। उनका संगठन के लिए और परिणामतः राष्ट्र के लिए कैसे उपयोग करना इसका नित्य चिंतन आवश्यक होता है। इतना ही नहीं तो उनमें सूक्ष्मरुप से जो गुण होते हैं उनको बड़ा समझ कर अपने जीवन में उन्हें विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि-
‘मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा-
स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयतः ।
परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं
निज हृदि विकसंतः संति संत: कियंतः॥”
अर्थात् ऐसे कितने संत हैं कि जिनके शरीर, बुद्धि और मन पुण्यपीयूष या अमृत से पूर्ण हैं, जो त्रिभुवन को अपनी उपकार परंपरा से प्रसन्न करते हैं और जो दूसरों में दृष्ट परमाणु समान गुण को भी पर्वत जैसा विशाल समझकर अपने ह्रदय में उसका विकास करते हैं।
अनेक वर्षों से अपना संघकार्य हम अच्छा चला रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि कार्य करने की क्षमता बढ़ने के पश्चात् भी अनेक कार्यकर्ता किसी समस्या के कारण अथवा अविरत कार्य करने से मानसिक थकावट आने के कारण निष्क्रिय बने हैं। अनेक बार हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे निष्क्रिय हुए कार्यकर्ताओं के प्रति गंभीर रुप से विचार न करने वाले सक्रिय स्वयंसेवक अनुदार शब्दों का प्रयोग करते हैं अर्थात् वाड्.मय तप का आचरण नहीं करते। वास्तव में ऐसे निष्क्रिय बने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का आकलन कर उनके प्रति आज के सक्रिय कार्यकर्ताओं को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने अपनी संगठन की गाड़ी को अविरत परिश्रम कर बहुत दूरी तक खींचा है और कार्य बढ़ाया है। इतना मात्र भी स्वंयसेवक ने विचार किया तो उसके मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होगा। शारीरिक रोग अथवा थकावट के कारण अस्वस्थ स्वंयसेवक की हम सेवा शुश्रुषा करते हैं ना? ऐसा नहीं सोचते कि यह निष्क्रिय हो गया है, अपितु अपना सोचने का व्यवहार करने का दृष्टिकोण आत्मीयता का एवं भूतदया का होता है। साथ ही हम यह भी सोचते हैं कि यह शारीरिक रोग से अथवा थकावट से मुक्त हो जाएगा और पुनः कार्य करने में जुट जावेगा। अतः आत्मीयता से हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार जो मानसिक थकावट आने से निष्क्रिय हुआ है, वह भी थकावट दूर होने पर पुनः कार्य में जुट जावेगा। यह उसके संबंध में विचार करने का और उसके प्रति व्यवहार करने का अपना दृष्टिकोण होना चाहिए।
अतः उससे नित्य सम्पर्क रखना, कार्य की गतिविधियों की उसको जानकारी देना, किसी विशेष प्रसंग पर उत्सव के समय उसको सूचना देना, यह अपना स्वभाव बनाना चाहिए। इसके बदले हम अनुदार हो जाते हैं। गहराई से यदि विचार किया तो यह अनुभव होगा कि ‘मैं अविरत कार्यरत हूँ और यह अलसाया है’ यह अहंभाव भी वास्तव में उसके संबंध में अनुदार विचार उत्पन्न करता है। यह न हो और हम उसे ठीक प्रकार से समझ सके इसलिए हमने यदि अपने बारे में सोचने का ठीक दृष्टिकोण अपनाया तो यह मनोमालिन्य नहीं होगा। ‘मुझ पर परमात्मा की कृपा है, उससे मुझे प्रेरणा एवं शक्ति मिली है इसलिए मैं कार्यरत हूँ। कौन कहे मेरी भी शक्ति क्षीण हो सकती है। मैं निष्क्रिय हो सकता हूँ यह यदि हमने विचार किया, तो उसके प्रति सहानुभूति धारण कर सकेंगे। पिछले आपातकाल ने तो यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसे निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की भी कार्य के लिए उपयोगिता सिद्ध हुई। उनके निष्क्रिय होने के कारण पुलिस की उन पर निगरानी नहीं थी। परिणामतः अपने असंख्य अज्ञातवासी कार्यकर्ता निश्चिंत होकर उनके घरों में, (सरकारी अधिकारियों के घरों में भी) निवास कर, कार्य का संचालन कर सके।
पुनः हम यह अनुभव करते हैं कि निष्क्रिय बने अनेक कार्यकर्ता थकावट दूर होने पर अथवा सेवा से निवृत्त होने पर पुनः कार्य में जुट गए हैं। उनकी शक्ति कार्यवृद्धि के लिए उपयोग में आये यह अपनी इच्छा होने के कारण और अधिक पुराने स्वयंसेवकों को कार्य में जुटाने का अपना प्रयत्न है। कार्य से बहुत दिनों तक उनका संबंध न होने के कारण वे संघ कार्य के पहले स्वरुप की, जब वह प्रारंभिक अवस्था में था याने केवल संघ स्थान के कार्यक्रम ही थे की कल्पना करते हैं, उसका व्यापक और अनेकविध स्वरुप उनकी समझ में नहीं आता । संघ स्थान, वहाँ होने वाले कार्यक्रम एवं उनके माध्यम से पारस्परिक सहयोग से कार्य करने के संस्कार यह तो आवश्यक एवं अपरिहार्य अंग है। परंतु यथासमय संगठन के पौधे का विकास होकर, वह वृक्ष बना है, उसकी शाखाएँ फैली हैं, उसमें फूल लगे हैं और अब फल भी लग रहे हैं। वह वृक्ष अधिक फूले और फले यह राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए आवश्यक है। परंतु इस ओर पुनः सक्रिय हुए इन पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं जाता। आज का सक्रिय कार्यकर्ता यदि उन्हें यह समझाता है तो यह उनकी समझ में नहीं आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने संघ का अलग ही रूप देखा है और यह कार्यकर्ता हमें और कई बातें बताता है, जो संघ कार्य से संबद्ध नहीं हैं। अतः यह सोचते हैं कि यह अनुभवहीन है, इसलिए वे उसे उपदेश करने लगते हैं। संघ के आज के कार्यकर्ता को उनकी बातें सुनकर अटपटा सा लगता है, वह सोचता है कि ‘वे आज तक निष्क्रिय रहे और आज हमें उपदेश करते हैं’ परिणामतः दोनों में सामंजस्य नहीं होता। इसका वास्तव में कारण है दोनों में विद्यमान अहंकार । अतः दोनों को आत्मचिंतन कर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक होता है । निवृत्ति से लौटे और सक्रिय हुए कार्यकर्ता को वास्तव में यह सोचना चाहिए कि आखिर यह कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत है, यह कुछ अपनी बात नहीं करता अपितु आज के कार्य की स्थिति देखकर, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जो योजना बनाते हैं, समझते हैं, करने की प्रेरणा देते हैं वहीं यह कहता है, करता है और नित्य कार्यरत नए कार्यकर्ता को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार इन पुराने लोगों ने अपनी युवावस्था में अत्यंत परिश्रम कर कार्य किया है, सेवा में रहते हुए उन्होंने जीवन में कुछ अनुभव, ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उस प्रतिष्ठा के कारण वे लोगों को त्वरित प्रभावित कर उन्हें सहयोग करने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। याने दोनों के गुणों से संगठन को, परिणामतः राष्ट्र को लाभ होने वाला है।
यह अनुभव कर एक दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना चाहिए। वैसे भी दूसरों की बातों को शांत चित्त से सुनना यह सफल कार्यकर्ता बनने की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है। ऐसे लब्धप्रतिष्ठ एवं सक्रिय कार्यकर्ता में यदि कुछ त्रुटियाँ दिखाई दी तो ऊपर वर्णन किए अनुसार उनकी ग्रहणानुकूल मनोभूमिका होने पर उनसे एकांत में इस संबंध में बात करना चाहिए। कभी कभी हंसते खेलते अपने स्वयं के संबंध में विनोद करते हुए भी दोष दूर करने का प्रयास करना होगा। पुनः प्रत्येक, सजीव इकाई होने के कारण सबके लिए एक ही प्रकार के उपाय का अवलंब संभव नहीं है। एक प्रकार का उपाय किसी में सुधार कर सकता है, तो दूसरों को वह अनुपयोगी हो सकता है। पेनीसिलीन संजीवनी औषधि सिद्ध हुई है। परंतु जिसे उसकी एलर्जी है उसे वह मारक होती है। इस प्रकार दोनों के द्वारा एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण समझा कर पारस्परिक सहयोग से कार्य का व्यवस्थित रुप से संचालन किया जा सकता है।
संबंध में आने वाले व्यक्तियों के विषय में विशेष रूप से स्वयंसेवकों के विषय में ठीक परख करने की कुशलता हम लोगों को अपने में विकसित करना कार्यसिद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। स्वयंसेवकों की निष्ठा एवं कर्तव्य की परख कर उन्हें कार्य सम्पादन का दायित्व सौंपना अति फलदायक होता है। ये दोनों गुण कार्यकर्ता में होना नितांत आवश्यक है। निष्ठा की कमी होने पर कर्तृत्व रहा तो व्यक्ति को कार्य के संपादन का दायित्व सौंपने पर बहुत हानि होती है। कर्तृत्व है परंतु निष्ठा नहीं ऐसे लोगों को कार्य का दायित्व सौंपने के कारण हुई हानि के उदाहरण तो अपने इतिहास में बहुत उपलब्ध है। आज भी राष्ट्र में उनकी कमी नहीं है। ऐसे कार्यकर्ता को बहुत जिम्मेवारी का काम नहीं देना चाहिए। परंतु वह अपने से दूर न हो इसलिए साधारण दायित्व का कार्य सौंपना चाहिए और साथ ही अपने आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से उसमें ध्येय निष्ठा बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से निष्ठा शत प्रतिशत है परंतु कार्य संपादन के दायित्व के अनुपात से कर्तव्य नहीं है तो उसके कारण भी होने वाली हानि के उदाहरण प्रचुर मात्रा में पहले हुए हैं और आज के युग में भी बहुत है। उचित यह होगा कि निष्ठा होने पर कर्तृत्व कितनी मात्रा में है यह परख कर उसे उतना ही दायित्व सौंपा जाय। प्रायः होता यह है कि किसी निष्ठावान स्वयंसेवक की आज्ञाकारिता के कारण उसके प्रति अनुराग अथवा ममता निर्माण होती है। उसके कर्तव्य की परख करने में वह बाधक बनती है। परिणामत: उसमें बहुत कर्तव्य है यह भ्रम निर्माण होता है। हम उसे दायित्व सौंपते हैं और कर्तव्य के अभाव में वह कार्य पूरा नहीं कर पाता । निष्ठा एवं कर्तव्य होने पर भी यदि किसी कार्यकर्ता का अपने से कार्यसंपादन की पद्धति में अंतर हो अथवा अन्य किसी प्रकार के मतभेद हो तो अनेक बार मनोमालिन्य और कभी कभी द्वेष भी निर्माण होता है। फिर हम उसे कार्य नहीं सौंपते । परिणामतः कार्यसिद्धि नहीं होती। ऐसे प्रसंग आने पर उसे दायित्व सौंपने योग्य साहस भी हमारे में होना आवश्यक है । सार यह है कि निष्ठा एवं कर्तृत्व की ठीक ठीक परख कर राग एवं द्वेष से रहित होकर हमें कार्यकर्ता को संपादन का दायित्व सौंपना चाहिए।
यह भी सत्य है कि व्यक्ति के संभाव्य विकास का सम्यक आकलन कर उसके कर्तव्य से थोड़ा अधिक दायित्व सौंपना उसके विकास में कभी कभी सहायक होता है और कार्यसिद्धि भी होती है। तथापि इस प्रकार प्रयोग करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है।
व्यक्तिनिष्ठा नहीं ध्येयनिष्ठा
अनेक बार यह अनुभव किया जाता है कि कार्यकर्ता की गुणविशेषताओं के कारण कोई व्यक्ति कार्य से जुड़ता है। उसकी प्राथमिक अवस्था में यह स्वाभाविक भी है। तैरना सीखते समय तुमड़ी का सहारा आवश्यक होता है। परंतु बाद में अधिक अभ्यास होने पर तुमड़ी का त्याग करना भी आवश्यक है तभी कोई अच्छा तैराक हो सकता है। तुमड़ी के सहारे तैरने वाला व्यक्ति तुमड़ी फूटने पर डूबता है। इसलिए कार्यकर्ता की कुशलता इस पर निर्भर करती है कि वह अपने प्रति निष्ठा को ध्येयनिष्ठा में परिवर्तित करे अन्यथा उस कार्यकर्ता के न रहने पर वह भी निष्क्रिय हो जावेगा। यह तब ही संभव होगा जब दूसरे कार्यकर्ताओं से भी उसका लगाव बढ़ेगा। तदर्थ दूसरे कार्यकर्ताओं से भी वह मिले, उनकी बात वह सुने और उसको क्रियान्वित करे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। समूचे संगठन से और परिणामतः राष्ट्र से समरस होने का लक्ष्य उसके सम्मुख अपने आचरण से प्रस्तुत करना चाहिए।
कार्य करते हुए जब कार्यकर्ता की गुणवत्ता अधिक बढ़ती है, तब स्वाभाविक रुप से उसे अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र सौंपा जाता है। उसके हाथ के नीचे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती है। सौंपे गये कार्य में शीघ्र प्रगति हो यह भावना कार्यकर्ता में होना स्वाभाविक है। वह बढ़ना चाहिए । यह वरिष्ठ कार्यकर्ता अपेक्षा भी करते हैं । परंतु इस सौंपे गये कार्य को संपन्न करने की धुन में वह अनेक बार यह भूल जाता है कि आखिरकार उसके हाथ के नीचे कार्य करने वालों का विकास करने की ओर भी उसे ध्यान देना चाहिए। उनके गुणों को, प्रवृत्तियों को, रुचियों को, परख कर उन्हें कार्य सौपना चाहिए और उस सौंपे गये कार्य को उन्हें अपनी प्रेरणा से सूझबूझ से करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। कार्य संपन्न करने और वह भी शीघ्र सम्पन्न करने की धुन में उसका इन बातों की ओर ध्यान नहीं जाता और वह अपने हाथ के नीचे कार्य करने वालों को केवल आदेश (Dictation) देता जाता है कि “अमुक एक कार्य अमुक एक पद्धति से करो”। परिणामतः तात्कालिक कार्य सम्पन्न होता होगा परंतु इस व्यवहार का यह भी परिणाम होता है कि उसके हाथ के नीचे कार्यकर्ता “सांगकाम्या’ हो जाते हैं (सांगकाम्या यह मराठी भाषा का शब्द है) जिसका शब्दार्थ है कि बताया हुआ कार्य करने वालों परंतु उसमें यह भी अर्थ निहित है कि “अपनी बुद्धि का प्रसंग आने पर भी उपयोग न करते हुए निर्दिष्ट कार्यमात्र करने वाला, फिर उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। अतः कार्यकर्ता को अपनी सूझबूझ से कार्य संपादन करने के लिए स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।
स्वतंत्र रूप से काम का अवसर देने से लाभ होता है
वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कोई विशेषता, अपनी कोई रुचि एवं कोई प्रकृति होती है। आदेश देने की धुन में उन गुण विशेषताओं की ओर दुर्लक्ष कर उनकी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार यदि काम न दिया गया और एक ही प्रकार से कार्य करने का आदेश दिया गया तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर कार्य नहीं कर सकेगा, पारस्परिक सामंजस्य भी नही रहेगा, कार्य की भी हानि होगी, और वह निष्क्रिय हो जावेगा अथवा सांगकाम्या’ होकर उसका विकास अवरुद्ध होगा।
अतः अपनी विशेषताओं के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर अपने व्यक्तित्व को विकसित कर अपना जीवन कृतार्थ करने की ओर सबके साथ सहजरूप से समायोजन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक कार्यकर्ता को मिलना आवश्यक है। इस सत्य का विचार कर उसे कार्य सौंपना चाहिए । स्वतंत्ररूप से और अपनी प्रेरणा से कार्य करते समय, संभव है कि उसके हाथों गलती हो तथापि ठोकर खाकर वह अच्छे प्रकार से पाठ सीखेगा, अनुभव प्राप्त करेगा और उसका विकास होगा। अंतत: उसके गुणों के विकास से अपना और संगठन का भी विकास होगा। संभव है कि उसे स्वतंत्ररुप से कार्य करने के अवसर देने से थोड़ी अव्यवस्था निर्माण होगी, कार्य के संपादन मे थोड़ा विलंब होगा, परंतु बहुत नहीं। इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा नियंत्रण रखा तो कार्यसिद्धि हो सकती है और उसका विकास भी हो सकता है । सार यह कि विकास के लिए स्वतंत्रता में और व्यवस्था के लिए नियंत्रण में सामंजस्य करना यह सफल कार्यकर्ता का लक्षण हैं। उदाहरणार्थ विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए हम किसी को काशी जाने के लिए कहते हैं तो उसे कौन सी गाड़ी से अथवा बस से जाना यह स्वतंत्रता से जाने वाले को देना चाहिए। जाने से पूर्व सहज मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। साथ ही मक्का ले जाने वाली गाड़ी में वह न बैठे इतना नियंत्रण पर्याप्त है। कार्य करने के लिए स्वतंत्र अवसर न मिलने से कार्यकर्ता का विकास नहीं होता और स्वतंत्रता प्राप्त होने पर उसका विकास सुव्यवस्थित रूप से होता है। आपात्काल के पश्चात् मुझे अनेक वकील, डॉक्टर, व्यापारी और किसान मिले, जिन्होंने कहा कि हम जब अपना व्यवसाय करते थे तब हमारा लड़का व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देता था। अतः अकस्मात कारागार में जाने का प्रसंग आने पर हम बहुत चिंतित थे। परंतु मुक्त होकर आने पर हमने अनुभव किया कि उसने हमारा कारोबार बहुत अच्छे प्रकार से संभाला, इतना ही नहीं तो उसे बढ़ाया भी। अपनी अगली पीढ़ी को स्वतंत्रता नहीं दी, इसलिए उसका विकास अवरुद्ध था यह वास्तविकता है। विवश होकर जब उसे स्वतंत्रता देनी पड़ी तब उसका विकास हुआ और व्यक्तित्व निखरा यह सामने है।
ध्येय के प्रति निरपवाद समर्पण
इन सारे गुणों को जो अब तक मोटे तौर पर निर्दिष्ट किये गये हैं (और भी कई हो सकते हैं) उन्हें हम आत्मसात् कर सकें और अपने अन्य कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का विकास करने में हम सहायक हो सकें इसलिए नित्य चिंतन आवश्यक है। संस्कार करने के लिए जो प्रयोग किये गये, उनमें कौन से सफल हुए कौन से विफल हुए इसका निरीक्षण कर, आवश्यक सुधार- पूर्वाग्रह दूषित मत छोड़ कर करना, संस्कार करने के लिए, नये प्रयोग करना यह कार्यकर्ता का स्वभाव होना चाहिये, क्योंकि यहां जीव पर, चैतन्य पर संस्कार करने का कार्य करना है। निर्जीव पर संस्कार करने के लिए एक ही प्रकार के प्रयोग सफलता दे सकते हैं। परंतु यहां ‘पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना’ होने से सबके लिए एक ही प्रकार का प्रयोग सफल होगा ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए निरीक्षण एवं चिंतन कर आवश्यकतानुसार संस्कार करने के लिये नये प्रयोग करने की प्रवृत्ति के लिये ध्येय के प्रति निरपवाद समर्पण होना नितांत आवश्यकहोता है।
ध्येय के लिए निरपवाद समर्पण किये बिना पूर्व में लिखे अनुसार राग और द्वेष से रहित होकर योग्यता परखना और उसकी परख कर उसे कार्य के संपादन का दायित्व सौंपना अथवा उसके विकास में अपना विकास है यह अनुभव कर उसे कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देना सर्वथा असंभव है।
ध्येय के लिए निरपवाद समर्पण करना यह एक बहुत कठिन कार्य है। उसमें अनेक बाधाएँ आती हैं।
व्यक्ति के अपने कुछ गुण, कुछ विशेषताएँ होती हैं। उदाहरणार्थ, कोई अच्छा वक्ता, कोई लेखक, कोई अच्छा खिलाड़ी अथवा वैज्ञानिक कोई प्रसंग का अवधान रखकर दूसरों के आक्षेपों का तर्क द्वारा खण्डन करता है। ये गुण और उनका भान व्यक्ति के निरपवाद समर्पण में बाधक होते हैं।
इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अपने कुछ दोष होते हैं जो लोक संग्रह करने में अथवा ध्येय प्राप्ति में बाधक होते हैं। उनका ज्ञान होने पर भी उन दोषों को दूर कर अपने में सुधार करने का व्यक्ति प्रयास नहीं करता अपितु यथास्थिति प्रिय होता है। ये दोष और उनका ज्ञान होने पर भी यथास्थितिप्रियता निरपवाद समर्पण में बाधक होती है।
व्यक्ति के अपने पूर्वाग्रह दूषित कुछ मत होते हैं। वह सोचता है कि मैं स्वतंत्ररूप से विचार करता हूँ इसलिए उनके संबंध में उसका अपना एक अभिनिवेष भी होता है। वास्तव में मैं स्वतंत्ररूप से विचार करता हूँ, यह अनुभव भी एक बड़ा भ्रम है। वह जिस देश और समाज में जन्मा उनके विचार, जिस कुल और परंपरा में जन्मा उसके विचार, जिस समय जन्मा, पला और बढ़ा, उस समय की समस्याओं को सुलझाने के लिए कभी एक व्यक्ति ने और कभी दूसरे व्यक्ति ने आंशिक रूप से व्यक्त किये विचार, उसने जो साहित्य पढ़ा उसमें व्यक्त किये विचार, उसके चारों ओर विचरण करने वाले लोगों के विचार एवं उसने पूर्वजन्म में किये कर्म के परिणामस्वरुप उसका जो आज स्वभाव है, प्रकृति है, उसके आधार पर बने उसके विचार लेकर उसका मत बनता है। इन सब बातों से वह प्रभावित होता है। फिर उसे स्वतंत्ररूप से विचार करने के लिए कहां अवसर होगा? हां उसके लिए केवल एक व्यक्ति अपवाद हो सकता है, जो विचार एवं आचार में पूर्णरूप से स्वतंत्र है। जो शुद्ध हैं, बुद्ध है, मुक्त है,
सच्चिदानन्द स्वरुप में स्थित है । समस्त चराचर विश्व से अदृश्य, अचिन्त्य शक्ति से परमात्मा से एकात्मकता पाता है वह अवश्य ही स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है। सामान्य व्यक्ति तो ऊपर लिखे कारणों से पूर्वाग्रह दूषित मत बनाता है और उसके संबंध में अपना अभिनिवेष रखता है। परिणामतः सामूहिक मन से समायोजन करने में वह असमर्थ होता है। इसी कारण कभी वह निष्क्रिय हो जाता है तो कभी विरोध भी करता है। अतः उसकी यह मनोवृत्ति निरपवाद समर्पण में बाधक होती है।
फिर व्यक्ति की कुछ सूक्ष्म अभिलाषाएं होती है, जिनका अनेक बार उसे भान भी नहीं होता। उनकी पूर्ति के लिए सैद्धान्तिक आवरण में तर्कशुद्ध समर्थन करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। अतः ये अभिलाषाएं तथा सैद्धांतिक आवरण में उसका समर्थन करने की उसकी प्रवृत्ति निरपवाद समर्पण में बाधक होती है।
पुनः व्यक्ति का अपना अहंकार होता है। उसके द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है उसके कर्तृत्व का उसे अभिमान होता है, जो कार्य संपादन में सफलता मिलने पर उन्माद में परिणत होता है। यह अहंकार एवं उन्माद निरपवाद समर्पण में बाधक होते हैं।
वास्तव में ऊपर लिखे समस्त प्रकार के दोष, अहंकारजनित ही होते हैं।
गहराई में जाकर विचार किया जाय तो यह समझ में आवेगा कि यह अहंकार भी अज्ञानमूलक होता है। उदाहरणार्थ कल्पना कीजिए कि कोई अच्छा वक्ता है। असंख्य लोग उसका भाषण सुनते हैं। भाषण में ताली बजाते हैं तो क्या इस सारे कार्यक्रम को सफल करने का सारा श्रेय उस वक्ता को है, जो समय निकाल कर आया या उन्हें भी जिन्होंने कार्यक्रम होगा यह प्रकाशित किया। उन लोगों को भी है जिन्होंने संगठित होकर लोगों को एकत्रित किया । पुनः लाउड स्पीकर का प्रबंध ठीक नहीं होता तो लोग कैसे भाषण सुन सकते थे ? अतः उस प्रबंधक को भी है और लाउडस्पीकर की विद्युत पूर्ति करने वाले विद्युत मंडल के समस्त कर्मचारियों अथवा बैटरी निर्माण करने वाले कारखानेदार के श्रेय का अनुल्लेख कृतघ्नता का परिचायक होगा। इन सब सहायकों के अभाव में किसी निर्जन स्थान पर अथवा निर्जन हाल में यदि उस वक्ता का भाषण होता तो कौन से वृक्ष, पत्थर, अथवा हाल के खंभे भाषण सुनते ? और अंत में उस बोलने वाले को शक्ति अथवा प्रेरणा देने वाले उस अदृश्य, अचिंत्य नियामक शक्ति के बिना कार्यक्रम सफल होना सर्वथा असंभव था ।
सार यह है कि अहंकार अज्ञानमूलक है। वह व्यक्ति एवं समाज में व्यवच्छेदक है, अलगाव निर्माण करता है। इसलिए आत्मिक उन्नति में बाधक है। अहंभाव याने ‘अहमिति भावः’। मैं दूसरों से भिन्न हूँ यह भाव। इसलिये अपनी अहंता को समाज तक, राष्ट्र तक, अनंत तक व्यापक करने का ध्येय सम्मुख रखना चाहिये। वह करने के लिये नित्य आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक होता है। अपने द्वारा किये गये परोपकारक सत्कर्म भी कितनी मात्रा में अहंकार को जन्म देने वाले हैं। इसकी छान बीन करना यह आत्मनिरीक्षण की कठोर कसौटी है। इस अहंभाव को दूर करने से व्यापक व्यक्तित्व की अनुभूति होती है। वह व्यक्तित्व सर्व समावेशक है। परन्तु अहंकार रहित व्यक्ति का भी अस्तित्व होता है उसे हम अस्मिता कह सकते हैं। व्यवहारिक भाषा में आस्मिता शब्द का भी वही अर्थ
है।
परन्तु दार्शनिक भाषा में जो अस्मिता है वह सबसे व्यवच्छेदक नहीं अपितु सबसे निरन्तर एकात्मता अनुभव कराती है। एकात्मता पर आधारित परस्पर
पूरकता का अनुभव कराती है। लोक संग्रह कर उस स्थिति को ध्येय पूर्ति के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। एकात्मता पर आधारित परस्पर पूरकता यह दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति का रहस्य है। भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि-
‘परस्परं भावयंतः,
श्रेयः परमवाप्स्यथ। ‘
मुक्तसङ्गोऽ नहंवादी, धृत्युत्साह समन्वितः ।
सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोशुचिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥
क्रियान्विति
अब तक हमने लोकसंग्रह करने के शास्त्र का विचार किया। लोगों को विशेषरूप से स्वयंसेवकों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए उनमें ध्येयनिष्ठा निर्माण करने के लिए, इनका कर्तृत्व विकसित करने के लिए और पारस्परिक सहयोग से कार्य करने के लिए इस शास्त्र पर आधारित कौन से व्यवहार हो सकते हैं, अब हम इसका विचार करेंगे।
संस्कार करने के लिए सामान्यरूप से चार साधन होते हैं। (१) श्रवण (२) दर्शन (३) पठन और (४) सामूहिक एवं व्यक्तिगत संगमन अथवा समागम । पांचवा भी एक अतिमहत्वपूर्ण साधन है वह है किये गये प्रयास के संबंध में चिंतन |
श्रवण करने का पुरातन साधन है उपदेश करना। महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करना। आज के युग में इसके अतिरिक्त रेडियो एवं टेपरेकॉर्ड सुनना यह भी एक साधन उपलब्ध है।
दर्शन कराने के लिए पुरातन समय में प्रत्यक्ष दृश्य दिखाने का अथवा नाटक का प्रयोग किया जाता था। आज चित्रपट और दूरदर्शन का आविष्कार होने से वे साधन भी अपनाये जाते हैं।
तीसरा साधन है पठन। पुराणों का अच्छे साहित्य का, महापुरुषों की जीवनियों का, उनके विचार एवं भाषणों का पठन करना यह भी पुरातन समय से उपलब्ध है।
इन तीनों साधनों से अपने विचारों से सहमति निर्माण की जा सकती है। आज के जनतंत्र के युग में इसका भी अपना महत्व है । परन्तु दुष्कर्मों से निवृत्ति एवं सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति इनके माध्यम से होती ही है ऐसा अनुभव नहीं है । संभव है कि ‘पिण्डे – पिण्डे मतिर्भिन्ना’ के न्याय से किन्हीं लोगों में इन माध्यमों से तदर्थ प्रेरणा जागृत हो जाय । परन्तु वे अपवाद स्वरुप होते हैं और पारस्परिक सहयोग से कर्म करने की प्रेरणा इन माध्यमों से जिन्हें प्राप्त हुई, उनकी संख्या नगण्य ही है।
इस दृष्टि से प्रेरणा देने वाला प्रभावी साधन है संगमन अथवा समागम अथवा संगति, और वह भी उन लोगों की संगति जो तत्व के जानकार हैं और जिन्होंने ध्येयनिष्ठा अपने जीवन में उतारी है।
यह अपना नित्य का अनुभव है। नाटक चित्रपट अथवा दूरदर्शन देखने से अथवा आम चौराहे पर हुए भाषणों को सुनने से इनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, परन्तु इनकी अपेक्षा बौद्धिक वर्ग का भाषण संस्कार करने का प्रभावी साधन है। बौद्धिक वर्गों द्वारा प्राप्त संस्कारों की तुलना में बैठकों में और अधिक संस्कारक्षम वातावरण होता है। बौद्धिक वर्गों में वक्ता जो मार्गदर्शन करना चाहता है, वही बोलता है। श्रोता के मन में विद्यमान सारी समस्याओं का निराकरण इससे होता ही है, ऐसा हम नहीं मान सकते। परन्तु बैठकों में जो चर्चा होती है, स्वयंसेवक जो प्रश्न पूछते हैं उनके कारण बैठक का संचालन करने वाला यह समझ सकता है कि श्रोता की जिज्ञासा क्या है ? फलतः इसका उत्तर देकर उसका वह समाधान कर सकता है। तथापि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अतिफलदायक अनौपचारिक (informal) बैठकें और व्यक्तिगत संपर्क और समागम होता है।
पांचवा भी एक साधन है जो अतिमहत्वपूर्ण है। वह है चिंतन । भिन्न-भिन्न लोगों पर संस्कार करने के लिए यंत्र जैसा एक ही प्रकार का व्यवहार सब पर संस्कार करने के लिए सक्षम नहीं होता। अतः संस्कार करने के लिए अपने द्वारा किये गये प्रयासों का अनुकूल अथवा प्रतिकूल क्या परिणाम हुआ यह निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार नये प्रयोग करने के लिए चिंतन करना और सफलता के अभाव में अंगीकृत पद्धति में परिवर्तन कर, संशोधन कर नये प्रयोग अपना कर प्रयास करना यह इस साधन से ही संभव होगा।
प. पू. डॉक्टर साहब के जीवन काल में कार्य की व्याप्ति कम थी। इसलिए अनौपचारिक बैठकों के लिए बहुत समय देना उन्हें संभव होता था। मेरे जैसा कॉलेज में पढ़नेवाला सामान्य व्यक्ति भी उनकी बैठक में जाकर बहुत समय तक बैठ सकता था । उन बैठकों में स्वयंसेवकों के मन में क्या विचार है ? कौनसी समस्या है ? राष्ट्र के उत्थान के बारे में उनकी क्या संकल्पना है ? वह ठीक है अथवा नहीं? राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका क्या दृष्टिकोण है ? उनके दृष्टकोण में कोई गलती है क्या ? यह सब गपशप करते हुए हास्य विनोद करते हुए आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से स्वयंसेवकों को वे समझाते थे। उनकी गहराई वे नापते थे। आज के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी अपना युवावस्था में कार्य की व्याप्ति कम होने के कारण अनौपचारिक पद्धति से संस्कार करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाते थे ।
परन्तु समय के साथ हमारी ज्येष्ठता (Seniority) और अब वृद्धावस्था एवं परिणामतः अस्वास्थ्य भी बढ़ता गया । कार्य भी बढ़ता गया। हम लोगों के कार्यक्षेत्र भी धीरे-धीरे विस्तृत होते गये। संघ का परिवार भी बढ़ा। अब बहुत व्यापक हुआ है। प्रवास में आज यहां और कल वहां इस प्रकार करने के लिए हम विवश हुए हैं। परिणामतः हमारे कार्यक्रम, हमारी बैठकें औपचारिक बैठकों के लिए विशेष रूप से नवनिर्मितों से मिलने जुलने के लिए, हास्य विनोद करते हुए तत्व समझाने के लिए हमारे पास समय नहीं । उदा. हम जहां जाते हैं वहां बौद्धिक वर्ग में भाषण होते हैं। बैठक में हम प्रश्न पूछते हैं और कनिष्ठ कार्यकर्ता अथवा सामान्य स्वयंसेवक उसका उत्तर देता है। तथापि उसका उत्तर यदि अलग प्रकार का हो तो क्यों अलग है? उसके मन में कौन से विचार हैं, ये वास्तविकताएं जो अनौपचारिक व्यवहार में परखी जाती हैं, ज्ञात होती है, वे आज हमें ज्ञात नहीं होती। अथवा ज्ञात होती हो तो आंशिकरुप में ज्ञात होती हैं। इस स्थिति में उसे निःशंक कर संपूर्ण शक्ति से कर्म करने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकेंगे? और फिर बैठक में उसके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का तर्कनिष्ठ उत्तर देकर हम अपने कार्य की इतिश्री मान लेते हैं। अनौपचारिकरुप से मिलते-जुलते उसकी मनोभूमिका समझ कर जो आत्मीयता पर आधारित उसके अंतःकरण को स्पर्श करने वाली बात होनी चाहिये उसे इन बैठकों में करने में समय के अभाव में हम असमर्थ होते हैं। बुद्धि से हम भले ही उसे समझाते हों पर अंतःकरण से समझाने के लिए जो समय चाहिये वह हमारे पास नहीं। मनुष्य की विशेषतः, कनिष्ठ कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति अनुकरणशील होने के कारण, अपने कनिष्ठ कार्यकर्ताओं की, औपचारिक बैठकों का मात्र आयोजन करने की प्रवृत्ति बनती है। संस्कृत में एक सुभाषित है कि ‘गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः ।’ उनकी यह समझ में नहीं आता कि अपने वरिष्ठ अधिकारी समय के अभाव के कारण या उनकी अस्वस्थता के कारण, अब औपचारिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और हम अपना कार्यक्रम मर्यादित होने के कारण, परिणामतः अपने पास अधिक समय होने के कारण तथा आयु कम होने से एवं अपना स्वास्थ्य ठीक होने के कारण हमें केवल औपचारिक कार्यक्रम ही नहीं, अपितु अनौपचारिक व्यवहार करना चाहिये। वास्तव में संस्कार करने का वही अधिकतम प्रभावी साधन है। एक बार औपचारिक कार्यक्रम हमने संपन्न नहीं किये तो चलेगा, परन्तु अनौपचारिक पद्धति से मिलने जुलने की ओर दुर्लक्ष नहीं करना चाहिये ।
यही व्यवहार धीरे-धीरे शाखाओं का संचालन करने वाले कार्यवाह एवं मुख्य शिक्षक तक पहुंचता है और उनका सारा व्यवहार औपचारिक एवं यंत्रवत् हो जाता है। बहुतांश शाखाधिकारियों की यह स्थिति है । याने शाखा का संचालन, जो वास्तव में चिंतनीय कर्म है, वह अपने पुरातन वाक्य प्रयोग के अनुसार ‘कर्मकांड’ हो जाता है। (आगे जाकर अकर्मण्यता के रोग की चिकित्सा के बारे में लिखते समय इस व्यवहार को स्पष्ट किया जावेगा) उसकी समझ में नही आता कि अनौपचारिक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार एवं संगति, संस्कार करने का अधिकतम प्रभावी साधन है और वह यह अनुमान करने में असमर्थ होता है कि उसका निर्माण अपने वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी युवावस्था में अपने अनौपचारिक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से ही किया है, जब कि आज उपरिनिर्दिष्ट कारणों से उनके लिए वह संभव नहीं ।
प्रवास में अनेक स्थानों पर मैंने यह अनुभव किया है कि कहीं कोई कार्यवाह अथवा मुख्य शिक्षक मिलता है जिसकी शाखा की उपस्थिति अच्छी, कार्यक्रम अच्छे और आकर्षक होते हैं और सामान्यरूप से अन्य सब कार्यवाही एवं मुख्यशिक्षकों की शाखाओं की उपस्थिति कम और कार्यक्रम यथातथा होते हैं। पहली श्रेणी के कार्यकर्ता जब सड़क से गुजरते हैं, तब उनकी शाखा के स्वंयसेवक उन्हें देखकर उनसे मिलने घर से बाहर आते हैं। दूसरी श्रेणी के कार्यकर्ता को सामने से आते देखकर उसकी शाखा के स्वयंसेवक रास्ता बदल कर, अन्य मार्ग से जाते हैं। उनसे मिलना टालते हैं। यह सत्य इन कार्यकर्ताओं ने बैठकों में प्रश्न पूछने पर मान्य किया है।
स्वयंसेवकों की इस भिन्न मनःस्थिति का यदि विश्लेषण कर चिंतन किया तो समझ में आवेगा कि पहली श्रेणी का कार्यकर्ता अपनी प्रेरणा से सूझबूझ काम करता है। स्वयंसेवकों को कौनसी बातें कौनसे विषय रोचक लगते हैं इसका निरीक्षण करता है। अपने प्रयासों का उन पर क्या परिणाम हुआ इसका वह निरीक्षण करता है और अपनी कल्पकता से वह काम करता है, जब कि दूसरी श्रेणी का कार्यकर्ता यंत्र जैसा काम करता है। (मराठी भाषा में ‘सांगकाम्या’ यह उसके लिए बहुत अन्यर्थक शब्द हैं) । यंत्र चलाया तो वह चलता है। चैतन्य के अधिष्ठान के अभाव में वह तमोगुण से व्याप्त होता है। अपने चलने से इष्टफल प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं इसका निरीक्षण वह नहीं कर सकता। फिर वह क्यों नहीं होती इसका चिंतन वह कैसे कर सकेगा? बस; यही स्थिति इस दूसरी श्रेणी के कार्यकर्ता की होती है। इन्हें यदि मार्गदर्शन किया कि ‘अनुपस्थित स्वयंसेवकों से मिला करो, उनसे बात करो, पूछो, तो संभव है वे आवेंगे।’ तो फिर वह उनसे अवश्य पूछेगा कि शाखा में तुम क्यों नहीं आये? उनके न आने पर वह फिर बार-बार पूछने का उनसे मिलने का काम करेगा। यह धैर्य अच्छा है। परन्तु अतिशय आग्रह करने का परिणाम यह होता है कि वह स्वयंसेवक इस कार्यकर्ता से अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहता है कि ‘आऊंगा’ और फिर न आता है, न मिलना चाहता है, क्योंकि इसे भय होता है कि भेंट होने पर फिर पूछा जावेगा ‘तुम शाखा में क्यों नहीं आये?’ और उसने यदि शाखा में आने की ‘गलती’ की तो यह ‘सांगकाम्या’ कार्यकर्ता उसे दूसरा प्रश्न पूछता है कि ‘तुम आये तब तुम अपने पड़ोस में रहने वाले दूसरे स्वयंसेवक को क्यों नहीं लाये ?’ इस प्रश्न का परिणाम उसके मन पर यह होता है कि ‘लो! मैं मनसे कितना संघर्ष कर आया हूं यह मैं जानता हूं और यह मुख्यशिक्षक अब मुझे दूसरा कठिन कार्य सौंपता है कि दूसरे पड़ोसी को भी लाया करो’ यथार्थ में मैंने शाखा में आने की गलती की है, मन की इस उद्वेलित अवस्था में वह भेंट करना टालता है। अब यंत्रवत् कार्य करने वाला यह ‘सांगकाम्या’ कार्यकर्ता यह निरीक्षण नहीं करता अथवा करने में असमर्थ होता है कि अनियमित स्वयंसेवकों को शाखा में उपस्थित करने का उसने जो प्रयास किया अथवा इसके आने पर, ‘दूसरे पड़ोस के स्वयंसेवक को क्यों नहीं लाया’ यह जो प्रश्न पूछा, उसका ही यह दुष्परिणाम है कि वह उससे मिलना टालता है। और जब वह मिलना नहीं चाहता तब मैं उस पर कैसे संस्कार करूँगा? यह स्पष्ट है कि ‘संघ में क्यों नहीं आया, अवश्य आओ, यह बार-बार उपयोग में लाई गयी भाषा उस स्वयंसेवक की समझ में नही आती, अथवा उसे ये प्रश्न अरोचक लगते हैं, पूछने वाले के प्रति उसके मन में उद्वेग उत्पन्न करते हैं।’ अतः कार्यकर्ता को बार-बार उसे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिये । शाखा में आने की बात कभी-कभी करनी चाहिये। उसे कौन से विषय की रुचि है इसका निरीक्षण कर इस विषय के संबंध में उससे बात करनी चाहिये यह वास्तव में उस मुख्य शिक्षक की समझ में नहीं आता ।
यंत्र जैसी कार्य करने की यह प्रवृत्ति उसकी प्रत्येक क्रिया में होती है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने चाहा कि नये एवं पुराने सब स्वयंसेवकों को अपने कार्य का स्मरण रहे, सब के एकत्रीकरण से आत्मविश्वास बढ़े और अपने कार्यकर्ताओं का सब स्वयंसेवकों से नित्य संपर्क रहे इस दृष्टि से दिशा बोध करने के लिए सोच विचार कर उपस्थिति दिवस संपन्न करने का आयोजन किया जाये और तदनुसार सर्वत्र सूचनाएं भेजी जाये तो यह सांगकाम्या कार्यकर्ता उस उपस्थिति दिन के पूर्व एड़ी-चोटी का पसीना एक कर उसे सफल बनाने का भरसक प्रयास करेगा-(यद्यपि यह भी करना आवश्यक है) परन्तु एक बार वह कार्यक्रम संपन्न हो गया कि बाद में पुराने स्वयंसेवकों से मिलना, बात करना बंद कर देगा। उपस्थिति दिन संपन्न करने का यह आयोजन वास्तव में दिशाबोध करने के लिए है, इसका उसे विस्मरण हो जाता है और एक कर्मकांड के रुप में वह उसे संपन्न कर लेता है। यंत्र-निरीक्षण नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता यह स्वाभाविक है। वह निर्जीव है। परन्तु यह कार्यकर्ता सजीव है, चैतन्ययुक्त है। उससे निरीक्षण, चिंतन एवं आवश्यकतानुसार प्रयास के प्रयोग में परिवर्तन करना अपेक्षित है। परन्तु वह विचार नही करता । विचार करने के लिए उसमें क्षमता नहीं, प्रेरणा नहीं, यह मुझे अमान्य है, क्योंकि अपने व्यक्तिगत जीवन में अध्ययन अथवा व्यवसाय करते समय निरीक्षण कर गतिरोध दूर करने के लिए अपनी प्रेरणा एवं कल्पकता से वह प्रयास करता है। परन्तु संघ का कार्य करते समय वह यंत्रवत् कार्य करता है।
यह समझ में तब ही आवेगा जब वह अपने प्रयासों के परिणाम क्या हुए इसका निरीक्षण करेगा, चिंतन करेगा, स्वयंसेवक की प्रवृत्ति को और रुचि को समझ लेने का प्रयास करेगा। उनकी प्रवृत्ति एवं रुचि को शाखा के समय के अतिरिक्त उनके साथ शाखा में खेलना चाहिये। शाखा के समय के अतिरिक्त उनके साथ मिलना और गपशप करना होगी। इस व्यवहार का परिणाम यह होगा कि शाखा में मुख्य शिक्षक एवं स्वयंसेवकों में जो थोड़ा औपचारिक संबंध-थोड़ी दूरी (respectable distance) होती है, और शाखा में अनुशासन के संस्कार करने के लिए जो आवश्यक ही है, वह दूर होगी। दोनों हिल मिल कर निःसंकोच रूप से व्यवहार करेंगे।
औपचारिक संबंधों में स्वयंसेवक जरा सावधानी से व्यवहार करता है। सोचता है कि अपने गुणों का वरिष्ठों को परिचय होना चाहिये, परन्तु साथ ही यह भी सावधानी से प्रयास करता है कि अपने दोषों का कमजोरियों का – उन्हें पता न लगे, ऐसा व्यवहार करना चाहिये। परिणामतः इसके वरिष्ठ अधिकारी को इसके गुण दोषों का सम्यक ज्ञान नहीं होता, फिर वे उसका विकास कैसे कर सकेंगे? परन्तु हिलमिल कर नि:संकोच व्यवहार हुआ – जैसा कि स्वाभिवक रूप से खेलों में होता ही है, तो मन की असावधानता के क्षणों (unguarded moments) में इसके गुण एवं दोष भी प्रकट होंगे। विचार एवं आचार का इसका स्तर ज्ञात होगा। परिणामतः उसमें ध्येयनिष्ठा कैसे जागृत करना और ध्येयनिष्ठा के अनुकूल उसके गुणों का कैसे विकास करना और उसके दोषों को कैसे दूर करना इसका आत्मीयता के उस आधार पर विचार करना संभव होगा। संस्कार आत्मीयता के आधार पर ही किये जा सकते हैं। यदि आत्मीयता रही तो उसके दोषों को अथवा मतभेदों को सहन करते हुए इसका विकास करेगा ही, इसमें और मुझमें जो हिन्दुत्वजनित एकात्मता की भावना है, उसका उपयोग संस्कार करने के लिए होगा ही यह विचार एवं व्यवहार करने का दृष्टिकोण रहेगा। इतना ही नहीं तो इस स्वयंसेवक के विकास में मेरा विकास है यह अनुभूति रहेगी और गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा।
एक कमरे में बैठे अंधे व्यक्ति को बाहर जाते समय यदि दीवार सामने आने से गतिरोध उत्पन्न हुआ तो बायीं अथवा दायीं ओर अपने डंडे से टटोल कर बाहर जाने का मार्ग ढूंढ कर उसे तय करता है। पूज्यपाद श्री विवेकानंद जी ने जीवन की व्याख्या की है कि Life is a development and unfoldment of a being under Circumstances trying to press it down? अर्थात् ‘चारों ओर से बाधक होने वाली परिस्थिति के बावजूद जिसका विकास एवं उन्मीलन होता है वह जीवन है।’ ठीक इसी व्याख्या के अनुरूप पहली श्रेणी का मुख्य शिक्षक गतिरोध आने पर अपनी कल्पकता का उपयोग करता है।
भोपाल में गणेशोत्सव में शाखा उपस्थिति कम हो जाती है। यह अनुभव कर एक चिंतनशील मुख्य शिक्षक ने दूसरे वर्ष अपनी शाखा के लिए गणेशोत्सव का आयोजन किया। शुल्क एकत्रित कर एक स्वयंसेवक के घर में गणेश आयोजन किया। पूजा आरती के समय सबका एकत्रित होना अनिवार्य किया गया। शाम की आरती शाखा के बाद होती थी। शाखा में आने वाले बाल किशोर स्वयंसेवकों ने उत्सव में सोत्साह भाग लिया। कार्यक्रमों गणगीत एवं व्यक्तिगत गीत, सूर्य नमस्कार, कबड्डी की स्पर्धा, महापुरूषों की जीवनी के विषय में भाषण, बौद्धिक वर्ग इन सब कार्यक्रमों का उस मुख्य शिक्षक ने आयोजन किया। उसका परिणाम यह हुआ कि शाखा में न आने वाले बाल किशोरों ने भी इसमें भाग लिया और संबंध बढ़ने से बाद में वे भी शाखा में नियमित आने लगे। शाखा की उपस्थिति कम होने के बदले बढ़ी। परन्तु अन्य मुख्य शिक्षकों ने यह कल्पकता नहीं अपनायी । अतः इनकी शाखा की उपस्थिति गणेशोत्सव के कारण घटी।
इस प्रकार हिलमिल कर निःसंकोचवश से स्वयंसेवकों के साथ व्यवहार करने पर आत्मीयता बढ़ेगी, स्वयंसेवकों की रुचि अरुचि की जानकारी मिलेगी और यह समझ में आवेगा कि प्रत्येक की रुचि भिन्न हो सकती है। इस रुचि के आधार पर उसके व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास करना चाहिये। सामान्यरूप से बाल, किशोर, एवं तरुण स्वयंसेवकों की यह इच्छा होती है कि अपनी शारीरिक शक्ति बढ़े। परन्तु इच्छा होने पर भी व्यायाम करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी इस प्रवृत्ति को, एवं शारीरिक शक्ति के होने से सहज रूप से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, इस सत्य को स्मरण रखकर, व्यायाम करने के लिए इन्हें मुख्यशिक्षक द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिये। शाखा में सूर्य नमस्कार आदि शारीरिक प्रयोग, अनुशासन एवं सहज रूप से सबके साथ सहयोग करने के संस्कार की दृष्टि से सामूहिक रूप से करवाये जाते हैं। वे पर्याप्त हैं। परन्तु शारीरिक शक्ति का विकास करने के लिए उतना व्यायाम अपर्याप्त होता है। शाखा में जबरन अधिक व्यायाम करवाया तो व्यायाम करने के लिए आंतरिकप्रेरणा जागृत नहीं हो सकती। उसका मनपर स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ेगा शायद विपरीत परिणाम भी हो सकता है। Compulsion always breed revulsion स्पष्ट है कि अंत: प्रेरणा जागृत करने के लिए व्यायाम करने का शौक निर्माण करना चाहिये। परन्तु उनमें शौक तब ही उत्पन्न होगा जब उनके कार्यवाह, मुख्य शिक्षक को व्यायाम करने का शौक होगा और वे प्रभात में अथवा सायं शाखा की समाप्ति के पश्चात् संघ स्थान पर दंड, बैठकें, नमस्कार, दौड़ लगाना, मुद्गल घुमाना आदि व्यायाम करेंगे। और उससे प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन, हंसते खेलते अर्थात् उपदेश करने की भूमिका से नहीं अपितु सहजरूप से अपने स्वयंसेवकों के सामने करेंगे। व्यायाम में रुचि बढ़ाने के लिए शाखा समाप्ति के पश्चात् नमस्कार अथवा प्रहार लगाने की स्पर्धा का कार्यक्रम भी अपनाया जा सकता है। परन्तु ये कार्यक्रम अनिवार्य रुप से नहीं, ऐच्छिक होने चाहिये। परिणामतः शाखा समाप्ति के पश्चात् अनेक स्वयंसेवक व्यायाम करना प्रारंभ करेंगे। यदि चार छः स्वयंसेवक भी इस प्रकार देखा देखी प्रत्येक उपशाखा में व्यायाम करने लगे तो वह भी कोई साधारण उपलब्धि नहीं। अपने वरिष्ठों का अनुकरण करना यह विशेष कर बाल किशोरों का स्वभाव होता है। इसी कारण से उन्हें व्यायाम करने का शौक उत्पन्न होगा, उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और शाखा के औपचारिक कार्यक्रमों के पश्चात् भी स्वयंसेवकों के साथ अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का व्यवहार करने का उनके अधिकारियों को अवसर प्राप्त होगा। अनौपचारिक समागम अधिकतम प्रभावी साधन होता है। इसके अतिरिक्त जब स्वयंसेवक कमरे में (Indoor) अथवा मैदान के (out door) खेल छुट्टी के समय खेलेंगे, जब मुख्य शिक्षक के और अन्य गणशिक्षकों को स्वयंसेवकों के साथ खेलना चाहिये।
वर्षा ऋतु में अनुकूल हवा होने पर एवं सर्दी के प्रत्येक महिने में शाखा के स्वयंसेवकों का वनविहार का कार्यक्रम तय करना चाहिये। कभी अलग-अलग शाखाओं का और कभी दो शाखाएं मिलाकर कार्यक्रम होना चाहिये। इस कार्यक्रम से साहस की वृत्ति बढ़ाती है । पुन: उतने अधिक समय तक उनकी संगत में मुख्य शिक्षक एवं कार्यवाह रह सकेंगे। शाखा की दैनिक उपस्थिति से अधिक उपस्थिति वन विहार के कार्यक्रम में होती है। और यह अनुभव सिद्ध बात है
कि इस वनविहार के परिणामस्वरूप दैनिक उपस्थिति में भी वृद्धि होती है। जहां सुविधा हो वहां अपने स्वयंसेवकों को तैरना सिखाना, मलखंब सिखाना, ऐसे कार्यक्रम आत्मीयता बढ़ाने के साधन होते हैं। बौद्धिक वर्गों की अपेक्षा बाल एवं किशोरों में उत्साह बढ़ाने में ये कार्यक्रम अधिक सहायक होते हैं। उनके लिए बौद्धिक विषय भी विवेचनात्मक नहीं वर्णनात्मक रखे जाये। विशेषरूप से महापुरुषों के जीवन चरित्र से संबंधित हो तो अधिक हितावह हो सकते हैं।
ऊपर यद्यपि यह विचार व्यक्त किया गया है कि बाल, किशोर एवं तरुण स्वयंसेवकों में यह इच्छा होती है कि अपनी शारीरिक शक्ति बढ़े, फिर भी कुछ ऐसे स्वयंसेवक होते हैं जिनकी शारीरिक शक्ति बढ़ाने में कोई रुचि नहीं होती। व्यायम करने पर ऐसे कुछ व्यक्ति बीमार भी हो जाते हैं। इस वर्ग के छात्र प्रायः बुद्धिमान होते हैं। पढ़ने की ओर उनकी रुचि होती है। अतः अधिकारियों ने उन्हें उतना ही व्यायाम करने के लिए कहना चाहिये जितना शाखा में अनुशासन तौर पर किया जाता है। शेष समय में प्रथम श्रेणी में और प्रथम क्रमांक पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की आकांक्षा जागृत कर अध्ययन करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये। किसी विषय में वे यदि कमजोर हो तो प्रबंध करना चाहिये। उन स्वयंसेवकों को महापुरुषों की जीवनियों एवं अन्य विवेचनात्मक ग्रंथ पढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना उचित होगा। फिर अपनी अपनी शाखा में उस विषय पर बोलने के लिए उन्हें कहा जाये। परिणामतः अन्य स्वयंसेवकों को बोलने का अभ्यास करवाने की दृष्टि से छुट्टी के दिन दोपहर वाद विवाद के कार्यक्रम आयोजित करना उचित होगा। जिनकी लेखन की और कविता रचने की ओर प्रवृत्ति है, उन्हें उन विषयों ने प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए कहना चाहिये ।
कुछ ऐसे स्वयंसेवक होते हैं जिनकी न शारीरिक और न बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति होती है। उनमें से जिनकी आवाज अच्छी हो उनको गीत का अभ्यास करा सकते हैं। जिनका झुकाव कलाओं की ओर होगा, उन्हें महापुरुषों के चित्र निकालने के लिए अथवा अच्छे बोध वाक्य पटल पर लिखने के लिए प्रवृत्त करना चाहिये। उनकी इन प्रवृत्तियों के स्वस्थ विकास के लिए यदि हमने प्रत्यत्न नहीं किया तो वे सिने संगीत गायेंगे अथवा सिनेमा की नटनटनियों के चित्र निकालेंगे। सार यह कि व्यक्ति की अन्तर्निहित विशेषताओं को नष्ट न होने देते हुए उनका विकास करना यह अपने धर्म की विशेषता है। उसी को मार्गदर्शन तत्व मानकर स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए निरपेक्ष रूप से सहायक होने वाले ध्येयनिष्ठ कार्यवाह अथवा मुख्य शिक्षक का स्मरण भी स्वयंसेवकों को मन की विचलित अवस्था में कर्त्तव्य निर्वाह करने की प्रेरणा देगा और शिथिलता को नष्ट करेगा।
नगरों में संचालित शाखाओं में और दूसरे नगर की शाखाओं में भी कबड्डी आदि खेलों की स्पर्धा का आयोजन उत्साह एवं उपस्थिति बढ़ाने के लिए सहायक होगा। शाखाओं में विस्तीर्णता के अनुसार विदेशी खेलों के कार्यक्रम अपनाना भी आकर्षक हो सकता है। छात्रों को यथासंभव सायं शाखाओं में आने का आग्रह भी शाखा में उपस्थिति एवं परिणामतः उत्साह बढ़ाने के लिए सहायक होगा। उत्साह बढ़ा तो संस्कारक्षम वायुमंडल भी निर्माण होगा। जिन छात्रों को सायं शाखाओं में आना संभव न हो उन्हें प्रभात शाखा में आने के लिए आग्रह किया जाये ।
चुने हुए होनहार स्वयंसेवकों का शाखा के अधिकारियों के साथ एक साप्ताहिक वर्ग होना आवश्यक है। यह वर्ग आवश्यकतानुसार दो तीन उपशाखाओं के लिए एक ही स्थान पर होना चाहिये। इस कार्यक्रम से उनकी शारीरिक चुस्ती बढ़ेगी और उनका समुचित विकास होकर शाखा संचालन के योग्य उन्हें ढाला जा सकेगा।
प्रत्येक तहसील केन्द्र में अथवा तहसील के अंतर्गत बड़े कस्बों में कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करने के लिए तथा उनका गुणात्मक विकास करने
के लिए अपने प्रयासों को केन्द्रित करना यह आज की प्राथमिक आवश्यकता है। एतदर्थ अपने तरुण विभाग प्रचारकों को ऊपर लिखे अथवा ऐसी ही कोई • और सुझावों के अनुसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का दायित्व देना चाहिये । उनके विभाग में चलने वाले अन्य कार्यों की ओर वे ध्यान दें यह अपेक्षा होती है, परन्तु मैं समझता हूं कि अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने का दायित्व वयस्क विभाग प्रचारकों को ही सौंपना उचित होगा और तरुण विभाग विचारक, जिला, तहसील एवं नगर प्रचारकों को इस गुणात्मक विकास के लिए लक्ष्य केन्द्रित करना उचित होगा।
आज यह अनुभव आता है कि नये विस्तारक अथवा प्रचारकों की संघ आयु भी अत्यल्प है। ऐसे अनेक हैं जिन्होंने गटनायक, गण प्रमुख अथवा मुख्य शिक्षक का दायित्व कभी निभाया नहीं। गण भी लिया नहीं । केवल भावना के कारण वे कार्य करने को प्रवृत्त हुए हैं। भावना आवश्यक है, परन्तु साथ ही अपनी कार्यप्रणालियों से उनका परिचित होना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से गटयोजना का महत्व, गण लेने की कुशलता, तदर्थ नित्य अभ्यास, शारीरिक व्यायाम का शौक, बौद्धिक क्षमता का विकास आदि होना भी आवश्यक है। साथ ही आत्मीयता एवं उसे दृढ़ करने के लिए व्यक्तिगत संबंधों की आवश्यकता का महत्व उन्हें ज्ञात होना चाहिये। स्वयंसेवकों की योग्यता को, गुणावगुणों को परखने की क्षमता को उनमें विकसित करने की आवश्यकता है। पुनः अपने द्वारा जो लोकसंग्रह करने का प्रयास किया जाता है, इसके अनुकूल प्रतिकूल क्या परिणाम हुए इस संबंध में नित्य चिंतन कर आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करने की उनमें प्रवृत्ति निर्माण करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रशिक्षण देने के लिए इन उपरिनिर्दिष्ट कार्यकर्ताओं के वर्ग प्रांतशः लेकर उन पर ये संस्कार करना यह आज की प्रथम आवश्यकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। प्रांत प्रचारक स्तर के कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण वर्ग का संचालन कर सकते हैं ऐसा विश्वास है।
वयस्क विभाग प्रचारकों को अथवा जिला प्रचारकों को तथा व्यवसायी स्वयंसेवकों को जिलों में एवं तहसीलों के ग्रामों में कार्य के संख्यात्मक विकास के लिये लक्ष्य केंद्रित करना चाहिये। इसी प्रकार से उनके कार्यक्षेत्र में चलनेवाले अन्य कार्यों की ओर भी लक्ष्य केन्द्रित करने के लिए उन्हें कहा जाये। दायित्व का यह विभाजन करना उचित होगा ऐसा मैं समझता हूँ ।-
ऐसा भी कुछ अनुभव है कि कार्यकारी मंडलों की बैठकों में कार्यक्रम मात्र का ही विचार होता है। अर्थात् गुरुदक्षिणा, पथसंचलन, केन्द्रीय अधिकारियों का प्रवास उनका प्रभावी स्वरूप एवं कोई अभियान अथवा परंपरागत उत्सव ये ही बैठकों में चर्चा के विषय होते हैं। मानों कार्यक्रम संपन्न कर लेना यही मुख्य कार्य है। उदाहरण स्वरूप मध्य भारत के धार जिले में कुक्षी नगर के कुछ नगर में कुछ वर्ष पूर्व प.पू. सरसंघचालक जी का प्रवास हुआ। वनवासी क्षेत्र का बहुत विशाल कार्यक्रम था यह। यह मान्य है कि उसका भी अपना महत्व है। वायुमंडल निर्माण करने की दृष्टि से उसका लाभ भी हुआ। तथापि यह सर्वमान्य होगा कि इतना करने से संतुष्ट होना उचित नहीं । परंतु आज वैसा ही हो रहा है। कुक्षी की शाखा न उसके पूर्व चालू थी और न बाद में चालू रही। कार्यक्रम से निर्माण हुए इस उत्साह को बनाये रखने के लिए कार्य के विस्तार की योजना बनाना, उसके द्वारा नये कार्यकर्ता तैयार करना यह कार्य नहीं हुआ। अतः कार्यक्रम संपन्न करना, उससे उत्पन्न वायुमंडल का उपयोग कर कार्यकर्ता संस्कारित करना एवं कार्य का विस्तार करना आदि की दृष्टि से कार्यकारी मंडलों की बैठकों में विचार करना एवं योजना बनाना आवश्यक है। इस दृष्टि से चिंतन करना आवश्यक है। कार्यकर्ता की संकल्प शक्ति बढ़ाना आवश्यक है।
सायं शाखाओं के कार्यकर्ताओं की बैठकें तथा प्रभात शाखाओं के कार्यकर्ताओं की बैठकें अलग-अलग होना चाहिये। वयस्क व्यवसायी लोगों की बैठकें समय पर होना कठिन होता है। उनकी शिथिलता का बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है और कई बार अपेक्षा भंग (Frustration) होकर कार्यकर्ता धैर्य खोता है, निष्क्रिय हो जाता है। यह न हुआ तो भी प्रौढ़ों की शिथिलता का विकिरण (radiation) तो उस पर होता ही है।
शाखा के समय पर अपना संघ स्थान यह संस्कार करने का एक पवित्र स्थान होता है। परंतु अतिरिक्त समय पर भी स्वंयसेवक सहजरूप से एकत्र हो सके इसलिये कार्यालय होना आवश्यक हो गया है। गत दिनों बाल, किशोर अथवा तरुण स्वयंसेवक एक दूसरे के घर एकत्र होते थे । परंतु परिवार के निवास के स्थान अब एक दो अथवा तीन कमरों तक सीमित होने के कारण यह सुविधा अब प्रायः समाप्त हो गयी है। बड़े नगरों में यद्यपि कार्यालय है, तथापि उनसे सब मोहल्लों को लाभ नहीं होता । अतः बड़े नगरों में दो, तीन मोहल्लों के लिए एक छोटा कार्यालय होना आवश्यक हो गया है ताकि अनौपचारिक रूप से बातें, गपशप, हास्य विनोद कर निःसंकोच रूप से स्वंयसेवक संस्कारित किये जा सके। कहना होगा कि स्वयंसेवकों को वहां आने के लिये आकर्षण बना रहे, बढ़े इसलिये वहां स्वच्छता एवं सुव्यवस्था होना तथा आने जाने वालों के बारे में पूछताछ होना, उनसे बात करना अपेक्षित है।
सायं शाखाओं में संस्कार करने के लिए क्या करना फलदायक होगा इसका अब तक विचार किया । प्रातः एवं रात्रि शाखाओं में प्रायः व्यवसाय करने वाले कर्मचारी किसान अथवा मजदूर आते हैं। उनकी आयु अधिक होने से उनके लिये रोचक विषय बिल्कुल भिन्न प्रकार के होना स्वाभाविक है। इस बात को ख्याल में रखकर कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। तथापि सम्यक दृष्टिकोण प्राप्त कर वे अपना विकास कर सके इसलिये सायंशाखा जैसा ही जितना अधिक मात्रा में अनौपचारिक संबंध होगा उतना ही अधिक मात्रा में हम उन पर संस्कार कर सकेंगे। फिर आत्मीयताके आधार पर ही उनका विकास करने का प्रयास होना चाहिये। उनकी भिन्न रुचि के अनुसार उनके लिये रोचक विषय बौद्धिक स्वरुप के हो सकते हैं। उन बौद्धिक विषयों को केवल राष्ट्र एवं संघ से संबंधित विषयों तक सीमित न रखते हुए, अपने तथा अन्य देशों के इतिहास, भूगोल, विज्ञान के विषय, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक वायुमण्डल तथा अपने यहाँ की राजनैतिक एवं सामाजिक समस्यायें ‘Ninety minutes at Entebbe’ जैसे साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन, अथवा ज्ञानवर्धक अन्य कार्यक्रमों का आयोजन प्रति-सप्ताह एक बार किया तो उपस्थिति की दृष्टि से लाभ होगा। वनविहार जैसे यदाकदा किये गये कार्यक्रम भी उपस्थिति बढ़ाने में सहायक हो सकेंगे। इस वनविहार के कार्यक्रम के कारण उनके अपने प्रतिदिन के व्यावसायिक जीवन से एक दिन दूर रहने से उनका मानसिक तनाव भी दूर होगा। सबके भिन्न व्यवसाय एवं भिन्न रुचि होने के कारण उस व्यवसाय की समस्याएं, उन्हें दूर करने के उपाय आदि विषयों के बारे में भी विचार करते विचार करते हुए बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।
इस प्रकार यद्यपि लोक संग्रह का कार्य कठिन है परंतु उसके शास्त्र को ठीक प्रकार से समझकर और बुद्धिमत्तापूर्ण क्रियान्विति से उसे अत्यंत सरल बनाया जा सकता है।
***********
| साभार संदर्भ |
| माननीय भाऊसाहेब भुस्कुटे उपाख्य श्री गोविन्द कृष्ण भुस्कुटे द्वारा महाकौशल प्रान्त में अपने प्रवास के समय व्यक्त विचारों का संकलन इस पुस्तिका में है । मा• भुस्कुटे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाकौशल एवं मध्यभारत प्रान्तों के क्षेत्रीय प्रचारक हैं। महाविद्यालयीन छात्र जीवन में नागपुर में आप स्वयंसेवक बने । संघ संस्थापक परम पूज्य डा. हेडगेवार जी से उनका अति निकट का सम्बंध रहा। सन् १९३८ में बी. ए., एल.एल. बी. तक शिक्षा पूर्ण कर वे संघ के प्रचारक बने । संस्कृत व अंग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार है। घर गृहस्थी का कार्य भी उन्होंने यशस्विता से सम्हाला । इस पुस्तिका में उनके विचार संघ के स्वयंसेवकों के लिए तो बहुमूल्य है ही साथ ही संघ-कार्य को समझने की इच्छा रखने वाले तथा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले बंधुओं के लिए भी उनकी उपादेयता है। साभार- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महाकौशल प्रांत, जबलपुर |