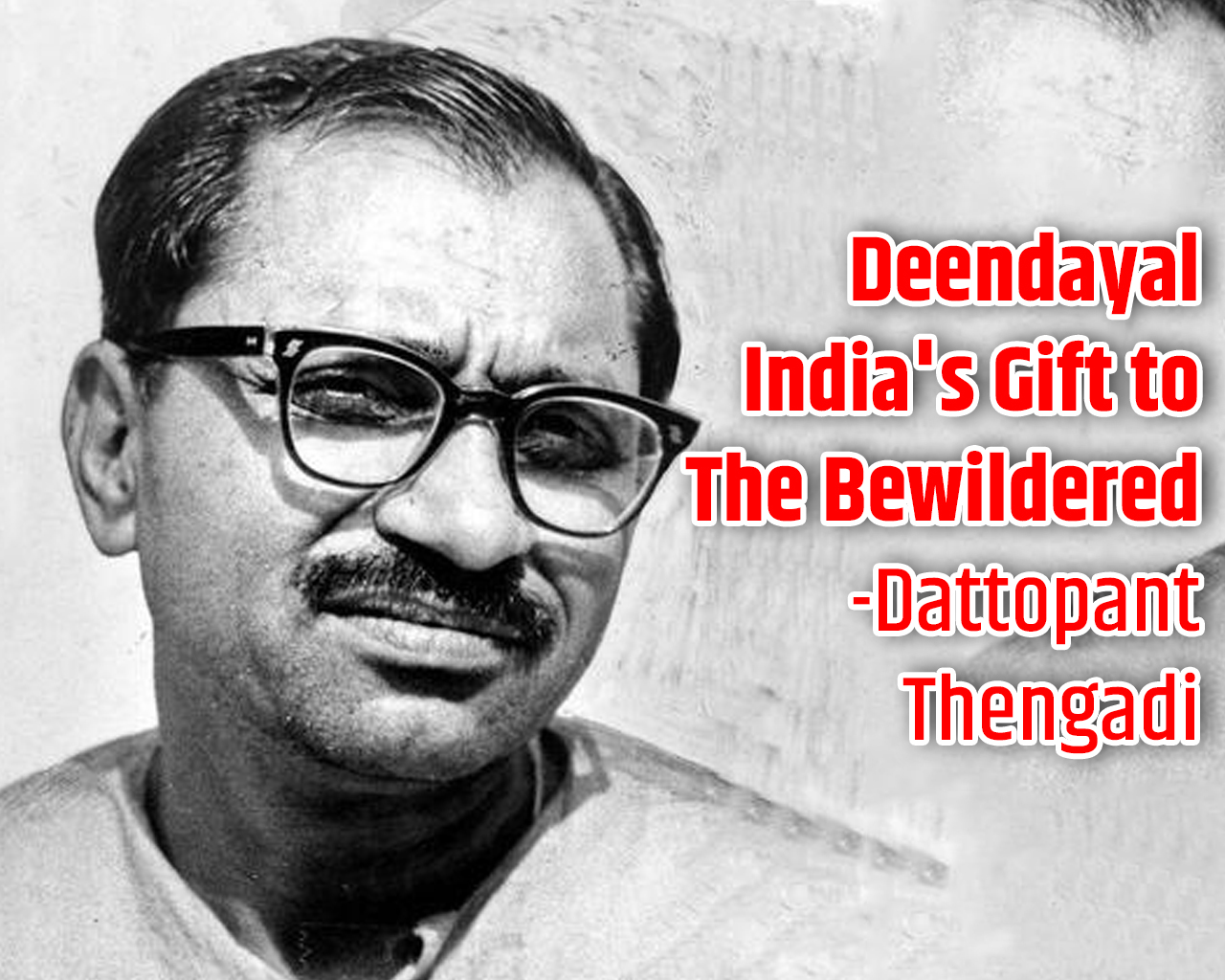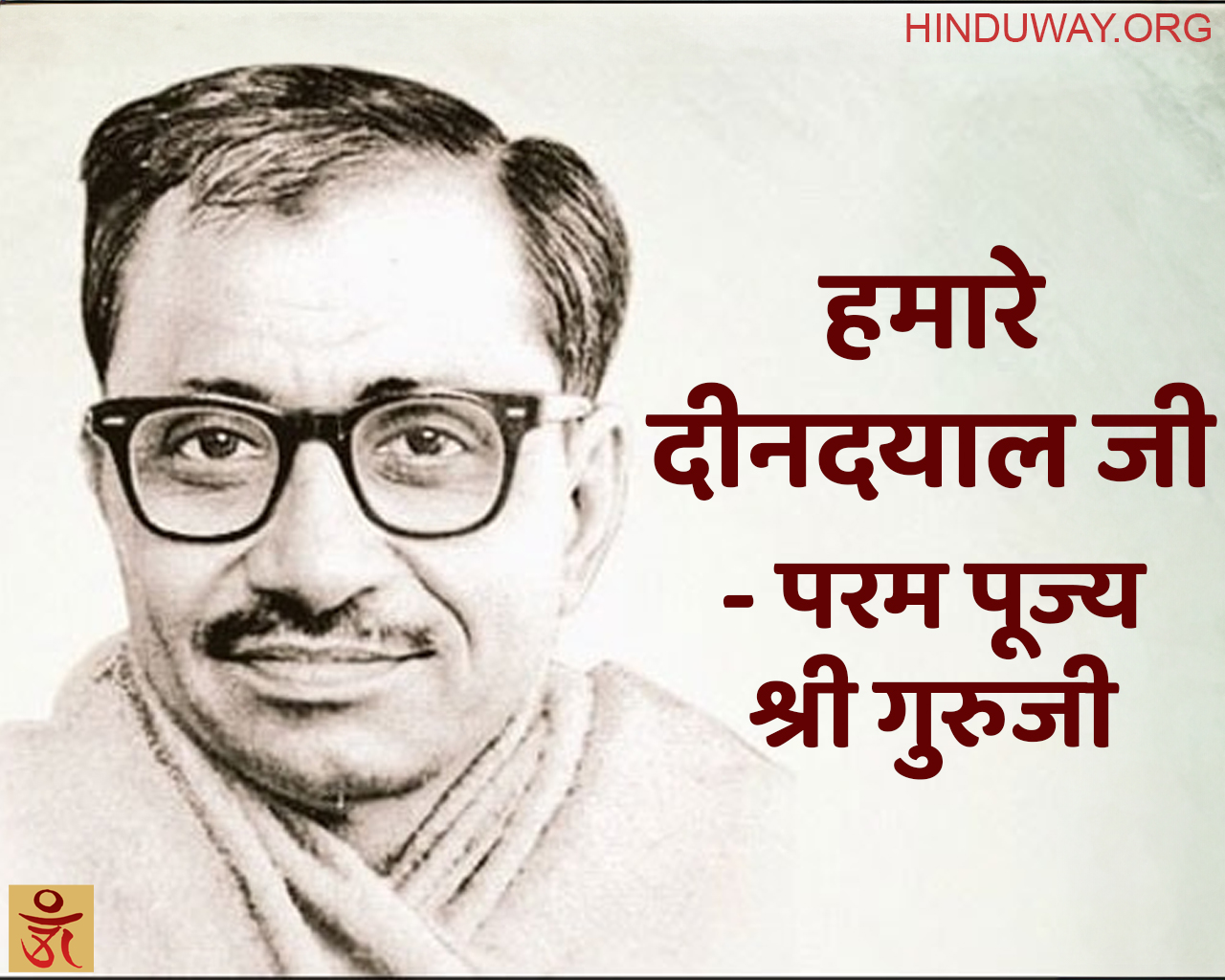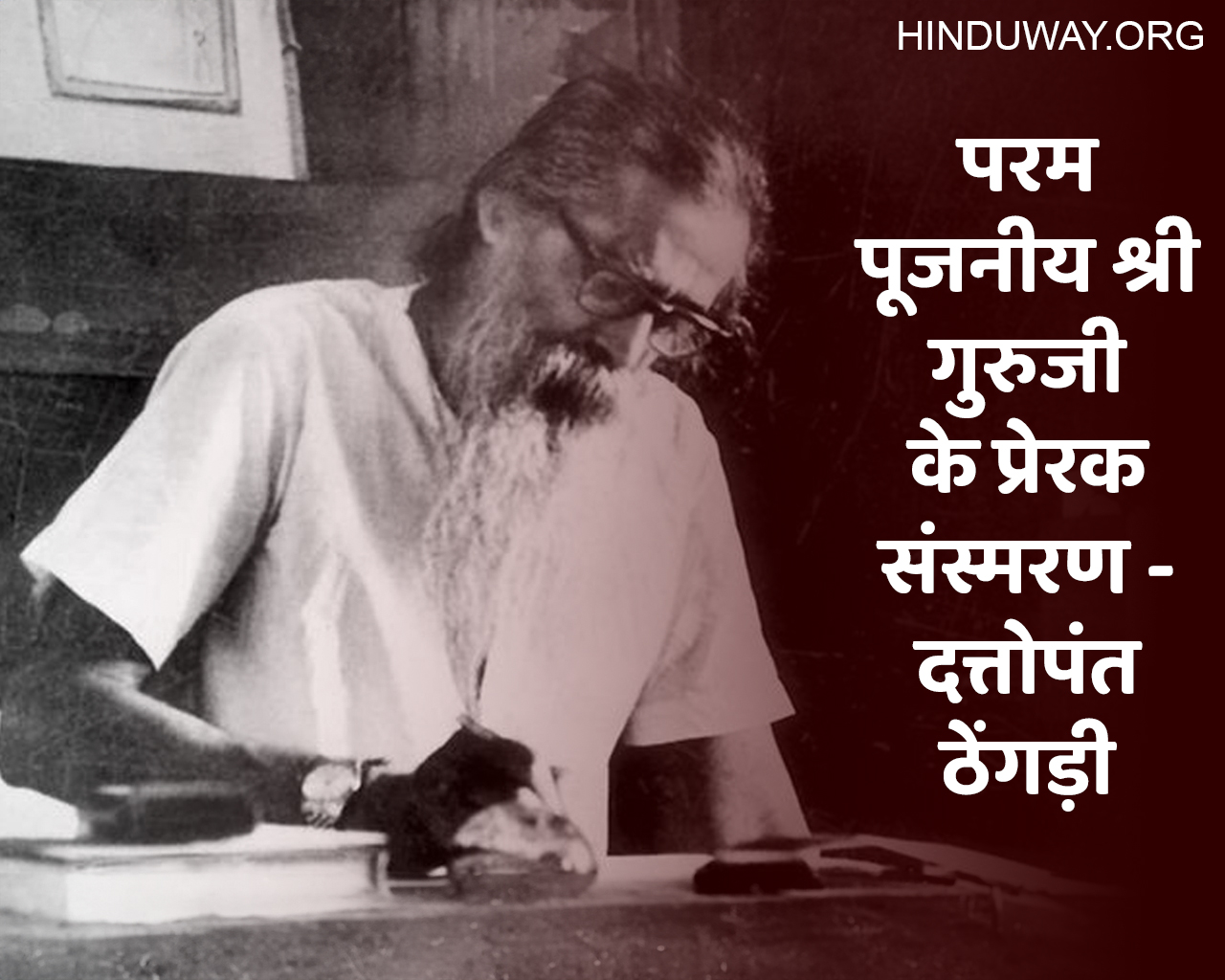दिनांक १४ अप्रैल, १९८३ को “सामाजिक समरसता मंच” की स्थापना हुई । इसकी स्थापना का कारण मूलगामी परिवर्तन प्रक्रिया से जुड़ा विचार है । (दत्तोपंत ठेंगड़ी)
सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से देश की परिस्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है । नित्य नवीन समस्याएं खड़ी हो रही हैं । शरीर का रक्त दूषित हो जाता है तो उसके कारण होने वाले फोड़े-फुंसियों को केवल मरहम-पट्टी करने से काम नहीं चलता । उसके लिए रक्त-शुद्धि का उपाय करना आवश्यक हुआ करता है । राजनीतिक नेताओं को तो हर बात की जल्दी रहती है । इस कारण वे रोग का निदान करने के पचड़े में नहीं पड़ते । धैर्य का अभाव होने के कारण तात्कालिक इलाज करके वे अपना काम चलाते रहते हैं । परिणामस्वरूप, कभी पंजाब सुलगता है तो कभी असम, कभी जम्मू-कश्मीर तो कभी दार्जिलिंग सुलग उठता है । राजनीतिक नेता किसी भी समस्या का स्थायी हल खोजने का प्रयास तक नहीं करते ।
देश की वर्तमान समस्याओं का किसी ने गहराई से विचार किया है क्या? उनका कोई निदान खोज लिया है क्या? इनका कोई इलाज सोचा है क्या? इन बातों का विचार करने पर ऐसा दिखाई देता है कि जिन महापुरुषों ने समस्याओं का ठीक-ठाक निदान खोज लिया था, उनकी समाज ने उपेक्षा की है, लेकिन भविष्य में समाज को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ेगी । ऐसे कुछ श्रेष्ठ पुरुष अभी-अभी हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने समस्या के मूल कारण खोज लिए थे । उन्होंने कुछ उपाय-योजना भी बनाई । ऐसे ही दो महापुरुषों का जन्म-दिन वर्ष १९८३ में संयोग से १४ अप्रैल को ही था । इन श्रेष्ठ पुरुषों में एक का नाम है श्रद्धेय बाबासाहब अम्बेडकर, और दूसरे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूज्य डा. केशवराव बलिराम हेडगेवार । इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज की समस्याओं का ठीक-ठाक निदान ही नहीं खोजा, वरन् समुचित उपाय भी किए ।
मैं श्रद्धेय बाबासाहब अम्बेडकर की ओर किस प्रकार आकृष्ट हुआ, सर्वप्रथम यह बताना ठीक होगा । मैं था एक सामान्य युवा कार्यकर्ता और वे थे अखिल भारतीय प्रतिष्ठाप्राप्त नेता । यह बात ध्यान में रखने से हमारे परस्पर के सम्बन्ध का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा । मैंने सन् १९५० तक बाबासाहब-अम्बेडकर का केवल नाम सुन रखा था । मेरी यह धारणा थी कि वे एक वर्ग विशेष के नेता हैं । तब तक मुझे न तो उनके जीवन-विषयक जानकारी थी और न ही उनके कार्य की ।
सर्वप्रथम सन् १९५० में हम कुछ युवक उनके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए । उस समय मैं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा था । देश का युवा वर्ग उन दिनों दो नेताओं से अत्यधिक प्रभावित हुआ था । वे दोनों डॉक्टर थे । प्रभावित होने का कारण था पंडित नेहरू के मंत्रिमण्डल से दोनों का त्याग-पत्र । ये दो नेता थे, डॉ० बाबासाहब अम्बेडकर और डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी । इन दोनों नेताओं के त्याग-पत्र देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की महत्वपूर्ण घटना थी । सर्वसाधरण लोगों की दृष्टि में यह एक अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था, क्योंकि यह आम- धारणा है कि मंत्रिमण्डल में स्थान पाना बड़े भाग्य की बात है और एक बार यदि मंत्रिपद मिल गया तो जैसे-तैसे उसी पद पर बने रहना चाहिए । हो सकता है, पंडित नेहरू ने उन्हें वित्त मंत्री बनाने का आश्वासन दिया होगा और वैसा नहीं किया तो इसी बात पर त्याग-पत्र देना तो कोई बुद्धिमानी नहीं हो सकती । एक बार गाड़ी में बैठ जाने पर कभी-न-कभी गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी ही । “को काल: फलदायक: “, कभी न कभी तो भाग्योदय होगा ही, “किन्तु सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धान्तों की केवल घोषणा करना और सत्ता में पहुचने पर उन सिद्धान्तों को भुला देना तथाकथित प्रगतिवादी लोगों के इस मार्ग को अपनाने के बजाय इन दोनों डाक्टरों ने सिद्धान्त के लिए शासन का उपयोग करना और शासन में रहते हुए यदि सिद्धान्तों पर अमल न हो पाता हो तो सत्ता का त्याग करने का पागलपन किया था । इस कारण ही देश के युवावर्ग के हृदय में इन दोनों नेताओं ने अपना स्थान बना लिया । मेरे मन में भी श्रद्धेय बाबासाहब के प्रति श्रद्धा जाग्रत होने का यही कारण था । श्रद्धेय बाबासाहब से अपनी प्रथम भेंट में ही मुझे उनके व्यक्तित्व में विशिष्टता के दर्शन हुए । मैं उस समय विश्वविद्यालय से निकला ताजा-ताजा ३१ वर्षीय युवक था । इस कारण मनुष्य का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति कम थी । फिर भी कुछ घटनाओं के कारण उनके असाधारण व्यक्तित्व की छाप मन पर अवश्य थी । उनमें से एक घटना इस प्रकार है :
प्रथम निर्वाचन के पूर्व बाबासाहब का नागपुर आगमन हुआ । सार्वजनिक सभा के पश्चात एक पत्रकार परिषद में बाबासाहब ने अनेक प्रश्नों का समाधान किया । नागपुर टाइम्स के प्रतिनिधि और मेरे मित्र श्री शरद शेवडे ने पत्रकार परिषद के बाद अकेले में प्रश्न किया कि “आपने कहा है कि हमारा शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन केवल एक विरोधी दल की भूमिका निभाने के लिए ही चुनाव नहीं लड़ रहा, वह तो अपनी सरकार बनाने की भी आकांक्षा रखता है । यदि ऐसा है तो क्या आप बता सकते हैं कि यह कितने वर्षों में संभव हो सकेगा?” बाबासाहब ने उत्तर दिया, “यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से पूछना ठीक होगा ।” श्री शेवडे ने कहा, “फिर भी आपका क्या अनुमान है ?” इस पर श्रद्धेय बाबासाहब बोले, “आप जरा इंग्लैण्ड का इतिहास देखिए । वहां की ब्रिटिश लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई और उसने अपना मंत्रिमण्डल कितने दिन बाद किस वर्ष बनाया ?” इसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा ।
बाबासाहब अम्बेडकर की उस समय की आयु को देखते हुए यह स्पष्ट था कि शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के माध्यम से अपने जीवनकाल में भारत का प्रधानमंत्री बनने का विचार उन्होंने निश्चित रूप से नहीं किया होगा । यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वयं की प्रधानमंत्री बनने की संभावना न होते हुए भी उन्होंने वृद्धावस्था में नया राजनीतिक दल बनाने का कष्ट क्यों किया? अर्थात् स्वत: की स्वार्थ सिद्धि ही प्रत्येक कार्य की प्रेरक शक्ति हुआ करती है, इस प्रकार की भूमिका से सोचने वाले सर्वसाधारण समाज का बाबासाहब अम्बेडकर के द्वारा नवीन राजनीतिक दल बनाने में किसी प्रकार की बुद्धिमानी दिखाई न देना स्वाभाविक था ।
दूसरा प्रसंग भी ऐसा ही है । भंडारा क्षेत्र का उपचुनाव था । वहां के सुरक्षित चुनाव क्षेत्र में एक सुरक्षित तथा दूसरे सामान्य स्थान के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी था । विपक्ष से सुरक्षित स्थान के लिए बाबासाहब अम्बेडकर तथा सामान्य स्थान के लिए अखिल भारतीय पार्टी के प्रत्याशी एक प्रसिद्ध नेता थे । स्थिति ऐसी थी कि शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के लोगों का दूसरा मत जिस किसी कांग्रेस विरोधी प्रत्याशी को मिलता, वह निश्चित रूप से विजयी होता । लेकिन सुरक्षित स्थान पर बाबासाहब अम्बेडकर के जीतने की संभावना नहीं थी, क्योंकि जिस पार्टी से समझौता किया गया था वह पार्टी येन-केन- प्रकारेण दूसरे पक्ष के मत हथिया लेने के लिए प्रसिद्ध थी और अपने समर्थकों के मत जिस दल से समझैता होता उसे दिलाने में उदासीन रहा करती थी । बम्बई में भी एक बार ऐसा ही अनुभव आने के कारण सभी कार्यकर्ताओं का यह विचार था कि इस समझौते का कोई लाभ नहीं है ।
इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए जो बैठक हुई उसमें एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उपस्थित था । गर्मागर्म बहस हुई । अधिकांश लोगों का कहना था कि हमने यदि अपना दूसरा वोट विपक्ष को (अर्थात् जिससे समझौता हुआ है) दिया तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, और बाबासाहब की हार होगी । इसलिए अपना दूसरा वोट जला दिया जाए अर्थात् किसी को भी न दिया जाए । यह चर्चा चल ही रही थी कि बाबासाहब भी बैठक में पहुंच गए । उनके पूछने पर लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम अपना दूसरा वोट व्यर्थ कर देंगे, तभी आप जीत सकते हैं ।
यह सुनकर बाबासाहब गंभीर होकर बोले, “मैने भारत का संविधान बनाया है । मैं यह बात कभी नहीं कह सकता, और न ही इसे सहन कर सकता हूं । मैं अपने अनुयायियों को संविधान के विरुद्ध व्यवहार करने अर्थात् दूसरे वोट का प्रयोग न करने के लिए कभी नहीं कह सकता । न तो मैं इसके लिए अनुमति दूंगा और न ही संविधान के विरुद्ध इस व्यवहार को सहन करूंगा । चुनाव में हार जाना मैं इससे बेहतर समझूंगा ।” फलस्वरूप, बाबासाहब चुनाव हार गए और सामान्य सीट पर खड़े वे नेता जीत गए । चुनाव जीतने का इतना सरल नुस्खा उपलब्ध होते हुए भी उसे न अपनाकर उन्होंने हार जाना स्वीकार किया । वह भी केवल इसलिए कि भारत के जिस संविधान का निर्माण उन्होंने किया उसकी रक्षा हो । उनकी इस सिद्धान्त निष्ठा से भी उनके असाधारण व्यक्तित्व का परिचय मिला । तीसरी घटना है उनके धर्म परिवर्तन के समय की । नागपुर के श्याम होटल में बाबासाहब के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी । भारतीय बौद्धजन समिति के मंत्री श्री वामनराव गोडबोले के द्वारा बैठक बुलाई गई थी । धर्मान्तरण की पूर्व संध्या अर्थात् दिनांक १३ अक्तूबर, १९५६ का यह प्रसंग है । वहां पर चाय का प्रबन्ध मेरी ओर था । बैठक में बाबासाहब अम्बेडकर ने कहा, “हम परिवर्तन करने वाले है इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी भावी योजना भलीभांति समझ लेना चाहिए । हमारे जो सिद्धांत हैं उन्हें सुदृढ़ आधार देना आवश्यक है । हमें अपनी भावी व्यूह-रचना भी निश्चित करनी होगी ।”
इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “शिड्यूल्ड कारूर के रूप में समाज का जो वर्ग है, वह अपना ही है । हम अब बौद्धमत अपनाने वाले हैं । शिड्यूल्ड कास्ट में से कुछ लोग बौद्ध बनेंगे । जो लोग बौद्ध नहीं बनेंगे, वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के होने के कारण पहले से ही अपने हैं । बौद्धमत को हमें शिड्यूल्ड कास्ट्स तक ही सीमित नहीं रखना है । शिड्यूल्ड कास्ट के बाहर भी इसका प्रचार करना होगा । इससे जो शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं वे, और जिन्हें बौद्धमत के प्रति आकर्षण है वे लोग भी हमारा साथ देंगे । और गैर-शिड्यूल्ड कास्ट्स बौद्ध के रूप में भी एक वर्ग तैयार होगा । अर्थात् (१) बुद्धिस्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स, (२) शिड्यूल्ड कास्ट्स नॉन बुद्धिस्ट, और (३) नॉन शिड्यूल्ड कास्ट्स बुद्धिस्ट, इस प्रकार के वर्ग निर्मित होंगे । इन तीनों वर्गों का सहयोग हमारे द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडेरेशन के रूप में निर्मित होने वाली राजनीतिक पार्टी को भी मिलेगा । हमारी पार्टी पश्चिम के जनतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर काम करेगी ।
मैं यह जानता हूं कि आप लोगों को धर्म की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि है, लेकिन मुझे राजनीति से अधिक धर्म के प्रति आकर्षण है । शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने दलित वर्ग में स्वाभिमान एवं आत्मगौरव का भाव जगाया है । दलित वर्ग के लोगों ने अपने और शेष समाज के बीच एक दीवार खड़ी कर ली है । स्थिति यहां तक पहुंची है कि अस्पृश्य वर्ग के प्रत्याशी को अन्य लोग अपना मत नहीं देते और वे भी अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को अपना मत नहीं देते । इसलिए जिन लोगों को दलितों के प्रति सहानुभूति है, ऐसे लोगों को साथ लेकर एक राजनीतिक दल की स्थापना करके अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ काम करने का प्रयत्न करना चाहिए । अब परिस्थिति का सिंहावलोकन करने का समय आ गया है । हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के सिद्धान्तों से जो सहमत होंगे, राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे लोग भी हमारा साथ देंगे । इनमें से कुछ शिड्यूल्ड कास्ट्स के होगे और कुछ शिड्यूल्ड कास्ट्स के बाहर के भी होंगे । कुछ बौद्धमत को मानने वाले होंगे तो कुछ बौद्धमत को न मानने वाले भी होंगे । इसका अर्थ है कि हमारे साथ शिड्यूल्ड कास्ट्स और बौद्ध रिपब्लिकन्स के रूप में रहेंगे, और ऐसे भी लोग रहेंगे जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, रिपब्लिकन और बौद्ध नहीं हैं । ऐसी स्थिति में एक धर्ममत, एक राजकीय मत तथा एक सामाजिक वर्ग के जितने भी विनिमयन और समुच्चय हो सकते हैं, उन सबको मिलाकर विभिन्न प्रकार के लोग हमारा साथ देंगे और इस प्रकार अपने सिद्धान्तों के लिए अनुकूल एक सामाजिक अधिष्ठान का निर्माण होगा ।” यह विषय उन्होंने कार्यकर्ताओं के समाने विस्तार से रखा था । साथ ही एक चेतावनी भी दी थी कि “ध्यान रखने की बात है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सामाजिक इकाई के रूप में जो वर्ग खड़ा हो वही धर्म का भी मुखौटा लगा ले, और वही राजनीतिक दल के रूप में भी काम करे ।”
यह बात अक्तूबर, सन् १९५६ की है । उस समय उनके स्वास्थ्य, उनकी आयु और उनके द्वारा प्रस्तुत व्यूह-रचना को सुनकर यह एक बात तो किसी के भी ध्यान में आ सकती थी कि “इतनी दीर्घकालीन योजना को फलीभूत देखने के लिए वे स्वयं जीवित नहीं रहेंगे । लोगों ने यह अनुभव किया कि उनका ध्येय स्पष्ट है, ध्येय सिद्धि देखने के लिए रहें या न रहें किन्तु पूरी निष्ठा के साथ वे वृद्ध सज्जन ध्येय सिद्धि के प्रपत्र की पराकाष्ठा कर रहे हैं । अपने सुखी जीवन की ओर से मुंह मोड़कर स्वेच्छा से दुःख और कष्ट का मार्ग अपना रहे हैं ।” राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत नेता इसे बुद्धिमानी नहीं कहेंगे । वे तो यही सलाह देंगे कि समझदार व्यक्ति बुढ़ापे में कभी भी आम, बेल या कैथ के पौधे का रोपण नहीं किया करते । क्योंकि उनके जीते जी न तो ये वृक्ष फल देने वाले हैं और न ही वे उसका उपभोग कर सकेंगे । तो फिर ऐसी स्थिती में उस वृद्ध सज्जन ने व्यर्थ ही क्यों परेशानी मोल ली? केवल इसलिए कि उनके सामने भव्य- दिव्य ध्येय था, और यही उनके महान् व्यक्तित्व का परिचायक है । ऐसी ही कुछ घटनाओं से बाबासाहब अम्बेडकर के विषय में मेरे हृदय में श्रद्धा का निर्माण हुआ । उनके संगठनात्मक विचार से बाबासाहब के विषय में मेरे मन में आत्मीयता की वृद्धि हुई ।
बाबासाहब अम्बेडकर उच्च सिद्धान्तों के प्रतिपादन के साथ हो संगठन के लिए अपेक्षित व्यवहार की साधारण दिखाई देने वाली बातों का भी ध्यान रखते थे ।
इस सम्बन्ध में एक प्रसंग स्मरण आता है । १४ जुलाई, १९५२ को बम्बई के दामोदर हाल में आयोजित सभा में भवन-निर्माण फण्ड के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा था, “हमारे लोगों ने जो धनराशि एकत्रित की है, उसमें जिन विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने पच्चीस रुपए अथवा इससे अधिक की धनराशि दी है, उसका कुल योग २५, ७०१ रुपए ४ आने हुआ है । पच्चीस रुपए से कम देने वालों की धनराशि १००० रुपए से कम हुई है, और जिस राशि के स्रोत का पता नहीं, वह धनराशि ५००० रुपए है । इन पांच हजार रुपयों का विवरण क्यों उपलब्ध नहीं हुआ? कारण स्पष्ट है, पावती पुस्तकें वापस जमा नहीं हुई। उन पावती पुस्तकों में और भी धनराशि जमा होने की संभावना है । यह अनुल्लिखित धनराशि लोगों के द्वारा हड़प किए जाने का संदेह निर्माण होना स्वाभाविक है । इस संदेह को दूर करने के लिए लोगों के द्वारा ली गई समस्त पावती पुस्तिकाओं को उनके द्वारा प्राप्त धनराशि के साथ जमा करना होगा । पावती पुस्तकों को वापस न करना अथवा प्राप्त धनराशि को जमा न करना, कानून की दृष्टि से दण्डनीय अपराध है । यह बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए ।”
इस प्रसंग पर मुझे शिक्षित लोगों से भी दो शब्द कहने है । गरीब जनता द्वारा दी गई धनराशि का हिसाब आपको ठीक प्रकार से रखना होगा । एक पैसे की भी गड़बड़ न होने पाए, इसकी सावधानी रखनी होगी । सार्वजनिक धन का हिसाब व्यवस्थित रखकर उसे समय-समय पर जनता के सन्मुख रखने से बढ्कर पवित्र और कोई कार्य नहीं हो सकता और सार्वजनिक धन का आहार करने जैसा नीच कृत्य भी दूसरा कोई हो नहीं सकता ।”
ऐसे ही प्रसंग पर उन्होंने अपना यह भाव प्रकट किया था कि “मुझसे अनेक लोग पूछा करते हैं, आप भाषण क्यों नहीं देते? संदेश क्यों नहीं देते? मैं भाषण या संदेश नहीं देता इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मुझे आपकी चिंता नहीं, आपके प्रति आत्मीयता नही, या मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता । अवसर देखकर काम करना पड़ता है । शत्रु कौन है? मित्र कौन है? किस समय क्या करना चाहिए? इन सब बातों की जांच भी करनी पड़ती है । ऐसी स्थिति में रुककर सोचने के सिवाय कोई भी उपाय नहीं होता ।”
जीन कसे हुए घोड़े पर सवार होना अलग बात है और किसी संगठन को खड़ा करना एक भिन्न प्रक्रिया है । संगठन खड़ा करने वाले नेता को धरती से सम्बन्ध रखना पड़ता है । उसी से उसमें कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने की पात्रता आती है । कार्यकर्ताओं से बाबासाहब अम्बेडकर की चर्चा की कुछ बानगी देखिए । वे कहते हैं : “अपना घर छोड़कर दूसरे के बंगले में घुसना निरी मूर्खता है । अपनी झोपड़ी सलामत रखो, अन्यथा अपनी अवस्था ब्राह्मणेतर पार्टी जैसी हुए बिना नहीं रहेगी ।” ब्राह्मणेतर पार्टी की क्या दुर्गति हुई, यह आप जानते ही हैं । सन् १९३२ तक हम परस्पर सहयोग से काम कर रहे थे । उस समय कुछ ब्राह्ममणेतर नेताओं का विचार हुआ कि कांग्रेस के बाहर रहने से कोई लाभ नहीं । कांग्रेस में प्रवेश करके अन्दर से उसके दुर्ग में दरार डाली जाए । यह काम बाहर से संभव न होगा । यह सोचकर वे कांग्रेस में गए । मैंने उन्हें ऐसा न करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी । अब वे अपनी भूल मान रहे हैं । किन्तु अब वे अपनी झोपड़ी बांध भी सकेंगे या नहीं, इसकी मुझे शंका है । झोपड़ी मिटाकर समझौता करना मुझे बिल्कुल मान्य नहीं । झोपड़ी कायम रखकर ही हमसे जो कुछ संभव होगा, हम करेंगे । जो मिल रहा है उसे स्वीकार करके शेष मांगों के लिए संघर्षरत रहने का हमारा स्वभाव होना चाहिए । “कै हंसा मोती चुगे, कै तो रहे उपास” इस कहावत वाली वृत्ति अच्छी नहीं । इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं ।
किसी भी राजनीतिक दल से हमारी सहमति का अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि हम अपने संगठन का अस्तित्व ही समाप्त कर दें । कांग्रेस, सोशलिस्ट, पीजेंट्स एण्ड वर्कस पार्टी जैसा कोई भी राजनीतिक दल हो, उनसे सहयोग करते समय हम इस बात को अवश्य ध्यान में रखें । राजनीतिक क्षेत्र में अकेले व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती । मुझे भी आज कांग्रेस पार्टी तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो सम्मान प्राप्त है, इसका कारण मेरे साथ शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन का संगठन है । इसका समर्थन खो देने पर मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कोई नहीं पूछेगा । इसीलिए राष्ट्र-रक्षा की भावना हृदय में धारण कर, राजनीतिक क्षेत्र में “शत्रु-मित्र”, के सम्बन्ध को जानकर स्वत: के स्वत्व की रक्षा करते हुए सतर्कता से शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नेतृत्व में कार्य करना चाहिए ।
मनुष्य को केवल स्वार्थ का ही विचार नहीं करना चाहिए । कुछ परमार्थ भी आवश्यक है । मैं भी इसी भावना से फेडरेशन का कार्य कर रहा हूं । यह प्रेरणा मुझे “धर्म” से प्राप्त हुई । स्वत: का पेट भरना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है । पेट तो भिखमंगे भी भर लेते हैं । स्वयं के परिवार के भरण-पोषण के साथ-साथ समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करते रहना चाहिए ।
अब हम अपना मन शुद्ध करें । सद्गुण प्राप्ति की हमें धुन हो । हम धार्मिक बनें । शिक्षित होना ही सब कुछ नहीं है । शिक्षा प्राप्ति के साथ चरित्र सम्पन्न भी बनना होगा । चरित्र के बिना शिक्षा निरर्थक हो जाती है । ज्ञान दुधारी तलवार के समान होता है । व्यक्ति के हाथ की तलवार का सदुपयोग या दुरुपयोग उस व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है । तलवार से किसी की हत्या भी की जा सकती है और प्राणरक्षा भी । ज्ञान का भी दोहरा प्रयोग होता है । शिक्षित व्यक्ति यदि चारित्र्य सम्पन्न होगा तो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेगा । यदि वह दुश्चरित्र होगा तो उसका ज्ञान लोगों को पीड़ित करने का माध्यम बनेगा । शील अर्थात् चारित्र धर्ममय जीवन का परिपाक है । शिक्षित व्यक्ति यदि केवल अपना ही पेट भरता है, स्वार्थ के अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं देता, परमार्थ की ओर उसकी लेशमात्र भी प्रवृत्ति नहीं है तो ऐसे शिक्षित व्यक्ति का जीना व्यर्थ है ।
कार्यकर्ताओं की यह धारणा बनी है कि निर्वाचन यानी राजनीति, निर्वाचन के बिना राजनीति का कोई अर्थ नहीं । इसीलिए निर्वाचन के समय टिकट प्राप्ति के लिए भाग-दौड़ किया करते हैं । निर्वाचन के बाद सभी निष्क्रिय हो जाते हैं । लेकिन समाज के दीर्घकालीन जीवन में राजनीति एक अल्पकालिक घटना मात्र है । राजनीति ही सबकुछ नहीं है । अन्य कार्य इससे भी अधिक महत्व के हैं । केवल राजनीति से समाज की उन्नति नहीं होती । समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि अन्य -क्षेत्रों में भी कार्यकर्ताओं को कार्य करना चाहिए । राजनीति को अत्यधिक महत्व देने के कारण ही चुनाव के समय टिकट प्राप्ति के लिए भाग-दौड और वह न मिलने पर समाज में गुटबाजी का निर्माण, चुनाव में हार जाने पर सार्वजनिक जीवन से मुंह मोड़ लेना, विजयी होने पर विधानसभा अथवा संसद में कुर्सी की शोभा बढ़ाने के अतिरिक्त कुछ न करना ही आजकल कार्यकर्ताओं ने सबकुछ समझ लिया है ।
व्यक्तिश: किसी भी कार्यकर्ता से मेरा विशेष स्नेह होने का प्रश्न ही नहीं है । मुझे तो कार्य प्रिय है । जो अधिक कार्य करेगा, वही मुझे प्रिय होगा । चुनाव भी क्रिकेट के मैच के समान है । मैच में हारने वाली टीम खेल खेलना नहीं छोड़ देती । वह भविष्य में होने वाले मैच में विजय प्राप्ति की आकांक्षा लेकर ले उत्साह से तैयारी में जुट जाती है । हमारे कार्यकर्ताओं को इसी मनोभूमिका से कार्य करना चाहिए । मेरी इच्छा के अनुसार ही संस्था का कार्य चलना चाहिए, यह प्रवृत्ति अत्यंत घातक है ।
राजनीति में विवाद तो होंगे ही । उन्हें भूल जाने का अभ्यास करना होगा । मतभेद के अंकुर को मन में पनपने देना उचित नहीं । मेरा हृदय निर्मल होने पर भी अन्य लोगों से मेरे मतभेद होते हैं, लेकिन उन्हें मैं तत्काल भुला देता हूं । मनुष्य का मन पुष्प जैसा स्वच्छ एवं प्रफुल्लित रहना चाहिए । अपने फेडरेशन में बहुत से बाजारू लोग एकत्र हो गए हैं । फेडरेशन को समाप्त करने का यदि उनका विचार हो तो वे अभी से फेडरेशन छोड़कर चले जाएं । फेडरेशन में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है । दो घोड़ों पर सवारी नहीं हो सकती । फेडरेशन का यह वृक्ष जल्दी फल देने वाला नहीं है । यह निश्चित रूप से देर से ही फलने वाला है । लेकिन यह दीर्घकाल तक के लिए काम देगा । जो वृक्ष अल्पकाल में फल देते हैं, उनका जीवन भी अल्पकालीन ही होता है । इस प्रकार के वृक्ष हमें अपेक्षित नहीं हैं । इसलिए जिन्हें तत्काल फल की अपेक्षा है उन्हें अन्यत्र चले जाना चाहिए ।
जिसमें धैर्य नहीं, वह नेतृत्व नहीं कर सकता । जो मरने के लिए सदैव तैयार रहता है, उससे मृत्यु भी दूर भागती है, जो मृत्यु से डरता है, वह मृतवत् है ।
यदि कोई राजनीतिक क्षेत्र में ही कार्य करना चाहता है तो उसे राजनीति का गहन अध्ययन करना चाहिए । अध्ययन के बिना इस दुनिया में कुछ भी साध्य नहीं हुआ करता । हमारे कार्यकर्ताओं को राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना चाहिए । जिन्हें समाज का नेतृत्व करना है उन्हें नेतृत्व के लिए अपेक्षित कर्तव्य तथा दायित्व का बोध होना आवश्यक है । हमारे समाज के नेताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहन करनी होती है । अन्य समाज के नेतृत्व वर्ग और हमारे समाज के नेतृत्व वर्ग की स्थिति बिल्कुल भिन्न है । अन्य समाज के नेताओं के कार्य की परिसमाप्ति सभा में उत्तेजक भाषण देकर तालियां बजवा लेना और पुष्पमालाओं से लदे हुए घर वापस आने में ही हो ही जाती है । हमारे समाज के नेतृत्व वर्ग के लिए इतने से काम नहीं चलेगा । अध्ययन, चिंतन और मनन के साथ-साथ समाज की उन्नति के लिए अहर्निश शारीरिक श्रम करना भी हमारे समाज के नेता के लिए आवश्यक होगा । तभी उसके द्वारा समाज का थोड़ा बहुत भला हो सकेगा । समाज तभी उसका नेतृत्व स्वीकार करेगा । शायद आप सोचते हैं कि नेता बनना सरल है । लेकिन मेरे विचार से नेता बनना बहुत ही कठिन कार्य है । मेरा तो यही अनुभव है । क्योंकि अन्य लोगों जैसा मेरे नेतृत्व का स्वरूप नहीं है । मैंने जब यह आन्दोलन प्रारम्भ किया तब आज जैसा कोई संगठन नहीं था । मुझे ही सब काम करना पड़ता था । संगठन खड़ा करने के लिए भी मुझे ही खपना पड़ता था । समाचारपत्र शुरू करना भी मेरा ही सिरदर्द हुआ करता था । “मूक नायक”, “बहिष्कृत भारत”, जनता आदि समाचारपत्र चलाना हो या प्रिंटिंग प्रेस चलाना हो, सभी मोर्चे मुझे ही संभालने पड़े थे । संक्षेप में यही कहना होगा कि मुझे शून्य में से सृष्टि का निर्माण करना पड़ा ।
क्रोध का स्वरूप दो प्रकार का होता है : एक द्वेषमूलक और दूसरा प्रेममूलक । बधिक का क्रोध द्वेषमूलक होता है और मां का अपनी संतान पर किया जाने वाला क्रोध प्रेममूलक होता है । वह यदि अपने पुत्र को एक चपत लगाती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती । पुत्र सदाचारी बने, सुयोग्य बने, यही उसकी आन्तरिक इच्छा हुआ करती है । मेरे द्वारा भी आप लोगों को प्रताड़ित किए जाने के मूल में भी आपके कल्याण की कामना ही रहा करती है । आप लोगों में समता और बंधुता का भाव स्थायी रूप से रहे, मेरी यह इच्छा होने के कारण ही मैं आप लोगों को राजनीति से अलग होने के लिए कहा करता हूं ।”
किसी भी संस्था या संगठन के कार्यकर्ता, संगठक अथवा प्रचारक के लिए उपर्युक्त व्यावहारिक मार्गदर्शन उपयोगी हो सकता है । इसकी उपयोगिता परिस्थिति और काल निरपेक्ष है । श्रद्धेय बाबासाहब अम्बेडकर का यह विचारधन सबके लिए उपलब्ध कराने के लिए श्री डी. के. पोखर्णीकर तथा श्री मा.फ. गांजरे बधाई के पात्र हैं ।
भारत के संविधान निर्माता के द्वारा कार्यकर्ता की मनःस्थिति को ध्यान में रखकर इतने विस्तार से व्यावहारिक मागदर्शन करना सचमुच सराहनीय है । इसे पढ़ते समय मुझे गगनबिहारी गरुड़ पक्षी का स्मरण होता है । गगन में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला यह पक्षी अपना घोंसला हवा में नहीं, धरती पर खड़े किसी वृक्ष पर ही बनाता है । बाबासाहब अम्बेडकर ने कार्यकर्ताओं का जो मार्गदर्शन किया, वह इसी श्रेणी में आता है । यह सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के लिए पाथेय का काम दे सकता है । स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक होने के कारण मैं इस प्रकार के मागदर्शन का महत्व भलीभांति जानता हूं । वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत नेताओं के विचार और व्यवहार का विचार करने पर बाबासाहब अम्बेडकर का मार्गदर्शन मुझे विशेष महत्व का लगता है ।
जो लोग पिछड़े वर्ग के नहीं थे, उनके लिए बाबासाहब का व्यवहार कुछ स्पष्टवादिता तथा उपेक्षापरक अनुभव होना स्वाभाविक था । जिन लोगों को साथ लेकर काम करना है उन्हें उन्हीं की भाषा में अपनी बात समझानी आवश्यक होती है । बाबासाहब की यह विशेषता थी कि अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्तर जानकर वे उसके समझ में आने वाली भाषा और वाक्य का प्रयोग तथा प्रचलित कहावत-मुहावरों का उपयोग किया करते थे । शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के प्रारम्भिक काल के नागपुर के अध्यक्ष श्री दशरथ पाटिल से श्री बाबासाहब की मित्रवत् चर्चा हो रही थी । मैं भी संयोग से वहां उपस्थित था । “लाडवण” शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा चल पड़ी । बाबासाहब ने अपना मत प्रदर्शित करते हुए ऐसे कुछ विशिष्ट ग्रामीण बराड़ी शब्द का प्रयोग किया कि उसे सुनकर मैं भौंचक्का सा खड़ा रह गया । भारत के संविधान निर्मात्री परिषद में दिए गए उनके विद्वतापूर्ण भाषणों की प्रशंसा मैंने अवश्य सुनी थी । वे बराड़ी भाषा के मुहावरे का प्रयोग भी उतनी ही कुशलता के साथ कर सकते हैं, यह देखकर हर्ष हुआ । जिन लोगों को जोड़ना है, लोकसंग्रहकर्ता को उनके ही धरातल पर उतरकर उनमें समरस होना पड़ता है, अन्यथा लोकसंग्रह संभव ही नहीं हो सकता ।
बाबासाहब अम्बेडकर के विचार इतने सुस्पष्ट तथा मौलिक रहा करते थे कि उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए निर्भीकता और कभी-कभी अप्रियता को स्वीकार करने की भी तैयारी रखनी पड़ती थी । उनके बात करने की शैली को “दो टूक बात” करने की शैली की श्रेणी में रखा जा सकता है । इस कारण उनके विषय में अनेक बार गलत धारणा भी बन जाया करती थी । वे स्वयं भी इसका अनुभव करते थे । एक बार अपनी इस तुनकमिजाजी का स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने बताया, “यद्यपि मेरा स्वभाव कुछ क्रोधी है और सत्ता में बैठे हुए लोगों से मेरी झड़पें भी अनेक बार होती रहती हैं किन्तु इससे उन्हें मेरे विषय में ऐसी गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए कि मैं विदेशों में भारत के विरुद्ध भी बोलूंगा । मैंने देश के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं किया है । देश का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है । गोलमेज सम्मेलन के समय मैं गाधी से भी दो सौ मील आगे था ।”
दूसरे एक प्रसंग पर वे बोले, “बहुत से हिन्दू मुझे शत्रुवत समझते हैं, किन्तु ब्राह्मणों में भी मेरे अपने मित्र हैं । जो ब्राह्मण हम लोगों के साथ कुत्ता-बिल्ली जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को उनकी समाजद्रोही करतूतों के लिए बड़ी फटकार लगाने का काम मेरे भाग्य में लिखा है । इसके लिए मैं विवश हूं ।”
वस्तुत: उनके सभी कार्यो में ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च वर्ण के लोगों ने अनेक बार भरपूर सहायता की थी । इस विषय में बाबासाहब ने अनेक बार सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता भी प्रकट की है । व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा सामाजिक समस्याओं का निदान, दोनों भिन्न बातें हैं, परन्तु उनकी स्पष्टवादिता के कारण अनेक बार भ्रम निर्मित होते रहे ।
यह सर्वविदित है कि बाबासाहब के ग्रंथ ” थाट्स ऑन पाकिस्तान,” ने तूफान खड़ा कर दिया था । हिन्दुत्व के समर्थकों को इससे जर्बदस्त धक्का लगा था । तत्कालीन भावना के आवेश में यह सोचने के लिए भी किसी के पास समय नहीं था कि इस ग्रंथ के द्वारा प्रस्तुत मंतव्य के पीछे भी कोई तर्क हो सकता है । बाबासाहब के इस ग्रंथ के निष्कर्षों से पूर्णत: और अंशत: असहमत हुआ जा सकता है लेकिन उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, उसका सभी को, और विशेष रूप से हिन्दुत्व के समर्थक लोगों को अवश्य विचार करना चाहिए । बाबासाहब का यह सुचिंतित निष्कर्ष है कि “मुसलमानों के लिए उनका मजहब सर्वोपरि होने के कारण उन्हें जनतंत्र की कल्पना समझ में नहीं आ सकती । उनकी राजनीति भी मजहब प्रधान होती है । वे समाज-सुधार के भी विरोधी हैं । अपने प्रतिगामी विचारों के कारण ही वे संसार में पहचाने जाते हैं । मुसलमान अपने मजहब को विश्व का मजहब मानता है । लेकिन इस्लाम का बंधुत्व सर्वव्यापक तथा सार्वत्रिक नहीं है । उनका बंधुत्व भाव केवल मुसलमानों तक ही सीमित होता है । जिस देश पर मुस्लिम शासन नहीं, उसे वह ”शत्रु भूमि” समझता है । मुसलमान अपने मजहब के लोगों के सिवाय अन्य धर्मियों से घृणा करते हैं, उन्हें शत्रु समझते हैं । ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि इस प्रकार की भावना किसी भी मुसलमान के मन को न छू सके कि “हिन्दुस्थान हमारी मातृभूमि है तथा हिन्दू हमारे भाई है।”
आक्रामक वृत्ति मुसलमान के रग-रग में समाई होने के कारण, हिन्दू समाज की दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए वे गुंडागर्दी का रास्ता अपनाते हैं । मुसलमानों की प्रतिगामी तथा अराष्ट्रीय वृत्ति के सम्बन्ध में बाबासाहब ने बड़े ही कटु शब्दों में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन उनके मित्रों ने उसे प्रकाशित नहीं होने दिया । उनका यह निश्चित मत था कि “मुसलमान जब तक अपने को मुसलमान समझता रहेगा, उसे हिन्दुस्थान के राष्ट्र-देह में आत्मसात् नहीं किया जा सकता । मुसलमानों को साथ लेकर अखण्ड हिन्दुस्थान कभी नहीं बन सकेगा और न ही हिन्दुस्थान का समाज जीवन एकरस हो सकेगा । समुद्र में जहाज न डूबे, इसके लिए आवश्यकता से अधिक जो सामान होता है, उसे फेंक देना पड़ता है और जहाज को डूबने से बचा लिया जाता है । ” उनका यह स्पष्ट मत था कि मुसलमान जब तक भारत में रहेंगे तब तक केन्द्र में प्रभावी सरकार का निर्माण संभव नहीं है ।
बाबासाहब यह बार-बार दोहराया करते थे कि मुसलमानों को हम आत्मसात नहीं कर सकेंगे । किसी विदेशी तत्व को राष्ट्र के शरीर में रखने की अपेक्षा उसे निकाल देना ही उचित है । कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में एक बार जब मैं उनके वक्तव्य के स्पष्टीकरण के लिए उनसे मिला था तो वे आवेश में आकर बोले, “देशभक्ति के विषय में मैं आप लोगों से एक कदम भी पीछे नहीं हूं लेकिन फर्क केवल इतना ही है कि जूता कहां काटता रहा है, इसका मुझे हमेशा-हमेशा अनुभव होता रहता है, जबकि आप लोगों को जूता काट रहा है इसकी भी अनुभूति नहीं होती । कश्मीर घाटी को यदि भारत में रखना हो तो वहां के समस्त मुसलमानों को हिन्दू समाज द्वारा आत्मसात कर लेना चाहिए । यदि ऐसा न हुआ तो यह एक कांटे की तरह सतत चुभती रहेगी । यह समस्या हमारे राष्ट्र के सिर पर सदैव के लिए एक टंगी तलवार जैसी रहेगी । हम अर्थात् ”हरिजन” भी तो आपके ही अंग हैं, फिर भी आप हमें अब तक आत्मसात नहीं कर सके । कश्मीर के सभी मुसलमानों को आत्मसात् करने की शक्ति सवर्ण हिन्दुओं में है क्या? आपकी (सवर्ण हिन्दुओं की) पाचनशाक्ति का अनुमान करने के बाद ही मैंने कहा था कि, यह विदेशी तत्व राष्ट्र शरीर के अंदर रहने देने के बजाय इसे बाहर कर देना श्रेयस्कर होगा ।”
उनका यह निष्कर्ष विवाद का विषय हो सकता है । मैंने इस संदर्भ मैं जो कुछ कहा उन्होंने एक अज्ञानी युवक के विचार जैसा ही महत्व दिया । उस समय भी यह निश्चत ही अनुभव हुआ कि बाबासाहब का निष्कर्ष वर्तमान हिन्दू समाज क पाचन- शाक्ति का दु:खद भाष्य है ।
फरवरी, १९४२ मे बम्बई के वागले हॉल में “थॉट्स ऑन पाकिस्तान” विषय पर बोलते हुए बाबासाहब ने कहा था, “जो पाकिस्तान के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों के साथ वाद-विवाद करने मे कोई लाभ नहीं है । उन्हें यदि पाकिस्तान का निर्माण अन्याय प्रतीत हो रहा होगा तो पाकिस्तान बनना उनके लिए एक भयंकर घटना सिद्ध होगी । लोगों को इतिहास भुला देने के लिए कहना एक भारी भूल होगी, क्योंकि इतिहास को भुलाने वाले इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते । भारतीय सेना को मुसलमानों के प्रभाव से मुक्त करके सेना को एकरस और राष्ट्रभक्त बनाना ही बुद्धिमानी होगी, अपनी मातृभूमि की रक्षा हमीं करेंगे । यह धारणा बिल्कुल निराधार है कि पाकिस्तान बन जाने पर मुसलमान सम्पूर्ण हिन्दुस्थान पर अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे । यदि वे ऐसा करेंगे तो हिन्दू उन्हें धूल चटा देंगे । इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि स्पृश्य हिन्दुओं से मेरा संघर्ष होता रहता है, मैं आप सब लोगों के सम्मुख यह प्रतिज्ञा करता हूं कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी अर्पण कर दूंगा ।”
बाबासाहब अम्बेडकर की कुछ सांकेतिक निषेधात्मक कार्यवाही से सनातनी हिन्दुओं का उत्तेजित होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें भी बाबासाहब को मनोभूमिका को समझने का प्रयत्न करना चाहिए ।
कलाकार को अपनी कलाकृति और साहित्यकार को अपनी रचना के प्रति अपनत्व अनुभव होना स्वाभाविक होता है । बाबासाहब ने भी भारत के संविधान का निर्माण किया था । सम्पूर्ण राष्ट्र ने उन्हें “आधुनिक भारत के मनु” के रूप में गौरवान्वित किया । यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी । ध्येय समर्पित जीवन होने के कारण इस गौरव को उन्होंने अतीव निर्लिप्त भाव से स्वीकार किया । संविधान के निर्माण में भी उन्होंने ध्येय के लिए अनुकूल व्यवस्था की । यदि यह संभव न होता तो केवल “आधुनिक मनु” के रूप में गौरवान्वित होने में उन्हें कभी संतोष न होता । स्वयं निर्मित संविधान के प्रति उनमें दिखावटी प्रेम नहीं था । संविधान में जो कमियां रह गई थीं, वे उन्हें भलीभांति जानते थे । उनकी सूक्ष्म दृष्टि का एक उदाहरण देखिए । उन्होंने कहा था : –
“छब्बीस जनवरी, ११५० को हम एक अन्तर्विरोधों से युक्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं । राजनीति में हम समानता की दुहाई देंगे किन्तु हमारे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता विद्यमान होगी । राजनीति में हम एक मनुष्य का एक मत, और एक मत का एक ही मूल्य वाले सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे तो दूसरी ओर हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में इसी सिद्धान्त की धज्जिया उड़ाते रहेंगे । अन्तर्विरोधों से भरपूर इस प्रकार का जीवन हम कब तक जीते रहेंगे । अपने सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में समानता को अपनाने से हम कब तक इंकार करते रहेंगे? यदि अधिक समय तक हम समानता को स्थापित करने का विरोध करते रहेंगे तो अपने जनतंत्र को ही संकट में डाल देंगे । इसलिए इन अन्तर्विरोधों को हमें अविलम्ब दूर करना होगा अन्यथा इस संविधान निर्मात्री समिति के द्वारा परिश्रमपूर्वक निर्मित इस जनतंत्र के ढांचे को विषमता से पीड़ित लोग विध्वंस कर डालेंगे ।”
अपनी ध्येय-पूर्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध होने वाली प्रत्येक बात पर निर्णायक हमला करना उनका स्वभाव था । उनके द्वारा किए गए मनुस्मृति के दाह से सनातनी बंधुओं का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था । लेकिन इस प्रकरण में उन्हें बाबासाहब की मनोभूमिका का भी विचार करना चाहिए था । वे यह भी कहा करते थे कि “यदि मेरे द्वारा निर्मित भारत का संविधान भी मेरी ध्येय-पूर्ति में बाधक बनेगा उसे भी जलाने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा ।”
२ सितम्बर, १९५० को संविधान सभा में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था, “बहुमत वाली सरकार के अनुरोध पर मैंने इस संविधान का निर्माण किया । मुझे जनमत का ध्यान रखकर संविधान का निर्माण करना पड़ा । इसके लिए मैं विवश था । भारत के संविधान में अछूतों की सुरक्षा के विशेष अधिकार राज्यपाल को न होने से यदि उनकी रक्षा न हुई तो मैं ही इस संविधान को भस्म करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा ।”
जो निष्कर्ष उन्होंने मनुस्मृति पर लागू किया वही स्वयं निर्मित “भीमस्मृति” अर्थात् भारतीय संविधान पर भी लागू किया । इस बात को समझ लेने पर बाबासाहब के प्रति उत्पन्न अनेक दुराग्रहों से मुक्त होने में सहायता मिलेगी ।
बाबासाहब अम्बेडकर के समस्त विचारों का अधिष्ठान धर्म था । अर्थात् धर्म के नाम पर ही ब्राह्मण वर्ग ने बहुजन समाज का शोषण किया । उनके लिए ज्ञान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के द्वार बंद करके उन्हें चिरकाल तक धार्मिक दासता में रखने का प्रबन्ध करके अपने निहित स्वार्थ सदा के लिए सुरक्षित किए । ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वे इस प्रकार की कटु आलोचना किया करते । फिर भी वे यह कहते थे कि “इसमें दोष ब्राह्मणों का है, धर्म-कल्पना का नहीं ।” उनका कहना था कि “दुनिया में कम्युनिस्टों को छोड़कर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा, जिसे धर्म की आवश्यकता नहीं है । अतएव धर्म हमें भी चाहिए लेकिन वह सद्धर्म हो । जहां लोग समानता का अनुभव कर सकें, जहां सभी को अपनी उन्नति के अवसर समान रूप से उपलब्ध हों, वही यथार्थ धर्म है । अन्य सभी अधर्म हैं । “हिन्दू तत्वज्ञान के अनुसार यदि सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है तो वह मेहतर और चमार में भी होना चाहिए । फिर हिन्दू धर्म में असमानता और विषमता क्यों? भगवान् बुद्ध का महाप्रयाण हुए दो हजार से अधिक वर्ष बीत चुके हैं । अभी भी इस धर्म का विस्तार हो रहा है । उसका न तो कोई शास्ता है और न ही कोई सर्वाधिकारी । भगवान् बुद्ध से अन्तिम समय में उनके शिष्यों ने पूछा, “भगवान, आपके महाप्रयाण के पश्चात इस धर्म का क्या होगा? आप किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए । भगवान् बुद्ध ने कहा, “मेरे पश्चात धर्म ही तुम्हारा शास्ता रहेगा । यदि आप लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं । भिक्षुओ, विशुद्ध मन से स्वीकार किए हुए धर्म को ही अपना शास्ता समझो ।”
दुनिया के सब व्यवहार धर्म से नियंत्रित होते है । किसी मां को उसके नवजात पुत्र के विषय में यह बताया जाय कि यह तेरा पुत्र ही तेरा शत्रु है, तू इसे स्तनपान मत करा, इससे तू दुर्बल होगी जल्दी वृद्ध होगी, तेरा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, तेरा यह पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा”, तो क्या वह मां बातों को मानेगी? कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी अस्वस्थ हो, फिर भी वह अपने बालक को स्तनपान कराए बिना नहीं रह सकती । संतान का भरण-पोषण करना ही उसका धर्म है । दुनिया के सारे व्यवहार इसी धर्म से चला करते हैं ।
पुणे के विभित्र कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को प्रतिदिन टिफिन पहुंचाने वाले स्वयं आधापेट रहते हुए भी टिफिन में यदि मिष्टान्न भी हो तो उसे खाने की इच्छा नहीं करते । उनकी यह कर्तव्य-बुद्धि, यह प्रामाणिकता ही धर्म है । इस प्रकार मनुष्य के सभी व्यवहार धर्म के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं । इसलिए धर्म का पालन सभी को करना चाहिए । लेकिन वह सद्धर्म हो, अधर्म नहीं । हमें सुकर्म चाहिए, दुष्कर्म नहीं ।”
एक बार भगवान बुद्ध से उनके विशाख नामक शिष्य ने प्रश्न किया, “धर्म किसे कहते है ?” उत्तर मिला, “मलिन मन को निर्मल करना ही धर्म है ।”
अस्पृश्यता मार्ग का कोई ऐसा रोड़ा नहीं है कि समाज सुधारक उसे मार्ग से अलग कर सकें । मानसिकता में परिवर्तन आने से ही यह समस्या हल होगी ।
शिक्षा का महत्व अवश्य है । परन्तु उससे भी अधिक महत्व है चारित्र्य और शील का, इसके अभाव में शिक्षा आत्मघातक भी बन सकती है । चारित्रय और शील का उद्गम धर्म में से ही होता है।
छह फरवरी, १९५४ को श्री अत्रे की “महात्मा फुले” फिल्म का उद्घाटन करते हुए बाबासाहब ने कहा था, “आज देश में सर्वत्र चारित्र्य का अभाव है । जिस देश में राष्ट्रीय चारित्र्य न हो उस देश के भविष्य पर प्रश्न-चिह्न लग जाता है । चाहे श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हों, चाहे और कोई, चारित्र्य के अभाव में देश का भविष्य अंधकारमय ही होगा । जिसे धर्म के यथार्थ में बोध हुआ हो, वही देश का उत्थान कर सकता है । महात्मा फुले ऐसे ही धर्म सुधारक थे । विद्या, प्रज्ञा करुणा, शील तथा मैत्रीभाव आदि धर्मतत्वों के आधार पर ही व्यक्ति को अपने चरित्र का गठन करना चाहिए । करुणा-शून्य विद्वान व्यक्ति को मैं कसाई समझता हूं । करुणा का अर्थ है मानव मात्र पर प्रेम । मनुष्य को इससे भी आगे जाना होगा ।”
तेरह जून, १९५३ को बम्बई के वरली कैम्प की महिलाओं केसमक्ष भाषण देते हुए बाबासाहब ने कहा था, “प्रत्येक मनुष्य को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना होगा……. हमने धर्म के लिए सत्याग्रह किया । धर्मान्तरण करने का प्रस्ताव पारित किया । हम सबकुछ कर चुके । अब हमें अपने मन को पवित्र करना होगा । सदगुण प्राप्ति का हमें प्रयास करना होगा । अर्थात् हमें अब धार्मिक बनना होगा । केवल शिक्षित होना ही सबकुछ नहीं है । शील अर्थात् सच्चरित्रता धर्म का अविभाज्य अंग है ।
धर्म दुराचरण को नियंत्रित करता है । आप लोगों की समझ में आ सके, इसके लिए मैं बैलगाड़ी का उदाहरण देता हूं । बैलगाड़ी में दो पहिए, दो बैल तथा एक उसे हांकने वाला होता है । गाड़ी के पहियों की धुरी में समय-समय पर तेल देना पड़ता है जिससे गाड़ी आसानी से चलती रहे । बैलगाड़ी की धुरी के समान व्यक्ति के जीवन-रथ की धुरी का काम करता है “धर्म” । “धर्म” के बंधन के बिना कोई भी कार्य स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता ।”
श्रद्धेय बाबासाहब भौतिक-आर्थिक उन्नति का महत्व भी जानते थे । वे यह जानते थे कि “मनुष्य को धर्म तथा अर्थ, दोनों की आवश्यकता होती है । लेकिन वे इस बात पर जो भी जोर देते थे कि केवल अर्थ अर्थात् समृद्धि अनर्थ का कारण बनेगी । धर्माधिष्ठित अर्थोपार्जन ही श्रेयस्कर है । धर्म की सबसे अधिक आवश्यकता पददलितों को है । संसार में धर्म की आवश्यकता का अनुभव समाज के निम्न श्रेणी के लोगों को ही हुआ । रोमन, इटालियन साम्राज्य में ईसाई धर्म को सर्वप्रथम गरीबों ने ही अपनाया ।”
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बाबासाहब अम्बेडकर का प्रेरणा-स्रोत विदेशी नहीं, विशुद्ध भारतीय था । धर्म ही उसका अधिष्ठान था । वे सद्धर्म चाहते थे, अधर्म नहीं । शताब्दियों से पददलित, परन्तु अब जाग्रत हो रहे समाज की स्वाभाविक प्रवृत्ति, प्रतिशोध, प्रतिकार तथा आक्रमण की ही हुआ करती है । इससे देश की एकात्मकता खण्डित होने के साथ ही शांति और व्यवस्था भी भंग होती है । बाबासाहब के अनुयायियों में भी प्रतिशोध की भावना रखने वाले लोग थे । बाबासाहब उन्हें समझाते थे कि “भैया रे, यह आत्मघात का मार्ग है । कुछ लोग कहते हैं कि दलित फेडरेशन आक्रामक नीति नहीं अपनाता है । आक्रामक नीति का अर्थ क्या है? आक्रामक नीति हमारे लिए हितकर है क्या? हमने यदि आक्रामक नीति अपनाई तो उसके परिणाम हमको ही भुगतने होंगे । हमारे कारावास में जाने के बाद वे लोग आपको यातना देंगे । कहेंगे, आप लोग अम्बेडकर का साथ देते हैं न । अत: आप सबको सबक सिखाया जाएगा । इससे संघर्ष के बजाय आप लोग कष्ट उठाएं, अपना मन निर्मल करें, भेदभाव इससे दूर होगा ।”
ग्यारह जनवरी, १९५० को बम्बई के नरेस पार्क की सभा में अपने सार्वजनिक सम्मान के अवसर पर बाबासाहब ने कहा, “वर्तमान राजनीति की मैं इस समय चर्चा नहीं करूंगा, फिर भी कुछ बातों का उल्लेख अवश्य करूंगा । “
प्रारम्भ में हमारी राजनीति शत्रुता से प्रेरित थी । मेरी दृष्टि में प्रारम्भ में अस्पृश्य वर्ग के सभी नेता कुछ संकुचित दृष्टि के थे और उनके द्वारा वैसा ही व्यवहार भी होता था । मैं भी थोड़ा बहुत इसके लिए उत्तरदायी था । लेकिन अब इसे बदलना होगा ।
हमें अब एक बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी कि हम अपने लोगों अर्थात् अपने समाज के हितसाधन में लगे थे । इसे आगे भी चलाते रहना होगा । लेकिन इसी के साथ हमें अब इस बात का भी विचार करना होगा कि हम अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार करेंगे? पूर्व काल में अपना देश स्वतंत्र होने के बाद पुन: पराधीन हुआ था । पहले मुसलमानों ने और फिर अंग्रेजों ने हमें अपने अधीन किया । स्वतंत्रता की आवश्यकता जितनी उच्च वर्ग को है, उतनी ही निम्न वर्ग को भी है । अंग्रेजों की दासता से हम मुक्त हुए है । अब यदि पुन: पराधीन हुये तो यह हमारा अत्यंत दुर्भाग्य होगा । इसीलिए अपने देश की स्वतंत्रता कि रक्षा करना में अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए ।”
भारत के पददलित वर्ग को कम्युनिस्टों की सफलता से प्रभावित होने की संभावना को देखकर बाबासाहब उन्हें चेतावनी देते हुए कहते है : ”साम्यवाद की सफलता रो भ्रमित न हों । मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान् बुद्ध को प्राप्त ज्ञान का यदि एक दशांश प्रकाश भी हमें प्राप्त हुआ तो हम प्रेम, ज्ञान और सद्भाव के द्वारा वही परिणाम प्राप्त कर सकेंगें।
बाबासाहब जनतंत्र के प्रबल समर्थक थे । वे कहा करते थे, ”जिस शासन पद्धति से रक्तपात के बिना समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सके, वही यथार्थ में जनतंत्र है ।” उनके कम्युनिज्म के विरोध का यह भी एक कारण था । विशुद्ध भौतिकवाद उन्हें नहीं सुहाता था ।
भौतिक सुख में आकण्ठ डूबे हुए समाज के सम्बन्ध में वे कहा करते थे, “भौतिक सुख ही मानव का सब कुछ नहीं है । उसके प्राप्त होने पर भी मानव के दु:ख का अन्त नहीं होगा । मनुष्य केवल रोटी के लिए ही नहीं जीता, उसे सुसंस्कृति की भी आवश्यकता रहा करती है ।”
मार्क्सवादियों से वे कहते हैं : मनुष्य जीवन का लक्ष्य रोटी प्राप्त करना नहीं है । उसके पास मन भी है । मन को विचारों की खुराक चाहिए । धर्म मनुष्य के हृदय में आशा का संचार कराता है । उसे कार्य प्रवृत्त करता है । पददलितों के उत्साह पर हिन्दू धर्म ने तुषारापात किया है । इसी कारण मुझे बौद्ध धर्म अपनाने की आवश्यकता पड़ी, और मैंने बौद्ध धर्म अपनाया । बौद्ध धर्म कालातीत है । वह किसी भी देश में फल-फूल सकता है । जिस देश के लोग मानसिक संस्कारों के बजाय भौतिक समृद्धि को ही प्रधानता देते हैं, ऐसे देश से मैं सम्बन्ध नहीं रखूंगा । यदि हिन्दू धर्म ने दलित वर्ग को शस्त्रधारण करने की छूट दी होती तो यह देश कभी भी गुलाम नहीं होता ।”
नागपुर के दीक्षा समारोह के समय बाबासाहब ने कहा था, “मानव मात्र के कल्याण के लिए धर्म की अत्यंत आवश्यकता रहा करती है । मैं जानता हूं कि कार्ल मार्क्स की प्रेरणा से एक पंथ का निर्माण हुआ है । उसके कथनानुसार ”धर्म” अफीम के समान है । मनुष्य के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । उसकी दृष्टि में उनका सम्पूर्ण तत्वज्ञान यह है कि मनुष्य को सुबह के नाश्ता में पावरोटी, मक्खन, दोनों समय के भोजन में मुर्गी की टांग, भरपेट भोजन और गहरी नींद मिल जाय तो मनुष्य ने सब कुछ पा लिया । मैं इसे नहीं मानता ।”
सितम्बर, १९३७ में मैसूर में सम्पन्न दलित वर्ग के जिला सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में बाबासाहब ने कहा था : “मेरे कम्युनिस्टों से मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता । अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले कम्युनिस्टों का मैं जानी दुश्मन हूं ।” पुस्तकों के कीड़े इन कम्युनिस्टों को देश की धड़कन का पता नहीं है । वे कहते हैं : “भारत का श्रमजीवी वर्ग, गरीब होने पर भी, क्या यह कहा जा सकता है कि वह अमीर और गरीब के अतिरिक्त कोई भेद नहीं जानता? क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का निर्धन वर्ग जाति, पंथ, ऊंच-नीच के भेद को नहीं मानता? वर्गभेद के अतिरिक्त यदि वे अन्य भेद भी मानते हैं, और यह वस्तुस्थिति है तो फिर ऐसा श्रमजीवी वर्ग, सम्पन्न वर्ग के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्ष के लिए एकजुट कैसे होगा? और यदि श्रमजीवी एकजुट नहीं हो सके तो क्रान्ति कैसे संभव होगी ।” (एन्निहिलेशन ऑफ कास्ट, पृ० १८)
बाबासाहब के तत्वज्ञान का मूल स्रोत धर्म था । संवैधानिकता तथा जनतांत्रिकता उनके स्वभाव में थी । भगवान् बुद्ध, महात्मा कबीर तथा ज्योतिबा फुले – तीनों उनके गुरु स्थान पर थे । विद्या, विनय और शील उनके लिए आराध्य देव के समान थे । ऐसी मानसिक पृष्ठभूमि का महापुरुष हमें तथाकथित अस्पृश्य वर्ग से प्राप्त हुआ, इसे देश का सौभाग्य ही कहना होगा ।
बाबासाहब के विषय में ऐसी अनेक गलत धारणाएं प्रचलित थीं जिनका कोई आधार नहीं था । यहां पर कुछ नमूने प्रस्तुत हैं :
महाराष्ट्र में श्री गोपाल गणेश आगरकर आदि लोगों ने समाज सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी । राजनीति से अधिक वे समाज सुधार को महत्व देते थे । इसका मतलब यह नहीं कि वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए बेचैन नहीं थे । लेकिन ऐसा होने पर भी समाज सुधारकों के सम्बन्ध में उस जमाने में अनेक भ्रान्त धारणाएं फैलाई गई थीं । बाबासाहब के सम्बन्ध में भी यही हुआ ।
यह एक भ्रान्त धारणा है कि बाबासाहब स्वराज्य के विरोधी थे । किन्तु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था : “स्वराज्य में संविधान के माध्यम से शासन पर अधिकार करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे । शासन पर अधिकार किए बिना आप अपने लोगों का उत्थान कर सकेंगे । अपने लोगों के अधिकाधिक कल्याण का विचार करो और मुझे विश्वास नहीं है कि आप लोग स्वराज्य प्राप्ति को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करेंगे ।”
गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने अपनी इसी भूमिका को स्पष्ट किया था कि “हमें ऐसा शासन अपेक्षित है, जिसमें शासक लोग देश के हित को ही सर्वोपरि मानकर अपनी समग्र निष्ठा उसे समर्पित करें । हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जिसमें सत्तासीन लोगों को इस बात का विवेक हो कि नियम के पालन की सीमा-रेखा क्या है और प्रतिकार का प्रारम्भ कहां से होता है, और जो सरकारे न्याय और विवेक के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक कानूनों में संशोधन करने में नहीं हिचकिचाएगी ।”
स्वराज्य प्राप्त करना उनका भी ध्येय था । लेकिन उस स्वराज्य के संविधान में दलितों का क्या स्थान होगा, इस प्रश्न को वे सर्वाधिक महत्व देते थे ।
भगवा ध्वज के विषय में उनकी भूमिका श्री धनंजय कीर के शब्दों में ही देनी उचित होगी । श्री कीर कहते हैं : “डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर संविधान समिति की ध्वज समिति के भी सदस्य थे । संविधान समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक लेखन समिति का गठन करके डॉ. अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाए जाने के पहले की यह बात है । वे ३ जुलाई, १९४७ को दिल्ली से बम्बई आए थे । उस समय राष्ट्रध्वज के स्वरूप पर सर्वत्र जोरों से चर्चा चल रही थी । कुछ महाराष्ट्रियन तथा बम्बई प्रांतीय हिन्दू सभा के कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलकर उन्हें राष्ट्रध्वज का रंग भगवा रखने का सुझाव दिया । डाँक्टर साहब ने कार्यकर्ताओं से कहा, “यदि प्रभावशाली लोग इसके लिए प्रभावी जनमत का निर्माण करेंगे तो झंडा समिति में ध्वज का रंग भगवा रखने के प्रश्न को मैं उठाऊंगा ।” डॉ. साहब ने यह आश्वासन श्री अनंतराव गद्रे, प्रबोधनकार ठाकरे तथा मराठा मंदिर के श्री गावडे को दिया था । १० जुलाई को जब डॉ० अबेडकर बम्बई से दिल्ली जाने के लिए निकले तो सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर बम्बई प्रान्तीय हिन्दू सभा तथा मराठा समाज के कुछ नेताओं ने डॉ० अम्बेडकर को एक भगवा ध्वज भेंट किया था । उस समय उन्होंने कहा था, “भगवा ध्यज के लिए यदि कोई आन्दोलन हुआ तो उसे मेरा समर्थन रहेगा ।” हिन्दू सभा के नेता श्री बाबासाहब बोले तथा श्री अनंतराव गद्रें से डॉ० अम्बेडकर ने कहा, “एक महार के पुत्र के द्वारा आप संविधान समिति पर ध्वज लगाने की अपेक्षा कर रहे हैं, यह ठीक है न ?” बाद की घटनाएं सर्वविदित हैं । डॉक्टर साहब की अपेक्षानुसार भगवे ध्वज के लिए कोई आन्दोलन नहीं हो सका ।
बाबासाहब ने अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भिक काल में समरसता की भावना जगाने का विशेष प्रयास किया था । वे इस बात को जानते थे कि केवल सवर्ण समाज का विरोध फलदायी नहीं होगा । बडोदरा के महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ तथा राजे शाहू छत्रपति के द्वारा अस्पृश्योद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों की उन्हें जानकारी थी । आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, थिओसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं के द्वारा अस्पृश्योद्धार के लिए किए जा रहे कार्य से भी वे परिचित थे । सवर्ण हिन्दुओं के सार्वजनिक नेताओं के द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए की गई घोषणाओं का भी उन्हें ज्ञान था । इसी कारण २० जुलाई, १९२४ को बम्बई में स्थापित बहिस्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के पद पर उन्होंने श्री चिमनलाल सीतलवाड़, रंगलेकर पराजपे, बालासाहब खेर जैसे उच्चवर्णीय व्यक्तियों को रखा था । इस संस्था में अन्य उच्चवर्णीय लोगों को भी लिया गया था । अपनी भूमिका स्पस्ट करते हुए बाबासाहब ने कहा था : “जिस वर्ग के उत्थान के लिए संस्थाएं निर्माण की जाती हैं, उस वर्ग के अथवा उसी प्रकार की परिस्थिति से पीड़ित वर्ग के कार्यकर्ताओं को संस्थाओं में लिए बिना उन संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं हो सकती, यह मान्य करने पर भी जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, वे यह भलीभांति जानतें हैं कि उच्च वर्ण के सम्पत्र तथा सहानुभूति रखने वाले लोगों की सहायता के बिना अस्पृश्य वर्ग के उत्थान का यह प्रचण्ड कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, और ऐसा न करना अपने ही बंधुओं के उत्थान के इस महान कार्य को हानि पहुंचाने के समान होगा ।” प्रारम्भ में बाबासाहब की यही भूमिका थी । लेकिन अपने आपको धर्म के ठेकेदार समझने वाले कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण उन्हें अपनी भूमिका में परिवर्तन करना पड़ा ।
बौद्ध धर्म अपनाने के बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व धर्मान्तरण की चर्चा के समय स्वातंत्र्य वीरसावरकर, डॉ० मुंजे व कांची शंकराचार्य आदि हिन्दुत्ववादी नेताओं के आग्रह पर बाबासाहब ने सिख धर्म अपनाने का निर्णय किया था । उस समय भी उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि “इस्लाम अथवा ईसाई मत को स्वीकार करने पर धर्मान्तरित लोग राष्ट्रविरोधी हो जाएंगे ।” हिन्दू सभा के नेताओं से उनके सम्बन्ध थे । लेकिन उनका मत था कि सनातनी वर्ग पर हिन्दू सभा की पकड़ नहीं है और जिनका उस पर प्रभाव है वे लोग हिन्दू सभा के नेताओं जैसे विचार नहीं रखते । इस बात का उन्हें दु:ख था कि इसी कारण समाज में मान्यता प्राप्त लोगों का हृदय परिवर्तन करने में अपने को सफलता नहीं मिलती ।
यथास्थितिवादियों की हठवादिता के कारण जीवन के संध्याकाल में बाबासाहब को यद्यपि प्रतिक्रियात्मक भूमिका निभानी पड़ी , यह सत्य होने पर भी उनकी भूमिका मूलत: समन्वयात्मक थी । इसे स्वीकार करना होगा । इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । सन् १९३० में उनके द्वारा प्रतिपादित भूमिका देखिए । भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम० एच० बेग तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस ने अभी ऐसा सुझाव दिया है कि “अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय एकात्मकता एवं मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाय ।” उनके इस सुझाव का सर्वत्र स्वागत किया गया । लेकिन न्यायमूर्ति बेग के इस सुझाव के ५४ वर्ष पूर्व उस समय की अत्यंत विषम परिस्थिति में भी बाबासाहब ने भी इसी प्रकार के विचार रखे थे । उनकी इस बात को लोगों ने भुला दिया है कि “यह समाज अनेक जाति और पंथो में विभक्त है । अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की संविधान में व्यवस्था किए बिना यह समाज एकरस और स्वयंशासित समाज के रूप में खड़ा नहीं हो सकेगा । इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । लेकिन अल्पसंख्यकों को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जातियों और पंथों के कारण विभक्त होने पर भी हमारा ध्येय अखण्ड और एकात्म भारत का निर्माण करना ही है । इस लक्ष्य में बाधक बनने वाली किसी भी प्रकार की मांग अल्पसंख्यकों की ओर से नहीं आनी चाहिए ।”
इस भूमिका में बाबासाहब ने जिस संतुलन का परिचय दिया है, वह सराहनीय है । स्पष्ट है कि यदि यथास्थितिवादियों ने बाबासाहब को निराश न किया होता तो उनकी योग्यता तथा कर्तव्य का और अधिक रचनात्मक लाभ देश को मिलता ।
भारतीय परिस्थिति में सामाजिक समता की समस्या अत्यंत उलझनपूर्ण बन गई है और उसे बहुआयामी स्वरूप प्राप्त हो गया है । इसका सम्यक ज्ञान न रखने वाले सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने में लगे हुए राजनीतिक नेताओं के उत्तेजना फैलाने वाले आन्दोलनों से यह समस्या अधिकाधिक उलझती जा रही है । फिर भी परिवर्तित परिस्थिति की पृष्ठभूमि में इस समस्या के सम्बन्ध में विचारवान लोगों के द्वारा निकाले जाने वाले निष्कर्ष दोनों पूजनीय डाक्टरों (डाक्टर अम्बेडकर और डाक्टर हेडगेवार) के सुचिंतित निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं । उदाहरण के रूप में अभी-अभी प्रकाशित “कम्पीटिग इक्वलिटीज” नामक ग्रंथ में मार्क गलैण्टर ने भारत में हो रहे सामाजिक अन्याय, उसके विरुद्ध हुए विद्रोह, संविधान में निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब तक किए गए सवैधानिक आन्दोलनों का इतिहास और उससे उत्पन्न विवादों में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दिए है ।
ग्रंथ के प्रारम्भ में ही श्री गलैण्टर ने लिखा है : “अतीतकाल से समाज के जो वर्ग पीड़ित और शोषित रहे हैं, उन वर्गों को विशेष राहत देने की भारतीय पद्धति की व्याप्ति तथा उसका विस्तार अभूतपूर्व है । भारत ने समाज में प्रचलित विषमता की बारीकियों का सुस्पष्ट और मूल्यात्मक अध्ययन करके समानता को मूलभूत रूप से स्वीकार किया है । समाज के विभिन्न वर्गों मे बद्धमूल विषमता की भावना को समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है । परिणामस्वरूप, इस प्रकार की अनेक योजनाएं बनाई गई, जिनको मैं क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाने वाला भेदभाव कहता हूं । समाज के एकदम निम्नतम स्तर के वर्ग की उपेक्षा करने की राष्ट्र की प्रवृत्ति को देखकर यही कहा जा सकता है कि विगत तीस वर्षों में क्षतिपूर्ति के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव की यह नीति बड़े आग्रह के साथ निरंतर क्रियान्वित की जा रही है । यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कार्यान्वयन हमेशा कठोरता तथा प्रभावी ढंग से किया गया है ।”
किसी विदेशी विद्वान के द्वारा भारत की इन उलझन भरी आंतरिक समस्याओं का इतना परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया जाना निश्चित रूप से सराहनीय है । इसके लिए भारतवासी उसके प्रति कृतज्ञ हैं । लेकिन इस देश के समाज की धड़कन का ज्ञान न होने तथा अमेरिका के नीग्रो वंश के उत्थान के लिए किए गए अमेरिकन प्रयासों के इतिहास की पृष्ठभूमि मन में होने के कारण इन समस्याओं के मूल में पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो सका । फिर भी गहन अध्ययन के पश्चात निम्नलिखित निष्कर्ष तक वे पहुंच सके कि “सर्वसाधारण समता और क्षतिपूर्ति के न्याय के प्रश्न से जो परस्पर विरोधी मांगें उठ रही हैं, उनकी जटिलताओं को ध्यान में रखकर निर्माण होने वाले संभावित अनिष्ट परिणामों को न्यायालय ही अपने संतुलित निर्णयों के द्वारा टाल सकते हैं । लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का जो मूल्य चुकाना पड़ेगा अथवा उसके परिणामस्वरूप जो अपेक्षा भंग होगी उसका सामना करने की पर्याप्त क्षमता का परिचय संभवतया न्यायालय नहीं दे सकेंगे ।”
शासकीय सेवाएं, शिक्षा तथा राजपत्रित अधिकारियों की आरक्षण सम्बन्धी नीतियों के कारण उठे देशव्यापी तूफान के संदर्भ में उठ रही जातीय समस्याओं अप्रभावकारिता की गंभीरता तथा व्याप्ति की कल्पना ध्यान में आती है । उपर्युक्त ग्रंथ से यह स्पष्ट होता है कि संविधान, कानून और न्यायालयों के द्वारा सामाजिक न्याय तथा तदन्तर्गत सामाजिक समता सुलझनी संभव नहीं है ।
“इक्वलिटी एण्ड इनइक्वलिटी थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस” शीर्षक से एक नया ग्रंथ प्रकाशित हुआ है । इसका सम्पादन श्री आन्द्रे बतील (मण्ताट प्तवटा1०) ने किया है । ग्रंथ में इस विषय के विद्वानों के लेखों का संग्रह है । इसमें विषय के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । उस ग्रंथ में संकलित लेखों से यह स्पष्ट होता है कि केवल संविधान में संशोधन करने अथवा कानून बनाने से “सामाजिक समता” निर्माण नहीं हो सकती । इस ग्रंथ का निष्कर्ष है कि सार्वजनिक शिक्षा की कमियों को कानून से दूर नहीं किया जा सकता । सम्पादक महोदय अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं : “भारतीय लोग सामाजिक समता के आदर्श को प्रभावी ढंग से व्यवहार में ला सकते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि उनके द्वारा निर्मित की जाने वाली संस्थाओं के पालन में वे कितनी दृढ़ता से जुटते है ।”
जो लोग इस समस्या की ओर निष्पक्ष तथा अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं, ऐसी लगन वाले विचारकों में से एक विद्वान डा. शिवरामैय्या की यह प्रतिक्रिया है कि “संविधान के मूलभूत अधिकारों में समानता के आधारभूत कानून के समाविष्ट किए गए प्रावधान और शासन के निदेशक सिद्धान्त में जो परस्पर विरोध और विसंगति है उसके कारण अवरोधों में वृद्धि हुई है । इनमें से अधिकांश विसंगतियों का निर्माण साधनों के अभाव में से हुआ है । इस अभाव के कारण एक ओर समाज के दुर्बल घटकों के प्रति कर्तव्य की पूर्ति तथा दूसरी ओर उनमें गुणवत्ता का निर्माण करना शासन के लिए संभव नहीं हो पाता । ऐसी स्थिति में निदेशक सिद्धान्त अभावग्रस्त लोगों का उपहास ही प्रतीत होते हैं । बेरोजगार लोग काम का अधिकार किस प्रकार प्राप्त करें अथवा साधनहीन लोगों को न्याय प्राप्ति के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता किस प्रकार प्राप्त हो, इसका कोई समाधान निदेशक सिद्धान्तों में उपलब्ध नहीं है ।”
संविधान के अनु.१६ में उपबंधित समता की गुणवता पर आधारित तथा विशिष्ट प्रमाण को निश्चित करने वाली कल्पना का जो संतुलन रखा गया है उसमें से कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं । समान अवसर की गुणवत्ता पर आधारित अधिकार यदि व्यक्ति को न्याय प्रदान करने वाला हो तो सुरक्षित स्थान रखने वाला भेदभाव विशिष्ट वर्ग का पक्षपात करने वाला प्रतीत होता है । प्रथम प्राप्त अधिकार यदि न्यायालय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो दूसरे प्रकार का अधिकार विधान सभाओं के नीति निर्धारण तथा शासन के द्वारा उनके क्रियान्वयन पर आधारित है । शासन के दोनों विभागों – न्यायपालिका और कार्यपालिका – द्वारा मूलभूत अधिकारों के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर विशेष जोर देने के कारण कभी-कभी संघर्ष के प्रसंग भी उत्पन्न होते हैं ।”
इस ग्रंथ की समालोचना में श्री श्यामलाल ने जो अभिप्राय व्यक्ति किया है वह एक प्रकार से ग्रंथ में प्रतिपादित विषय का समापन है । श्री श्यामलाल लिखते हैं : “इस ग्रंथ के लेखक सुलभ तथा संभ्रमित निष्कर्षों के प्रति सजग हैं । उनकी सारी उठापटक का उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करना है कि उलझी हुई परिस्थिति हमारी सामान्य कल्पना से भी अधिक पेचीदगियों से भरी हुई है । गरीबों के मसीहा बनकर एक विशिष्ट प्रकार के वक्तव्य देने वाले लोगों के बताए हुए उपायों से यह समस्या हल होने वाली नहीं है । ग्रंथ के लेखकों ने बार-बार इसी को ध्यान में लाने का प्रयास किया है । इस समस्या का समाधान न तो उदार गांधीवादी और न ही मार्क्सवादी सांचेबंद विचारों से होने वाला है । यह समस्या अपेक्षा से अधिक जटिल है ।”
इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि यह समस्या राजनीतिक आन्दोलन अर्थात् सतही उपायों से हल होने वाली नहीं है । इस प्रकार के उपाय तत्काल फलदायी भले ही प्रतीत होते हों, लेकिन सम्पूर्ण सामाजिक समता के निर्माण में वे अपर्याप्त ही हैं और भविष्य में भी अपर्याप्त सिद्ध होंगे । इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मौलिक और गहन चिंतन के प्रकाश में दीर्घकालीन व्यावहारिक उपाय योजना की आवश्यकता है । इसके अभाव में चुनाव जीतने के लिए मत भले ही मिल जाएंगे, लेकिन समस्या यथावत बनी रहेगी ।
उपरिनिर्दिष्ट दोनों भारतीय महापुरुषों (डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार) की वृत्ति संत तुकाराम जैसी थी । “सत्य-असत्य का विवेक द्वारा निर्णय करके बहुमत को अस्वीकार कर दिया ।”
इस कारण ये दोनों डाक्टर- डॉ. हेडगेवार तथा डॉ. अम्बेडकर – सुगम प्रतीत होने वाले उपायों के मोह से प्रभावित नहीं हुए । मूलगामी विचार द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने दीर्घकालीन उपाय-योजना से समस्या के स्थायी समाधान का मार्ग अपनाया । बाबासाहब का मानस किस प्रकार काम कर रहा था, इसकी कल्पना ऊपर दिए गए उदाहरणों से की जा सकती है । अत्यंत उत्तेजक वातावरण तथा विस्फोटक परिस्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन कायम रखते हुए शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक मार्ग से ही उन्होंने अपना आन्दोलन जारी रखा । अनेक बार उन पर हमले हुए । उनके अनुयायी भी जवाबी हमलों के लिए उतावले हो रहे थे । बाबासाहब ने यदि अपने अनुयायियों को संयम में न रखा होता तो भीषण दंगे भी हो सकते थे । ऐसी विषम परिस्थिति में भी उनके द्वारा सामाजिक समता का उद्घोष किया जाना उनकी महानता का परिचायक है । उनके सम्मुख समताधिष्ठित भारत का एक भव्य चित्र था । उनके मन में विशुद्ध देशभक्ति का भाव था । उन्होंने कहा था, “मेरे भारत में जयचन्द तथा राजा दाहिर के मंत्रियों जैसे लोग पैदा नहीं होंगे ।” उन्होंने सवर्ण लोगों को भी समझाने का प्रयास किया । लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्हें विवश होकर अन्य मार्ग अपनाने पड़े । फिर भी वे मार्ग धर्माधिष्ठित तथा संवैधानिक ही थे । उनके इस संयम, मानसिक संतुलन तथा विवेक का विचार करने पर उनके मनश्चक्षु के सम्मुख भावी भारत का जो चित्र था, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं ।
ऐसी विषम परिस्थिति में से मार्ग निकालने के लिए तात्कालिक उपचार के रूप में राजनीतिक हल का प्रयोग करना आवश्यक प्रतीत होने पर भी इस राष्ट्रीय रोग का बाबासाहब ने जो निदान किया था उसे जान लेना उचित होगा । उनका यह स्पष्ट मत था कि “हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि अपने देश में वर्ग संघर्ष, वर्गयुद्ध जैसी स्थिति का निर्माण न हो । सम्पूर्ण समाज में एकात्मता निर्माण होने पर ही सभी समस्याओं का हल हो सकेगा ।”
ध्यान देने की बात यह है कि एक विशिष्ट भूमिका को अपनाने के कारण उन्होंने सत्य के एक ही पहलू पर विशेष बल दिया है । (सत्य एक होने पर भी उसके कई पहलू होते हैं और विभिन्न लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है) । उन्होंने इस बात पर सबसे अधिक बल दिया कि वर्ग और जाति के आधार पर देश का विघटन न हो । लेकिन उच्चवर्गीय लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसी कारण विवश होकर बाबासाहब को सरकार तथा उच्चवर्ण के लोगों के विरुद्ध हरिजन बंधुओं को संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ा ।
सत्य के दूसरे एक पहलू पर बल देकर ऐसे ही एक महापुरुष ने, जिन्हें लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता डा. हेडगेवार के रूप में जानते हैं, इस समस्या को हल करने के लिए अन्य मार्ग का अवलम्बन किया । डॉ. हेडगेवारजी की भूमिका यह थी कि हमें वर्गभेद, जातिभेद और उससे उत्पन्न होने वाले संघर्ष नहीं चाहिए, यह तो ठीक है, लेकिन उन्हें समाप्त करने का मार्ग क्या है? यह कहना तो सरल है कि यह घातक है । इसे छोड़ा जाए । लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर यह दिखाई देगा कि निषेधात्मक भूमिका से अनेक बार प्रतिक्रिया का निर्माण होता है । “भेद भूलो भेद छोड़ो” कहने का एक प्रकार हो सकता है और दूसरा प्रकार है “हममें सतही भेद दिखाई देने पर भी हम एक ही अधिष्ठान पर खड़े हैं, इसलिए कि हम सब एक हैं ।” दृष्टिकोण में अन्तर आने से शब्द-रचना तथा मनोभूमिका में भी अन्तर हो जाता है । बात वही होने पर भी किसी बात पर विशेष बल देने तथा उसको प्रस्तुत करने की पद्धति में बदल करते ही मनोवैज्ञानिक परिणाम भिन्न हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में एक रोचक दृष्टान्त बताया जाता है । एक जादूगर ने गांव में जाकर यह घोषणा की कि “मेरे पास जादू की एक ऐसी लकड़ी है जिसे मंत्रोच्चार के साथ थाली में भरे जल में घुमाने से उस थाली का सारा जल सोने में परिवर्तित हो जाता है ।” इस प्रयोग का शुल्क अत्यल्प रखा गया है । यह सुनकर उसके पास लोगों की भीड़ जमा होनी स्वाभाविक थी । इतना सस्ता सौदा कौन नहीं चाहेगा? लेकिन उसके पास आने वालों से वह एक कर्मकाण्ड कराता, “स्नान करो, यहां बैठो, ऐसे बैठो, नेत्र मूंदों, जादुई लकड़ी हाथ में लो, मन को स्थिर करके मंत्र जपो ।” और अन्त में वह एक चेतावनी देता, “यह सब करने से अब जल सोने में परिवर्तित होने वाला है, केवल एक बात का ध्यान रखो कि आपके ध्यान में कहीं बंदर का स्मरण न आ जाए । बंदर का स्मरण आते ही मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और अभीष्ट परिणाम नहीं निकलेगा ।” मंत्रोच्चार के समय “बंदर को ध्यान में मत लाना ।” यह बताने के कारण जो भी व्यक्ति शुल्क देकर जादुई लकड़ी के साथ आसन पर बैठकर मंत्रोच्चार प्रारम्भ करता उसे हठात् बंदर का ध्यान आ जाता । पानी सोना न बनता तो वह व्यक्ति यह सोचता कि मंत्र तो शक्तिशाली है, लेकिन क्या करें, बंदर के ध्यान से वह प्रभावहीन हो गया । मेरे ही भाग्य में ही खोट है ।
तात्पर्य यह है कि उपदेश अच्छा होने पर भी यदि वह निषेधात्मक रूप में किया गया तो जिस बात का निषेध किया जाता है, वही बात मन में बैठ जाती है । इसलिए डॉक्टर हेडगेवारजी ने वर्ग-भेद, जाति-भेद आदि का निषेध करने के बजाय “हम सब एक है” की विधायक भूमिका को अपनाकर एकान्तिक प्रयोग प्रारम्भ किया । उन्होंने जातियों के अस्तित्व को ही मान्यता नहीं दी । कहा – “हम सभी हिन्दू हैं, कहां है अस्पृश्यता? हमारे लिए सभी हिन्दू के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं ।” उनकी इस भूमिका से समाज के हिताहित का निर्णय तो भविष्य में होगा, लेकिन आज तो इतना ही कहा जा सकता है कि यह अभिनव प्रयोग डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा प्रारम्भ हुआ । डॉक्टर हेडगेवार के इस प्रयोग से भगवान बुद्ध का उपदेश स्मरण हो आता है ,भिक्षु संघ का सम्बोधन करते हुए भगवान् बुद्ध ने कहा, “हे भिक्षुओ, तुम विभिन्न जातियों तथा विभिन्न देशों से यहां एकत्र आए हो । अपने प्रदेश में बहते समय सभी नदियों का पृथक अस्तित्व रहा करता है, लेकिन उनके समुद्र में मिल जाने पर अपना पृथकत्व खोकर वे महासागर कहलाने लगती हैं । बौद्ध संघ भी महासागर के समान है । इस संघ में सभी समान होते है ।”
डॉक्टर हेडगेवार जी का संघ भी सागर के समान है । दोनों डाक्टरों का लक्ष्य सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना था । लेकिन दोनों भिन्न परिस्थिति में होने के कारण लक्ष्य एक ही होते हुए भी वहां तक पहुंचने के मार्ग भिन्न रहे । दोनों ने भिन्न पहलुओं पर बल दिया । सन् १९३४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीत शिविर वर्धा में पूज्य महात्मा गांधी के आश्रम के पास ही लगा था । पूज्य बापू ने शिविर देखने की इच्छा प्रकट की । वर्धा के संघचालक श्रीमान् अप्पाजी जोशी ने शिविर में उनका स्वागत किया । पूज्य महात्मा जी ने बड़ी बारीकी से शिविर की व्यवस्था का निरीक्षण करने के पश्चात पूछा, “इस शिविर में हरिजन कितने हैं ?” अप्पाजी ने कहा, “यह बताना कठिन है, क्योंकि हम सभी को हिन्दू के रूप में ही देखते हैं और इतना ही हमारे लिए पर्याप्त होता है ।” पूज्य महात्मा जीने कहा, “क्या मैं आप के स्वयंसेवकों से पूछताछ कर सकता हूं ?” अप्पाजी ने कहा, “जैसी आपकी इच्छा ।” महात्मा जी के द्वारा अनेक स्वयंसेवकों से उनकी जाति पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि शिविर में अनेक हरिजन बंधु भाग ले रहे हैं, और परस्पर की जाति जानना वे आवश्यक नहीं समझते । भोजन आदि सभी कार्यक्रमों को वे साथ-साथ करते हैं । दूसरे दिन नागपुर से आने पर डा. हेडगेवारजी महात्मा जी से मिलने गए । पूज्य महात्मा जी ने डा. हेडगेवारजी से यह जानना चाहा कि संघ में अस्पृश्यता निवारण का कार्य किस प्रकार किया जाता है? डॉक्टरजी ने बताया, “हम अपस्पृश्यता दूर करने की बात नहीं करते, वरन् हम स्वयंसेवकों को इस प्रकार विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम सभी हिन्दू हैं । एक परिवार के सदस्य हैं ।” जिसके कारण स्वयंसेवकों के मन से स्पृश्यास्पृश्य की भावना स्वत: दूर हो जाती है । सन् १९१६ में अनुशीलन समिति के एक प्रमुख नेता श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती को डॉ. हेडगेवार ने कहा था, “जब तक हिन्दू समाज के व्यक्ति-व्यक्ति की सोच में परिवर्तन नहीं होता, तब तक केवल अंग्रेजों के चले जाने से विशेष लाभ होने वाला नहीं है । समाज के व्यक्ति-व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन लाने का कार्य मैं प्रारम्भ करने वाला हूं ।”
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल प्रेरणा है कि सम्पूर्ण हिन्दू समाज एक बृहत परिवार है । कुछ वर्ष पूर्व श्रीगुरुजी के भाषणों को लेकर योजनापूर्वक गलत धारणा फैलाने का प्रयास किया गया था । परन्तु विपरीत प्रकार की वह आंधी-शान्त होने के बाद जनसाधारण को श्रीगुरुजी की भूमिका समझना संभव हो सका । उसके पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक श्री बाबासाहब देवरस के द्वारा पुणे की वसंत व्याख्यानमाला में इसी विषय पर दिए गए भाषण से तो बची-खुची भ्रान्तियां भी पूरी तरह से धुल गई । श्रीगुरुजी कहा करते थे कि “सवर्णो के हृदय की संकुचितता के कारण यह समस्या निर्माण हुई है । अपने आपको उच्च वर्ग का समझने वाले लोगों के मन में जड़ जमाकर बैठी अस्पृश्यता को उखाड़ना ही मुख्य काम है । नवजाग्रत अस्पृश्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है । सवर्ण लोगों के मन की अस्पृश्यता समाप्त करना ही इस समस्या का एकमात्र हल है । नवजाग्रत अस्पृश्य वर्ग में जो विद्रोह का भाव पनप रहा है उससे उनकी प्रगति का पथ प्रशस्त होगा । फिर भी समस्या का स्थायी हल भावात्मक पारिवारिक भावना से ही संभव होगा ।” श्रीगुरुजी के कथानानुसार “आज चातुर्वर्ण्य में से न तो किसी वर्ण का अस्तित्व है और न ही किसी जाति का । आज तो हम सभी का एक ही वर्ण और एक ही जाति है और वह है “हिन्दू ।” यह भी सच है कि अपने स्वाभाव के अनुकूल न होने के कारण डाक्टरजी अथवा श्रीगुरुजी ने अन्य समाज सुधारकों जैसा समाज को सुधारने या उपदेश करने वाले नेता की भूमिका नहीं अपनायी । दोनों का ही स्पष्ट मत था कि यह कार्य धर्माचार्यो का है । श्रीगुरुजी ने परस्पर कभी एकत्र न आने वाले धर्माचार्यो को विश्व हिन्दू परिषद के माध्यम से सन् १९६६ में एकत्र लाकर यह कठिन कार्य सम्पन्न किया । बाबासाहब अम्बेडकर भी कहा करते थे कि किसी धार्मिक अथवा सामाजिक समस्या के सम्बन्ध में यदि श्री गोलवलकर एक निर्णय देते हैं और उसी समस्या के सम्बन्ध में शंकराचार्य भिन्न निर्णय देते हैं तो ऐसी स्थिति में सनातनी सवर्ण हिन्दू किसके निर्णय को शिरोधार्य मानेगा? अर्थात् शंकराचार्य का ही निर्णय माना जाएगा । शंकराचार्य को मानता कौन है? कौन है यह शंकराचार्य? इस प्रकार कहने वाले हमारे तथाकथित प्रगतिवादी लोगों को श्रीगुरुजी शांति से समझाते थे : “भले लोगो, यह मुख्य प्रश्न नहीं है कि शंकराचार्य को हम और आप मानते हैं या नहीं, महत्व का प्रश्न यह है कि जिन सर्वण लोगों को आप और हम छुआछूत की भावना त्यागने को कह रहे हैं, वे किसे मानते हैं? वे मुझे भी नहीं मानते और आपको भी नहीं मानते । वे तो धर्माचार्यो का ही आदेश मानते हैं । मेरी और आपकी बात वे मानने को आज तैयार नहीं हैं । ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए उन्हें धर्माचार्यो का आदेश प्राप्त कराना ही एक मात्र उपाय हो सकता है ।” कोई भी निष्पक्ष, विवेकशील व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा । इस दृष्टि से विश्व हिन्दू परिषद द्वारा किया गया कार्य समाज सुधारकों के द्वारा किए जाने वाले प्रचारात्मक कार्य जैसा न होते हुए भी अधिक मूलग्राही है । डॉक्टर हेडगेवार द्वारा अपनाई गई भूमिका के सफल परिणाम सामने आ रहे है । डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी यही भावना थी, यह मैंने उनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की है ।
अब तक तो जातिगत भेद ही थे, अब उसमें राजनीतिक दलों के भेद की वृद्धि हो चुकी है । यह भी एक चिंता की बात है । बाबासाहब ने समापन के अपने अन्तिम भाषण में अपने हृदय की तड़पना को व्यक्त करते हुए कहा था कि “हमें अपनी राष्ट्रीय एकता को हर कीमत पर अक्षुण्ण रखना होगा ।” इस बात का विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों महापुरुषों की भावना तथा लक्ष्य एक ही था । अन्तर केवल समस्या को हल करने के उपाय में था । बाबासाहब भी यह जानते थे कि सामाजिक समरसता के बिना समता का निर्माण असंभव है । २५ नवम्बर, १९४७ को उन्होंने दिल्ली में दिए गए अपने भाषण में इसे स्पष्ट किया था । उन्होंने कहा था, “हम भाईचारे को अपने व्यवहार में नहीं लाते, यह हमारी दूसरी कमजोरी है । हम सभी भारतीय परस्पर भाई हैं । सभी भारतीयों के मन में परस्पर जो आत्मीयता का भाव होता है, उसे ही “बन्धुभाव” कहा जाता है । सामाजिक जीवन में एकता का अमृत-सिंचन करने वाला यह “बंधुभाव” ही है । इस भावना को नित्य के व्यवहार में सफलतापूर्वक निभाना विकट कार्य है । भारत में अनेक जातियां हैं इसी के कारण समाज में अलगाव पैदा होता है । यह देश की एकता के लिए घातक है । ये जातियां इसलिए भी घातक हैं कि वे परस्पर घृणा और द्वेष भावना पैदा करती हैं । यदि हमें राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है तो इन सभी बाधाओं को दूर करना ही होगा । राष्ट्र भावना के जागरण से ही बंधुत्व की भावना निर्माण हुआ करता है और बिना बंधुभाव के समता और स्वतंत्रता की बातें कोरी बकवास बनकर रह जाती हैं ।”
हिन्दू समाज की एकात्मकता के अभेद्य दुर्ग में सामाजिक विकृतियों के कारण जो दरारें पड़ी हैं, उसकी कल्पना बाबासाहब को अच्छी प्रकार से थी । इसी कारण उनका हृदय अत्यन्त व्यथित रहा करता था । उनकी आन्तरिक इच्छा थी कि सामाजिक समरसता शीघ्रातिशीघ्र निर्माण हो । सामाजिक समरसता की परिभाषा और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा था : “सामाजिक समरसता के लिए किसी सामूहिक कार्य में सभी का सहभाग आवश्यक हुआ करता है । तभी प्रत्येक व्यक्ति में अन्य लोगों को कार्यप्रवृत्त करने के लिए आवश्यक भावना का स्पन्दन होता है और उस कार्य के साथ वह एकाकार होने लगता है । उस कार्य की सफलता अथवा असफलता को वह अपनी सफलता अथवा असफलता मानने लगता है । यही व्यक्ति-व्यक्ति को परस्पर जोड़ने वाली सशक्त कड़ी हुआ करती है । इसी के सहारे समाज खड़ा हुआ करता है । समाज कार्य में सहभागी होने में जाति व्यवस्था बाधक बनी और इसी कारण हिन्दू लोग एकात्म जीवन तथा आत्मगौरव की भावना के साथ समाज के रूप में कभी खड़े ही नहीं हुए ।”
हिन्दू समाज के लिए श्रद्धेय बाबासाहब के हृदय की यह तड़पन डॉक्टर हेडगेवारजी के हृदय की बेचैनी से भिन्न थी, यह कहना बौद्धिक अप्रामाणिकता होगी ।
डॉ० हेडगेवारजी का समरसता तथा श्रद्धेय डॉ० बाबासाहब अम्बेडकर की समता, दोनों ही आवश्यक हैं । लेकिन समरसता के बिना समता का निर्माण कदापि संभव नहीं । मनोविज्ञान के अनुसार यदि मनुष्य में समाज के प्रति समरसता का भाव न रहा तो विषमता का निर्माण होना निश्चित है । सम्पूर्ण समाज के प्रति समरसता का भाव न होने पर बुद्धिमान लोगों द्वारा भोलेभाले लोगों का, बलवानों द्वारा निर्बलों का, धनी लोगों द्वारा निर्धनों का शोषण क्यों नहीं होना चाहिए इसका कोई न्यायसंगत उत्तर नहीं दिया जा सकता । इसलिए अन्य लोगों के शोषण की क्षमता होने पर भी किसी का भी शोषण न करते हुए व्यक्ति अपने कर्तृत्व का उपयोग अन्य लोगों के कल्याण के लिए तभी करेगा जब उसमें समाज के प्रति समरसता का भाव होगा । इसलिए समता के लिए पहली शर्त होगी समरसता और पारिवारिक भावना । सम्पूर्ण समाज मेरा परिवार है, इस भावना में से निर्माण होती है “समरसता” । समरसता में से स्वाभाविक रूप से निर्मित होती है “समता” । विषमता दूर होकर “समता” का निर्माण आवश्यक होने पर भी “समता” गन्तव्य अर्थात् अन्तिम पड़ाव नहीं हो सकती । उसे एक बीच का पड़ाव ही कहा जा सकता है । अन्तिम प्राप्तव्य तो “समरसता” ही होगी । उसके अभाव में ”समता” की अवस्था प्राप्त होने पर भी वह स्थायी नहीं हो सकेगी । बाबासाहब के एक भाषण से भी यही भाव प्रकट हुआ था । उन्होंने कहा था, ”मेरे तत्वज्ञान का अधिष्ठान है “धर्म” । उसे राजनीति से जोड़ना भूल होगी । मैने गुरुस्थान पर भगवान बुद्ध को स्वीकार किया है । उनके उपदेशों से मैंने अपने तत्वज्ञान का स्वरूप निर्धारित किया है । मेरे तत्वज्ञान में स्वातंत्र्य और समता को प्रमुखता दी गई है । लेकिन असीमित स्वतंत्रता से समता का नाश होता है और विशुद्ध समता में स्वतंत्रता का विकास नहीं होता । मेरे तत्वज्ञान में स्वतंत्रता तथा समता का दुरुपयोग न हो, इसके लिए कुछ निर्बन्ध रखे गए हैं । लेकिन ये निर्बन्ध स्वतंत्रता तथा समता के सम्बन्ध में होने वाले उल्लंघन से रक्षा कर सकेंगे, इस पर मेरा विश्वास नहीं । स्वतंत्रता तथा समता का संरक्षण केवल बन्धुभाव से ही संभव है ।” इसी बंधुभाव को मानवता कहते हैं और मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है । इसी बंधुभावना को सामाजिक समरसता भी कहते हैं । यही मानवता है, यही है धर्म । भगवान् बुद्ध की मैत्री और करुणा में से समरसता ही फलती-फूलती है । इसी के माध्यम से समता का जन्म होता है । समता को अन्तिम गंतव्य बताने वाले प्रोग्रेसिव, लिबरल, रैडिकल, रेवाल्यूशनरी आदि लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि वे मुझे दुनिया के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण दिखा दें कि जहां समता पर ही बल देकर समता स्थापित हुई हो । प्रत्येक क्रान्ति हमें यही बताती है कि जो आप्रेस्ड अर्थात् शोषित थे उन्होंने ही शोषण करने वालों के विरुद्ध विद्रोह किया है । लेकिन प्रसिद्ध विचारक श्री फायर का कथन है कि जब-जब शोषित लोग शोषण करने वालों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो उस विद्रोह अर्थात् क्रान्ति का नेतृत्व दो प्रकार के लोगों के हाथ में होता है; एक तो वे लोग, जो शोषक वर्ग को हटाना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन-मूल्यों से उनका कोई विरोध नहीं होता, उन्हें वे यथावत रखना चाहते हैं । अन्तर केवल इतना ही होता है कि वर्तमान शोषकों को हटाकर उनका स्थान वे स्वयं लेना चाहते हैं । श्री फ्रायर का कथन है कि ऐसी स्थिति में क्रान्ति तो सफल होती है, शोषक वर्ग समाप्त हो जाता है, शोषित वर्ग के नेताओं के हाथ में सत्ता भी आ जाती है, लेकिन उन नवीन सत्ताधारियों के जीवन-मूल्य उनके पूर्ववर्ती शोषक वर्ग के ही होने के कारण वे उसी शोषण को दुगुनी गति से प्रारम्भ कर देते हैं । इस कारण जनता की स्थिति, “आकाश से गिरे और खजूर पर अटके” वाली कहावत जैसी हो जाती है । शोषण करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन उनका स्थान लेने वाले “जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ” की कहावत को चरितार्थ करने वाले होते हैं । शोषण का चक्र पुन: प्रारम्भ हो जाता है ।
नेताओं का दूसरा भी एक वर्ग होता है जिनका जीवन-मूल्य शोषण करने -वाले वर्ग से भिन्न होता है । वे शोषकों को हटाकर उनके जीवन-मूल्यों को भी बदलना चाहते हैं । इसलिए क्रान्ति के सफल होने के बाद सत्ता प्राप्त होते ही वे समाज रचना में आमूलाग्र परिवर्तन करना प्रारम्भ कर देते हैं । लेकिन श्री फ्रायर ने यह भी कहा है कि “अब तक जो क्रांतियां हुई हैं उनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि शोषण करने वाले वर्ग से भिन्न जीवन-मूल्यों में विश्वास करने वाले क्रान्तिकारी , ऐसे नेता अपवाद स्वरूप ही हुआ करते हैं । शोषक वर्ग के ही जीवन-मूल्यों में विश्वास करने वाले नेताओं के कारण, राज्य सत्ता क्रान्तिकारियों के नेता ले लेते हैं, लेकिन उनके भी जीवन-मूल्य पूर्ववर्ती शोषकों के होने के कारण पुन: शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और क्रान्ति की पुन: आवश्यकता निर्माण हो जाती है । यह बात माऔ-त्से- तुंग ने भी कही है । माओ ने कहा है: “सन् १९४९ में हमने अपने यहां क्रान्ति की । किन्तु क्रांतिकारियों को शासन सूत्र सौंपने पर हमें यह अनुभव हुआ कि कल के क्रान्तिकारी आज प्रतिक्रान्तिवादी हो गए हैं । उन्हें हटाने के लिए पुन: सांस्कृतिक क्रान्ति की आवश्यकता अनुभव होने लगी ।” इसका औचित्य उन्होंने सांस्कृतिक क्रान्ति का सूत्रपात करते समय बताया था । लेकिन उन्होंने ईमानदारी के साथ स्वीकार किया कि “इस प्रकार पुन: क्रान्ति करके पुराने क्रान्तिकारी नेतृत्व को बदलने से ही इसकी इतिश्री नहीं होने वाली है । क्योंकि सत्ता में आने वाले क्रान्तिकारी बार-बार प्रतिक्रान्तिवादी होते रहेंगे और उन्हें बदलने के लिए पुन: पुन: क्रान्ति भी करते रहना पड़ेगा । अर्थात् प्रत्येक दस-पन्द्रह वर्ष के बाद क्रान्ति की आवश्यकता निर्माण होती रहेगी । माओ-त्से-तुंग के द्वारा प्रतिपादित सतत क्रान्ति का सिद्धान्त सभी को पता है ।
इस प्रकार जब-जब शोषण के विरुद्ध शोषित वर्ग का विद्रोह, प्रतिक्रिया अथवा प्रतिकार होता है तो उसमें प्रतिशोध की भावना तीव्र होने के कारण अनियंत्रित भीड़ के द्वारा विध्वंस अपरिहार्य हो जाता है । उसमें से समाज को एक सूत्र में बांधने वाली किसी व्यवस्था का निर्माण संभव ही नहीं है । शोषित वर्ग के कल्याण की भी कोई संभावना नहीं रहती । क्रान्ति का नेतृत्व करने वाले नेता ही शोषक बन जाते हैं । नामोल्लेख के बिना भी समझा जा सकता है कि किसी समय जिन लोगों ने सम्पत्र वर्ग तथा वर्ण के लोगों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, वे ही अब प्रतिष्ठित बन चुके हैं, और उन्हीं का साथ देने वाले लोग अब उनके ही विरुद्ध विद्रोह का झण्डा लेकर खड़े हैं । इसीलिए शोषण करने वाली व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होने पर भी उसमें से उस समस्या का स्थायी हल संभव नही । समस्या का स्थायी हल प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार की अप्रियता को सहने की मानसिक सिद्धता रखनी होगी । शोषित वर्ग का नेतृत्व करने वाले को निहित स्वार्थ वाले, अर्थात् नवीन क्रान्ति के सफल होने पर जिनके स्वार्थ पर आंच आने वाली है, तथा होने वाले शोषण से उत्तेजित होकर उग्रवादी बनने के लिए प्रस्तुत शोषित वर्ग का रोष सहते हुए संवैधानिक एवं संतुलित पद्धति से काम करना होगा । यह करते समय शोषक हो या शोषित, हम सभी एक ही समाज के अंग-प्रत्यंग हैं और जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर एक इकाई बनती है, और उसमें मां का स्तनपान करने वाले शिशु से लेकर शिथिलगात्र होकर खटिया पर पड़ा रहने वाला वृद्ध और लंगड़े-लूले, अंधे अथवा मानव रोगी, सबका समावेश होता है । उन सबकी अधिक देखभाल की जाती है । उसी प्रकार सम्पूर्ण समाज को एक परिवार मानने के बाद उसके सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े सदस्यों की विशेष देखभाल स्वाभाविक रूप से की जानी चाहिए । इसके लिए सामाजिक समरसता ही रामबाण उपाय है । सामाजिक समरसता का निर्माण न होने पर उसकी जो प्रतिक्रिया होगी, वह अखण्ड क्रान्ति की ओर ही ले जाएगी । लेकिन यह कभी भी उचित नहीं होगा । इस संदर्भ में महात्मा फुले ने अपने अनुभव के आधार पर जो विचार प्रदर्शित किए हैं, वे निश्चित ही मननीय हैं । उन्होंने कहा था, “इस बलस्थान के भिल्ल, कोली आदि समस्त शूद्रातिशूद्र विद्वान हों, विचार करने योग्य हों, क्योंकि सबके साथ “एकमय” हुए बिना “नेशन” अर्थात् “राष्ट्र ” की कल्पना मूर्तरूप नहीं ले सकेगी ।”
“विद्रोही शोषितों के जीवन-मूल्य शोषक राज्यकर्ताओं के जीवन-मूल्यों के ही समान होने पर शोषितों की विजय होने के पश्चात उनके नेता स्वयं शोषितों का शोषण दुगुने वेग से प्रारम्भ कर देते हैं ।” फ्रायर के इस विचार को पुष्ट करने वाली अनेक घटनाएं इतिहास में अंकित हैं । उनमें से नीग्रो जाति से सम्बन्धित एक घटना का उल्लेख में यहां करता हूं ।ब्रिटिश गुएना में नीग्रो लोगों की संख्या तैंतीस प्रतिशत तथा भारतीयों की ५२ प्रतिशत है । अंग्रेजों के साम्राज्य में नीग्रो जाति पर बहुत अत्याचार हुआ करते थे । इसी कारण नीग्रो लोगों में अंग्रेजों के प्रति घृणा और द्वेष था और अन्य लोगों में नीग्रो लोगों के प्रति सहानुभूति थी ।
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने जिस प्रकार अन्य देशों में वहां के लोगों को सत्ता सौंपी वैसी ही ब्रिटिश गुएना में भी सत्ता का हस्तान्तरण हुआ । मतदान का अधिकार प्राप्त होते ही ऐसी आशा बंधी कि अब भारतीयों को स्वराज्य में अच्छे दिन देखने को मिलेंगे । लेकिन उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय धूर्त शक्तियों (अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा हालैण्ड) ने केरेबियन आयोग स्थापित करके नव स्वतंत्र गुएना में वंशवाद के आधार पर नीग्रो लोगों को भारतीयों के विरुद्ध भड़काया । नीग्रो लोगों की संख्या कम होने से स्वाभाविक रूप से भारतीयों का शासन होना था, लेकिन धूर्त राष्ट्रों की चौकड़ी ने चुनाव की एक नवीन पद्धति थोपकर अल्पसंख्यक नीग्रो लोगों के लिए सत्ता हथियाने का मार्ग प्रशस्त किया । इस चुनाव प्रणाली को अनुपस्थितों द्वारा किया गया प्रतिनिधि मतदान कहा जाता है ।
इस चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले गुएना के लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया । बहुसंख्यक भारतीयों को चालाकी करके अल्पसंख्यक बना दिया गया । डॉ० छेदी जगन से शत्रुभाव रखने वाले अमेरिका की इस में प्रमुख भूमिका थी ।
धूर्त विदेशी शक्तियों की सहायता से सत्ता हथियाने के बाद नीग्रो लोगों ने अपना रुख बदला । अंग्रेजों के प्रति घृणा और शत्रुता का जो भाव था वह अब भारतीयों के प्रति तीव्र हो गया । अंग्रेज तथा नीग्रो एक हो गए । २५ मई, १९६४ को कराए गए “बिस्मार” की पुनरावृत्ति स्थान-स्थान पर होने लगी ।
नेशलन सर्विस स्कीम जैसी योजना शुरू करके उसके माध्यम से भारतीय महिलाओं पर बलात्कार किए जाने लगे । भारतीय महिलाओं को नीग्रो लोगों द्वारा वासनापूर्ति का निशाना बनाया जाने लगा । शासकीय सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यक नीग्रो बहुसंख्यक भारतीयों का खुलकर उत्पीड़न करने लगे ।
अतएव शोषित समाज का विद्रोही होना ही पर्याप्त नहीं, उनके जीवन-मूल्य भी शोषकों के जीवन-मूल्यों से भिन्न होना आवश्यक है । ऐसा न होने पर विजय प्राप्ति के बाद शोषित समाज ही स्वयं शोषक बनकर दुगुने वेग से शोषण करना प्रारम्भ कर देता है । गुएना, त्रिनिदाद तथा सूरीनाम के नीग्रो इसके जीते-जागते उदाहरण है ।
यहां पर यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि महात्मा फुले द्वारा प्रतिपादित “एकमय” को ही हम “समरसता” कहते हैं ।
हिन्दू समाज में स्पृश्यास्पृश्य का जो विभाजन है, उसकी तुलना अमेरिका के काले-गोरे अथवा प्राचीन ग्रीस के गुलाम और नागरिक के विभाजन के साथ नहीं की जा सकती । ऐतिहासिक काल का यह घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण होने पर भी “हम सभी एक राष्ट्र के घटक है” इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता । लेकिन महात्मा फुले के द्वारा प्रतिपादित कटु सत्य निश्चित रूप से सबको विचार करने के लिए विवश करेगा । वे कहते हैं, “भारतीय समाज में वर्ग-भेद रहते सामूहिक मन का निर्माण संभव नहीं और सामूहिक मन के अभाव के रहते क्या राष्ट्र की कल्पना संभव है ?” इसमें से राष्ट्रवादी तथा राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं को सामाजिक दायित्व का बोध होता है । समाज से अलगाव के भाव का निर्मूलन कर परस्पर एकत्र रहने का संकल्प सबके मन में दृढ़ करने का ही नाम “सामाजिक समरसता” है । इसी के माध्यम से अब तक चली आ रही सामाजिक विषमता दूर करके विशुद्ध राष्ट्रीयत्व का भाव समाज के व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय में जाग्रत किया जा सकेगा ।
समता स्थापित करने तथा उसे स्थिर रखने के लिए भी सामाजिक समरसता का ही सहारा लेना होगा । समरसता ही समता की गारंटी है । समाज में आज बड़ी-बड़ी घोषणा करने वालों के प्रति अविश्वास है । व्यक्ति-व्यक्ति से सम्पर्क और बिना शोरगुल के कार्य करने की संघ की एकान्तिक पद्धति से समाज जाग्रत होगा, भले ही इसमें समय कुछ अधिक लगे । लोगों की स्वार्थ भावना जगाकर अथवा समाज के विभिन्न वर्गो में परस्पर संघर्ष कराकर एकता का निर्माण नहीं किया जा सकता । रोग को जड़मूल से नष्ट करने की आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसी ही इस समस्या का स्थायी हल ढूंढने की आवश्यकता है । इसलिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं तथा दावे न करते हुए धीरे- धीरे परन्तु ठोस कदम बढ़ाते हुए समाज में सामाजिक चेतना जगाकर स्वाभाविक परिवर्तन लाने का कार्य करना होगा ।
क्या होगा? कैसे होगा? इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं । एक बार ठीक मार्ग पर चल पड़ने के बाद गति बढ़ाने का ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रयत्न अवश्य ही फलदायी होते हैं उसमें लगने वाला समय हमारी गति पर निर्भर करेगा । हमें ऐसा दिखाई देता है कि जिनके विषय में यह धारणा थी कि उनका अपनी धार्मिक संस्थाओं में निहित स्वार्थ है और वे समाज सुधारक नहीं बन सकते, ऐसे लोगों ने भी परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखकर जो निर्णय किए (पू० डाक्टरजी का प्रयास हो या महामान्य बाबासाहब का प्रयास) उन सभी का संकलित परिणाम निश्चित रूप से होता है । इस संदर्भ में विश्व हिन्दू परिषद की धर्म संसद का अधिवेशन मेरे कथन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है । धर्म संसद में सर्वसम्मति से पारित आचारसंहिता के पांचवें सूत्र में कहा गया है “समाज में श्रम की प्रतिष्ठा का भाव जाग्रत करते हुए उपेक्षित एवं पिछड़े हुए बंधुओं को समता एवं एकात्मकता की अनुभूति कराना ।” इस सूत्र में “समता एवं समरसता” दोनों बातों का अन्तर्भाव हुआ है” उसी आचारसंहिता के दूसरे सूत्र में कहा गया है कि “समाज के दुर्बल वर्ग के साथ अस्पर्श अथवा घृणा का व्यवहार जहां कहीं भी किया जा रहा हो उसका परिमार्जन करके समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर सौहार्द के सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पदयात्राओं का आयोजन करने की धर्माचार्यों से प्रार्थना है ।” विभिन्न लोगों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के संकलित परिणाम का यह एक उत्कृष्ट नमूना है । अधीर और उतावले लोग भले ही निराशा का अनुभव करते हों, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि सभी बातों का संकलित परिणाम होता ही है । इस बात को ध्यान में रखकर किसी प्रकार की उतावली न करते हुए पू० श्रीगुरुजी के शब्दों में “धीमे- धीमे जल्दी करो” की पद्धति से काम करना होगा । “सामाजिक समता” की स्थापना रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने जैसे कार्य में बाल-गोपालों के समान सभीको अपनी-अपनी लाठी लगानी होगी ।
डाक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस पर अपने बधाई संदेश में वीर सावरकर ने कहा था, “श्री अम्बेडकर के व्यक्तित्व में उनकी विद्वत्ता, संगठन, कुशलता तथा नेतृत्व करने की क्षमता का संयोग होने के कारण ही आज वे राष्ट्र के आधार-स्तम्भ माने जाते हैं । अस्पृश्यता का उन्मूलन और अस्पृश्य वर्ग में साहस, आत्मविश्वास एवं चैतन्य निर्माण करने में उन्हें जो यश प्राप्त हुआ है, उसके कारण उनके द्वारा देश की महान सेवा हुई है । उनका कार्य राष्ट्र की गौरव वृद्धि करने वाला मानवतावदी और चिरंतन स्वरूप का है । श्री अम्बेडकर जैसे महापुरुष का तथाकथित अस्पृश्य कुल में जन्म अस्पृश्य वर्ग के हृदय का हीनभाव समाप्त करने वाला तथा उच्चवर्णीय लोगों के अहंकार को चुनौती देने वाला सिद्ध होगा । श्री अम्बेडकर के महान् व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा सम्पत्र कार्य के प्रति हृदय में सम्मान का भाव रखकर मैं उनके दीर्घ आयुष्य, आरोग्य तथा भविष्य में उनके द्वारा महान कार्य के सम्पादन होने की कामना करता हूं ।”
सन् १९६२ में डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा उनके ७३ वें जन्मदिन पर प्रकाशित विशेषांक के लिए गुरुजी ने एक छोटा परन्तु अत्यन्त ही अर्थपूर्ण संदेश दिया था । श्रीगुरुजी लिखते हैं : “वन्दनीय डॉ. अम्बेडकर की पवित्र स्मृति का अभिवादन करना मैं अपना स्वाभाविक कर्तव्य समझता हूं । भारत के दिव्य संदेश की घोषणा से सारे विश्व को आन्दोलित करने वाले स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि दीन, दु:खी, दरिद्र तथा अज्ञान में पड़े भारतवासी ही मेरे देवता हैं । उनकी सेवा करना, उनके सुप्त चैतन्य को जगाना, उनके भौतिक जीवन को सुखमय तथा उन्नत करना ही यथार्थ में ईश्वर सेवा है । उन्होंने सवर्ण समाज की “छुऔ मत” प्रवृत्ति से निर्मित रूढ़ियों पर कठोर प्रहार किए । समाज की पुनर्रचना करने का आह्वान किया । राजकीय तथा सामाजिक उपेक्षा से क्षुब्ध डॉ० बाबासाहब अम्बेडकर ने स्वामी विवेकानन्द के इसी आह्वान को स्वीकार करके समाज की पुनर्रचना करने का कार्य प्रारम्भ किया । अज्ञान, कष्ट तथा अपमानित जीवन बिताने वाले समाज के एक बहुत महत्व के वर्ग के लिए डॉ० अम्बेडकर ने सम्मान का जीवन जीना संभव बनाया, यह उनका असामान्य कार्य है । अपने राष्ट्र पर उन्होंने जो महान उपकार किया उससे उऋण होना संभव नहीं ।
स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य की बुद्धिमत्ता तथा भगवान बुद्ध की करुणा से परिपूर्ण विशाल हृदय के संगम से ही भारत का उद्धार होगा । डॉ. अम्बेडकर ने बौद्धमत का स्वीकार तथा प्रवर्त्तन पर स्वामी विवेकानन्द की अपेक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग पूरा कर लिया है । उनकी कुशाग्र तथा विलक्षण बुद्धि को बौद्धमत की कमियों का ज्ञान था । उसका उन्होंने उल्लेख भी किया है । फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि सामाजिक व्यवहार की समानता, शुचिता, परस्पर की आत्मीयता और इन समस्त गुणों से प्राप्त होने वाली मानव मात्र की उन्नति की विशुद्ध प्रेरणा और बौद्धमत के प्रति श्रद्धा में उत्पन्न होने वाले राष्ट्र तथा मानव मात्र की उन्नति के लिए अनिवार्य जानकर ही उन्होंने बौद्धमत को अपनाया होगा । भगवान बुद्ध ने भी धर्म का स्वरूप विशुद्ध बनाए रखने तथा समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किए थे । उनका उद्देश्य समाज से अलग होने का नहीं था । आज भी डॉ० बाबासाहब अम्बेडकर ने समाज कल्याणार्थ तथा धर्महितार्थ अपने चिरंजीव समाज को निर्दोष एवं निर्मल रखने के लिए ही कार्य किया है । समाज से अलग होकर पृथक पंथ का निर्माण उनका उद्देश्य नहीं था, ऐसी मेरी श्रद्धा है और इसीलिए इस युग में भगवान बुद्ध के सुयोग्य उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पावन स्मृति को मैं हृदय से अभिवादन करता हूं ।”
भारत के दलित समाज और अमेरिका के नीग्रो समाज की समस्याओं में कोई समानता नहीं है । भारत का तथाकथित दलित वर्ग हमारे ही रक्त और वंश का है । अमेरिका का उदाहरण भारत पर लागू नहीं होता । फिर भी नीग्रो समाज के संघर्ष से वहां की राजनीति तथा सामाजिक समस्याओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है । इस दृष्टि से पिछले दशक में प्रकाशित स्टर्लिग टकर की पुस्तक “फार ब्लैक्स ओनली” अध्ययन करने योग्य है ।
पुस्तक की प्रस्तावना में प्रकाशक ने लिखा है : “अमेरिका में काले और गोरे उग्रवादी लोगों के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चल ही रही है । वे सरकार उलटने तथा सड़े-गले रंगभेद मानने वाले समाज को नष्ट करने पर उतारू है । लोगों की आवाज को किसी भी प्रकार दबाकर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने का पक्षधर एक दूसरे प्रकार का वर्ग भी है । यह वर्ग और अधिक कड़े कानून बनाने, अधिक कठोर दंड देने, पुलिस और नेशनल गार्ड फोर्स का खुलकर प्रयोग करने की मांग करता रहता है । सरकार उलटने की बात करने वाले यदि हिंसक हैं तो उनका दमन करने की मांग करने वाले भी तो हिंसक ही कहे जाएंगे । हम लोगों को केवल इन दोनों वर्गो की ही आवाज सुनाई देती है, इस कारण हमें ऐसा लगता है कि इन दो प्रकार के लोगों में से ही किसी एक को हमें चुनना होगा ।” सन् १९६२ के “मार्च ऑन वाशिंगटन” के लिंकन मेमोरियल की भाषणमाला में जॉन लुई ने कहा था : ”नागरिक अधिकारों का विधेयक अपूर्ण तो है ही, बहुत देर से भी लाया गया है । इस विधेयक में पुलिस के अत्याचारों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है । सैकड़ों वर्ष हमने प्रतीक्षा में बिताए हैं । अब न्यायालयीन कार्यवाही के लिए हम नहीं रुक सकते । हम अब राष्ट्राध्यक्ष, न्यायालय, कांग्रेस आदि से कोई अपेक्षा नहीं करते । अब हम समस्त सूत्र अपने हाथ में लेकर राष्ट्रीय परिधि के बाहर अपने सत्ता केन्द्र निर्माण करेंगे…… क्रान्ति अब दहलीज पर खड़ी है….. काले लोग आगे कूच कर रहे हैं । हम अपनी दग्ध भू-रणनीति को कार्यान्वित करेंगे । अहिंसात्मक उपायों से हम अपने विरोधियों को झुकने के लिए विवश करने के लिए ऐसा जबर्दस्त तूफान खड़ा कर देंगे कि अब तक किए गए सारे आदोलन उसकी तुलना में फीके पड़ जाएंगे ।”
सन् १९६४ में नीग्रो आन्दोलन के दूसरे एक नेता बेअर्ड रस्टिन ने कहा था : ”नीग्रो समाज अब मार्टिन लूथर छाप की अहिंसा को नहीं अपनायेगा । नीग्रो समाज के नेतृत्व की इच्छा रखने वाला कोई भी नेता गोरे लोगों के साथ प्रेम से रहने की बात नहीं करेगा । मैं स्वयं भी ऐसा नहीं कहूंगा । इस प्रकार की मानसिक बेईमानी को अब मैं प्रोत्साहन नहीं दे सकता । नीग्रो समाज का गोरे लोगों पर प्रेम नहीं है, और इस प्रकार के प्रेम की नीग्रो लोगों को आवश्यकता भी नहीं है । जो लोग ऐसा दुर्व्यवहार करते हों उनके साथ कौन प्रेम करेगा?”
जिस अमेरिका में अब्राहम लिंकन, बुकर टी वाशिंग्टन तथा मार्टिन लूथर किंग जैसे महापुरुष हुए, वहां भी दोनों ओर के उग्रवादी नेतृत्व के कारण कुछ समय तक वंशवाद ने इतना सिर उठाया कि दोनों पक्षों में सामंजस्य की प्रक्रिया कुछ समय तक बंद रही । परिस्थिति की विस्फोटकता तथा दोनों पक्षों की मनःस्थिति में दो ध्रुवों का अन्तर निर्माण होने पर भी नीग्रो समाज के कुछ नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन कायम रखते हुए विवेक से काम लिया, यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ऐसे ही नेताओं में से एक श्री स्टर्लिंग टकर ने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा था :
”मेरी दृष्टि से वास्तविकता तथा समझदारी के माध्यम से परिवर्तन लाना सुलभ एवं सुगम है । ” उन्होंने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए आन्दोलन और उनमें मिली असफलता का विवचेन प्रारम्भ में ही किया है । ”नीग्रो समाज की शक्ति” शब्द-प्रयोग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है, ”इस संकल्पना से प्रारम्भ में स्वस्थ क्रियाशक्ति को प्रेरणा मिली, लेकिन समाज नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के आन्दोलन को सुस्पष्ट लक्ष्य, सुसंवादी स्वरूप तथा बल प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध हुआ । राष्ट्रीय मनोभूमिका का सिंहावलोकन करते हुए उन्होंने दिखा दिया कि भय और आपराधिक मनोवृत्ति के कारण नीग्रो समाज के क्षोभ का गोरे अमेरिकन लोग आकलन नहीं कर सके । नीग्रो लोगों की विध्वंसक गतिविधियों को विपरीत दृष्टिकोण से देखकर गोरे अमेरिकन लोगों ने ”कानून और व्यवस्था” को अत्यधिक महत्व देकर न्याय की हत्या कर दी ।
और फिर समस्या को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली व्यावहारिक नीति का उन्होंने विश्लेषण किया है । उग्रवादी अश्वेतों को अमेरिकन परिस्थिति का सम्यक् आकलन नहीं हो सका, इस बात को स्पष्ट करके उन्होंने अलगाववाद का एक संकल्पना के रूप में विचार किया है । एक विचारधारा और उसको साकार करने के मार्ग के खतरे तथा एक शतरंज की चाल के रूप में उसकी विधायक उपयोगिता का भी दिग्दर्शन किया है । मोर्चों के प्रश्न का विस्तार से विवेचन करके अश्वेतों के संगठन से निष्कासित गौरवर्णीय लोगों को संगठन में पुन: सम्मान के साथ लेने के मार्ग भी सुझाए हैं ।
अर्बन लीग फील्ड सर्विसेज के प्रमुख के रूप में प्राप्त अनुभवों के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया है कि ”व्यापक सामाजिक भूमिका से शिक्षा, रोजगार, अपराध, पुलिस विभाग तथा शासन आदि समस्याओं से निपटने के लिए समाज के विभित्र वर्गो को संगठित करके प्रवृत्त किया जा सकता है । ” सम्पूर्ण विवेचन में इसी बात पर बल दिया गया है कि उग्रवादियों के आक्रामक रख के विरुद्ध काले वर्ण के अमेरिकनो के प्रक्षोभ को परिवर्तनों के कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है और विशेष बात यह है कि यह कार्य आज के अमेरिकन समाज की उपलब्ध व्यवस्था में ही किया जा सकता है ।
जिस अर्बन लीग का नेतृत्व श्री टकर कर रहे हैं उसका कार्य यद्यपि सन्न १९१॰ से प्रारम्भ हुआ, किन्तु उसे ”जनाधिकारआन्दोलन” का स्वरूप सन् १९६० के पश्चात ही प्राप्त हुआ । इस आन्दोलन ने यद्यपि विभिन्न रणनीति का प्रयोग किया, फिर भी सबका एक ही उद्देश्य था, और वह था समरसता ।
श्री टकर कहते हैं : “यह प्रमुख प्रश्न था कि समरसता किसी प्रकार अविलम्ब प्राप्त हो सकती है । अश्वेतों के कुछ छोटे-छोटे गुटों के अतिरिक्त अलगाव की भाषा कहीं सुनाई नहीं देती थी । मुसलमानों का भी यह विचार नहीं था । इस वैधानिक आन्दोलन की मान्यता थी कि अलगाव से विषमता पैदा होती है और दृढ़मूल होती है । “स्वाट बनाम पेंटर” और “ब्राउन बनाम टोपेको” सन् १९५० और १९५४ के सफल ऐतिहासिक मुकदमों के लिए अथक परिश्रम करने की प्रेरक शक्ति यह श्रद्धा थी कि ”समरसता के माध्यम से ही समता” का निर्माण हो सकता है ।
इस बीच दोनों पक्षों के उग्रवादियों का हौसला बढ़ाने वाली कुछ घटनाएं हो जाने के कारण अर्बन लीग के काम में बाधाएं आईं । फिर भी श्री स्टर्लिंग टकर का अभी भी पूर्ण विश्वास है कि ”समरसता” के निर्माण से ही समता स्थापित हो सकती है । इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने अपने नीग्रो बंधुओं को भावी रणनीति के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक में मार्गदर्शन किया है । इसके पूर्व नीग्रो लोगों ने भावना के वशीभूत होकर जिस उग्रवादी मार्ग का अवलम्बन किया गया था उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे थे । नीग्रो लोगों द्वारा श्री टक्कर की प्रतिपादित भूमिका को अपनाने का यह भी कारण था । श्री टकर की रणनीति का संक्षिप्त रूप है : केवल वंशवाद के आधार पर संगठन खड़ा करके आन्दोलन चलाना आत्मघाती होगा । नीग्रो समाज के संगठन की आवश्यकता होते हुए उसका आधार संकुचित नीग्रोवाद रखना ठीक नहीं है । नीग्रो समाज के उत्थान की इच्छा रखने वाले अनेक गोरे अमेरिकन भी हैं । संकीर्ण भूमिका को अपनाने से नीग्रो समाज उन लोगों की सहानुभूति तथा समर्थन खो बैठेगा । इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो गोरे तथा अश्वेत अमेरिकन समाज के गरीब लोगों के लिए समान रूप से परेशानी का कारण बनी हुई है । ऐसी समस्याओं के आधार पर गोरे और काले समाज के गरीब लोगों को एक मंच पर लाना संभव है और उपयुक्त भी । जिस नीग्रो समाज की संख्या गत सत्तर वर्षों में घटते-घटते अब जनसंख्या का ग्यारह प्रतिशत रह गई उसने यदि बृहत संयुक्त मोर्चे का विचार न किया तो वह अपनी ही संकीर्णता के कारण अन्य लोगों की सहानुभूति खो देगा । इतनी अल्पसंख्या में होने के कारण इस विषम संघर्ष में एकाकी लड़कर विजय प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं होगा ।” श्री टकर कहते हैं : “हम काले गरीब और गोरे गरीब, काले मजदूर- और गोरे मजदूर एक ऐसी व्यवस्था में पिस रहे हैं जहां उत्पादन का वितरण कल्पनातीत रूप में विषम है….. ।
हम अश्वेत लोगों को यदि अमेरिका में सुख-शांति से रहना और दुःख-दारिद्रय से मुक्ति पानी है तो हमें शोषित-पीड़ित और गौर वर्ण लोगों को भी साथ लेना होगा । गौर-वर्ण होने के कारण हो सकता है उन्हें हमसे कुछ अधिक सुविधाएं मिल रही हों, तो भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वे भी हमारे जैसे ही शोषण के शिकार हैं । उन्हें साथ लेकर धनवानों का पोषण और गरीबों का शोषण करने वाले कर-विषयक कानूनों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा लगाना चाहिए । न्यूनतम वार्षिक आय की प्राप्ति के लिए चल रहे संघर्ष में उन्हें एक मंच पर लाना चाहिए । एक इटालियन अमेरिकन कैथोलिक धर्मगुरु फादर जेनो बारोनी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि “संकट गंभीर स्वरूप का है । सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उतावले, वोटों के भूखे राजनीतिज्ञ, समाज के विभिन्न वर्गो के दु:ख और कष्ट को ही अपनी पूंजी मानते हैं और जिन्हें परस्पर स्वाभाविक मित्र होना चाहिए उन्हीं में फूट डालने का वे प्रयत्न करते हैं ।
इस संदर्भ में यह भी ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पांच करोड़ है । इसमें नीग्रो, टोंरिकी, मेक्सिकी आदि का अनुपात उनकी जनसंख्या के परिमाण में अधिक है । और यदि सम्पूर्ण देश की जनसंख्या का विचार किया जाए तो गरीब लोगों में नीग्रो लोगों से गोरे लोगों की संख्या अधिक है । हां, केवल नीग्रो जनसंख्या में गरीब नीग्रो का परिमाण बहुत अधिक और केवल गोरे लोगों का परिमाण कम है । गोरे लोगों में गरीबों का परिमाण बीस प्रतिशत है । इन सभी बातों का विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि श्वेत तथा अश्वेत समाज के गरीबों का कुछ चुने हुए प्रश्नों पर संयुक्त मोर्चा बनने की श्री स्टर्लिंग टकर की भूमिका ठीक है । इसके लिए सर्वसंग्राहक नीति को रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने वाले नवीन नेतृत्व की आवश्यकता होगी । अब तक का नेतृत्व वंशवाद में ही अपना निहित स्वार्थ देखता था । इस रणनीति में सस्ता नेतृत्व प्राप्त हो जाता था ।”
श्री टकर ने भावी रणनीति के सम्बन्ध में जो बात नीग्रो समाज के लिए कही, वही बात भारत के दलित समाज के लिए भी लागू होती है कि ”जहां भी मान्य किए गए महान सिद्धान्तों तथा अर्थहीन उपदेश के कारण व्यावहारिक परिवर्तन में बाधा आती है और नेताओं की प्रतिभा जनता की प्राप्ति को कुण्ठित करने का कारण बनती है, वहीं सामूहिक लेन-देन का मार्ग प्रशस्त होता है । नई राह का नेता अपना पुरुषार्थ दांव पर लगाने को सिद्ध रहता है । किसी छोटे-से-छोटे कार्य के माध्यम से भी वह अपनी महानता प्रकट कर सकता है । वह जिस माध्यम को अपनाता है उसके अस्तित्व तथा उसकी मर्यादा बनाए रखने का वह विशेष ध्यान रखता है । इसके लिए लोगों का दुःख-दर्द शांति के साथ सुनने के लिए वह सदैव तैयार रहता है ।
पहले जिन संगठनों का अश्वेत वर्ग में प्रभाव था उनमें चर्च, गिल्ड्स, विभिन्न सोसाइटीज तथा क्लबों का समावेश था । ये सभी संस्थाएं अभी भी सक्रिय हैं । साधारण क्लब भी लोक कल्याण के कार्यों द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं । अश्वेत समाज भी अब समाज जीवन के विभिन्न पहलुओं का विचार करने लगा है । पहले इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं की मानी जाती थी । शनै: शनै: समाज ही अब इन कामों को करने लगा है । परिणामस्वरूप समाज में नया नेतृत्व उभर रहा है । पुराने नेताओं की ठेकेदारी समाप्त हो रही है । समाज के निम्न वर्ग में से उभर रहे इन नेताओं को जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है । इसके पूर्व सीमित क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं की उपेक्षा हुआ करती थी । उनका विशेष प्रभाव भी नहीं होता था । लेकिन अब इस प्रकार की संस्थाएं भी स्थानीय निकायों को प्रभावित करने लगी हैं । गांव के किसी एक कोने में प्रभाव रखने वाला सामान्य नेता भी यदि ग्राम रचना के विषय में कुछ सुझाव देता है तो उसकी भी बात को ध्यान से सुना जाता है । जनतांत्रिक प्रक्रिया का इसे प्रारम्भ कहा जा सकता है । अश्वेत वर्ग के वरिष्ठ नेताओं को जनता की समस्याओं को समझने, उन्हें हल करने के लिए प्रस्तुत होने तथा जनता के साथ अधिकाधिक समरस होने के लिए नवनिर्मित परिस्थिति बाध्य कर रही है ।
केवल सभा-मंचों से गरजने वाले नेता अब इतिहास के खाते में जमा हो गए हैं । एडम क्लेशन पावेल की कार्यपद्धति इसी प्रकार की थी, इसीलिए वह हार गया । प्रारम्भ में उसने अपने क्षेत्र में सेवाकार्य किए थे, लेकिन फिर वह केवल नेतागिरी करने लगा । आज का अश्वेत समाज इतने से ही संतुष्ट नहीं है । ऐसे नेता बिना किसी प्रयास के ही अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हैं ।
आज हम ऐसा नेतृत्व उभरते हुए देख रहे हैं जो जनता का अपना है, समाज के निम्न स्तर के लोगों के सुख-दु:ख की जिसे जानकारी है, लोगों के अभाव और आवश्यकताओं का जिसे न केवल ज्ञान है, अपितु जो उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील भी रहता है । जब तक उनकी यह मानसिकता रहेगी तब तक वे लोकमान्य बने रहेंगे । इन नवीन नेताओं को जनादेश प्राप्त है, और वे कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं ।
*********
| साभार संदर्भ |
| 14 अप्रैल 1983 एक यादगार दिन है. क्योंकि हिन्दू कालक्रम के अनुसार पू.डाॅ. हेडगेवार और अंग्रेजी कालक्रम के अनुसार आज ही के दिन पू.डॉ.बाबा साहब अंबेडकर की जन्मतिथि आई थी। यह एक असाधारण योग था। इस अवसर पर पुणे में ‘सामाजिक समरसता मंच’ की स्थापना की गई। अगले वर्ष मंच की पहली वर्षगांठ बाबा साहब के जन्मदिन पर मनाई गई। इन दोनों अवसरों पर श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा दिए गए भाषणों पर आधारित यह पुस्तिका पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें सात्विक प्रसन्नता हो रही है। यदि इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद नवरूढ़िवादी प्रगतिशील विचारक सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता के अंतर्संबंध पर पुनर्विचार करने को तैयार हों तो हमें लगेगा कि हमारा परिश्रम सफल हो गया। |