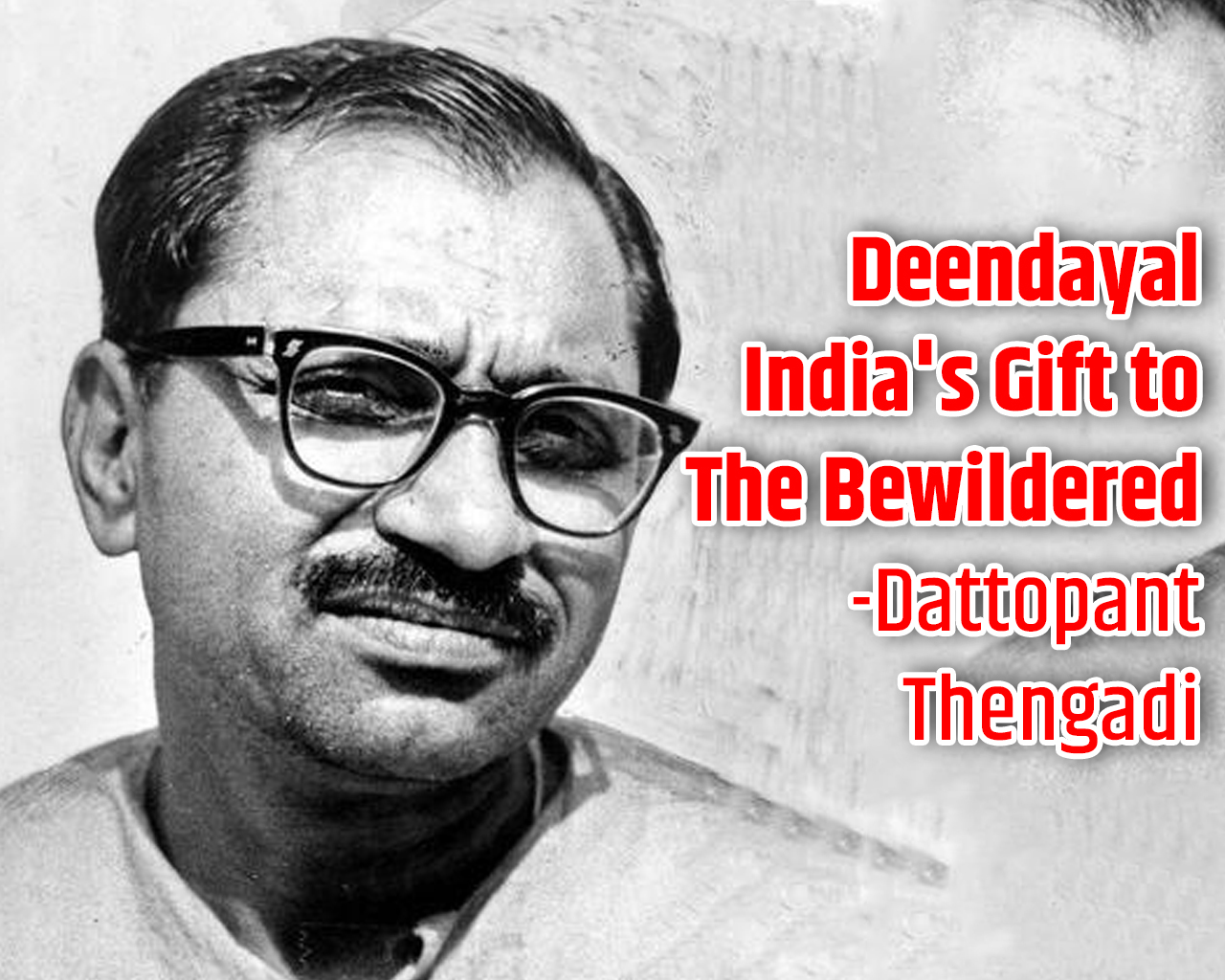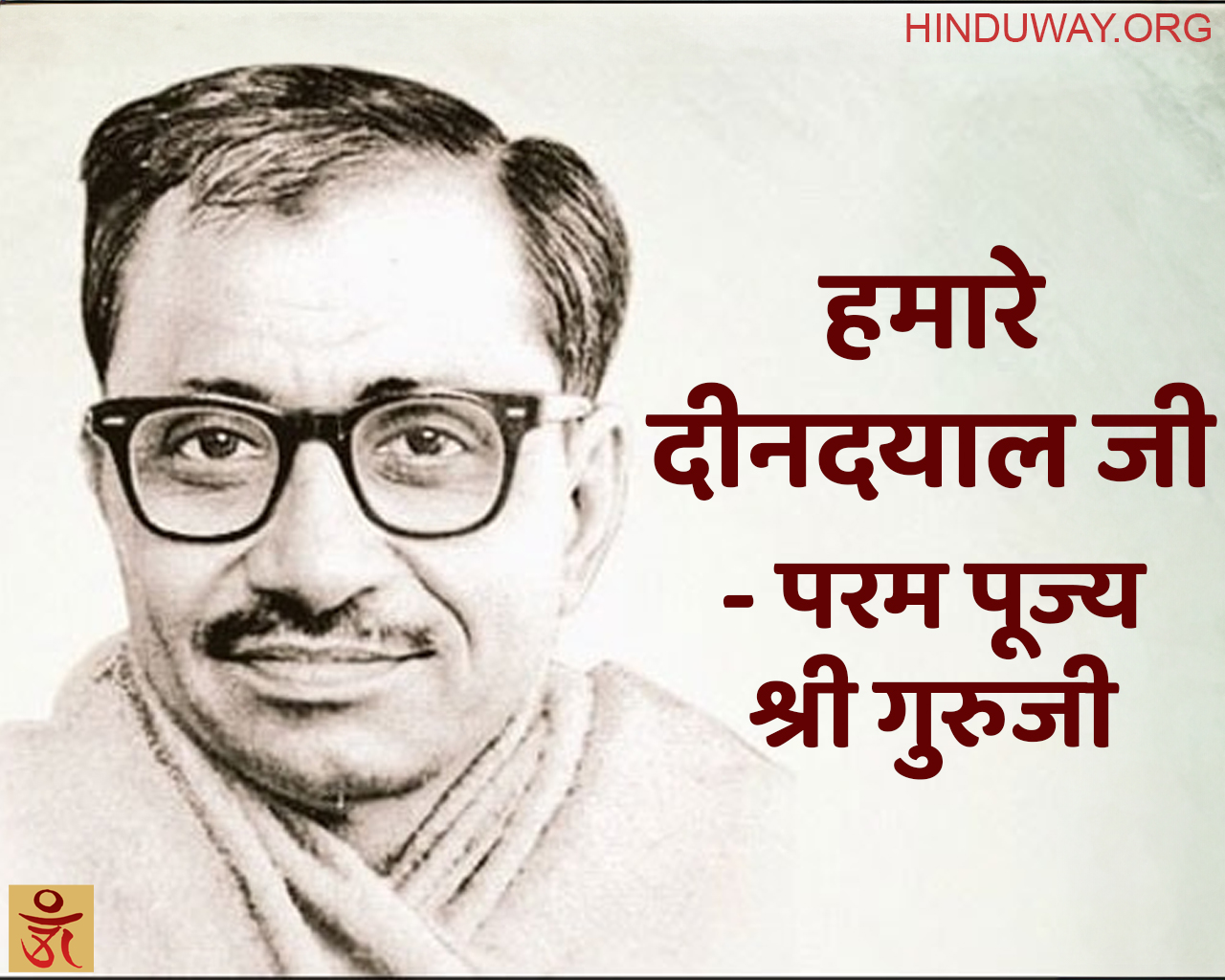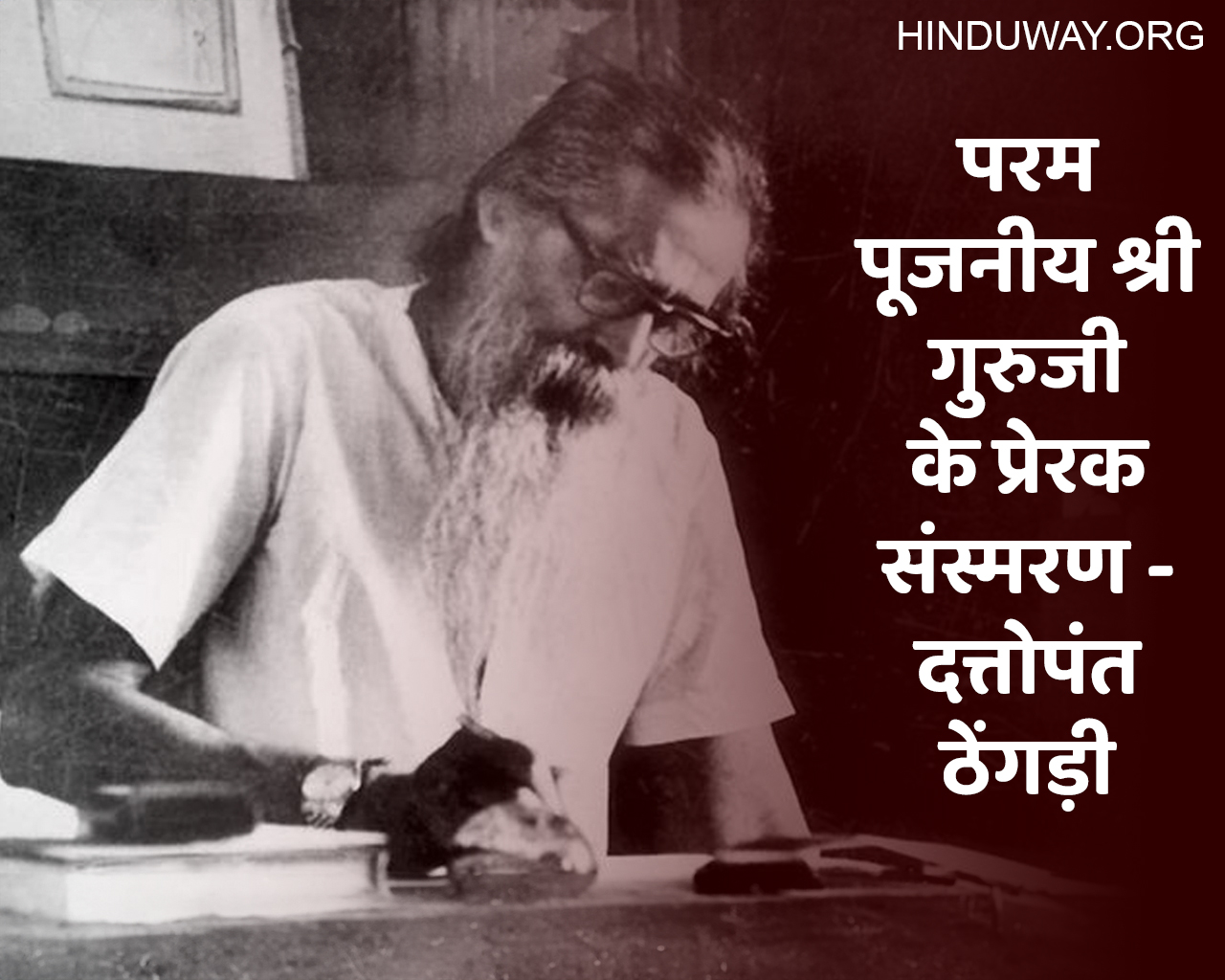सभी महान व्यक्तियों के समक्ष कोई न काई बाधा रही है। यह सत्य ही कहा गया है कि जॉनसन जैसे महान व्यक्ति विरले ही होते है, परन्तु उनकी जीवनी लिखने वाले बॉसवेल जैसे व्यक्ति तो और भी कम होते है। पर्वत शिखर पर खड़े एकाकी वृक्ष की भांति महान व्यक्ति भी सबसे भिन्न सबसे ऊपर रहता है। फिर भी इस पवित्र अवसर पर प्रत्येक सच्चे भारतीय को एक राजनीतिक दल के उस साधु स्वभाव वाले पथ—प्रदर्शक का स्वत: ही स्मरण हो जाता है, जिसने एक दृढ़ निश्चिय के साथ राजनीति में प्रवेश किया था।
जैसा की हम सभी जानते है, पंडीत दीनदयाल उपाध्याय सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनकी राष्ट्रीयता की धारणा मात्र काल्पनिक न थी, अपितु वह बड़ी व्यवहारिक थी। इसके साथ उनकी राष्ट्रभक्ति उनके अंतर राष्ट्रीयवादी होने में बाधक नहीं थी। उल्टे, अन्तर्राष्ट्रीयता उनके प्रगतिशील राष्ट्रवाद का स्वाभाविक परिणाम थी। उन्होंने यह अनुभव किया था कि किसी व्यक्ति का परिवार से लेकर ब्रह्राण्ड तक सभी से लगाव उसकी चेतना के विकास की बाह्रा अभिव्यक्ति मात्र है। उसकी जितनी ही अधिक विकसित हुई रहेगी, उतने ही उच्च तथा विस्तृत क्षेत्र से या समाज के अंग से उसका लगाव होगा। परन्तु यह विकास की एक प्रक्रिया है, उच्चस्तर की चेतना निम्नस्तर की चेतना से विकसित होकर ही प्राप्त होती है। उस चेतना में अन्य सभी स्तरीय चेतनाओं का समावेश रहता है, वे उससे पृथक नहीं रहती। इस प्रकार, समाज के सभी अंगों के साथ समान रूप से तथा एक साथ ही, उसमें से किसी एक के साथ भी बिना कोई अन्याय किये, लगाव बनाया रखा जा सकता है। आवश्यकता होती है एक यथार्थवादी तथा भेद—विहीन दृष्टिकोण की। मानव की भी कल्पना भेद विहीन रूप में की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क, दृष्टि एवं आत्मा की कल्पना सम्यक् रूप से ही, न की अलग — अलग करनी चाहिए।
समन्वयकारी मानववाद
इसी के आधार पर उपाध्यायजी ने अपने ‘समन्वयकारी मानववाद’ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो पाश्चात्य देशों की संकुचित एवं सीमाबद्ध विचारधाराओं के ठीक विपरित है। इन विचारधाराओं के ही कारण जीवन के सभी स्तरों तथा क्षेत्रों में पारस्परिक झगड़े तथा संघर्ष उत्पन्न हो गये है। बीज, अंकुर, तना,शाखा, तथा फल एक ही अबाधित विकास प्रक्रिया के अंग है। उनमें आपस में कोई विपरितता या अनन्यता नहीं है।
सच तो यह है कि पंडीत जी की कल्पना मानवजाति तक ही सीमित न थी। उनका समन्वयवाद इस बात घोतक है कि मानव चेतना विश्वव्यापी चेतना के रूप में विकसित हो सकती है। इसलिए, वे संकुचित दायरे वाले न होकर मानववादी थे। फलत: उन्होंने सोचा की उनकी विचार प्रणाली के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त नाम ‘समन्वयवाद’ ही होगा। चूंकि उनके क्रियाकलाप का क्षैत्र बड़ा व्यवहारिक था इसलिए उन्होंने सोचा कि तात्कालिक संदर्भ में ‘समन्वयाकरी मानववाद’ अधिक सुविधापूर्ण पद होगा, जो उनकी चरम कल्पना तथा सामान्य धारणा के बीच का एक पद था। बाद में इसे अधिक उपयुक्त नाम ‘एकात्म मानववाद’ दिया गया। वे ‘वाद’ शब्द का प्रयोग भी इसलिए करते थे कि सामान्य लोग इसे ही समझ सकते थे और सनातन धर्म की ‘वाद’ विहीनता को समझना उनकी बुद्धि के परे था।
धर्म के अग्रदूत होने के नाते वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गये। वे जानते थे कि जब तक राष्ट्र एक दृड आधार पर संगठित नहीं हो जाता, सिद्धान्तों के प्रतिपादन से कोई लाभ नहीं। उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारे राष्ट्र के मनोवैज्ञानिक एवं धारणा के अनुकूल है। उन्होंने संघ की वर्तमान शाखाओं को आदर्श राष्ट्र के आधारभूत ढांचे के रूप में देखा और उसे दृढ बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया।
वे राष्ट्रशक्ति के प्रतिशील विकास के लिए राजनीतिक क्षैत्र में भारतीय जनसंघ को एक उपयुक्त माध्यम मानते थे।
‘विराट’ राष्ट्र का प्राण
वे देश के पहले राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने राष्ट्र की पारम्परिक परिभाषा एवं तत्संबंधी धारणा को एक नया रूप दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना अन्त:करण अपना चित् होता है। राष्ट्र को जागरूकता एवं चेतना प्रदान करने वाली शक्ति एवं उर्जा उसका ‘विराट’ है। वह चित् द्वारा उपयुक्त दिशा में प्रेरित होता है। किसी राष्ट्र के जीवन में ‘विराट’ का वही स्थान है, जो शरीर में प्राण का। जिस प्रकार प्राण शरीर के विभिन्न अंगों को शक्ति प्रदान करता है, बुद्धि को ताजा करता है और मानसिक एवं शारीरिक संतुलन ठीक रखता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र में शक्तिशाली ‘विराट’ के रहने से ही लोकतंत्र सफल हो सकता है तथा सरकार कारगार हो सकती है। जब ‘विराट’ जागा हुआ रहता है तो विभिन्नता पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न नहीं करती, तथा राष्ट्र के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते है, जैसे मानव शरीर के विभिन्न अंग या किसी परिवार के विभिन्न सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते है।
भारतीय जनसंघ के संविधान के अनुच्छेद 370, सीमावर्ती राज्यों, भाषावार राज्यों, एकात्म प्रकार की सरकार, गोवा, कच्छ, चीनी, तथा पाकिस्तानी आक्रमणों जैसे विभिन्न प्रश्नों के संबंध में जो दृष्टिकोण अपनाया था, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पण्डित जी को मुख्य पथ प्रदर्शक के रूप में पाकर इस राजनीतिक दल ने किस प्रकार राष्ट्र के ‘विराट’ को फिर से जगाने का श्रेष्ठ कार्य पहले से ही अपना लिया था।
राज्य : धर्म का अंग
स्वतन्त्रता के बाद के युग में पंडितजी ही पहले राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मानव को सर्वाधिक आवश्यकता है एक धर्म—राज्य की, न कि मात्र बहुसंख्यक द्वारा शासन की। उन्होंने बड़े यत्न से यह समझाया कि धर्म सामान्य अर्थ में कहे जाने वाले धर्म से तथा धर्मराज्य धर्मतन्त्र से किस प्रकार भिन्न होता है। परन्तु धर्म तो सर्वोपरि है। राज्य तो धर्म के विभिन्न अवयवों एवं अगों में से एक है, नि:सन्देह वह महत्वपूर्ण है, परन्तु धर्म से ऊपर नहीं। वह धर्म के अधीन है। सार्वभौमिकता तो धर्म की है। धर्म ही राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। संविधान भी धर्म के अनुकूल ही होना चाहिए। संविधान के वे अनुच्छेद, जो धर्म के विरूद्ध हो , अवैध समझे जाने चाहिए। विधानमण्डल तथा न्यायपालिका दोनों ही समान स्तर पर है। कोई दूसरे से बड़ा नहीं है। धर्म दोनों से बड़ा है, दोनों ही धर्म द्वारा शासित होते है। जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। परन्तु न तो जनता को और न सरकार को धर्म के विरूद्ध कार्य करने का अधिकार है।
स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र और धर्म
‘जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकारें’ यही लोकतंत्र की परिभाषा कही गयी है। इस परिभाषा में ‘की’ स्वतंत्रता का बोधक है, ‘द्वारा’ लोकतंत्र का, तथा ‘के लिए’ धर्म का। चुनाव तथा बहुमत यह निर्णय कर सकते है कि कौन सरकार बनायेगा, परन्तु बहुमत द्वारा सच्चाई का निर्णय नहीं हो सकता । अमेरिका के दक्षिणी राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए बहुमत के समक्ष अब्राहम लिंकन झुके नहीं, और न तो फ्रांस के दिगाल ने ही हिटलर के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पक्ष में व्यक्त किये गये बहुमत को स्वीकार किया, क्योंकि बहुसंख्यकों द्वारा व्यक्त किया गया मत धर्म के, जो किसी राष्ट्र के संदर्भ में वह कानून है, जो उस राष्ट्र के ‘चित्’ की अभिव्यक्ति तथा उसे बनाये रखने में सहायक होता है, अनुकूल नहीं था। धर्म राष्ट्र के ‘चित्’ का संग्रहालय है। यदि धर्म नष्ट हो जाता है, तो राष्ट्र का भी नाश हो जाता है।
राष्ट्र की ‘इच्छा’ व्यापक
पंडितजी यह जानते थे कि किसी राष्ट्र के सभी नागरिकों की इच्छाओं का योग राष्ट्र की इच्छा नहीं कही जा सकती, यद्यपी अधिकांश मामलों में दोनों एक ही जैसी हो सकती है। राष्ट्र की इच्छा उसके नागरिकों की इच्छाओं के योग से कहीं अधिक व्यापक तथा उसके ऊपर होती है। अपने नागरिकों की इच्छा से बिल्कुल अलग राष्ट्र की अपनी ‘इच्छा’ होती है, क्योंकि राष्ट्र की उसके नागरिकों के समूह से अलग एक अपनी सत्ता होती है, और प्रत्येक सत्तावान वस्तु की अपनी इच्छा होती है। बीजगणित का एक समीकरण है, जिसके अनुसार ‘अ’ और ‘ब’ यदि अंसगठित रूप में एक साथ जुट जाते है, तो बिना वास्तविक जोड़ के यदि उनका वर्ग कर दिया जाय, तो परिणाम मिलता है —अ2+ब2। परन्तु यदि उन्हें संगठित कर दिया जाये, अर्थात् इस मामले में उन्हें कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाय, तो फिर उनका वर्ग किया जाय, यानी (अ+ब)2तो परिणाम होगा अ2+ब2+2 अ ब,न कि केवल अ2+ब2। यह 2 अ ब कहां से आय गया? इस प्रकार संगठन की अपनी अलग सत्ता तथा इच्छा होती है।
नित्य नूतन चिर पुरातन
राष्ट्रवादी होने के नाते पंडितजी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की समस्याओें के सम्बन्ध में बड़े चिन्तित रहते थे। उन्होंने पाश्चात्य देशों तथा प्राचीन भारत की विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया। उनका मस्तिष्क अतीत से जुड़ा हुआ था, वर्तमान में सक्रिय रहता था तथा भविष्य की चिंता करता रहता था। हमारे कुछ उग्र—सुधारवादियों की भांति वे प्रत्येक पाश्चात्य बात को ‘प्रगतिशील’ मानने को तैयार नहीं थे, और रूढ़िवादियों की भांति वे सभी परम्पराओं—मान्यताओं से महज इसलिए नहीं चिपके रहना चाहते थे कि वे भारतीय है। वे जीवन—सम्बन्धी भारतीय मान्यताओं तथा आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के बीच एक तालमेल बैठाना चाहते थे। वे आधुनिक युग की मांगों को, धर्म के सनातन आदर्शों के आधार पर पूर्ण करना चाहते थे। श्री गुरूजी की भांति, पंडित जी भी यह सोचा करते थे कि राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे के विभिन्न अंगों में एकता उत्पन्न होते ही राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंग सक्रियता से तथा बिना किसी पारस्परिक विरोध के सम्यक् रूप से राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना आरंभ कर देगें। इस प्रकार का सजीव तथा विकासशील समाज प्राचीन विचारधाराओं, पद्धतियों तथा परम्पराओं के समूह में से उन्हें तो रख लेगा जो आवश्यक होगें तथा उसकी प्रगति में सहायक होगें, और उन्हें फेंक देगा जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है, तथा उनके बदले में नयी प्रणालिया विकसित करेगा। पुरानी व्यवस्था की समाप्ति पर किसी को आंसू नहीं बहाना चाहिए और न ही नयी व्यवस्था का स्वागत करने से झिझकना चाहिए। सभी चेतन एवं विकासशील वस्तुओं का यही स्वाभाविक नियम है। जब वृक्ष बढने लगता है तो उसकी पकी तथा सूखी पत्तियां गिर जाती है, ताकि उनके स्थान पर नयी पत्तियां आ जायें और बढ़ना जारी रहे। मुख्य बात मस्तिष्क में रखने की यह है कि हमारे सामाजिक ढ़ांचे के सभी अंगों में एकता रूपी जीवन—शक्ति का प्रवाह होता रहे। कोई भी पद्धति या प्रणाली जिस प्रकार इस जीवन—शक्ति को सिंचित करेगी, उसी प्रकार या तो वह जीवित रहेगा या बदल जायेगा या बिल्कुल ही नष्ट हो जायेगा। इसलिए वर्तमान सामाजिक संदर्भ में, इस प्रकार की सभी पद्धतियों के भविष्य के सम्बन्ध में विचार करना निरर्थक है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे समाज की अन्तर्निहीत एकता की भावना तथा उस एकता की महत्ता के प्रति जागरूकता को पुनर्जीवित किया जाय। अन्य सभी बात फिर अपने आप ठीक हो जायेगी।
पंडितजी ने यह विचार—शैली राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षैत्रों में लागू की। उदाहरण के लिए, आर्थिक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए पंडितजी कहते है — ”परन्तु एक बात तो स्पष्ट है कि बहुत—सी पुरानी संस्थाओं के स्थान पर नयी संस्थायें आ जायेगी। इसका उन लोगों के लिए बुरा परिणाम होगा, जिनका उन संस्थाओं में निजी हित निहित है। पुनर्निर्माण के प्रत्यनों से उन लोगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा जो स्वभाव से ही परिवर्तन के विरूद्ध रहते है। परन्तु रोग का उपचार औषधि से ही किया जाना चाहिए। व्यायाम तथा कठिन परिश्रम से ही शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हमें यथापूर्व स्थिति वाली मनोवृति का त्याग करना पड़ेगा और एक नया युग लाना होगा। पुनर्निर्माण के हमारे प्रयत्नों पर न तो पूर्वधारणाओं का कोई असर पड़ना चाहिए और न हमें जो कुछ बपौती के रूप में मिला है, उसका बहिष्कार ही कर देना चाहिए। इसके विपरित, हमें उन प्राचीन विचारधाराओं एवं परम्पराओं से चिपके रहने की कोई आवश्यकता नहीं, जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। ”
पश्चिम के अंधी नकल के विरोधी
गांधीवादी विचारधारा से उनका इस अर्थ में मतभेद था कि वे मशीनों के प्रयोग पर अधिक बल देते थे। परन्तु नेहरू दृष्टिकोण से भी उनका मेल नहीं खाता था। वे कहते थे कि पाश्चात्य देशों के औद्योगिक ढ़ांचे की पूरी तरह नकल करना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होगा । इसमें संदेह नहीं कि चरखे के स्थान पर मशीने आनी चाहिऐ, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि स्वचालित मशीने आयें, जिससे बेकारों की समस्या और बढ़ जाये, पूरी क्षमता भर काम न हो, वर्तमान उत्पादन साधनों का पूर्ण उपयोग न हो सके, विदेशी मुद्रा तथा देशी पूंजी की कमी हो जाय तथा उपलब्ध कच्चे माल की अत्यधिक बरबादी हो। हवा, पानी, भाप, तेल, गैस, बिजली, तथा आणविक—शक्ति, जो परिचालन—शक्ति प्रदान कर सकती है, जैसी वस्तुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। व्यवस्था सम्बन्धी उपलब्ध कौशल का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन किया जाना चाहिए। संक्षेप में, सातों ‘एम’ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमें उपयुक्त डिजायन की मशीन तैयार करनी चाहिए, उत्पादन के प्रचलित तरीकों में सुविधापूर्ण एवं उपयोगी परिवर्तन लाने चाहिए तथा एक भारतीय शिल्पविज्ञान का विकास करना चाहिए।
उद्योगों में उचित प्रकार की भिन्नता
वे बड़े उद्योगों पर अन्धाधुन्ध बल दिये जाने के विरूद्ध थे। आर्थिक व्यवस्था में सफलता लाता है अधिक उत्पादन। यह आवश्यकता नहीं कि सब बड़े उद्योगों से ही उत्पादन हो। छोटे तथा मध्यम आकार के बहुत से उद्योगों से अधिक उत्पादन सम्भव हो सकता है। वे उत्पादन की उस संस्था के आकार को वरियता देते थे, जो उत्पादन कार्य में भाग लेने वालों को इस योग्य बना सके कि वे उस संस्था के स्वामी बन जायें, उसे स्वयं चला सके तथा उसकी स्वयं व्यवस्था कर सकें। श्रमिक को ‘बचत मूल्य’ की व्यवस्था में, जिसकी व्यवस्था पूंजीवादी पद्धति में सेवायोजक तथा समाजवादी व्यवस्था में सरकार करती है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का संतोष होना चाहिए । वे उद्योगों में उचित प्रकार की विभिन्नता लाने के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि पर आधारित छोटे उद्योग चालू किये जाये, जिनमें अपना देशी शिल्प विज्ञान लगे तथा जिनमें बिजली की सहायता से उत्पादन की प्रक्रियों के विकेन्द्रीकरण पर अधिक बल हो और जिनमें घर, न कि कारखाना, उत्पादन का केन्द्र समझा जाय।
जनशक्ति : पूंजी का महत्वपूर्ण अंग
वे नगरों की आवश्यकता से अधिक बढ़ने वाली जनसंख्या की समस्या तथा गांवों में बेकारी की समस्या एक साथ ही हल करना चाहते थे। उन्होंने पूंजी निर्माण की समस्या का विस्तार से विवेचन किया। परन्तु जिस बात में वे आज के अर्थशास्त्रियों से सर्वथा भिन्न थे, वह यह थी कि वे भारत की जनशक्ति को उसकी पूंजी का एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे, जिसका आर्थिक पुनर्निर्माण में पूर्णतया उपयोग किया जाना चाहिए।
योजना छोटी से छोटी क्षेत्रीय इकाई के स्तर पर बने उनका यह दृष्टिकोण ही उन्हें गांधीवादियों तथा उग्र सुधारवादियों दोनों से ही अलग रखता है। नियोजन के संबंध में पंडित जी दोनों उग्र बातों —एक, योजना बने ही न, और दो, केन्द्र के बड़े नियन्त्रक में योजना बने— से भिन्न एक तीसरे मार्ग का अनुसरण करना चाहते थे। वे चाहते थे कि छोटी से छोटी क्षेत्रीय इकाई के स्तर पर योजना बने। इस प्रकार बनी हुई क्षेत्रीय योजनाओं का केन्द्र द्वारा उचित ढ़ंग से समन्वय किया जाना चाहिए। यह स्मरणीय है कि इस मत का समर्थन डॉ. डी. आर. गाडगिल ने भी किया था, यद्यपि योजना—आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बाद इस मामले स्वतन्त्र नहीं थे।
निजी तथा सरकारी क्षैत्र परस्पर पूरक
अपने निजी काम में लगे रहने वाले व्यक्तियों के कार्य को पंडितजी बहुत अधिक महत्व देते थे। वे जनता के क्षेत्र के हिमायती थे और कहते थे कि निजी तथा सरकारी क्षेत्रों को एक दूसरे की कमी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान परस्थितियों में दोनों के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है।
उद्योगों के स्वामित्व के ढ़ांचे के संबंध में उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यवहारिक था। वे न तो यही चाहते थे कि बिल्कुल ही राष्ट्रीयकरण न हो और न यही कि पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकरण हो। उद्योगों के स्वामित्व की अनेक प्रणालियां है। अलग—अलग उद्योगों का उनकी विशेषता का ध्यान रखते हुए, अलग—अलग ढ़ंग का स्वामित्व होना चाहिए, न कि किसी पूर्व—निश्चित धारणा या परम्परा के आधार पर।
नियोजन में वरीयता कम
गांवों के सम्बन्ध में वे यह चाहते थे कि किसान अपने खेत का मालिक हो, खेतिहर भूमि की सीमा निर्धारित हो तथा ऐसा करने से जो भूमि बचे वह तथा खेती करने योग्य परती भूमि का पून: बंटवारा हो। वे जन—सेवा करने वाली छोटी—छोटी सहकारी समितियों के समर्थक थे और सहकारी कृषि का विरोध इसलिए करते थे कि उसमें सहकारिता की भावना तो रहती नहीं। उन्होंने हमारे कृषि क्षेत्र का पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की, क्योंकि उनका ख्याल था कि नियोजन में उसे वह वरियता नहीं मिली थी जो उसे मिलनी चाहिए थी। कृषि, छोटे उद्योग, तब बड़े उद्योग—वरीयता का यह क्रम होना चाहिए था।
विशिष्ट आर्थिक विचारधारा
अन्त में, यह कहा जा सकता है कि पंडितजी न वह आर्थिक विचारधारा प्रदान की, जो उनके पहले वाले तथा उनके साथ के राष्ट्रीय विचारकों द्वारा प्रस्तुत की गयी विचार धाराओं से भिन्न थी। जनसंघ के प्रतिद्वन्द्वियों के लिए इससे कठिनाई उत्पन्न हो गयी। वे पंडितजी की विचारधारा को उसके कार्यक्रम के आधार पर दक्षिणपंथी नहीं कह सकते थे और न उन्हें वामपंथी ही कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें समाजवाद की डींग नहीं हांकी गयी थी। पंडितजी इस प्रकार का वर्गीकरण भारतीय परिस्थियों के लिए पूर्णतया असंगत मानते थे। वे भारतीय परिस्थितियों तथा परम्पराओं पर आधारित यथार्थवाद से मार्ग—दर्शन लेते थे। वे अव्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते थे। वे ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ के विरूद्ध थे, क्योंकि अनिवार्यत: उसका परिणाम एक दल विशेष की तानाशाही होती थी। निश्चय ही वे शोषण एवं असमानतायें समाप्त करना चाहते थे। इस हद तक वे लोकतंत्रीय समाजवाद के विरूद्ध नहीं थे। परन्तु वे समाजवादी नहीं थे, क्योकि वे जानते थे कि समाजवाद तब तक अपने घोषित लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक वह भौतिकवाद के सिद्धान्त से चिपका रहेगा।
भौतिकवाद के सिद्धांत का परिणाम
फ्रांसीसी क्रान्ति ने पाश्चात्य देशों को स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुत्व के अमूल्य सिद्धान्त प्रदान किये थे। परन्तु यह देखा गया कि जब स्वतन्त्रता का सिद्धान्त कार्यान्वित किया गया तो उसने घोर असमानतायें उत्पन्न कर दी, समानता का सिद्धान्त जब साम्यवादी देशों द्वारा आचरित किया गया तो सभी प्रकार की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी, और बंधुत्व का आदर्श एक स्वप्न ही बना रह गया। पाश्चात्य विचारधारा के भौतिकवाद के कारण ही यह ऐतिहासिक असफलता आयी। भौतिकवाद का सिद्धान्त जीवन में भौतिकवादी मान्यताएं ही उत्पन्न करेगा। यदि किसी के जीवन की मान्यतायें महज भौतिकवादी ही होंय, तो कोई कारण नहीं कि वह अपने से कमजोर लोगों का शोषण करने से तनिक भी हिचके, बशर्ते कि ऐसा शोषण उसे भौतिक समृद्धि प्रदान करे। यह सच है कि आर्थिक समानता कानून द्वारा बलपूर्वक लायी जा सकती है। पंडितजी ने यह भी कहा था कि देश में व्यय करने के लिए उपलब्ध अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच 20 और 1 का अनुपात होना चाहिए। परन्तु यदि कोई पूर्णरूपेण भौतिकवादी हो, और जीवन में उसके लिए भौतिकवाद के अतिरिक्त अन्य कोई मान्यता न हो तो कोई कारण नहीं कि वह अपने वैयक्तिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए अधिकाधिक कठिन परिश्रम करे, क्योंकि अधिक परिश्रम करने से उसके भौतिक लाभ में कोई विशेष अन्तर तो पड़ नहीं सकता, निर्वाह के लिए न्यूनतम आय तो निश्चित रूप से मिल ही जायेगी और उसके समक्ष गैर भौतिकवादी ऐसा कोई लक्ष्य है नहीं, जो उसे अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर सके।
भारतीय संस्कृति की समन्वित पद्धति
हिन्दू संस्कृति ने जीवन की भौतिकवादी तथा गैर भौतिकवादी मान्यताओं की एक ऐसी समन्वित पद्धति निकाली जो व्यक्ति के विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करती थी। जैसा कि भलीभांति ज्ञात है कि भारत की संस्कृति में भौतिकवादी पहलू की न तो उपेक्षा की गयी और न उसे आवश्यकता से अधिक बढ़ाया—चढ़ाया गया। फलत: प्रेरणा भी दो प्रकार की हुई— भौतिकवादी तथा गैर भौतिकवादी। भौतिकवादी के लाभ तथा भोग—विलास और गैर भौतिकवादी में मान्यताओं पर आधारित सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा। सभी को यह छूट थी कि वह जिस पथ का चाहे अनुसरण करे, परन्तु शर्त यह थी कि भोग—विलास और सामाजिक प्रतिष्ठा अनिवार्यत: उलटे अनुपात में होगें। सामाजिक प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी, भोग—विलास उतने ही कम होगें और भोग विलास जितने अधिक होगें, समाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही कम होगी। समाज में पूर्ण समानता थी, इसलिए भोग—विलास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का योग प्रत्येक के लिए बराबर था, यद्दपि भोग—विलास और सामाजिक प्रतिष्ठा अलग—अलग प्रत्येक व्यक्ति के मामले में भिन्न थे, और यह बात शतप्रतिशत व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर थी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई प्रेरणाओं के वृत की परिधि सदा ही एक जैसी अपरिवर्तित रहती थी। परन्तु वृत में दोनों ही प्रकार की प्रेरणाएं थी। यदि भौतिकवादी प्रेरणा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता था तो गैर भौतिकवादी का अपने आप ही कम हो जाता था क्योकि वृत तो अपरिवर्तनिय था। इसके विपरित यदि गैर भौतिकवादी प्रेरणा का विस्तार कर दिया जाए तो भौतिकवादी का अपने आप ही कम हो जायेगा और ऐसा करना संबंधित व्यक्तियों की इच्छा पर था। वास्तविक एवं स्थायी समानता लाने का यह आधार था, वैज्ञानिक हिन्दू तरीका। जीवन के चार लक्ष्यों की प्राप्ति की इस पद्धति ने, वास्तविक समानता के आधार पर समाज के ढ़ांचे के निर्माण में हिन्दूओं की सहायता की। पंडितजी को यह पूर्ण विश्वास था कि यदि समाजवाद कभी भी अपना घोषित लक्ष्य प्राप्त कर सका, तो ऐसा इसी भारतीय पद्धति के आधार पर हो सकेगा।
पंडितजी भारतीयता के केवल इसलिए समर्थक नहीं थे कि वह उनकी राष्ट्रीय बपौती थी। अपितु वे जानते थे कि मानवता के दोष, विशेष कर जगत के दोष, इसी भारतीय संस्कृति के आधार पर दूर किये जा सकते है। क्या पाश्चात्य संस्कृति व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक अनुशासन दोनों को साथ साथ स्वीकार करती है? पाश्चात्य देशों में भौतिकवादी स्वतंत्रता शीघ्र ही स्वैराचार में तथा अनुशासन, नियंत्रण में परिणित हो जाता है। पाश्चात्य देश बाह्य विभिन्नताओं के बीच वास्तविक एकता के कभी कल्पना ही नहीं कर सके क्योंकि वे एकरूपता को ही एकता समझते थे वे भारतीय सामाजिक—आर्थिक व्यवस्था के गुणों को कभी समझ ही नहीं सके, क्योंकि वे हमारे स्थाईत्व को गतिहीनता समझते थे और अपने अस्थाईत्व को गतिशीलता। कोई भी पाश्चात्य विचारक ऐसी एकात्मक प्रकार की सरकार की कल्पना ही नहीं कर सकता था जिसमें प्रशासकिय अधिकार अधिकाधिक विकेन्द्रिकृत हों क्योंकि वे यह सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा कोई विकेन्द्रिय सरकारी अधिकार स्थापित किया जा सकता है जो अत्यधिक नियंत्रण न रखे तथा क्षेत्रिय औद्दोगिक एवं नागरिक स्वशासन भी रहे जो बातें भारतीय सामाजिक व्यवस्था की विशेषता रही है। पाश्चात्य विचारक सोचते थे कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना दोनो साथ नहीं रह सकती। पाश्चात्य देशों में राष्ट्रीयता की भावना बिगड़कर साम्राज्यवाद का रूप ले सकती है तथा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना अपने देश के प्रति गद्दारी का रूप ले सकती है। पंडितजी द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद में पाश्चात्य देशों की संकुचित विचारधाराओं कि त्रुटियों, असंतुलनों तथा अनुपयोगिताओं को सिद्ध कर दिया । वे अपने एकात्मवाद के आधार पर एक ऐसे विश्व राज्य की कल्पना कर सके, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियां विकसित हो और एक ऐसा मानव धर्म उत्पन्न हो जिसमें सभी धर्मों का यहां तक की भौतिकवाद का भी समावेश हो।
युगदृष्टा
दीनदयाल जी एक दृष्टा थे। किसी काल चक्र की भांति स्वंय को शताब्दियों के आर—पार ले जा सकते थे। वे प्राचीन दृष्टाओं तथा आने वाली पीढ़ियों, दोनों का ही सामना कर सकते थे। वे प्राचीन ऋषियों कि बुद्धिमत्ता के सहारे, आधुनिक समस्याओं का हल हमारे लिए निकाल देते थे। वे पहले से ही जान गये थे और पहचान गये थे कि सुदूर भविष्य में मानव के समक्ष कौनसी समस्याएं आएगी और उनके लिए उन्होंने सनातन धर्म के आधार पर अचूक उपचार बतलाये।
कहा गया है कि अदूरदर्शी लोग नष्ट हो जाते है। बिना किसी दृष्टा के कोई राष्ट्र पतीत होकर अन्त में नष्ट हो जाता है। परन्तु हमारा धर्म सनातन है, अर्थात् वह अनादि एवं अनन्त है। इसलिए भारत माता कृपा करके प्रत्येक युग में एक ऐसे दृष्टा को जन्म देती है जो गलत आदर्शो का अनुसरण करने वाली निराशा युक्त मानव जाती को आशा का संदेश दे। आधुनिक युग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय त्रस्त मानवता के लिए इस धर्म भूमि की भेंट थी।

| साभार संदर्भ |